बात उन दिनों की है जब मुझे साहित्य और संस्कृति की परिभाषा की समझ नहीं थी। चूंकि विज्ञान का छात्र रहा तो इससे दूर ही रहा कि जीवन में जो कुछ भी होता है, उसमें साहित्य और संस्कृति की कोई भूमिका हो सकती है। पढ़ने-लिखने वाला एक अच्छा छात्र था मैं। रसायन शास्त्र के समीकरण थोड़ा जटिल जरूर लगते थे लेकिन रसायनों की परिकल्पनाओं से मन रोमांच से भर उठता था। बाजदफा तो मैं सपने में यह देखा करता था कि जब जमीन की कोख से लौह अयस्क निकाले जाते हैं तब उसे किस तरह से उपयोग के लायक बनाया जाता है। फिर हर चरण में उसके रसायनिक स्वरूप में किस तरह परिवर्तन आता होगा और यह भी कि कुदाल और अन्य उपयोगी उपकरणों में जो लोहा होता है, उसका रसायनिक गुण क्या होता है तथा क्यों होता है।
इस सपने के पीछे एक कहानी थी। दरअसल, उन दिनों मेरे घर तीन भैंसें हुआ करती थीं। मम्मी-पापा के लिए यह आय का अतिरिक्त साधन था। पापा भैंसों के मामले में विशेषज्ञ थे। पांच कोस की परिधि में सबसे उन्नत नस्ल की भैंस मेरे खूंटे पर रहती। उनको सानी-पानी देने और दूध निकालने की जिम्मेदारी हालांकि मुझे नहीं दी गयी थी। भैया यह सब संभालता जब पापा ड्यूटी करने जाते। मुझे इन सबसे मुक्त रखा गया था। मुझसे कहा गया था कि तुम पढ़ो। लेकिन आदमी कितनी देर तक पढ़ सकता है और वह भी तब जब मम्मी-पापा और भैया दिन-रात मेहनत कर रहे हों। आदमी तो आदमी इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि उसकी आंखों में पानी होता है। यहां पानी का मतलब सरोकार से है।
[bs-quote quote=”वर्ष 2015 में मैं उन आदिवासियों से मिलने पहुंचा जो लोहा गलाने का काम पारंपरिक तरीके से करते हैं। यह इलाका था लोहरदग्गा का। हालांकि चार जन ही मिले जो यह काम करते थे। उनके पास कई पत्थर थे, जिसे वे भट्ठी में डालते और लोहा तरल के रूप में निकलता। जो शेष बच जाता, उसे वह छाई करते। इसी तरह की छाई का उपयोग कई बार मैंने अपने इलाके में सड़कों के निर्माण में देखा था।” style=”style-2″ align=”center” color=”” author_name=”” author_job=”” author_avatar=”” author_link=””][/bs-quote]
तो हुआ यह कि मैंने और भैया ने मिलकर तय किया कि सुबह में भैंसों को सानी-पानी भैया दे और शाम को मैं। यह समझौता उस समय मेरे लिए ताशकंद के समझौते के माफिक था। भैया भी खुश रहने लगा था। हालांकि मैं दूध निकालने में महारत हासिल नहीं कर सका। एक लीटर दूध निकालते-निकालते हाथ की नसें चढ़ जाती थीं और मम्मी-पापा और भैया सब ठठाकर हंस पड़ते।
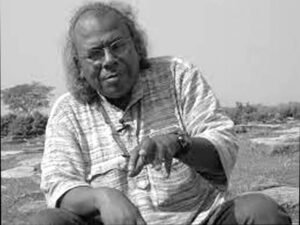
उन दिनों चारा काटने के लिए लोहे की मशीन थी हमारे यहां। इसे मैनुअली चलाना पड़ता था। दो लोगों की आवश्यकता होती थी। एक पीछे से मशीन में चारा डालता तो दूसरा मशीन के बेलन को पकड़कर घुमाता। मशीन में एक गंड़ासा हुआ करता था। एकदम तेज धार वाला। धार कम होने की स्थिति में लोहे की रेती होती थी, जिससे धार को तेज किया जाता था।
तो इस मशीन में तीन तरह के लोहे थे। एक लोहा जिससे वह मशीन बना था। उसे बूंदा का लोहा कहते हैं। गंड़ासा भी लोहे का ही था, लेकिन वह अलग तरह का था। और रेती, जिससे गड़ासे के धार को तेज किया जाता, वह तीसरे तरह का। मन में कई सवाल उठते थे। आखिर लोहा तो लोहा है, फिर उसके इतने रूप कैसे।
रसायन शास्त्र के शिक्षक थे शशिभूषण राय। शिक्षक क्या थे, इन्साइक्लोपीडिया थे। वे मुझे पसंद करते थे या नहीं, कह नहीं सकता था। लेकिन डांटते नहीं थे जब मैं उनसे उलूलजुलूल सवाल करता। लोहे से जुड़ा सवाल उन्हें बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने क्लास में तीन दिनों तक यही समझाया कि लोहा किस-किस रूप में हमारे सामने है और उसके गुण क्या-क्या हैं। इसी क्रम में उन्होंने यह जानकारी दी कि लोहा की खोज का श्रेय बिहार (तब झारखंड अलग नहीं हुआ था) के आदिवासियों को जाता है। यहां से पूरे विश्व में यह बात फैली कि लोहा नामक एक मेटल है जो कॉपर व अन्य मेटल से अधिक मजबूत और टिकाऊ है।
मेरे जीवन में यह पहला अवसर था जब मैं यह जान सका कि आदिवासियों ने मानव सभ्यता के विकास में कितनी बड़ी भूमिका निभायी। इसी अहसास ने मुझे आदिवासियों के प्रति कृतज्ञ बनाया।
लोहा गलाना एक श्रमपूर्ण काम है। लेकिन हमारे पूर्वजों ने यह किया और मानव जीवन को आसान बनाया।
इन सब अहासासों के बीच साहित्य और संस्कृति से मेरा वास्ता पड़ा और आज मैं लगभग हर दिन सोचता हूं कि इनमें ऐसी कौन-सी बात है जो गैर-आदिवासियों को आदिवासियों के साथ जोड़ती है। इस क्रम में मैंने यह पाया कि हमारे यहां जो परंपराएं हैं, बिल्कुल वैसी ही परंपराएं आदिवासियों की भी हैं। हमारे कुल देवता मिट्टी के पिंड हैं। आदिवासी भी अपने पुरखों को इसी रूप में याद करते हैं। मेरे घर में भी मनुषदेवा है और आदिवासियों के यहां भी। मेरे घर में भी कुल देवता को दारू की छांक दी जाती है तो आदिवासी भी यही करते हैं। मजे की बात यह कि मेरी शादी में जो नेग हुए, लगभग वैसे ही नेग आदिवासियों में भी होते हैं। जैसे एक नेग है – मिट्टी कोड़ने का, जिसे मटकोरवा कहा जाता है। यह विवाह संस्कार के पहले दिन होता है।
जब मेरा मटकोरवा हुआ तो मेरे घर की महिलाएं मेरी मां के नेतृत्व में एक खेत में गयीं। मुझे भी साथ ले जाया गया। वहां मेरी तेतरी फुआ ने कृत्रिम ठनगन करने के बाद मिट्टी कोड़ा और हम वापस लौट आए। इस नेग के दौरान महिलाओं ने गीत गाए। कुछ गीतों के बोल अश्लील जरूर थे लेकिन उनमें अपनापन था। मटकोरवा से प्राप्त मिट्टी का इस्तेमाल अगले दिन किया गया जब मंड़वा बनाया गया। प्राप्त मिट्टी के उपर एक मटका रखा गया और उसमें मेरे घर के पुरुषों ने पानी डाला। फिर उसके ऊपर आम की कोंपलें रख दी गयीं। साथ में हल और पालो। पालो वह जो खेत जोतते समय बैलों के कंधे पर रखा जाता है।
यह भी पढ़ें :
यह सब क्यों किया गया और इस नेग का मतलब क्या है, यह सब मुझे आदिवासी इलाकों में जाने के बाद समझ में आया। दरअसल, यह एक नए जीवन की कल्पना है। सबसे ऊर्वर खेत की मिट्टी के उपर पानी और आम के पत्ते। हमारे यहां तो पुरुषों के मंड़वा में सजावट कम होती है। लेकिन महिलाओं के मामले में मंड़वा का रूप देखते ही बनता है। मिट्टी, कलश और आम के पत्तों के साथ मिट्टी के पंछी।
अहा! कितना सुंदर है यह सब। सोचकर ही मन प्रसन्न हो उठता है।
अब सोचता हूं कि क्या आदिवासी साहित्य और संस्कृति एक महासमुच्चय है जिसमें अन्य शेष सभी शामिल हैं?
मेरा उत्तर सकारात्मक है। मेरे इस निष्कर्ष के पीछे आदिवासी लेखकों द्वारा किया गया काम है। मसलन, डॉ. रामदयाल मुंडा का काम। कल देर रात तक उनकी किताब आदिवासी अस्मिता और झारखंडी अस्मिता के सवाल पढ़ता रहा। कुछ और सवाल जेहन में आए हैं, जिनके बारे में कभी और लिखूंगा। फिलहाल तो इतना ही कि बहुजन साहित्य कहकर आदिवासी साहित्य पर कब्जे के प्रयासों की आलोचना होनी चाहिए। वजह यह कि आदिवासियों का साहित्य दलित साहित्य से बिल्कुल अलग है। ओबीसी साहित्य और आदिवासी साहित्य के बीच कुछ समानताएं अवश्य हैं लेकिन इतने नहीं कि दोनों मिला दिया जाय।
सोच रहा हूं कि एक महीने के अंदर हरिराम मीणा, रोज केरकेट्टा, निर्मला पुतुल, अनुज लुगुन, वाहरू सोनवणे, जमुना बीनी तादेर, फ्रांसिस्का कुजुर, सरिता सिंह बड़ाईक और विश्वासी एक्का आदि को पढ़ूं। निश्चित तौर पर आदिवासी साहित्य के कुछ अन्य आयामों के संबंध में जानकारी मिलेगी।
नवल किशोर कुमार फॉरवर्ड प्रेस में संपादक हैं





[…] […]
[…] […]