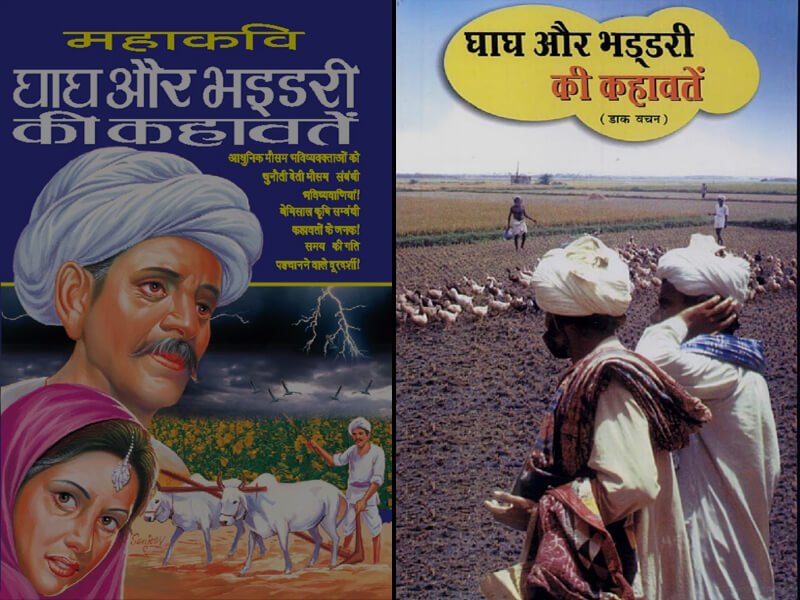जाति का उल्लेख किये बिना भारतीय समाज की कल्पना ही नहीं की जा सकती। कहने को यह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों में विभाजित है लेकिन इसमें जातियों एवं उपजातियों की इतनी पर्तें हैं कि इसकी बुनावट से पार पाना लगभग असम्भव है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को तो फिर भी एक वर्ग के रूप में चिह्नित किया जा सकता है लेकिन शूद्र में जातियों का संजाल है। यद्यपि जाति एक ऐसा विषय है जिस पर विशद चर्चा करने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है लेकिन यहाँ मैं यथावश्यक सीमा में ही इस पर चर्चा करने का प्रयास करूँगा।
चातुर्वर्ण व्यवस्था की अनेकानेक विशेषताओं में एक विशेषता यह भी है कि प्रथम तीन वर्ण उपभोक्ता की भूमिका में रहते हैं जबकि शूद्र उत्पादक की भूमिका में। कृषि, शिल्प, पशुपालन, भारवाहन, चित्रकारी, नृत्य, संगीत, विभिन्न उपकरणों का निर्माण, हर प्रकार के सेवा कार्य, कहने का तात्पर्य यह है कि हाथों से सम्पन्न होने वाले समस्त कार्यों को करने के लिये शूद्रों को बाध्य दिया कर गया है। साथ ही इन कार्यों कोे जातियों और उपजातियों में इस प्रकार बाँट दिया गया है कि जाति और कार्य एक दूसरे के पर्याय हो गये। बढ़ई, धोबी, नाई कुर्मी, अहीर, गड़ेरिया, चमार और इसी तरह की अनगिनत जातियाँ अस्तित्व में आयीं जिनकी जाति ही उनका पेशा बन गयी।
विडम्बना यह भी कि इन्हें अपने उत्पादन और श्रम का उचित मूल्य भी नहीं मिलता था। परिणामस्वरूप आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से ये इस कदर टूट गये कि इनके अन्दर प्रतिरोध करने की इच्छा शक्ति ही लुप्त हो गयी और वे इसे अपनी नियति मानकर जीने लगे लेकिन अपनी जातिगत चेतना से स्वयं को कभी भी अलग नहीं रख सके। इसके कारण उनके अन्दर स्वयं की जाति को अन्य जातियों से श्रेष्ठ सामने की मानसिकता विकसित हो गयी। जाति-व्यवस्था की सोपानीकृत संरचना इसका कारक तत्व बन गया। यह ब्राह्मणवाद की स्थायी जीत है। इसने आदमी को जाति में बदल दिया और जातियों का बीजारोपण असमानता की भावभूमि पर कर दिया। जब तक जातियाँ रहेंगी तब तक आदमी और आदमी में समता और भाईचारे की भावना सम्भव नहीं है। इसलिये शूद्र आपस में संगठित नहीं हो पाते। वे आपस में ही जातिगत श्रेष्ठता की लड़ाई लड़ते रहते हैं। इनकी इस लड़ाई में ब्राह्मणों की चाँदी कटती रहती है और वे इन्हें अपनी उँगलियों पर नचाते हुए इनका मनमाना शोषण करते रहते हैं।
ब्राह्मणवाद समाज को नियंत्रित करने की ऐसी यांत्रिकी है जिसकी चाभी पर ब्राह्मणों का एकाधिकारी कब्जा है। उन्हीं की बात अन्तिम है क्योंकि शास्त्रों की व्याख्या करने का अधिकार उन्हीं के पास है और उनके द्वारा की गयी व्याख्या को कोई चुनौती नहीं दे सकता अर्थात् ब्राह्मण की मर्जी सर्वाेपरि है और उसका कहा अन्तिम।
इसी एकाधिकार के डंडे का जबरदस्त एवं मारक प्रयोग शूद्रों के विरुद्ध करके उनसे मनुष्य के सारे अधिकार छीन लिये गये। उनके अन्दर कूट-कूटकर दासत्व का भाव भर दिया गया। उन्हें स्थायी रूप से बौद्धिक अपंग घोषित कर दिया गया। यह धारणा स्थापित कर दी गयी कि शूद्रों के यहाँ कोई योग्य बच्चा पैदा ही नहीं हो सकता। विडम्बना यह है कि यह धारणा आज भी कहीं से कमजोर नहीं हुई है। इस तथ्य से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि शूद्रों ने बार-बार स्वयं को साबित किया है और कर रहे हैं। अवसर से वंचित किये जाने के सुनियोजित षड़यंत्र को जब भी भेदने का अवसर मिला इन्होंने अपने आगे किसी को टिकने नहीं दिया। मेधा जन्म की मोहताज नहीं होती। वह धर्म और जाति का भी अन्तर नहीं करती। कोई भी कहीं भी जन्मा व्यक्ति असाधारण बौद्धिक क्षमता का हो सकता है लेकिन ऐसे व्यक्तियों के लिये ब्राह्मण महारथियों ने एक नायाब नुस्खा खोज लिया है और वह है येन केन प्रकारेण इन्हें ब्राह्मण सिद्ध करने का। कबीर और रैदास के उदाहरण हमारे सामने हैं। इसी कड़ी में घाघ का नाम भी जुड़ता है। इतिहास लेखन की प्रवृत्ति के अभाव के चलते यह धूर्तता आसानी से परवान भी चढ़ जाती है।
क्या किसी का नाम घाघ हो सकता है?
घाघ की ज्यादातर कहावतें कृषि से सम्बन्धित हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है और आज भी कमोबेश इसकी यह स्थिति बनी हुई है। कृषि पूरी तरह मौसम पर आश्रित उद्यम है और मौसम के मिजाज का पूर्वानुमान आसान नहीं है। घाघ इसी काम को आसान बनाते हैं। उनकी कहावतें मौसम के बारे में लगभग सटीक भविष्यवाणी करती हैं। इतना ही नहीं, वह विभिन्न फसलों को बोने के लिये जमीन और चक्र का भी निर्धारण करती हैं। अधिक पानी और कम पानी वाली फसलों की बात करती हैं। पशुओं की नस्लों की चर्चा करती हैं। किसानों की घर-गृहस्थी की बात करती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि घाघ की कहावतें स्वयं उनकी जाति को इंगित करती हैं।
कृषि एवं इससे सम्बन्धित उपकरण के निर्माण का कार्य शिल्प कार्य में आता है। यह कार्य केवल शूद्रों को आबंटित है। अन्य तीनों वर्णाें के लिये त्याज्य है। सारे संस्कृत ग्रन्थ ऐसे आदेशों से भरे पड़े हैं। यह स्वयं इस बात का सबूत है कि घाघ शूद्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकते। इसकी पुष्टि में इस तथ्य का भी उल्लेख किया जा सकता है कि घाघ ने जैसी कहावतों की रचना की है वह केवल वही कर सकता है जो जमीनी स्तर पर कृषि के साथ जुड़ा हो जबकि ब्राह्मणों ने इसे अपने लिये त्याज्य घोषित कर रखा है।
घाघ की कहावतों की न तो कोई टीका उपलब्ध है और न ही अलग से कोई जीवनी। कहावतों की जो पुस्तकें हैं उन्ही में इनके बारे में थोड़ी-बहुत जानकारी मिलती है। यदि वह ब्राह्मण होते तो पक्का मानिये कि उन्हें आदि मौसम वैज्ञानिक सिद्ध करने की होड़ में टीकाओं की लाईन लग जाती। अब एक नजर घाघ की जीवनी पर डालते हैं।
घाघ के जन्म और समय के अंतर्विरोध
रामनरेश त्रिपाठी ने अपने द्वारा सम्पादित पुस्तक ‘घाघ और भड्डरी में घाघ के काल, स्थान और जाति पर चर्चा की है। अपने निष्कर्षों के पूर्णरूपेण प्रमाणिक होने का दावा भी वह करते हैं लेकिन उनका दावा उनके द्वारा प्रस्तुत चर्चा में ही विरोधाभासी तर्को से टकराता है। उदाहरण के लिये वह घाघ के जन्म का वर्ष संवत् 1753 (सन् 1696) बताते हैं। वह उन्हें दो मुगल बादशाह हुमायूँ और अकबर के दरबार से जोड़कर देखते हैं। मैं इस संदर्भ में सम्पादक के ही शब्दों को उद्धृत करना चाहूँगा जो इस प्रकार हैं- ‘घाघ पहले-पहले हुमायूँ के राजकाल में गंगापार के रहने वाले थे। वे हुमायूँ के दरबार में गये। फिर अकबर के साथ रहने लगे। अकबर उनपर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि अपने नाम का कोई गाँव बसाओ। घाघ ने वर्तमान ‘चौधरी सराय’ नामक गाँव बसाया और उसका नाम रक्खा, ‘अकबराबाद सराय घाघ‘। अब भी सरकारी कागजात में उस गाँव का नाम ‘सराय घाघ’ ही लिखा जाता है।
‘सराय घाघ कन्नौज शहर से एक मील दक्खिन और कन्नौज स्टेशन से तीन फर्लांग पश्चिम है। बस्ती देखने से बड़ी पुरानी जान पड़ती है। थोड़ा सा खोदने पर जमीन के अन्दर से पुरार्नी इंटें निकलती हैं। अकबर के दरबार में घाघ की बड़ी प्रतिष्ठा थी। अकबर ने इनको कई गाँव दिये थे और इनको चौधरी की उपाधि भी दी थी। इसी से घाघ के कुटुम्बी अभी तक चौधरी कहे जाते हैं। सराय घाघ का दूसरा नाम चौधरी सराय भी है।’ (पृष्ठ 21)
ऊपर बताया जा चुका है कि घाघ की पैदाइश संवत् 1753 अर्थात् सन् 1696 में हुई मानी गयी है जो अनुमान पर आधारित है। हुमायूँ की मृत्यु 27 जनवरी, 1556 को तथा अकबर की 27 अक्टूबर, 1605 को हुई थी। यह ऐतिहासिक सत्य है अर्थात् घाघ की पैदाइश से 140 वर्ष पूर्व हुमायूँ की और 91 वर्ष पूर्व अकबर की मृत्यु हो चुकी होती है। इस सूचना के बाद और कुछ कहने को शेष नहीं रह जाता यह बताने के लिए कि घाघ हुमायूँ या अकबर के समकालीन नहीं थे लेकिन इससे बात पूरी नहीं होगी।
दो बातें और अविश्वसनीय हैं जिन्हें इंगित करना जरूरी है। अकबर के दरबार में टोडरमल जैसे भू-विशेषज्ञ और रहीम जैसे सशक्त कवि थे। ऐसी स्थिति में घाघ का एक कृषि कवि के रूप में इन दरबारियों के बीच अपनी जगह बनाना विशेष गुण-सम्पन्न होने की माँग करता है। इतना ही नहीं, अकबर इन्हें कई गाँव देते हैं और चौधरी की उपाधि भी। मुझे इस बात पर संदेह है कि अकबर के द्वारा चौधरी का खिताब भी दिया जाता था लेकिन यह कोई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है।
महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि अकबर द्वारा इतना महत्व देने के बावजूद किसी भी इतिहासकार ने घाघ का संज्ञान नहीं लिया। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि रामनरेश त्रिताठी अपनी इस स्थापना में खरे नहीं उतरते।
घाघ की जाति को भी लेकर त्रिपाठी जी पूर्ण आश्वस्त हैं। वह कन्नौज के उपरिलिखित पुरवे, चौधरी सराय में उनके वंशजों को खोज निकालने का दावा करते हैं। उनका कहना है कि ये दूबे हैं। उन्हीं के शब्दों में-‘ऊपर कहा जा चुका है कि घाघ दूबे थे। इनका जन्मस्थान कहीं गंगापार में कहा जाता है। अब उस गाँव का नाम और पता इनके वंशजों में कोई नहीं जानता। घाघ देवकली के दूबे थे और सराय घाघ बसाकर अपने उसी गाँव में रहने लगे थे।
उनके दो पुत्र हुए-मार्कंडेय दूबे और धीरधर दूबे। इन दोनों पुत्रों के खानदान में दूबे लोगों के बीस-पच्चीस घर अब उस बस्ती में हैं। मार्कंडेय दूबे के खानदान में बच्चू लाल दूबे और विष्णुस्वरुप दूबे तथा धीरधर दूबे के खानदान में रामचरण दूबे और श्रीकृष्ण दूबे वर्तमान हैं। ये लोग घाघ की सातवीं या आठवीं पीढ़ी में अपने को बतलाते हैं। ये लोग कभी दान नहीं लेते। इनका कथन है कि घाघ अपने धार्मिक विश्वासों के बड़े कट्टर थे। और इसी कारण उनको अंत में मुगल दरबार से हटना पड़ा था, तथा उनकी जमींदारी का अधिकांश जब्त हो गया था।
इस विवरण से घाघ के वंश और जीवन-काल के विषय में सन्देह नहीं रह जाता। मेरी राय में अब घाघ-विषयक सब कल्पनाओं की इतिश्री समझनी चाहिये। घाघ को ग्वाल समझने वालों अथवा बराहमिहिर की संतान मानने वालों को भी अपनी भूल सुधार लेनी चाहिए।’ (पृष्ठ 22)
कहीं का तीर कहीं का तुक्का जोड़ने की कोशिशें
सवाल यह है कि क्या एक भूल को दूसरी भूल से सुधारा जा सकता है? जीवनकाल की तरह वंशज वाली थ्योेरी भी इतनी लचर है कि यह तर्क की कसौटी पर एक पल के लिये भी नहीं ठहर सकती। यदि इस थ्योरी की पर्त दर पर्त उधेड़ी जाये तो यह स्वयं नतमस्तक हो जायेगी लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। बहरहाल मैं ग्वाल और बराहमिहिर की अवधारणा पर चर्चा करूँगा जिसका उल्लेख त्रिपाठी जी ने स्वयं किया है।
उन्होंने कपिलेश्वर झा के इस कथन को उद्धृत किया है- ‘‘पूर्व काल में वराहमिहिर ज्योतिषाचार्य अपना ग्राम सौं राजाक ओहि ठाम जाइत रहथि, मार्ग में साँझ भय गेलासे एक ग्वारक ओतय रहला। ओ गोआर बड़े आदर से भोजन कराय हिनक सेवार्थ अपन कन्याक नियुक्त कयलक। प्रारब्धवश रात्रि में ओहि गोपकन्या से भोग कयलन्हि। प्रातः काल चलवाक समय में गोप-कन्या के उदास देखि कहलथिन्ह जे यहि गर्भ से अहाँके उत्तम विद्वान् बालक उत्पन्न होएत ओ कतोक वर्षक उत्तर एकबेरि एत पुनः हम आएब, इत्यादि धैर्य दय ओहि ठाम से बिदा भेलाह।’’ (पृष्ठ 20)
यद्यपि यह कहकर कि यह कथा भड्डरी के सम्बन्ध में प्रचलित है त्रिपाठी जी ने अपना बचाव करने की कोशिश की है लेकिन वह भूल गये कि भड्डरी पर उन्होंने अलग से चर्चा की है। यदि यह कथा भड्डरी के बारे में प्रचलित है तो इसे वहीं शामिल करना चाहिये था।
इसी विषय पर निम्न टिप्पणियाँ भी ध्यातव्य है।
‘‘श्रीयुत वी.एन. मेहता, आई.सी.एस. अपनी युक्तप्रान्त की कृषि सम्बन्धी कहावतें में लिखते हैं-
‘घाघ’ नामक एक अबाहीर की उपहासात्मक कहावतें भी स्त्रियों पर आक्षेप के रूप में हैं।’ (पृष्ठ 20)
‘‘रायबहादुर बाबू मुकुन्दरलान गुप्त ‘विशारद’ अपनी ‘कृषि-रत्नावली’ में लिखते हैं-
‘‘कानपुर जिलान्तर्गत किसी गाँव में संवत् 1753 में इनका जन्म हुआ था। ये जाति के ग्वाला थे। 1780 में इन्होंने कविता की मोटिया नीति बड़ी जोरदार भाषा में कही।’ (पृष्ठ 20)
‘‘मैंने ‘शिव सिंह सरोज’ के आधार पर कविता-कौमुदी-प्रथम भाग में लिखा था-
‘घाघ कन्नौज, निवासी थे। इनका जन्म सं0 1753 में कहा जाता है। ये कब तक जीवित रहे, न तो इसका ठीक-ठीक पता है और न इनका या इनके कुटुम्ब ही का कुछ हाल मालूम है।’ (पृष्ठ 20-21)
पिलग्रिम्स पब्लिशिंग वाराणसी से प्रकाशित पुस्तक घाघ भड्डरी की भूमिका में इसके सम्पादक देव नारायण द्विवेदी ने भी घाघ की पैदाइश का वर्णन इस प्रकार किया है-’’ घाघ और भड्डर एक ही थे या दो, इस विषय में मतभेद है। इसलिये हम अपने पाठकों को इस विवादग्रस्त विषय में डालना नहीं चाहते। कहावतें दोनों की ही एक ही शैली की दिखायी पड़ती हैं। हमारा अनुमान है कि घाघ और भड्डर ये दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। कहावतों में बहुत जगह ऐसा आया भी है कि ‘कहें घाघ सुनु भड्डरी’ ‘कहें घाघ सुनु घाघिनी’ आदि। भड्डरी या घाघिनी उसकी स्त्री को कहते थे।
भड्डर की उत्पत्ति के सम्बन्ध में किंवदन्ति है कि इनकी माता अहिरिन थी और पिता ब्राह्मण ज्योतिषी। ज्योतिषी जी को कोई ऐसा मुहूर्त दिखायी पड़ा कि यदि उस मुहूर्त में कोई स्त्री गर्भ धारण करेगी तो उसके गर्भ से त्रिकालदर्शी विद्वान बालक उत्पन्न होगा। ज्योतिषी जी उस सुयोग से लाभ उठाने के लिये वहाँ से चल पड़े, क्योंकि उनकी स्त्री उन दिनों उनके साथ नहीं थी। वह रास्ते में ही थे कि वह मुहूर्त आ गया। उन्होंने देखा कि अब तो अपनी स्त्री के पास समय से पहुँचना असम्भव है। इसलिये वह बड़े चिन्तित हुए। इतने ही में उन्हें एक स्त्री दिखायी पड़ी। ज्योतिषी ने उससे अपना मन्तव्य प्रकट किया। स्त्री राजी हो गयी। उसने गर्भ धारण किया। समय आने पर उसके गर्भ से बालक उत्पन्न हुआ, जिसका नाम भड्डर पड़ा।’’ (पृष्ठ VII-VIII)
रामनरेश त्रिपाठी की अवधारणा का खण्डन भी द्विवेदीजी के इस कथन से हो जाता है- ‘‘कुछ लोगों का मत है कि घाघ का जन्म संवत् 1753 में कानपुर जिले में हुआ था। मिश्रबन्धु ने इन्हें कान्यकुब्ज ब्राह्मण माना है पर यह बात केवल कल्पना प्रसूत है। यह कब तक जीवित रहे इसका ठीक-ठीक पता नहीं चलता।’’ (वही पृष्ठ X)
पिछड़ी जाति की स्त्री के प्रति दुर्भावना और गर्हित मानसिकता
घाघ की पैदाइश को लेकर उक्त दोनों अन्तर्कथाओं में समानता होने के बावजूद द्विवेदी की कथा बेवकूफियों का पर्याय है। जिस विशेष मुहूर्त का पता ज्योतिषी महाराज ने अपनी विद्या के बल पर लगाया था, उस मुहूर्त में न जाने कितने बच्चे पैदा हुए होंगे, यह तय बात है।
दूसरे, उसको यह क्यों पता नहीं चला कि उस विशेष मुहूर्त में वह अपनी स्त्री के पास पहुँच कर उसके साथ संसर्ग स्थापित कर लेगा अथवा नहीं? तीसरे, रास्ते में मिली स्त्री जिसने उसके मन्तव्य को बिना न नुकुर के स्वीकार कर लिया क्या वह वेश्या थी क्योंकि अच्छे चाल-चलन वाली स्त्री उस ब्राह्मण ज्योतिषी का मुँह इस प्रस्ताव पर नोच लेती।
चौथा, इस कथा का स्पष्ट अर्थ यह है कि उस तथाकथित मुहूर्त का प्रभाव केवल उस स्त्री पर पड़ने वाला था जिसके साथ वह ब्राह्मण ज्योतिषी सम्भोग करता। यह सीधे-सीधे ब्राह्मण की कामुकता का मामला बनता है। संस्कृत ग्रन्थों में अनेकानेक आख्यान ब्राह्मणों की कामुकता को केन्द्र में रखकर गढ़े गये हैं जो अन्ततोगत्वा ब्राह्मणों को चरित्रहीन साबित करते हैं। इस लेख में उनपर अलग से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं हैं।
कबीर की तरह घाघ को भी ब्राह्मणवादी घृणा का शिकार होना पड़ा
घाघ ब्राह्मण नहीं थे इसकी पृष्टि रामनरेश त्रिपाठी की बातों से ही होती है। यदि वह घाघ के पूरी तरह ब्राह्मण होने के प्रति आश्वस्त होते तो बराहमिहिर की कथा का उल्लेख ही न करते। इसके अलावा अपनी भूमिका में उन्होंने पराशर के कृषि सम्बन्धी श्लोकों को घाघ पर वरीयता दी है और किसी लाल बुझक्कड़ को उनसे होड़ लेते हुए बताया है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि कोई भी घाघ को जाति के धुंध से बाहर नहीं निकाल सका।
ब्राह्मण स्थायी रुप से इस हीनग्रंथि का शिकार है कि वह सर्वश्रेष्ठ है। उसके अलावा और कोई योग्य नहीं हो सकता। यह एक तरह का मनोरोग है। इसका इलाज है लेकिन वह इलाज कराना नहीं चाहता। वह जानता है कि इससे उसके वर्चस्व का किला ढह जायेगा। इस किले की अचूक सुरक्षा कि लिये उसने पूरे समाज के कार्य एवं व्यवहार को जातिवार बाँटकर उसपर धर्मशास्त्र का मुलम्मा चढ़ा रखा है। किसी की मजाल नहीं कि धर्मशास्त्र के विरुद्ध जाकर बोले। इस प्रकार ब्राह्मण एकाधिकारी वर्चस्ववाद का नियंता हो गया है। उसके सभी कुकृत्य शास्त्रसम्मत बना दिये गये हैं। वह किसी भी स्त्री का भोग करने के लिये स्वतंत्र है। इसी शब्द का प्रयोग रामनरेश त्रिपाठी भी करते है जब वह कहते हैं- ‘प्रारब्धवश गोपकन्या से भोग कयलन्हि’ (पृष्ठ 20) इतनी पतित और चरित्रहीन जाति को अन्य समाज के लोगों द्वारा सर्वश्रेष्ठ मान लेना किसी अबूझ पहेली से कम नहीं है।
लेकिन मेधा किसी जाति विशेष की मोहताज नहीं होती। अन्य जातियों में हमेशा से मेधावी व्यक्ति पैदा होते रहे हैं। ऐसे लोगों ने हमेशा से ब्राह्मणों में बेचैनी पैदा की है। इससे उनकी स्वयं के लिये घोषित सर्वश्रेष्ठ एवं योग्यतम होने की अवधारणा खंडित होने लगती है। वे येन केन प्रकारेण ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण सिद्ध करने में जुट जाते है। इसके लिये कोई न कोई ब्राह्मण उस व्यक्ति की कल्पित माँ से संम्भोग करने के लिय ढूँढ़ लिया जाता है और चूँकि कलम पर इन्हीं की बपौती है, इसलिये मनमाना दस्तावेजीकरण करके उसको सच भी साबित कर देते हैं। घाघ भी अन्य अनेक अब्राह्मण विद्वानों की तरह इसी कुत्सित चाल के शिकार हैं।
मेरा अपना मानना कि घाघ ब्राह्मण नहीं थे। इससे भी अधिक कटु सत्य यह है कि वह किसी ऐसी शूद्र महिला के गर्भ से भी नहीं पैदा हुए थे जिसके साथ किसी ब्राह्मण ने संसर्ग किया था। मैं यह बात इस आधार पर कह रहा हूँ कि पूरा संस्कृत बाङ्मय ब्राह्मणों के यौनाचार से भरा पड़ा जहाँ आसानी से स्त्रियों के समर्पण के आख्यान हैं। व्यवहार में यह सम्भव नहीं है। स्त्रियाँ उच्छंªखल नहीं हो सकतीं। यह यहाँ के मूल निवासियों को बदनाम करने का षड्यंत्र है। घाघ किसान की ही किसी जाति में पैदा हुए होेंगे। प्रबल संभावना इस बात की है कि वह जाति के अहीर ही थे। इन पर प्रमाणिक शोघ करने का दायित्व हमारा बनता है। विश्वास है कि इस लेख को पढ़कर कोई शोधार्थी अवश्य आगे आयेगा!
मूलचन्द सोनकर हिन्दी के महत्वपूर्ण दलित कवि-गजलकार और आलोचक थे। विभिन्न विधाओं में उनकी तेरह प्रकाशित पुस्तकें हैं 19 मार्च 2019 को उन्होंने इस संसार को अलविदा कहा।