गुलामी एक साम्राज्यवादी बुराई है क्योंकि यह एक व्यक्ति के जीवन को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक आदि स्तरों पर प्रभावित करती है। लंबे समय से भौतिक रूप से गुलाम व्यक्ति कब बौद्धिक गुलामी को अपना लेता है, उसे इसका सहज बोध आसानी से नहीं हो पाता है। प्लेटो ने गुलामी को मृत्यु से भी अधिक भयावह माना है। संत रैदास ने गुलामी या पराधीनता को पाप बताया है।
डॉ. आंबेडकर ने मानसिक गुलामी को भौतिक गुलामी से ज्यादा खतरनाक माना है। किशन पटनायक ने इसी मानसिक गुलामी पर विचार करते हुए लिखा है कि अल्पकालीन गुलामी में सिर्फ राजनैतिक गुलामी होती है, जबकि दीर्घकालीन गुलामी में मानसिक गुलामी आ जाती है। इसलिए गुलामी के अभ्यस्त समूहों में गुलामी के प्रति तीव्र आक्रोश शिथिल होता है। यह आज के भारत में हर जगह दिखायी दे रहा है। वे गुलाम दिमाग की तार्किक प्रक्रिया का मूल्यांकन करते हुए लिखते हैं कि तर्क और निर्णय, दोनों स्तरों पर गुलाम का दिमाग कमजोर होता है। वह कुशाग्र बुद्धि का हो सकता है लेकिन जहाँ विचार से निर्णय निकालना पड़ता है, वहाँ वह आश्चर्यजनक ढंग से तर्क की गलती करता है. आखिरकार गुलामी एक अस्वाभाविक स्थिति है। स्वभाव से आदमी आजाद है। एक लंबे समय तक अगर कोई समूह या व्यक्ति गुलाम रह जाएगा तो उसका व्यक्तित्व बीमार हो जाएगा। कुछ चीजों में वह अपंग हो जाएगा।
आज भारत की राजनीति में समाजवादी सबसे अधिक गिरा हुआ है या कमजोर हो गया है क्योंकि समाजवादी आंदोलन में संगठन के प्रति कभी ध्यान नहीं दिया गया। संगठन की आत्मा है प्रशिक्षण। अनुशासन की धमकी देकर संगठन नहीं चलाया जा सकता। सदस्य या समिति कैसे बनाई जाएगी? संघर्ष की तैयारी कैसे हो? समाजवाद क्या है? संघर्ष के साथ-साथ रचनात्मक कार्य क्यों जरूरी है? समाजवाद और लोकतंत्र का क्या रिश्ता है? इन सारे सवालों पर जो सोचता-समझता रहेगा वही आंदोलन या क्रांति का संगठन चला पाएगा, जो इन सवालों पर सोचना छोड़ देगा, वह राजनीति में संकीर्ण हितों की तरफ चला जाएगा। व्यक्ति का हित, कुटुंब का हित, जातीय या सांप्रदायिक हित संकीर्ण हित हैं। राष्ट्र का हित, समाज का हित, शोषित वर्गों का हित – ये तीन ही राजनीति में वाजिब हित हैं। संकीर्ण हितों के लिए प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है, संगठन की भी कम से कम जरूरत होती है। क्रान्तिकारी लक्ष्यों के लिए ही संगठन और प्रशिक्षण की जरूरत होती है, जहाँ संगठन और प्रशिक्षण नहीं है वहाँ क्रांतिकारी और उदात्त लक्ष्यों की राजनीति देर तक नहीं चल सकती। किशन पटनायक का यह कथन राजनीति में युवाओं का मार्गदर्शन करता है। राजनीति में प्रवेश करने वाले जो युवा परम्परागत राजनीति के दलदल में फँसते जा रहे हैं, उन्हें किशन पटनायक के नौजवान और राजनीति शीर्षक आलेख से प्रेरणा लेनी चाहिए।
यह भी पढ़ें –उत्तर प्रदेश : जाति की राजनीति के बहाने विपक्ष को कमजोर करने की रणनीति
जाति भारत की सच्चाई है। बिना जाति पर बातचीत किए कोई चिंतक, लेखक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता होने का दावा नहीं कर सकता है। मानवतावादी चिंतकों ने जाति पर अपने-अपने नजरिये से विचार किया है। किशन पटनायक भी उन्हीं में से एक हैं और वे जाति को आर्थिक समूह के रूप में देखते हैं। उनका कथन है कि जाति भी एक आर्थिक समूह है। राजनीति में पिछड़ी जातियाँ समान ढंग से सोच रही हैं। इसलिए नहीं कि उनको जनेऊ नहीं मिला है, बल्कि इसलिए कि जनेऊ न होने के कारण उनको बड़ी नौकरियाँ मिलती नहीं हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय सहित अधिकांश भारतीय विश्वविद्यालयों ने समय-समय इसे प्रमाणित किया है। वे पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित प्रोफेसर एवं एसोसिएट प्रोफेसर के पदों को सिर्फ इसलिए ‘नॉट फाउंड सूटेबल’ करते हैं क्योंकि उसमें शामिल हो रहे पिछड़ी जातियों के अभ्यर्थियों के बदन पर जनेऊ नहीं होता है। इसीलिए इस भेदभाव को ‘नॉट फाउंड जनेऊ’ भी कहा जाता है। हैरानी यह है कि भारत की तथाकथित अकादमिक प्रगतिशीलता इस पर मौन रहती है। मानो यह सहज एवं स्वाभाविक घटना हो, कोई मनुवादी एवं वर्गीय वर्चस्ववादी बुराई नहीं।
जाति है तभी जातिगत जनगणना की माँग उठ रही है। बिना आँकड़ों के कोई नीति नहीं बनायी जा सकती है। इसीलिए जातिगत जनगणना, आर्थिक गणना सरकारी कर्मचारियों की गणना एवं उद्योगपतियों की गणना कराकर और उनका तुलनात्मक अध्ययन कर यह बताया जा सकता है कि कौन-सी जाति या समूह पिछड़ गया है और कौन अगड़ गया है? यह आजाद भारत के 75 साल के इतिहास के आधार पर बहुत कठिन कार्य नहीं है, बस इसके लिए मंशा चाहिए। फिर उस पिछड़े समूह को बराबरी पर लाने के लिए नीतियाँ बनाने में आसानी होगी। इतनी-सी बात देश के नीति-निर्माताओं की समझ में नहीं आती है।
बुद्धिजीवी व नागरिक समाज की यथार्थ स्थिति का मूल्यांकन राहुल सांकृत्यायन ने ‘दिमागी गुलामी’ शीर्षक पुस्तिका और एडवर्ड सईद ने ‘बुद्धिजीवी की भूमिका’ नामक निबंध में किया है। एडवर्ड सईद के लिए बुद्धिजीवी की भूमिका यह है कि वह यथास्थिति पर प्रश्न उठाये, सत्ता को चुनौती दे, खबरों की, सरकारी रिपोर्टों की तह तक पहुँचने की कोशिश करे, विद्वता और ज्ञान के रूप में जो प्रदान किया जा रहा है उसकी सतह के नीचे तक पहुँचाने का प्रयास करे। हालाँकि भारत का बुद्धिजीवी-वर्ग यह करने में असफल रहा है। क्योंकि वह सफल होता तो 2013 के सिविल सर्विसेज परिणाम की ही भांति 2024 के परिणाम पर भी 20-25 दिन लगातार अख़बारों में आलेख लिखता। लेकिन वह अंग्रेजी आधिपत्य और नवसाम्राज्यवादी दलाली को स्वीकार कर चुका है। इसीलिए भारत के दस हिंदी भाषी राज्यों के परीक्षार्थियों को ऊँट के मुँह में जीरा देने के बाद भी वह अंग्रेजी फ्रीज वाली दही अपने मुँह में चुपचाप जमाए हुए है।
यह भी पढ़ें –बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री ही नहीं सामाजिक न्याय के सूत्रधार भी थे भोला पासवान शास्त्री
किशन पटनायक की पुस्तक ‘विकल्पहीन नहीं है दुनिया : सभ्यता, समाज और बुद्धिजीवी की स्थिति पर कुछ विचार’ समाज में धारणाएं बनाने वाले बुद्धिजीवी-वर्ग की वैचारिक स्थिति पर मुकम्मल प्रकाश डालती है। वे लिखते हैं कि समाज की सारी गति और दुर्गति के लिए बुद्धिजीवी उत्तरदायी हैं। भारत को समृद्ध कर रही है तो भारत का बुद्धिजीवी प्रशंसा का पात्र है, भारत की दुर्गति हो रही है तो निंदा का। यह किसी व्यक्ति-विशेष का मूल्यांकन नहीं है। हरेक राष्ट्र का एक बुद्धिजीवी समूह होता है। बुद्धिजीवी का एक वर्ग के रूप में मूल्यांकन किसी लेखक, पत्रकार या वैज्ञानिक के मूल्यांकन से ज्यादा जरूरी है। विभिन्न समाजों के इतिहास में अंधकार-युग के नाम से एक अध्याय आता है। संभवतः यह अंधकार-युग उनके पहले वाले समय के बुद्धिजीवी समूह के लुच्चेपन का परिणाम है। हमारे समय के बुद्धिजीवी को इसी तरह के कटघरे में खड़ा करना होगा। जो यह मानते हैं कि अयोग्य लोग भाड़ में जा रहे हैं तो जाएं, लेकिन वे कहकर तो देखें- अपनी बात को शास्त्रीय भाषा में बोलने की कोशिश तो करें।
प्रेम सिंह, किशन पटनायक का समग्रता में मूल्यांकन करते हुए लिखते हैं कि वे देश के उन गिनती के लोगों में हैं जिन्होंने आधुनिक सभ्यता के नए अवतार वैश्वीकरण के चलते देश की गुलामी के खतरे को सत्तर के दशक में ही पहचाना और लगातार उसके मुकाबले के लिए जमीनी और वैचारिक संघर्ष किया। प्रेम सिंह किशन पटनायक के ‘गुलाम दिमाग का छेद’ और ‘प्रोफेसर से तमाशगीर’ आलेख का जिक्र तसल्ली से करते हैं। वे ‘प्रोफेसर से तमाशगीर’ के हवाले से लिखते हैं कि प्रणव राय अपनी शिक्षा का पेशा छोड़ कर प्रचुर धन की हविस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की चकाचौंध के वशीभूत पहले दूरदर्शन के कार्यक्रम निर्माता बनते हैं। वहाँ पच्चीस-तीस लाख की सालाना कमाई करके अपनी निजी टेलीविजन कंपनी के मालिक बन जाते हैं। 28 फरवरी 1994 को वित्तमंत्री मनमोहन सिंह के बजट पर प्रणव राय द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम का हवाला देकर किशन पटनायक बताते हैं कि कैसे नई आर्थिक नीतियां, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और बुद्धिजीवी एकजुट होकर देश के करोड़ों साधारण लोगों को अपने ही देश में अप्रासंगिक बना देते हैं।


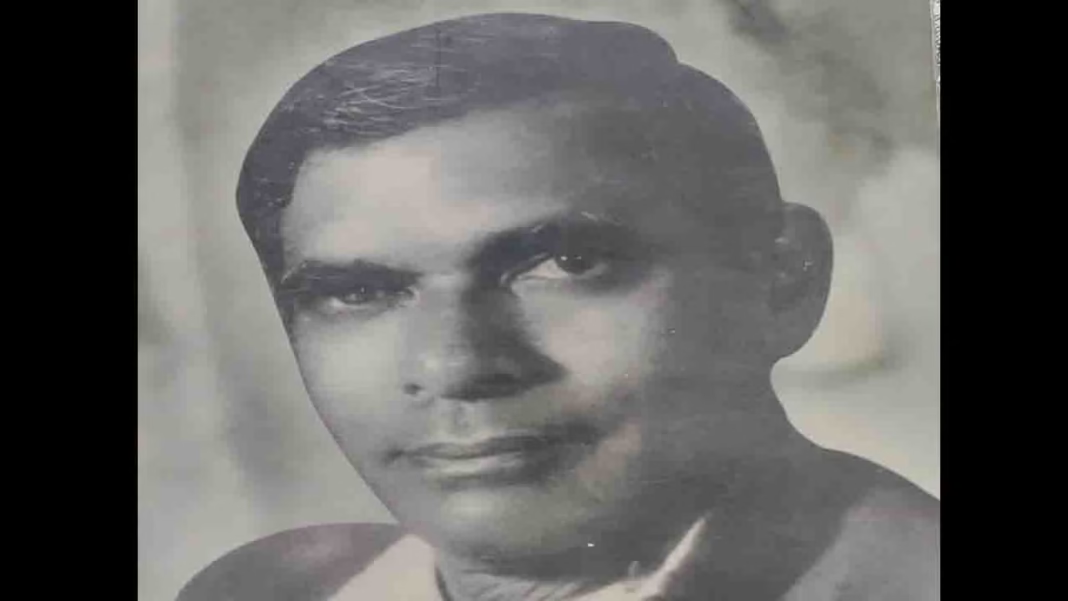

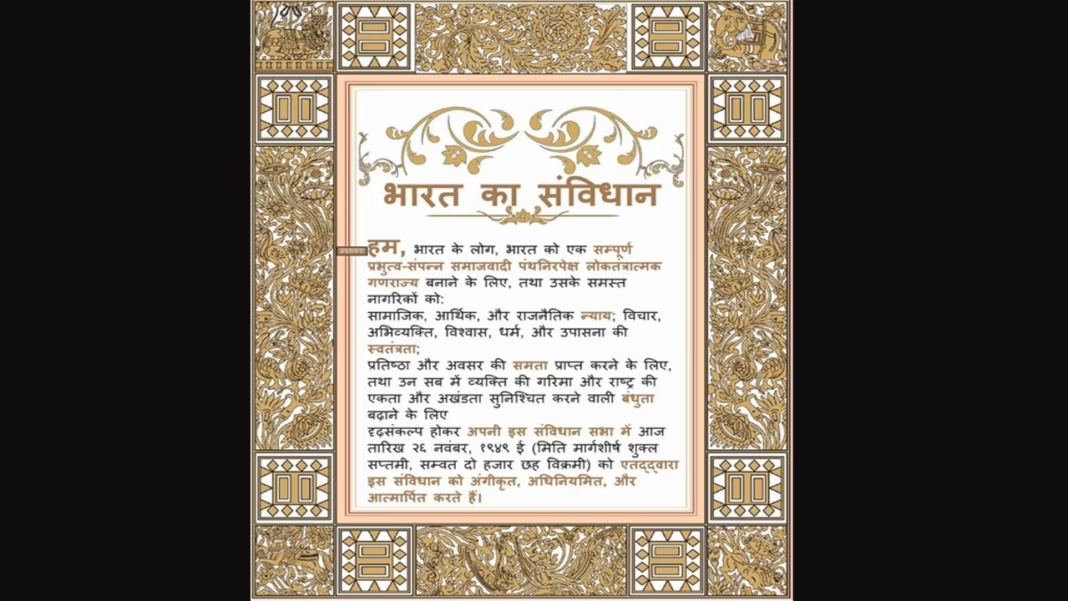
बहुत बढ़िया प्रस्तुति.
Hello. And Bye.
क्या आप हमेशा ध्यान आकर्षित करने में अच्छे हैं, या आपने इसे सिर्फ मेरे लिए बनाया है? इस वेबसाइट पर मुझे लिखें — rb.gy/3pma6x?Lok — मेरा उपयोगकर्ता नाम वही है, मैं इंतजार करूंगा ।