यूएन वाटर द्वारा इस वर्ष विश्व जल दिवस की थीम के रूप में ‘ग्राउंड वाटर:मेकिंग द इनविजिबल विज़िबल’ का चयन किया गया है।
भूजल अदृश्य जरूर है किंतु इसके महत्व को जानने वाले इसे भूमि में छिपे खजाने की संज्ञा देते हैं। विश्व का लगभग समस्त तरल स्वच्छ जल भूजल के रूप में ही है। जलवायु परिवर्तन ने इस भूजल पर संकट खड़ा किया है। यदि वैश्विक परिदृश्य की बात करें तो 50 प्रतिशत पेयजल हमें भूजल के माध्यम से ही उपलब्ध होता है, सिंचाई के लिए आवश्यक जल का 40 प्रतिशत हिस्सा भूजल ही देता है और औद्योगिक क्षेत्र की वैश्विक जल आवश्यकता का एक तिहाई हिस्सा भूजल ही पूर्ण करता है। दुनिया भर में 2.5 बिलियन लोग पीने के पानी और घरेलू आवश्यकताओं के लिए भूजल पर ही निर्भर हैं। भूजल पारिस्थितिक तंत्रों को स्थायित्व प्रदान करता है। यह नदियों के बेस फ्लो को बनाए रखता है। भूजल जलवायु परिवर्तन के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया का मुख्य घटक भी है।
प्रसिद्ध भूजल विशेषज्ञ जूड कॉबिंग उचित ही कहते हैं कि हम उसे ही महत्व देते हैं जो दिखाई देता है, जो हमारी नजरों के सामने नहीं है हम उसकी उपेक्षा करते हैं, यही कारण है कि हम भूजल जैसे महत्वपूर्ण संसाधन की रक्षा एवं समुचित उपयोग के प्रति लापरवाह बने हुए हैं।
विश्व मौसम विज्ञान संगठन की 2021 की स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज़’ रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर 2002-2021 के मध्य स्थलीय जल संग्रहण में 1 सेमी प्रति वर्ष की दर से गिरावट दर्ज की गई है। भारत में संग्रहण में कम-से-कम 3 सेमी प्रति वर्ष की दर से गिरावट रिकॉर्ड की गई है। देश के कुछ क्षेत्रों में तो यह गिरावट 4 सेमी प्रति वर्ष से भी ज्यादा मापी गई है। विश्व भर में भूजल का सर्वाधिक दोहन भारत द्वारा किया जाता है।1980 के दशक से हमारे देश में भूजल स्तर में गिरावट प्रारंभ हुई जो अब तक जारी है। विशेषज्ञों के अनुसार देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भूजल स्तर में गिरावट 8-16 मीटर तक हुई है।
यूनिसेफ द्वारा 18 मार्च 2021 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 9.14 करोड़ बच्चे गंभीर जल संकट का सामना
कर रहे हैं। बच्चों के जल संकट के लिए अतिसंवेदनशील माने जाने वाले 37 देशों में से एक भारत भी है। यूनिसेफ की रिपोर्ट कहती है कि वर्ष 2050 तक भारत में वर्तमान में मौजूद जल का 40 प्रतिशत समाप्त हो चुका होगा।
[bs-quote quote=”भूजल स्तर की गिरावट के साथ आर्थिक असमानता का विमर्श जुड़ा हुआ है। भूजल में गिरावट का सीधा अर्थ है – भूजल से की जाने वाली सिंचाई के खर्च में बढ़ोतरी। इसका परिणाम यह होता है कि आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग भूजल के दोहन में समर्थ होता है और निर्धन वर्ग इसके उपयोग से वंचित हो जाता है। ” style=”style-2″ align=”center” color=”” author_name=”” author_job=”” author_avatar=”” author_link=””][/bs-quote]
भारत में विश्व की 17 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है किंतु जल उपलब्धता मात्र चार प्रतिशत है। हम प्रति व्यक्ति वार्षिक जल उपलब्धता के संबंध में चीन, ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों से भी काफी पीछे हैं। यदि सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों को सही माना जाए तो भारत में भूजल की सर्वाधिक 89 प्रतिशत खपत सिंचाई क्षेत्र में होती है जबकि 9 प्रतिशत भूजल घरेलू उपयोग हेतु और 2 प्रतिशत व्यावसयिक प्रयोजन में प्रयुक्त होता है। उद्योगों द्वारा भूजल के अंधाधुंध दोहन के कारण भूजल स्तर में भारी गिरावट की खबरें छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, झारखंड,उड़ीसा और बिहार के उद्योग बहुल इलाकों से अक्सर सामने आती हैं किंतु इन्हें अनदेखा कर दिया जाता है। यही कारण है कि उद्योगों द्वारा भूजल के दोहन के आंकड़ों पर अनेक बार प्रश्नचिह्न लगते रहे हैं।
भूजल स्तर की गिरावट के साथ आर्थिक असमानता का विमर्श जुड़ा हुआ है। भूजल में गिरावट का सीधा अर्थ है – भूजल से की जाने वाली सिंचाई के खर्च में बढ़ोतरी। इसका परिणाम यह होता है कि आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग भूजल के दोहन में समर्थ होता है और निर्धन वर्ग इसके उपयोग से वंचित हो जाता है।
भूजल में कमी के कारण ऊर्जा का अपव्यय भी होता है। जल संसाधन मंत्रालय का आकलन है कि भूजल स्तर में 1 मीटर की गिरावट ऊर्जा की खपत को .4 किलोवाट प्रति घण्टे से बढ़ा देती है।
सुप्रीम कोर्ट ने दशक भर चली सुनवाई के बाद केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि भूजल के प्रबंधन एवं नियमन हेतु एक प्राधिकरण का गठन किया जाए। इसके बाद 14 जनवरी 1997 को केंद्रीय भूमि जल बोर्ड का गठन किया गया जो जल संसाधन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। केंद्रीय भूमिजल बोर्ड ने एक चौथाई सदी का सफर तय कर लिया है किंतु भूजल की गिरावट को रोकने में यह नाकाम रहा है।
अनेक विशेषज्ञ बोर्ड की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते रहे हैं। इन विशेषज्ञों का कहना है कि जल संरक्षण की पारंपरिक विधियों को यह बोर्ड महत्वपूर्ण नहीं मानता। ग्रामीण भारत में जल संरक्षण के लिए कुएं और तालाबों के निर्माण और रखरखाव की समृद्ध परंपरा की बोर्ड द्वारा अनदेखी की गई है। अनेक विशेषज्ञ तो बोर्ड को शुल्क लेकर भूजल के दोहन का अधिकार बांटने वाली संस्था के रूप में चित्रित करते हैं।
संसद में प्रस्तुत कैग की 2021 की एक रिपोर्ट (वर्ष 2004- 2017 तक के आंकड़ों पर आधारित) के अनुसार देश के केवल 19 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने भूजल प्रबंधन के लिए कानून बनाया है। उनमें से भी केवल चार राज्यों में यह कानून आंशिक रूप लागू किया गया है।
[bs-quote quote=”विश्व मौसम विज्ञान संगठन की 2021 की स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज़’ रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर 2002-2021 के मध्य स्थलीय जल संग्रहण में 1 सेमी प्रति वर्ष की दर से गिरावट दर्ज की गई है। भारत में संग्रहण में कम-से-कम 3 सेमी प्रति वर्ष की दर से गिरावट रिकॉर्ड की गई है। देश के कुछ क्षेत्रों में तो यह गिरावट 4 सेमी प्रति वर्ष से भी ज्यादा मापी गई है। विश्व भर में भूजल का सर्वाधिक दोहन भारत द्वारा किया जाता है।1980 के दशक से हमारे देश में भूजल स्तर में गिरावट प्रारंभ हुई जो अब तक जारी है। विशेषज्ञों के अनुसार देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भूजल स्तर में गिरावट 8-16 मीटर तक हुई है।” style=”style-2″ align=”center” color=”” author_name=”” author_job=”” author_avatar=”” author_link=””][/bs-quote]
यह रिपोर्ट बताती है कि भूजल प्रबंधन एवं विनियमन योजना वर्ष 2012 से वर्ष 2020 तक जारी रही। इसके लिए अनुमानित व्यय 3319 करोड़ रुपए था। बजट में इसके लिए 2349 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया। किंतु संबंधित मंत्रालयों द्वारा केवल 1109 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई। इस प्रकार भूजल के स्रोतों की प्रामाणिक जानकारी के एकत्रीकरण और प्रबंधन का कार्य अधूरा रह गया। स्थानीय समुदायों द्वारा भूजल प्रबंधन की तकनीकों की पहचान एवं उनके सशक्तिकरण का कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया।
कैग की इस रिपोर्ट के अनुसार देश में भूजल खपत का राष्ट्रीय औसत 63 प्रतिशत है। किंतु देश के 13 राज्यों में भूजल की खपत राष्ट्रीय औसत से अधिक है। यदि जिलेवार आंकड़े निकाले जाएं तो देश के 267 जिलों में राष्ट्रीय औसत से अधिक भूजल का दोहन किया गया है। देश के अनेक भाग ऐसे हैं जहाँ भूजल की खपत 385 प्रतिशत के डराने वाले स्तर पर पहुंच गई है। भारत के 4 राज्य -पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान- भूजल की 100 प्रतिशत से अधिक खपत कर रहे हैं।
कैग की इस रिपोर्ट में स्वयं केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर यह बताया गया है कि देश के अनेक क्षेत्रों में भूजल में आर्सेनिक, फ्लोराइड, नाईट्रेट, आयरन तथा लवणता निर्धारित स्तर से अधिक है। आश्चर्य यह है कि जिन राज्यों में भूजल का प्रदूषण सर्वाधिक है उन राज्यों का भूजल महकमा कर्मचारियों की भारी कमी से जूझ रहा है।
राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की और ब्रिटिश भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा पंजाब में सतलुज एवं ब्यास नदी तथा शिवालिक पहाड़ियों के मध्य स्थित नौ हजार वर्ग किलोमीटर विस्तार वाले बिस्त-दोआब क्षेत्र में भूजल के प्रदूषण के स्तर का परीक्षण करने के बाद बताया गया कि भूजल में विद्युत चालकता एवं लवणता का स्तर चिंताजनक रूप से बढ़ रहा है। भूजल में सिलेनियम, मोलिब्डेनम और यूरेनियम की घातक उपस्थिति है। इस अध्ययन ने सप्रमाण यह सिद्ध किया है कि मानव-जनित एवं भू-जनित घातक तत्व तलछटीय एक्विफर तंत्र से होकर गहरे एक्विफरों में प्रविष्ट हो रहे हैं जिससे भूजल प्रदूषित हो रहा है।
गंगा बेसिन के निचले हिस्सों के डेल्टा क्षेत्र में भूजल स्रोतों में आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रदूषण प्रायः देखा जा रहा है। औद्योगिक कचरे का सही ढंग से उपचार न करने पर मृदा तो नष्ट हो ही रही है अपितु इसके कारण खाद्य चक्र में कैडमियम जैसे घातक तत्व प्रवेश कर रहे हैं, जैसा हमने बंगाल के डेल्टा क्षेत्रों में होते देखा है।
औद्योगिक और व्यावसायिक संस्थानों में उपयोग में लाए गए जल की रीसाइक्लिंग के लिए अनेक प्रावधान बनाए गए हैं किंतु खर्चीली तकनीकों के कारण प्रायः औद्योगिक एवं व्यावसायिक अपशिष्ट को बिना उपचारित किए दूषित जल को नदियों में छोड़ने के मामले अक्सर देखने में आते हैं और बिना किसी कठोर कार्रवाई के औद्योगिक इकाइयां बच भी निकलती हैं।
फरवरी 2021 में साइंस एडवांसेस में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार भूजल के आवश्यकता से अधिक दोहन के कारण यदि भूजल की उपलब्धता समाप्त हो जाती है और अन्य स्रोतों से सिंचाई की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पाती है तो राष्ट्रीय स्तर पर जाड़े की फसलों के उत्पादन में 20 प्रतिशत की गिरावट हो सकती है जबकि गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों में यह गिरावट 68 प्रतिशत तक होगी। यदि नहरों के माध्यम से सिंचाई द्वारा भूजल के जरिए होने वाली सिंचाई को प्रतिस्थापित भी कर दिया जाए तब भी राष्ट्रीय स्तर पर फसल उत्पादन में 7 प्रतिशत और गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों में 24 प्रतिशत की कमी आ सकती है।
नहरों से सिंचाई की अपनी सीमाएं हैं। भूजल हर जगह उपलब्ध है और विकेन्द्रित सिंचाई व्यवस्था को सुलभ बनाता है जबकि नहरों से जुड़ी परियोजनाओं का वृहद स्वरूप इनके हर स्थान तक पहुंचने में बाधक है। फिर नहरों से सिंचाई मानसून पर आश्रित होगी जो जलवायु परिवर्तन के कारण वैसे ही अनिश्चित व्यवहार कर रहा है।
[bs-quote quote=”फसल चक्र परिवर्तन का प्रश्न जितना सरल दिखता है उतना है नहीं। खाद्यान्न उत्पादन में कमी लाने और ग्लोबल नार्थ की जरूरतों के लिए फसल उत्पादन करने का दबाव हम पर विकसित देशों द्वारा निरंतर डाला जा रहा है और कोई आश्चर्य नहीं कि कृषि के बाजारीकरण के हिमायती जलसंरक्षणवादियों के रूप में धान और गेहूं का रकबा कम करने की सिफारिश करते नजर आएं। देश में खाद्यान्न की आवश्यकता और किसानों के हितों को ध्यान में रखकर फसल चक्र में परिवर्तन किया जाना चाहिए।” style=”style-2″ align=”center” color=”” author_name=”” author_job=”” author_avatar=”” author_link=””][/bs-quote]
प्रख्यात भूजल गवर्नेंस विशेषज्ञ जेनी ग्रोनवाल के अनुसार भूजल का उपयोग और दुरुपयोग दोनों ही स्थानीय और सीमित प्रभाव वाले मुद्दे हैं। केवल भारत में ही 20 लाख पम्पसेट्स के माध्यम से ट्यूबवेल्स से भूजल का दोहन किया जाता है। इन ट्यूबवेल्स की मालकियत छोटे किसानों के पास है। इस परिस्थिति केंद्र से बनाई गई कोई भी नीति देश के सिंचाई व्यवहार में परिवर्तन नहीं ला सकती।
विशेषज्ञों का मानना है कि भूजल संरक्षण के हमारे प्रयास बहुआयामी होने चाहिए। कई विशेषज्ञ उत्तर भारत में चावल और गेहूँ की खेती के रकबे में 20 प्रतिशत की कमी लाने का सुझाव देते हैं और चावल एवं गेहूं जैसी बहुत ज्यादा जल की मांग रखने वाली फसलों के स्थान पर ऐसी फसलें लगाने का सुझाव देते हैं जो उतने ही भूजल का उपयोग करें जितने का पुनर्चक्रीकरण हो सकता है। अर्ध शुष्क, शुष्क अथवा ऊपरी क्षेत्रों में चावल एवं गेहूं के स्थान पर बाजरे की खेती की जा सकती है। इनका यह भी सुझाव है कि सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर्स और ड्रिप इरीगेशन का उपयोग हो तथा नहरों की कार्यक्षमता बढ़ाई जाए।

कुछ विशेषज्ञ यह मानते हैं कि राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना के काम में तेजी लाई जानी चाहिए जिससे अधिक जल उपलब्धता वाले क्षेत्रों से जल की कमी वाले इलाकों की ओर नदियों का पानी ले जाकर सिंचाई की सुविधा का विस्तार संभव हो सकेगा।
फसल चक्र परिवर्तन का प्रश्न जितना सरल दिखता है उतना है नहीं। खाद्यान्न उत्पादन में कमी लाने और ग्लोबल नार्थ की जरूरतों के लिए फसल उत्पादन करने का दबाव हम पर विकसित देशों द्वारा निरंतर डाला जा रहा है और कोई आश्चर्य नहीं कि कृषि के बाजारीकरण के हिमायती जलसंरक्षणवादियों के रूप में धान और गेहूं का रकबा कम करने की सिफारिश करते नजर आएं। देश में खाद्यान्न की आवश्यकता और किसानों के हितों को ध्यान में रखकर फसल चक्र में परिवर्तन किया जाना चाहिए। आधुनिक उपभोगवादी सभ्यता ने जल के साथ मनुष्य के सदियों से चले आ रहे दोस्ताने को भंग कर दिया है, हाल के वर्षों में मनुष्य ने जल को उपभोग की वस्तु मानकर इसका निर्ममता से दोहन किया है।
यह भी पढ़ें –
प्रधानमंत्रियों के चुनावी भाषण पहले कैसे थे अब कैसे होते हैं
भूजल का पुनर्चक्रण बड़ी सरलता से किया जा सकता है, स्थान विशेष की हाइड्रोलॉजी को ध्यान में रखकर रिचार्ज पिट, रिचार्ज ट्रेंच ,रिचार्ज ट्रेंच सह बोरवेल, तालाब, पोखर, सूखा कुंआ, बावली आदि निर्मित किए जा सकते हैं। सतही जल के संग्रहण की विधियां अपनाई जा सकती हैं। छोटे-छोटे चेक डेम भी बनाए जा सकते हैं। नवनिर्मित भवनों, कालोनियों, कार्यालयों तथा औद्योगिक इकाइयों में जल के पुनर्चक्रण की व्यवस्था के लिए नियम बनाए गए हैं किंतु इनका पालन कम उल्लंघन अधिक होता है।
विशेषज्ञों का अभिमत है कि जनजागरूकता और समुदाय की भागीदारी के बिना भूजल की रक्षा असंभव है, हमें अपने घर, मोहल्ले, गांव, कस्बे, शहर से शुरुआत करनी होगी। किंतु इसका आशय यह नहीं है कि सरकार का भूजल संरक्षण के प्रति कोई उत्तदायित्व नहीं है। सरकार को अंधाधुंध औद्योगिक विस्तार पर अंकुश लगाना होगा और भूजल के अनुचित दोहन तथा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों पर कठोर कार्रवाई करनी होगी। देश में अनेक व्यक्तियों और संस्थाओं ने अपने स्तर पर भूजल की रक्षा के लिए अनुकरणीय कार्य किया है। सरकार को इनके अनुभव का लाभ उठाना चाहिए।



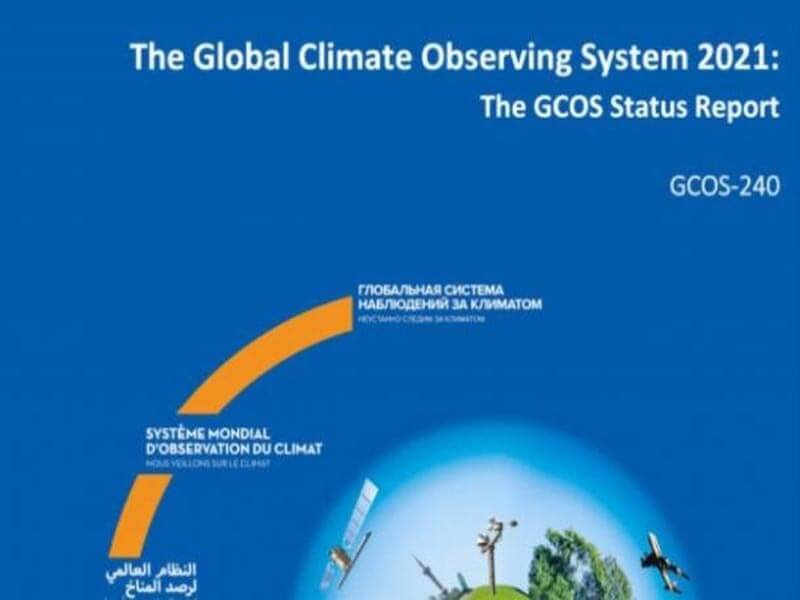


[…] भूजल की अनदेखी का एक और वर्ष […]