कल रात एक सपना देखा। सपना याद नहीं है कि उसे लिख सकूं। जेहन में बस इतना है कि वह सपना मौत को कुछ दिनों के लिए टालने की कोई वैज्ञानिक कवायद थी। कुछ-कुछ इच्छामृत्यु का वैज्ञानिक तरीका। सपने में वह तरीका बेहद कारगर लग रहा था। लेकिन अब चूंकि याद नहीं तो क्या दर्ज करूं।
वैसे इस सपने की पृष्ठभूमि समझ पा रहा हूं। बीते दो दिनों से कबीर के साहित्य के विभिन्न आयामों का अध्ययन कर रहा हूं। साथ ही कबीरपंथ के विभिन्न संस्कारों के बारे में भी।
कबीर का साहित्य अन्यों के साहित्य से अलहदा है। मुझे तो इसमें तीन बातें सबसे अधिक नजर आती हैं। पहला जड़ता का विरोध, दूसरा इश्क और तीसरा सतलोक। कबीर तीनों बातों को बड़ी ही दृढ़ता से रखते हैं। उनका इश्क वाला पक्ष तो इतना शानदार है कि आदमी जब कबीर को पढ़ने लगता है तो खुद-ब-खुद इश्क करने लगता है। दरअसल, इश्क करना मतलब जिंदगी को प्यार करना ही है और जिंदगी को प्यार करने का मतलब वे सभी, जो इस धरती पर हैं, सभी के साथ समता और करुणा का व्यवहार।
[bs-quote quote=”कबीर शांत कवि नहीं थे। उनके अंदर विद्रोह था। वे बड़ी सख्ती से मनुवादी कारखानों का विरोध करते थे। लेकिन यह तो कहना ही पड़ेगा कि वे अहंकारी नहीं थे। वे इश्क करते थे समाज से। वे चाहते थे समाज में समता हो, बंधुता हो।” style=”style-2″ align=”center” color=”” author_name=”” author_job=”” author_avatar=”” author_link=””][/bs-quote]
कबीर अपने साहित्य में जिस तरह जीवन का उत्सव मनाते हैं, उसी तरह अंत काे भी आनंद की तरह प्रस्तुत करते हैं। उनके साहित्य में मौत से खौफ नहीं है। उनकी एक पंक्ति देखिए–
भला हुआ जो मेरी मटकी फूटी रे,
मैं तो पनिया भरन से छूटी रे।
सूफी साहित्य में आप चाहे बाबा बुल्लेशाह को पढ़ें या अमीर खुसरो को या आप चाहें तो गालिब को पढ़ें। मौत अनेक रूपों में सामने आता है। कहीं यह चोला बदलने के जैसा है तो कहीं नैहर छूटने के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। लेकिन कबीर के साहित्य में यह कुछ और रूप लेता है। इसका उदाहरण है उपरोक्त पंक्तियां। इसके अलावा भी कबीर मिट्टी और कुम्हार के बिंब के जरिए बहुत सारी बातें कह जाते हैं। निर्गुण भक्ति की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करते समय कबीर मूर्तिपूजा का विरोध करते हैं। वह एकेश्वरवाद के समर्थक हैं जो कि ब्राह्मणवादी सोच के ठीक उलट है। कबीर एकदम साफ लफ्जों में कहते हैं–
मेरा साहिब एक है, दूजा साहिब न कोय,
जो कोई दूजा साहिब कहे, दूजा कुल का होय।
इस दोहे में वह इस अवधारणा को अभिव्यक्त करते हैं कि इस देश में एक ईश्वर है, जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है और संचालक भी वही है। यदि कोई दूसरे ईश्वर की बात करता है तो वह निश्चित तौर पर द्विज कुल का है। यहां दूजा का मतलब द्विज ही है और द्विज का मतलब दो बार जन्मने वाला। वहीं द्विज जिनके बारे में कबीर ने यह भी कहा–
जो तू बामन-बामनी जाया, फिर आन बाट कहे नहीं आया।
कबीर को पढ़ते समय एक बात को लेकर मेरा विश्वास पुख्ता होता जाता है कि ब्राह्मणवाद आधारित सामाजिक भेदभाव को खत्म किया जा सकता है। कबीर ने इसका सफल प्रयोग अपने जीवन में किया। उनहोंने कबीरपंथ की शुरुआत की। उन्होंने इस देश के कमेरा वर्ग को संदेश दिया कि वे पाखंड से बचें और सृष्टि के निर्माता ने सभी को एक समान अधिकार दिए हैं।
[bs-quote quote=”कबीर ने ब्राह्मणवाद के खात्मे तथा समाज में समता, बंधुता और न्याय की स्थापना के लिए ब्राह्मणवादी संस्थाओं की साख पर हमला बोल था। वे उन्हें पाखंड से परिपूर्ण बताते थे। आरएसएस उनकी इस नीति को दूसरे रूप में यानी नकारात्मक रूप में व्यवहार में ला रहा है। वह इस देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं को निरीह और अप्रसांगिक बना देना चाहता है।” style=”style-2″ align=”center” color=”” author_name=”” author_job=”” author_avatar=”” author_link=””][/bs-quote]
लेकिन कबीर के जाने के बाद ब्राह्ममणवादियों और वर्चस्ववादियों ने उनके प्रभाव को सीमित करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। उनके जीवन को आश्चर्यों से भर दिया। उनके जन्म और मौत दोनों को रहस्यमयी बना दिया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि लोग उनके उपर विश्वास न करें। यह हुआ भी। आज भी बहुत सारे लोग कबीर को भक्ति काल का भक्त कवि ही मानते हैं। जबकि वे संत कवि थे। और तुलसीदास जो कि एक भक्त कवि थे, उनको संत कवि बना दिया गया। यह सब ब्राह्मणवादियों की सफलता है।
दरअसल, कबीर का एक दोहा है। यह दोहा मुझे बार-बार प्रेरित कर रहा है कि सच क्या है। इस दोहे के अनेक रूप में मेरे सामने आए हैं। एक रूप वह जो पाकिस्तानी गायिका आबिदा परवीन ने गाया है–
जब जग में हम पग धरौ, सब हंसे हम रोय।
कबीरा कुछ कर चलो, पाछे हंसी ना होय।
इसी दोहे का भारतीय संस्करण है–
कबीरा जग में जब पैदा हुए, सब हंसे हम रोय,
कुछ ऐसा करा चलो, हम हंसे जग रोय।
दोनों रूपों में उल्लेखनीय अंतिम हिस्सा है। पहले रूप में कबीर कहते हैं पाछे हंसी ना होय, जबकि दूसरे में कहते हैं हम हंसे जग रोय। दोनों में एक खास अंतर है। मेरे हिसाब से जब वे पाछे हंसी ना हो, कहते हैं तो वे अहंकारवश नहीं कहते। जबकि दूसरे में अहंकार की भावना निहित है।
इन दोनों रूपों के आधार हम कबीर को समझने का प्रयास कर सकते हैं। कबीर शांत कवि नहीं थे। उनके अंदर विद्रोह था। वे बड़ी सख्ती से मनुवादी कारखानों का विरोध करते थे। लेकिन यह तो कहना ही पड़ेगा कि वे अहंकारी नहीं थे। वे इश्क करते थे समाज से। वे चाहते थे समाज में समता हो, बंधुता हो।
बहरहाल, कल भारत के लिहाज से एक बड़ा दिन था जब धर्म के नाम पर दिल्ली में पसमांदा मुसलमानों का घर ढाह दिया गया। हालांकि इनमें दलित वर्ग के लोगों के घर भी थे। कुछ लोग अपवाद में किसी पंडित का घर उजड़े जाने की बात भी कर रहे हैं। सबसे दिलचस्प यह रही कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन सहित तीन न्यायधीशों की खंडपीठ के आदेश को भाजपा सरकार ने ठेंगे पर रखा और आशियानों को ध्वस्त करती रही। सुप्रीम कोर्ट को दुबारा हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य होना पड़ा। लेकिन तब तक तो भाजपा सरकार अपना काम कर चुकी थी।
दरअसल, मैंने आज कबीर की इतनी लंबी चर्चा इसलिए की ताकि जो कुछ कल हुआ, उसके बारे में कुछ सोच सकूं। कबीर ने ब्राह्मणवाद के खात्मे तथा समाज में समता, बंधुता और न्याय की स्थापना के लिए ब्राह्मणवादी संस्थाओं की साख पर हमला बोल था। वे उन्हें पाखंड से परिपूर्ण बताते थे। आरएसएस उनकी इस नीति को दूसरे रूप में यानी नकारात्मक रूप में व्यवहार में ला रहा है। वह इस देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं को निरीह और अप्रसांगिक बना देना चाहता है।
खैर, यह समाज है जो सब देख रहा है। ठीक वैसे ही जैसे एक समय जर्मनी के लोगों ने हिटलर को देखा था और उसके बुरे अंत को भी। कबीर की यह पंक्ति शायद हमारे हुक्मरान को समझ में आए, इसलिए दुबारा उद्धूत कर रहा हूं–
जब जग में हम पग धरौ, सब हंसे हम रोय।
कबीरा कुछ कर चलो, पाछे हंसी ना होय।

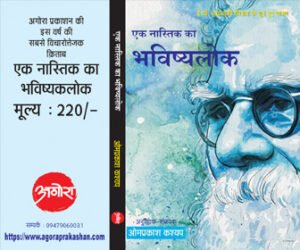
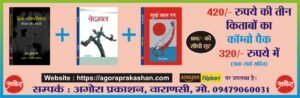
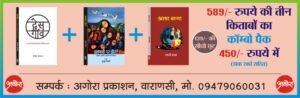






बहुत बढ़िया। यथार्थ का सटीक आकलन। धन्यवाद।