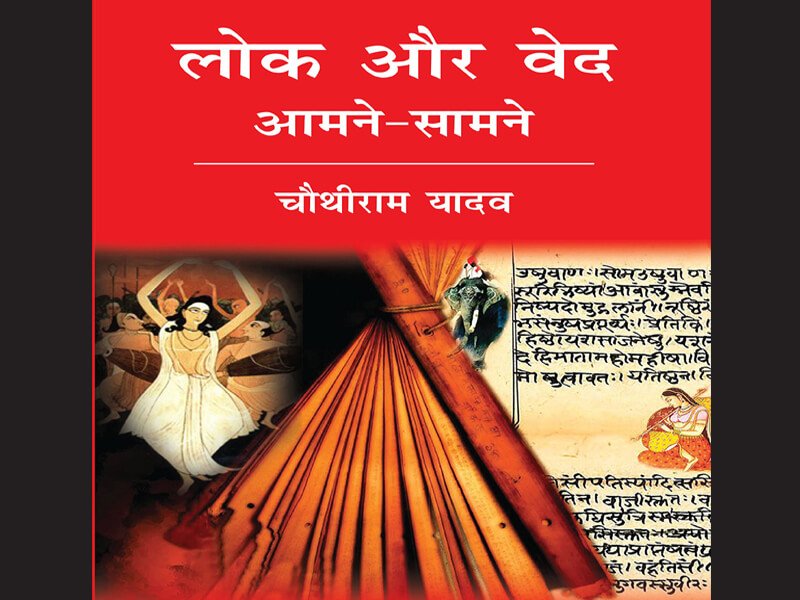दुनिया के अनेक विकासशील और पिछड़े देशों-समाजों की तरह भारतीय समाज में भी सामाजिक विषमता, आर्थिक गैरबराबरी और गहरे सामाजिक-सांस्कृतिक अंतर्विरोध मौजूद हैं। उत्तर-औपनिवेशिक दौर में आजादी की सांस लेते हुए अधिकतर मुल्कों ने अपने सामाजिक-आर्थिक विकास की नई-रणनीति तलाशने की कोशिश की। लेकिन विभिन्न कारणों से कई देशों में सामाजिक-आर्थिक तरक्की का रास्ता कुछ वर्गों-समुदायों तक सिमट कर रह गया और जिस तरह के विकास की उन्हें दरकार थी, वह हासिल नहीं हुआ। एशिया, लातिन अमेरिका और अफ्रीका के कई देशों में इसके उदाहरण मिल जाएंगे। भारत भी ऐसे मुल्कों में शामिल है।
यह भी सच है कि कई देशों ने अपने राजनीतिक-आर्थिक कार्यक्रमों की सफलता-विफलता से सबक लिया और वंचित समुदायों-समाजों की प्रगति और विकास में समान हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए अपनी नीतियों में बुनियादी बदलाव किए। इसमें कुछ लातिन अमेरिकी देशों के पास कई चमकदार उदाहरण मौजूद हैं। कुछ एशियाई देशों ने अपने अलग-अलग गवर्नेंस-माडल के बावजूद उत्पादन की शक्तियों और उत्पादकता में बड़ी कामयाबी हासिल करके अपने समाजों की प्रगति और मानव-विकास सम्बन्धी समस्याओं को हल करने की कोशिश की।
योजना, विकास और हाशिए के लोग
आजादी के बाद, भारत में भी प्रगति और मानव-विकास सम्बन्धी समस्याओं और चुनौतियों को संबोधित करने के लिए कई नए-नए प्रयोग किए जाते रहे लेकिन इसकी खास सामाजिक-संरचना और योजनाकारों के आर्थिक-राजनीतिक सोच की लगातार बदलती दशा-दिशा के चलते गवर्नेंस और विकास का कोई ऐसा मॉडल सामने नहीं आ सका, जो भारत को वह कामयाबी हासिल कराता, जिसका वह अपनी बड़ी कामकाजी आबादी, जल संसाधन, खनिज और शानदार भू-सम्पदा के चलते हकदार है। बीते दो-ढाई दशकों से आर्थिक सुधारों के दौर में हमारे बाजार-व्यापार और आर्थिक-गवर्नेंस में जिस तरह के संरचनात्मक फेरबदल और समायोजन की लगातार कोशिशें की गईं और की जा रही हैं, उससे वंचित तबके या हाशिए के लोग अपनी जीवन स्थितियों में बेहतरी और सतत विकास को लेकर बेहद निराश हैं। स्वयं सरकार या उसके द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समितियों आदि की समय-समय पर जारी की जाने वाली रपटें और सर्वेक्षण भी इसकी पुष्टि करते हैं। प्रगति-दर और जीडीपी के गिरते-बढ़ते आंकड़ों से हमारे समाज की असल तस्वीर नहीं उभरती। लोगों की असल माली-हालत के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य-चिकित्सा, रोजगार और जीवन के अन्य पहलू इस बड़ी तस्वीर के हिस्से हैं। साक्षऱता, औसत जीवन-वर्ष, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और कुपोषण के मामले में भारत की स्थिति अब भी कई विकासशील देशों के मुकाबले दयनीय है। दुनिया के 180 मुल्कों की सूची में हम मानव विकास(HDI) में 130वें नंबर पर हैं। असमानता कम करने के मामले में हम 180 देशों की सूची में हम 135वें नंबर पर हैं। प्रेस फ्रीडम का कुछ ही दिनों पहले जो नया ग्लोबल इंडेक्स-2017 जारी हुआ है, उसमें भारत पहले के मुकाबले 3 अंक नीचे लुढ़कर कर अब 136 वें नंबर पर आ गय़ा है। देश की 80 फीसद सम्पदा पर सिर्फ 10 फीसदी लोगों का कब्जा है। हमारा पड़ोसी श्रीलंका तक हमसे कई मामलों में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। हमारे कुछ ‘अति-राष्ट्रवादी’ इस बात से ‘परम संतोष’ कर सकते हैं कि दूसरा पड़ोसी पाकिस्तान वैश्विक मानव विकास सूचकांक में हमसे भी पीछे है।
पश्चिम के खास खेमे के कुछ अर्थशास्त्रियों और योजनाकारों ने आर्थिक सुधारों की गति तेज करने के लिए विकासशील देशों में अपने बहुचर्चित ‘टपकन सिद्धांत’ (ट्रिकल-डाउन थिउरी) का खूब प्रचार कराया। पर आर्थिक सुधारों के ढाई दशक इस बात के गवाह हैं कि वंचित तबके तक समृद्धि और प्रगति का वाजिब हिस्सा नहीं पहुंच रहा है। कथित आर्थिक उछाल और शानदार ग्रोथ रेट की असल कहानी कुछ और ही है। बीते कुछ वर्षों में देश के अमीरों और गरीबों के बीच खाई बढ़ी है। अमीर वाकई बहुत आगे बढ़े हैं। आर्थिक सुधारों के नाम पर आई चमक पहले से अमीर और उभरते मध्यवर्ग के ऊपरी हिस्से तक सीमित रह गई है। 68वें नेशनल सैंपल सर्वे आर्गनाइजेशन(एनएसएसओ) के एक ताजा सर्वे के मुताबिक देश के ग्रामीण हिस्से की 90 प्रतिशत आबादी का प्रतिदिन का प्रति-व्यक्ति खर्च 68.47 रूपए से भी कम है। इसी तरह, बेतहाशा महंगाई के दौर में शहरी क्षेत्र में 90 फीसदी आबादी के बीच प्रति दिन का प्रति व्यक्ति खर्च 142.70 रूपए से भी कम है। सिर्फ दो साल पहले एनएसएसओ सर्वे ने बताया था कि ग्रामीण भारत में 90 फीसदी आबादी के बीच प्रतिदिन का प्रति व्यक्ति खर्च 55 रूपए से कुछ कम था, जबकि शहरी भारत में यह आंकड़ा 122 रूपए से कुछ कम पाया गया था। अगर महंगाई बढने की दर, चिकित्सा, परिवहन और शिक्षा सहित अन्य जीवनोपयोगी सेवाओं की दर में हुई बढ़ोतरी की रोशनी में देखें तो देश की 80 फीसदी से ज्यादा आबादी की माली हालत और खराब होती गई है, आमदनी और रोजाना के खर्च के हिसाब से उसकी मुश्किलों में इजाफा हुआ है। शहरी अमीरों और ग्रामीण अमीरों के बीच भी भारी खाई है। दोनों की आमदनी और खर्च के हिसाब से देखें तो पाएंगे कि हमारे गणराज्य में वाकई दो तरह के देश-‘इंडिया’ और ‘भारत’ तेजी से पल और बढ़ रहे हैं। शहरी क्षेत्र के सर्वाधिक अमीरों की 10 फीसदी आबादी का मासिक खर्च ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वाधिक अमीर 10 फीसदी लोगों के मासिक खर्च के मुकाबले 221 प्रतिशत ज्यादा है।
ताजा आकड़ों के मुताबिक साक्षऱता, औसत जीवन वर्ष, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और बच्चों को पोषाहार मुहैय्या कराने के मामले में भारत अपने पड़ोसी चीन और ब्राजील जैसे विकासशील देशों से काफी पीछे है। गरीबी के विश्व बैंक के पैमाने की रोशनी में देखें तो चीन की 13 फीसदी आबादी गरीबी रेखा के नीचे है, ब्राजील में सिर्फ 6 फीसदी और भारत में 33 फीसदी। सबसे ह्रदयविदारक आक़डा कुपोषित बच्चों का है। ब्राजील में अत्यंत कुपोषित(उम्र और वजन के अनुपात एवं अन्य पैमाने की गणना सहित) पांच साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या 2 फीसदी आंकी गई है और चीन में 5 फीसदी। लेकिन भारत में यह तादात 44 फीसदी दर्ज की गई है। सब-सहारन अफ्रीकी देशों में यह आकड़ा 25 फीसदी दर्ज किया गया है। भारत की स्थिति उन देशों से भी बुरी है। कैसी विडम्बना है, इस भयानक तस्वीर के बावजूद हमारे खाते-पीते मध्यवर्ग के एक मुखर तबके और योजनाकारों को इस बात का गर्व है कि हमारे पास मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई आने के बाद अब वर्ल्ड क्लास के रिटेल-स्टोर खुलने वाले हैं या कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में अब भारत के कई उद्योगपति शामिल हो गए हैं और हमारा देश जल्दी ही महाशक्ति बनने वाला है। पर इससे सच्चाई को कैसे झुठलाया जा सकेगा! एक तरफ, हमारे समाज के दलित, आदिवासी और अत्यंत पिछड़े समुदायों की ग्रामीण आबादी 21 वीं सदी के भारत में भी बदहाली और लाचारी का ऐसा जीवन जी रही है और दूसरी तरफ, एफडीआई और ईएमआई के जाल में फंसी छोटी सी ‘खुशहाल दुनिया’ मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है।
संस्कृति,वर्चस्व और भूमंडलीकरण
सदियों के अपवर्जन और उत्पीड़न ने हमारी संस्कृति के सबसे सुंदरतम मानवीय मूल्यों का विनाश किया है। उसकी जगह वर्चस्व और नृंशसता के मूल्यों को स्थापित करने की कोशिश की गई है। लेकिन इस तरह की कोशिशों के खिलाफ समाज में प्रतिरोध हमेशा जारी रहा है। सामाजिक द्वन्द्व और विकास की यह सतत प्रक्रिया है। उत्तर-औपनिवेशिक काल में नए ढंग की साम्राज्यवादी रणनीति के चलते मौजूदा परिदृश्य पहले से ज्यादा उलझा हुआ है। उदारीकरण और भूमंडलीकरण के दौर की ‘ग्लोबल-विलेज’ की धारणा ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ जैसे व्यापक मानवीय सोच पर नहीं, पूंजी के विस्तार और मुनाफे के सुदृढीकरण पर आधारित है। लातिन अमेरिकी, अफ्रीकी और अन्य एशियाई देशों की तरह हमारा देश भी इसकी जद में है। जनतंत्र-सेकुलरिज्म पर आधारित आधुनिक मूल्यों वाले हमारे गणराज्य की संस्कृति इससे प्रभावित हुई है। उभरते हुए विशाल मध्य वर्ग का समृद्ध तबका इसका सबसे मुखर सांस्कृतिक दूत बनकर सामने आया है। फिल्म, प्रकाशन, मीडिया, इंटरनेट और मोबाइल, सब पर इसकी छाप है। एक्सक्लूजन या अपवर्जन की प्रक्रिया प्रगति और विकास के इन पंखों पर भी उतर आई है। गरीबों के पास मोबाइल फोन तो आ गए हैं लेकिन वे इसका उपयोग अपने जीवन-यापन के जरूरी उपक्रमों या वर्चस्व की शक्तियों की सेवा में ही कर सकते हैं, अपने ज्ञान-विस्तार में वे आज भी इसका ज्यादा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तकनीक से भाषा जुड़ गई है और वह वर्ग-भेद का आधार बन रही है। हाशिए के लोगों के पास पंचांग, भाग्य-दर्शन, भविष्य फल, सेक्स कथाएं या सांप्रदायिक विद्वेष व कट्टरता जैसी चीजें ज्यादा शिद्दत से पहुंचाई जा रही हैं। फिल्मों, घटिया टीवी कार्यक्रमों और सस्ते किस्म के पोर्न साहित्य के जरिए शहरी और कस्बाई गरीब और साधारण परिवारों के युवाओं को खासतौर पर ज्ञान और प्रतिरोध की संस्कृति से अलग रखने का अभियान चलाया जा रहा है। इस दिशा में विदेशी पूंजी और बड़े निगमों द्वारा नियंत्रित निजी टीवी चैनलों का खास योगदान है। इस तरह के सांस्कृतिक विद्रूपीकरण का असर हमारे सामाजिक-राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में भी साफ देखा जा सकता है। अगर सेक्स-अपराध, पाकेटमारी, ब्लैक-मार्केटिंग, छोटी-मोटी चोरी और उठाईगिरी के मामले में सबसे ज्यादा अपराधी स्लम-एरिया के लोगों, अन्य गरीबों और निम्न मध्यवर्ग के लगातार निर्धन होते परिवारों में पैदा हो रहे हैं तो इसकी ठोस वजह को सामने लाने के बजाय इन वर्गों-समुदायों को कलंकित किया जा रहा है। नृशंसता और वर्चस्व का नया आर्थिक-सांस्कृतिक तंत्र उभरा है। इस प्रगति और सुधार को देखकर अब तो यह लगता है कि आजादी के बाद एक ‘कल्याणकारी राज्य’ के रूप में हमारे देश में जो कार्यनीतियां और कुछेक एजेंडे लागू किए गए, भ्रष्टाचार और लालफीताशाही होने के बावजूद वंचित तबकों पर उनका ज्यादा गहरा और सकारात्मक असर पड़ा। इनमें भूमि-सुधार(जो कुछ ही प्रदेशों में संभव हो सका), सकारात्मक कार्रवाई के एक हिस्से के तौर पर आरक्षण की पहल, निर्धन या कमजोर वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियां, पब्लिक डिस्टिव्यूशन सिस्टम (पीडीएस), सीमित संख्या में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना और बाद में लागू की गई कई छोटी-बड़ी कल्याणकारी योजनाएं शामिल हैं। पर बाद के दिनों में जब कथित सुधारों की आंधी बही तो पब्लिक सेक्टर में व्याप्त भ्रष्टाचार और उसकी नीति सम्बन्धी संकटग्रस्तता का मामला इतना तेज उछला कि देश में मीडिया के जरिए एक तरह की पब्लिक ओपिनियन बनाई गई कि स्टेट की अधीनस्थ संस्थाएं या सरकारी क्षेत्र के तहत गरीबी या समाज की किसी समस्या का समाधान नहीं खोजा जा सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, उद्योग, सब कुछ निजी क्षेत्र के हवाले किया जाना चाहिए। इस अभियान में मुख्यधारा के राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं, योजनाकारों, बैंकर्स और मीडिया हस्तियों की एक ताकतवर लाबी साथ-साथ थी। ताकतवर पश्चिमी देशों की सरकारों और कंपनियों ने इस लाबी को हर तरह से सराहा और भारत में मजबूती दिलाने की कोशिश की। मीडिया में निजीकरण और विनिवेशीकरण के पक्ष में जबर्दस्त माहौल बनाया गया। यह वही दौर था, जब भारत का विशाल खनन क्षेत्र निजी कंपनियों के लिए खोला जा रहा था। बैंकिंग-बीमा आदि क्षेत्रों में भी पहल की जा रही थी। भारतीय समाज की खास विशिष्टताओं के चलते अभी सवर्ण गरीबों और अवर्ण उत्पीड़ितों के बीच जीवंत एका नहीं बनी है पर कई क्षेत्रों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। नव-उदारवादी नीतियों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया जैसे-जैसे तेज होगी, इन वर्गों-समुदायों के बीच नए किस्म के जीवंत रिश्तों का कायम होना लाजिमी होगा, जो हजारों साल के भारतीय सामाजिक इतिहास में शायद पहली बार घटित होगा। गांव के गरीब या मझोले किसान, चाहे वे जिस जाति-बिरादरी के हों, विकास-अवरुद्धता के संकट में फंसे हैं। कर्ज-फांस में उन्हें कई क्षेत्रों में आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा है। आम किसानों के पास ले-देकर सिर्फ थोड़ी-बहुत खेती का ही सहारा है। औद्योगिक विकास न होने की वजह से उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। यही कारण है कि अलाभकारी होने के बावजूद वे अपनी जमीन की हर कीमत पर रक्षा करना चाहते हैं। पिछड़े इलाकों में जब कभी कोई सरकार या सरकार-समर्थित परियोजना-एजेंसी किसी नए प्रकल्प के लिए भूमि-अधिग्रहण का प्रयास करती है तो उसे लोगों के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। भारत जैसा देश वस्तुतः य़ोजना और विकास के इसी रणनीतिक द्वन्द्व में फंसा हुआ है। आम जनता के वोटों से जीतकर कानून बनाने का अधिकार पाने वाले नेताओं को नीति और कानून बनाने का फैसले लेते समय कारपोरेट या बड़ी कंपनियों-बहुराष्टीय निगमों के पक्ष में पलटी मारने में देर नहीं लगती। यही कारण है कि हाल के दिनों में आम जनता के हितों पर कुठाराघात करने वाले कानून अंधाधुंध बने हैं। इससे आदिवासी, मछुआरे, कुम्हार, किसान, कलाजन-दस्तकार और अन्य सामान्य मेहनतकश लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।
रास्ता क्या है?
हाशिए के लोगों या वंचित तबकों के पक्ष में अगर विकास की धारा मोड़नी है तो सही अर्थों में बड़े राजनीतिक-आर्थिक सुधार करने होंगे और कल्याणकारी राज्य की भूमिका को जारी रखना होगा। बड़े लोगों के हितों की खुलेआम पक्षधरता पर आधारित मौजूदा आर्थिक नीतियों में तत्काल बदलाव की जरुरत है। बड़े पैमाने पर उभरते जन-असंतोष और उबलते जनाक्रोश को रोकने का भी यही रास्ता है। विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक-आईएमएफ और बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा संपोषित और प्रस्तावित आर्थिक सुधारों के बजाय देश की बड़ी आबादी के सरोकारों पर आधारित कारगर योजनाएं तैयार करनी होंगी। सतत विकास और ठोस प्रगति का सही रास्ता तभी निकलेगा। इसके लिए देश में ठोस राजनीतिक-सुधार की भी जरुरत है। यह सब चुनावी-सुधारों के बगैर असंभव सा है। कारपोरेट, कालेधन और योजनाओं के पैसे की लूट से उभरे नए माफिया-लंपट तंत्र के असर से चुनाव की प्रक्रिया को मुक्ति चाहिए। बुनियादी चुनाव सुधार पर देश में बहस होनी चाहिए और उसके नतीजों को कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए। बुनियादी चुनावी सुधार सिर्फ मौजूदा कानूनी प्रावधानों में चंद संशोधऩों से नहीं संभव होगा, इसके लिए कानूनी प्रक्रिया में बुनियादी बदलाव, संविधान संशोधन और सबसे बढ़कर जन सजगता की जरुरत है। समाज में जागरुकता, जनपक्षधर सोच और राष्ट्रव्यापी जन-गोलबंदी के बगैर बडे सुधार और बदलाव संभव नहीं होंगे। हाशिए की आवाजों को तभी सुना जा सकेगा और उत्पीड़ित-दमित लोगों को प्रगति और विकास की धारा, जो समाज के संसांधनों और उनके अपने श्रम व कौशल का नतीजा है, में वाजिब जगह मिलेगी।