मजदूर एक स्वतंत्र नागरिक है। उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसका स्वस्थ शरीर, श्रमशक्ति, उसका हुनर और रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए सदा गतिशील रहने की भावना है। कार्ल मार्क्स ने दुनिया के मजदूरों को एक होने का आह्वान इसी आधार पर किया होगा कि ‘तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है बंधनों के सिवा’। यदि मजदूर, बंधुआ मजदूर नहीं है तो बहुत हद तक वह स्वतंत्र रहता है। उसके पास बहुत कमाने और एकत्र करने की चिंता नहीं होती। वह वर्तमान मे जीवित रहता है। यह सच है कि सन नब्बे के दशक मे उदारीकृत विश्व अर्थ व्यवस्था मे मजदूरों के अधिकार काम हुए और उनके हालात भी बिगड़े। सुपरस्टार और ब्लॉकबस्टर फिल्मों के जमाने मे मजदूरों को केंद्र मे रखकर फिल्में कौन बनाता है। आज के समय मे किसानों, मजदूरों, घरेलू नौकरों, कारखाना मजदूरों, खनन मजदूरों, क्लीनर की कहानी अमीर निर्माता-निर्देशकों की नजर से देखना ही दर्शकों की मजबूरी है। बॉलीवुड की कुछ महत्वपूर्ण फिल्में जो मजदूरों और उनके जीवन पर केंद्रित हैं निम्न प्रकार हैं:
 दो बीघा जमीना (1953), बूट पोलिश (1954), जागते रहो (1956), नया दौर (1957), पैगाम(1959), सगीना महतो (1970), नमक हराम (1973), दीवार(1975), गमन (1978), काला पत्थर (1979), अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है (1980), कालिया (1981), कुली (1983), मजदूर (1983), मिर्च मसाला (1987), मै आजाद हूँ (1989), लाड़ला (1994), दस्तक (1996), कोयला (1997) स्वदेस (2004), स्लमडॉग मिलिनायर (2008), आई एम् कलाम ( 2010), पीपली लाइव (2010), चिल्लर पार्टी (2011), स्टैनले का डब्बा (2011), शंघाई (2012), सिटी लाइट्स (2014)।
दो बीघा जमीना (1953), बूट पोलिश (1954), जागते रहो (1956), नया दौर (1957), पैगाम(1959), सगीना महतो (1970), नमक हराम (1973), दीवार(1975), गमन (1978), काला पत्थर (1979), अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है (1980), कालिया (1981), कुली (1983), मजदूर (1983), मिर्च मसाला (1987), मै आजाद हूँ (1989), लाड़ला (1994), दस्तक (1996), कोयला (1997) स्वदेस (2004), स्लमडॉग मिलिनायर (2008), आई एम् कलाम ( 2010), पीपली लाइव (2010), चिल्लर पार्टी (2011), स्टैनले का डब्बा (2011), शंघाई (2012), सिटी लाइट्स (2014)।
बाल मजदूरी (प्रतिषेध एवं नियंत्रण) संशोधन अधिनियम 2016 मे 14 साल से काम उम्र के बच्चों की बाल मजदूरी पर रोक लगाई गई फिर भी बाल मजदूरी जारी है और उनके जीवन पर कई फिल्में बनी हैं।
एंग्री यंगमैन और मजदूरों का आक्रोश
दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन ने एंग्री यंगमैन के तौर पर मजदूरों और गरीबों के गुस्से को आवाज दी। उदारीकरण के बाद (1990) के बॉलीवुड ने किसानों और मजदूरों के मुद्दों पर आधारित फिल्में बनाना काम कर दिया। सन 1950 से लेकर 1970 के दशक तक किसान और मजदूर भारतीय सिनेमा के केंद्र मे रहे। नमक हराम (1973) ऋषिकेश मुखर्जी ने आम आदमी और उसके दुख दर्द पर बेहतरीन फिल्में बनाई। मध्यम वर्ग के मुद्दों को सिनेमा के केंद्र में लाते हुए उन्होंने इसे हिन्दी सिनेमा की अलग धारा के रूप में स्थापित किया। मुखर्जी की फिल्म नमक हराम दो दोस्तों विकी (अमिताभबच्चन) और सोनू (राजेशखन्ना) की कहानी है। विकी फैक्ट्री मालिक है और सोनू मजदूरों के यूनियन काली डर बन जाता है। भिन्न या यूं कहें विपरीत हितों के चलते दोनों दोस्तों में दूरी बढ़ जाती है। दोस्त की हत्या के जुर्म में विकी को जेल हो जाती है।इस फिल्म की कहानी सत्तर के दशक में उस दौर में लिखी गयी जब देश भर में टेक्सटाइल्स मिलों का दौर था।लेफ्ट की राजनीति थी और ट्रेड यूनियन भी प्रभावी थीं। मालिक और मजदूर के बीच आए दिन झगड़े और हड़ताल होती रहती थी।कभी-कभी ये लड़ाईयां हिंसक भी हो जाती थीं। उस दौर में कई फिल्में इस विषय पर बनी जिन में हड़ताल, तालाबंदी और फिर दोनों पक्षों के बीच समाधान को प्रस्तुत किया गया है। दीवार (1973) समाजशास्त्र के तुलनात्मकवंचना (relative deprivation ) सिद्धांत को अमिताभ बच्चन ने कई फिल्मों मे अपनी भूमिकाओं में जिया है। दीवार फिल्म में विजय (अमिताभ) के गरीब मजदूर और ट्रेड यूनियन लीडर पितापर चोरी और धोखाधड़ी का आरोप लगाकर उसके माथे पर ‘मेरा बाप चोर है’ लिखकर अपमानित किया जाता है। इतना ही नहीं उसके पिता की हत्या करके दो बच्चों और उसकी माँ को बेसहारा छोड़ दिया जाता है। बूटपालिश करते हुए सड़क किनारे बैठा हुआ लड़का अमीरों के फेंके हुए पैसे नहीं लेता। उसमें जो स्वाभिमान और बदले की आग है वह उसे गलत राह पर भी ले जाती है लेकिन वह अपने तर्कों से जस्टीफ़ाई भी करता है। अपने साथ हुए ज्यादतियों के लिए विजय ईश्वर तक को दोषी ठहराता है।मजदूरों का जीवन कितना कठिन होता हैऔर बिना बाप के बच्चे कैसे पलते हैं यही दीवार फिल्म की विषय वस्तु है जो बहुत ही मार्मिक है।
 काला पत्थर (1979) यश चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन को कोयला खान के मजदूर की भूमिका मे इस फिल्म मे प्रस्तुत किया जो झारखंड के चासनाला कोयला खान मे हुई एक सच्ची दुर्घटना पर आधारित थी। दुख ही जिनका सौभाग्य है ऐसे मजबूर मजदूरों की व्यथा को चित्रित करती यह फिल्म उनके अंदर पल रहे असंतोष और विद्रोह को भी सामने लाने का काम करती है। मजदूर (1983) दिलीप कुमार और राजबब्बर जैसे अभिनेताओं के माध्यम मिल मालिकों, मजदूरों और उनके मुद्दों को प्रभावी ढंग से यह फिल्म सामने लाती है जिसके एक गीत के माध्यम से यह दावा किया जाता है कि हम मेहनतकश इस दुनिया से एक बाग या खेत नहीं सारी दुनिया माँगेंगे। असल मे मजदूर और किसान ही इस दुनिया की उम्मीद हैं वे मांगने वाले नहीं बल्कि मालिक और सृजनकर्ता हैं। इस फिल्म मे दिलीप कुमार नेहरूवादी विजन के अनुसार उद्योगों को नए भारत का मंदिर बताने का संदेश देते हुए दिखते हैं। हड़ताल करने से मजदूरों को रोकते हैं और सबको साथ मिलजुल कर राष्ट्र निर्माण मे साथ आने का आव्हान करते हैं लेकिन उसमे मजदूरों का सम्मान और बराबरी का अधिकार सर्वोपरि रहता है। मुजफ्फर अली की फिल्म गमन गाँव से महानगरों की तरफ पलायन और टैक्सी चालकों की पीड़ा का एक दस्तावेज है। गमन (1978) फिल्म का नायक लखीमपुर खीरी का एक नौजवान है जो नौकरी की तलाश में मुंबई जाकर एक टैक्सी ड्राइवर बन जाए और अपनी जवान बीवी और बूढ़ी मां को देखने घर लौटने भर के पैसे न जुटा सके इस मजबूरी को सीने में जलन और तनहाई लिए किस तरह जीता है इसकी मार्मिक प्रस्तुति है। इस फिल्म के पहले दस्तक(1970) फिल्म बन चुकी थी जो रोजगार की तलाश मे पुरुषों के प्रवास के मुद्दे को चित्रित करती है। पुरुषों के बाहर जाने के कारण घर मे अकेली महिला की तनहाई को लता की आवाज मे प्रस्तुत करता गीत ‘माई री’ हर बिरहन की पीड़ा और तनहाई की आवाज है। पलायन से महिलाओं को अधिकतम शोषण और पीड़ा का शिकार होना पड़ता है यह एक तथ्य है।
काला पत्थर (1979) यश चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन को कोयला खान के मजदूर की भूमिका मे इस फिल्म मे प्रस्तुत किया जो झारखंड के चासनाला कोयला खान मे हुई एक सच्ची दुर्घटना पर आधारित थी। दुख ही जिनका सौभाग्य है ऐसे मजबूर मजदूरों की व्यथा को चित्रित करती यह फिल्म उनके अंदर पल रहे असंतोष और विद्रोह को भी सामने लाने का काम करती है। मजदूर (1983) दिलीप कुमार और राजबब्बर जैसे अभिनेताओं के माध्यम मिल मालिकों, मजदूरों और उनके मुद्दों को प्रभावी ढंग से यह फिल्म सामने लाती है जिसके एक गीत के माध्यम से यह दावा किया जाता है कि हम मेहनतकश इस दुनिया से एक बाग या खेत नहीं सारी दुनिया माँगेंगे। असल मे मजदूर और किसान ही इस दुनिया की उम्मीद हैं वे मांगने वाले नहीं बल्कि मालिक और सृजनकर्ता हैं। इस फिल्म मे दिलीप कुमार नेहरूवादी विजन के अनुसार उद्योगों को नए भारत का मंदिर बताने का संदेश देते हुए दिखते हैं। हड़ताल करने से मजदूरों को रोकते हैं और सबको साथ मिलजुल कर राष्ट्र निर्माण मे साथ आने का आव्हान करते हैं लेकिन उसमे मजदूरों का सम्मान और बराबरी का अधिकार सर्वोपरि रहता है। मुजफ्फर अली की फिल्म गमन गाँव से महानगरों की तरफ पलायन और टैक्सी चालकों की पीड़ा का एक दस्तावेज है। गमन (1978) फिल्म का नायक लखीमपुर खीरी का एक नौजवान है जो नौकरी की तलाश में मुंबई जाकर एक टैक्सी ड्राइवर बन जाए और अपनी जवान बीवी और बूढ़ी मां को देखने घर लौटने भर के पैसे न जुटा सके इस मजबूरी को सीने में जलन और तनहाई लिए किस तरह जीता है इसकी मार्मिक प्रस्तुति है। इस फिल्म के पहले दस्तक(1970) फिल्म बन चुकी थी जो रोजगार की तलाश मे पुरुषों के प्रवास के मुद्दे को चित्रित करती है। पुरुषों के बाहर जाने के कारण घर मे अकेली महिला की तनहाई को लता की आवाज मे प्रस्तुत करता गीत ‘माई री’ हर बिरहन की पीड़ा और तनहाई की आवाज है। पलायन से महिलाओं को अधिकतम शोषण और पीड़ा का शिकार होना पड़ता है यह एक तथ्य है।
 फूलों के बाजार मे काम करते हुए सिनेमा बनाने का सपना देखने वाले तमिल निर्देशक विनोदराज एक गरीब परिवार मे पैदा हुए थे। नौ साल की उम्र मे उन्होंने स्कूल छोड़ दिया क्योंकि उनके पिता की मृत्यु के बाद घर की जिम्मेदारी उनके कंधों पर या चुकी थी। उनके द्वारा निर्देशित फिल्म पेब्लस इस साल ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है। इसके पहले यह फिल्म कई अन्तराष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुकी है। न्यू यॉर्कर रिव्यू मे विनोद राज को ‘extraordinary observational filmmaker’ कहा है जिनकी फिल्में ‘a gendered vision of rage’ प्रस्तुत करती हैं। विनोदराज की यह फिल्म उनके खुद के जीवन मे घटी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। उनकी खुद की बहन को दहेज न दे पाने के कारण ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया था। पेब्लस फिल्म मे एक शराबी पिता अपने बच्चे को स्कूल से बाहर निकालकर लाता है और अपनी नाराज पत्नी के पास ले जाता है ताकि वह उसे वापस अपने घर ला सके। भारत देश मे बहुत सारी नवविवाहिता लड़कियों को दहेज के लिए न केवल घर से निकाल दिया जाता है बल्कि बर्बर तरीके से जलाकर भी मार दिया जाता है। एक बच्चे की नजर से उसके पिता और उसकी जर्नी को दिखाकर पृथ्वीराज अपने मन मे छुपे दर्द का बदला भी पुरुषों से लेने की कोशिश की है कि वह जलती धूप मे चलकर अपनी घर से बाहर की गई पत्नी के पास जाए उससे माफी मांगे और घर वापस लाने के लिए मिन्नतें करें।
फूलों के बाजार मे काम करते हुए सिनेमा बनाने का सपना देखने वाले तमिल निर्देशक विनोदराज एक गरीब परिवार मे पैदा हुए थे। नौ साल की उम्र मे उन्होंने स्कूल छोड़ दिया क्योंकि उनके पिता की मृत्यु के बाद घर की जिम्मेदारी उनके कंधों पर या चुकी थी। उनके द्वारा निर्देशित फिल्म पेब्लस इस साल ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है। इसके पहले यह फिल्म कई अन्तराष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुकी है। न्यू यॉर्कर रिव्यू मे विनोद राज को ‘extraordinary observational filmmaker’ कहा है जिनकी फिल्में ‘a gendered vision of rage’ प्रस्तुत करती हैं। विनोदराज की यह फिल्म उनके खुद के जीवन मे घटी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। उनकी खुद की बहन को दहेज न दे पाने के कारण ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया था। पेब्लस फिल्म मे एक शराबी पिता अपने बच्चे को स्कूल से बाहर निकालकर लाता है और अपनी नाराज पत्नी के पास ले जाता है ताकि वह उसे वापस अपने घर ला सके। भारत देश मे बहुत सारी नवविवाहिता लड़कियों को दहेज के लिए न केवल घर से निकाल दिया जाता है बल्कि बर्बर तरीके से जलाकर भी मार दिया जाता है। एक बच्चे की नजर से उसके पिता और उसकी जर्नी को दिखाकर पृथ्वीराज अपने मन मे छुपे दर्द का बदला भी पुरुषों से लेने की कोशिश की है कि वह जलती धूप मे चलकर अपनी घर से बाहर की गई पत्नी के पास जाए उससे माफी मांगे और घर वापस लाने के लिए मिन्नतें करें।
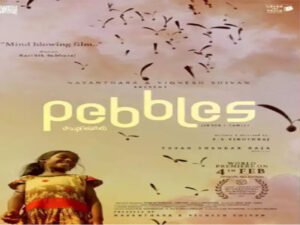
हॉलीवुड और मजदूरों की दास्तान
मध्यम और उच्च वर्ग का फिल्ममेकर जो ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाकर मुनाफा कमाने मे लगा है वह किसानों या मजदूरों की ज़िंदगी पर सिनेमा क्यों बनाएगा फिल्म उद्योग के सामने यह सबसे बडा सवाल है। गरीबों और अमीरों की जिंदगी के बीच जो फासले हैं, असमानताएं हैं वह आज भी पूरी दुनिया के सामने अनुत्तरित सवाल की तरह खड़ा है। ऐसा नहीं है कि मजदूरों के जीवन पर फिल्में बनाकर नाम और पैसा नहीं कमाया गया। भारत देश मे तो दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन मजदूरों और यतीमों के किरदार निभाकर महानायक और सुपरस्टार बन गए। उनकी फिल्मों ने अपने समय मे न केवल जन शिक्षण और मनोरंजन किया बल्कि मजदूरों के शोषण के विरुद्ध विद्रोह की आवाज बनकर भी उभरे।
हॉलीवुड मे मजदूरों और ट्रेड यूनियन पर बहुत सारी फिल्में बनी है लेकिन अब वहाँ भी इन विषयों पर कम फिल्में बनती हैं। कुछ फिल्मों का विवरण यहाँ दिया जा रहा है:
 द किलिंग फ्लोर (The Killing Floor 1984) प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की घटनाओं पर केंद्रित फिल्म है। बिल ड्यूक निर्देशित इस फिल्म मे अमेरिका के दक्षिण हिस्से से पलायनकरकेआएएकब्लैकमजदूरएक बूचड़खाने मे जानवरों की स्लटेरींग और मांस की पैकिंग का कार्य किया जाता है। गोरे और काले मजदूरों के बीच रंगभेद को लेकर जो संघर्ष है उसमे ट्रेड यूनियन के माध्यम से शोषित मजदूरों के संगठित होने की दास्तान पेश की गयी है। हॉलिवुड की अन्य महत्वपूर्ण फिल्मों मे नोरमा रे (Norma Rae1979), ब्रेडएंडरोजेज(2000), पैरासाइट (Parasite2019),अटलांटिस(a tlantics 2019), सॉरी टू बादर यू (Sorry to Bother You2018), द लैंड (The Land 1970), टाइगरटेल (Tigertail 2020), द ऑर्गनाइज़ेर (The Organizer1963), रोमा (Roma2018), द मोटर साइकिल डायरी (The Motorcycle Diaries 2004), माटेवान (Matewan 1987), मेड इन डागेनहाम (Made in Dagenham 2010) हैं जो मजदूरों की जिंदगी के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करती हैं।
द किलिंग फ्लोर (The Killing Floor 1984) प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की घटनाओं पर केंद्रित फिल्म है। बिल ड्यूक निर्देशित इस फिल्म मे अमेरिका के दक्षिण हिस्से से पलायनकरकेआएएकब्लैकमजदूरएक बूचड़खाने मे जानवरों की स्लटेरींग और मांस की पैकिंग का कार्य किया जाता है। गोरे और काले मजदूरों के बीच रंगभेद को लेकर जो संघर्ष है उसमे ट्रेड यूनियन के माध्यम से शोषित मजदूरों के संगठित होने की दास्तान पेश की गयी है। हॉलिवुड की अन्य महत्वपूर्ण फिल्मों मे नोरमा रे (Norma Rae1979), ब्रेडएंडरोजेज(2000), पैरासाइट (Parasite2019),अटलांटिस(a tlantics 2019), सॉरी टू बादर यू (Sorry to Bother You2018), द लैंड (The Land 1970), टाइगरटेल (Tigertail 2020), द ऑर्गनाइज़ेर (The Organizer1963), रोमा (Roma2018), द मोटर साइकिल डायरी (The Motorcycle Diaries 2004), माटेवान (Matewan 1987), मेड इन डागेनहाम (Made in Dagenham 2010) हैं जो मजदूरों की जिंदगी के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करती हैं।
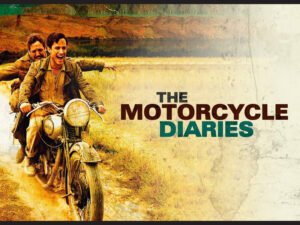
सिनेमा पर मजदूरों का बहुत ज्यादा कर्ज़ है
बॉलीवुड हो या हॉलीवुड सच यही है कि मजदूरों के मुद्दे सिनेमा से गायब हैं। ट्रेड यूनियन और हड़ताल भी बीते दिनों की बात हो चुकी हैं। बड़े कारखाने बंद होने लगे हैं क्योंकि मशीनीकरण और आटोमेशन के कारण मानव श्रम की जरूरत और महत्ता कम होती जा रही है। हड़ताल और तालाबंदी अब सुनने को नहीं मिलते। दुनिया भर के देशों मे तमाम ऐसे कानून बन चुके हैं जो मजदूरों की छंटनी और नौकरी से हटाने के एकतरफा अधिकार पूँजीपतियों को देते हैं। कोरोना काल की देशव्यापी बंदी मे अपने गांवों और घरों की तरफ लौटता बेहाल मजदूरों की हालत किसी से छुपी नहीं है लेकिन उनके ऊपर 1232 माइल्स को छोड़कर कोई अछि फिल्म ओटीटी प्लेटफार्म पर भी नहीं आई जो साबित करती है कि मजदूर और उनके मुद्दे फ़िल्मकारों के लिए कितनी अहमियत रखते हैं। कार्ल मार्क्स के हवाले से कहे तो इस दुनिया का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है जिसमे मजदूरों का शोषण जारी है, वह अलगाव मे जीने को मजबूर है, उसकी बेड़ियाँ अभी जोर से उसे जकड़े हूए हैं, मालिक उसे इतनी भी मजदूरी नहीं दे रहा कि वह खुद जिए और अपने बच्चों को जिंदा रख सके और निकट भविष्य मे दुनिया के मजदूरों के एक होने की संभावनाए दूर-दूर तक नजर नहीं आतीं। वे रोज-रोज खटने, लड़ने और मरने को बाध्य हैं पूरी दुनिया मे फिर भी मैं कहता हूँ कि मजदूर स्वतंत्र नागरिक है।
संदर्भ
पीटरसेन, हन्नाह एलिस (2021) फ्राम चाइल्ड लैबरर टू ऑस्कर होपफुल द एक्स्ट्रा ऑर्डनेरी लाइफ ऑफ पीएस विनोदराज, South Asia correspondent, Sun 21 Nov 2021




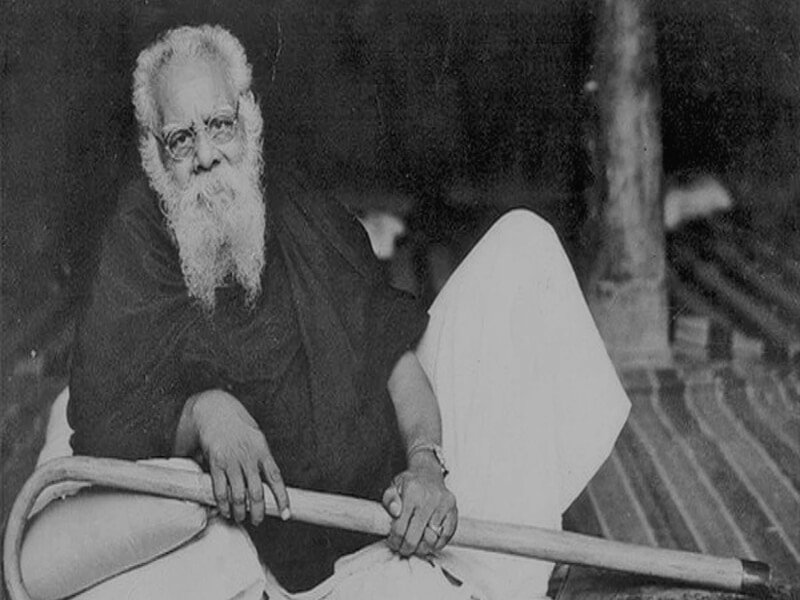
मजदूरों की मेहनत किसी भी कार्य को करने में भेद नहीं करती। उनके पसीने सभी के लिए समान रूप से निकलते हैं। मजदूरों की मेहनत को सलाम।
मजदूर की कोई जाती धर्म नही है मजदूर स्वयं में एक जाति धर्म है जो अपने और परिवार का भरण पोषण करने के लिए मेहनत का कार्य कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है।
विवेचनापूर्ण एवं पठनीय आलेख। बधाई।
राकेश पटेल जी द्वारा सिनेमा के माध्यम से भारतीय मजदूर के जीवन की पड़ताल करने का बहुत ही सकारात्मक प्रयास किया गया है । कार्ल मार्क्स ने दुनिया के मजदूरों को एक होने का आह्वान इसी आधार पर किया होगा कि ‘तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है बंधनों के सिवा’। यदि मजदूर, बंधुआ मजदूर नहीं है तो बहुत हद तक वह स्वतंत्र रहता है। उसके पास बहुत कमाने और एकत्र करने की चिंता नहीं होती। वह वर्तमान मे जीवित रहता है।
आज के समय में लोग जीवन की आप धापी में इतना व्यस्त हैं कि उनको सम के एक बड़े सर्वहारा वर्ग से कोई सरोकार नहीं है । किसानों, मजदूरों, घरेलू नौकरों, कारखाना मजदूरों, खनन मजदूरों, क्लीनर की कहानी अमीर निर्माता-निर्देशकों की नजर से देखना ही दर्शकों की मजबूरी है। भारतीय सिनेमा में दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन ने एंग्री यंगमैन के तौर पर मजदूरों और गरीबों के गुस्से को आवाज दी । किन्तु उसके बाद बॉलीवुड द्वारा इस वर्ग को लेकर समुचित विवेचन का कोई प्रायास नही किया गया । हॉलीवुड मे मजदूरों और ट्रेड यूनियन पर बहुत सारी फिल्में बनी है लेकिन अब वहाँ भी इन विषयों पर कम फिल्में बनती हैं।
मध्यम और उच्च वर्ग का फिल्ममेकर जो ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाकर मुनाफा कमाने मे लगा है वह किसानों या मजदूरों की ज़िंदगी पर सिनेमा क्यों बनाएगा फिल्म उद्योग के सामने यह सबसे बडा सवाल है। गरीबों और अमीरों की जिंदगी के बीच जो फासले हैं, असमानताएं हैं वह आज भी पूरी दुनिया के सामने अनुत्तरित सवाल की तरह खडे हैं । राकेश पटेल जी द्वारा इतने संवेदनशील मुद्दे पर कलम चलाना काबिले तारीफ है।
सर को बहुत बहुत बधाई….???
ज्ञानपरक शानदार लेख?
[…] […]
[…] […]