अक्सर यह सवाल खुद से पूछता हूं कि मुझे कैसा समाज चाहिए और जैसा समाज चाहिए उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं। कई बार तो मैं अपने ही सवाल को अपने नोट बुक के पन्ने पर लिखने के बाद फाड़ देता हूं और इस इत्मीनान के साथ आगे बढ़ जाता हूं कि समाज खुद कभी न कभी जवाब दे ही देगा। वजह यह कि समाज कोई अमूर्त चीज नहीं है। लेकिन कई बार खुद को जवाब भी देता हूं। मैं खुद को उदाहरण देता हूं कभी पश्चिम के समाज का तो कभी अफ्रीकी देशों के समाज का। जब उनसे भी मेरा अंतर्मन संतुष्ट नहीं होता तो उसे लोकल समाज के बारे में बताता हूं। कई बार उसे फुले, पेरियार और आंबेडकर के द्वारा समाज को लेकर किए गए चिंतन के बारे में समझाता हूं तो कभी खुद ही समाज की व्याख्या करता हूं। मेरी अपनी व्याख्या बहुत सरल है। सरल इस मायने में कि समाज का मतलब ही है कि आदमी सुकून के साथ जीवन व्यतीत करे और दूसरों को भी सुकून मिले, इसके लिए प्रयास करे। इसमें दूसरों को सम्मान देना बहुत जरूरी है। जबतक हम दूसरे को सम्मान नहीं देंगे, हम अपने लिए सम्मान की अपेक्षा नहीं कर सकते।
जब मैं पटना में अपने गांव में कुछ दिनों के लिए रहता हूं तब एक तरह की डांट लगभग रोज ही पापा से खानी पड़ती है। उनके मुताबिक, मैं सामाजिक आदमी नहीं हूं। वह चाहते हैं कि मैं गांव के समाज में हिस्सेदारियां लूं, ठीक वैसे ही जैसे मेरे बड़े भाई कौशल किशोर कुमार लेते हैं। उनका तो हाल यह है कि गांव में कुछ भी हो जाय, वे सबसे आगे खड़े रहते हैं। मैं उनके जैसा नहीं कर पाता। कई वजहें हैं। बड़ी वजह तो यही कि मेरे पास समय का बड़ा अभाव होता है। पढ़ने-लिखने से ही फुर्सत नहीं मिलती तो आदमी चाहे भी तो गांव के चौराहे पर बैठकर लोगों से बातचीत कैसे करे?
[bs-quote quote=”भी हाल ही बिहार में जीतन राम मांझी द्वारा दिया गया बयान चर्चा में है। उन्होंने अपने समाज के लोगों से ब्राह्मणवादी कर्मकांड का परित्याग करने का आह्वान किया। वे पहले ऐसे नहीं हैं, जिन्होंने ऐसा किया है। कबीर से लेकर फुले, आंबेडकर और पेरियार तक ऐसा कर चुके हैं। उनके पहले बिहार के मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद ने भी एक खूबसूरत नारा दिया था– पढ़ना-लिखना सीखो, ओ सूअर चरानेवालों, भैंस चरानेवालों, ताड़ी उतारनेवालों। चरवाहा विद्यालय का उनका एक कांसेप्ट बहुत अच्छा था। ” style=”style-2″ align=”center” color=”” author_name=”” author_job=”” author_avatar=”” author_link=””][/bs-quote]
गांव के समाज से एक बात याद आयी। मेरे गांव में अनेक जातियों के लोग रहते हैं। मैं अपने गांव को आदर्श गांव से थोड़ा सा कमतर मानता हूं। वजह यह कि मेरे गांव के लोगों में भी जातिगत अहंकार और कुंठाएं हैं। जिस जाति की आबादी गांव में कम है, वे लोग दबकर रहते हैं। कई बार तो मैंने यह भी देखा है कि मेरी ही जाति के युवा कम आबादी वाले जाति की महिलाओं को लेकर जातिगत टिप्पणियां करते हैं। मुझे बुरा लगता है तो मैं उन्हें टोक देता हूं। कई बार वे मान जाते हैं तो कई बार मुझसे उलझ भी जाते हैं।
दरअसल, यही हाल पूरे बिहार का है। झारखंड के समाज को मैं अलग मानता हूं। लेकिन यह मेरी प्राथमिक टिप्पणी है और इसके पीछे झारखंड में मेरे कुछेक दिनों का अनुभव और वहां की खबरें व रपटें हैं। दिल्ली का समाज अलग है। यहां समाज जैसा कुछ है ही नहीं। मतलब यह कि जिस तरह की सामूहिकता का दर्शन हम गांवों में करते हैं, दिल्ली में मुझे देखने को नहीं मिलता। अभी हाल की ही घटना है। मेरे रहवास के ठीक सामने रहने वाले एक युवा व्यवसायी का निधन हो गया। हालत यह थी कि उसकी लाश उठाने को मुहल्ले का एक आदमी भी आगे नहीं आया। जबकि कोरोना का कहर नहीं था। मैं यहां किराएदार के रूप में रहता हूं और मेरी अपनी आदतें, वैसी ही हैं जैसी पटना में रहने पर होती हैं।
दरअसल, समाज का निर्माण हम खुद ही खुद के लिए करते हैं। सभी ऐसा ही करते हैं और एक समाज बन जाता है। मेरी जेहन में एक घटना है। इस घटना को मैंने अपने पहले उपन्यास में भी दर्ज किया है। घटना यूं है कि एक गांव की दलित महिला ताड़ी बेचती है। उसका पति ताड़ के पेड़ से ताड़ी उतारता है। गांव के लोग बड़े मजे से उस महिला से ताड़ी खरीदते हैं और पीते हैं। महिला गांव के अधिकांश लोगों के लिए भौजाई लगती है तो लोग हंसी-मजाक भी करते हैं। एक बार उस महिला ने अपनी बेटी की शादी की तो उसे लगा कि गांव के सभी लोग उसमें शरीक होंगे। वजह भी थी कि सभी के साथ उसके अच्छे संबंध थे। लेकिन उसकी सोच धरी की धरी रह गई। गांव के ऊंची जाति के लोगों ने उसके घर जाकर उसकी बेटी की शादी में शामिल नहीं हुए।
मतलब यह कि महिला के हाथ से ताड़ी और चखना खरीदकर खाने-पीने से लोगों का धर्म संकट में नहीं आता। लेकिन उसके घर जाने और भोज में शामिल होने से समाज पीछे हट जाता है।
तो यह हालात आज भी है। अब तो मेरे गांव के समाज के कई टुकड़े हो चुके हैं। यादवों का अपना समाज है, कोईरी लोगों का अपना समाज है। जिनकी आबादी कम है, उनका भी अपना समाज है। सभी अपने समाज के लोगों को ही महत्व देते हैं।
[bs-quote quote=”अब सब तरह का अंतर है। जीतनराम मांझी ने जिस दर्द की अभिव्यक्ति की है, उसे समझा जाना चाहिए। मैं तो इसी तरह की घटना उत्तराखंड के चंपावत जिले में देख रहा हूं जहां सवर्ण बच्चों ने एक दलित महिला रसाेइया के हाथों का पका खाना खाने से इंकार कर दिया और राज्य सरकार का हाल देखिए कि उसने उस महिला रसोइया को काम से हटा दिया है। काम से हटाने की वजह राज्य सरकार के अधिकारी ने उसकी नियुक्ति में गड़बड़ी बताई है।” style=”style-2″ align=”center” color=”” author_name=”” author_job=”” author_avatar=”” author_link=””][/bs-quote]
मैं सोचता हूं कि इसके पीछे शिक्षा की बड़ी कमी ही जिम्मेदार है। शिक्षा मतलब केवल स्कूलों व कालेजों में पढ़ाई जानेवाली शिक्षा नहीं। वह शिक्षा जो लोगों को इंसान बनाती है, उसके प्रसार की आवश्यकता है। अभी हाल ही बिहार में जीतन राम मांझी द्वारा दिया गया बयान चर्चा में है। उन्होंने अपने समाज के लोगों से ब्राह्मणवादी कर्मकांड का परित्याग करने का आह्वान किया। वे पहले ऐसे नहीं हैं, जिन्होंने ऐसा किया है। कबीर से लेकर फुले, आंबेडकर और पेरियार तक ऐसा कर चुके हैं। उनके पहले बिहार के मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद ने भी एक खूबसूरत नारा दिया था– पढ़ना-लिखना सीखो, ओ सूअर चरानेवालों, भैंस चरानेवालों, ताड़ी उतारनेवालों। चरवाहा विद्यालय का उनका एक कांसेप्ट बहुत अच्छा था।
लेकिन मुझे लगता है कि पूंजीवाद और अब नवउदारवाद ने हमारे समाज को बदल दिया है। इस दिशा में विमर्श जरूरी है। टेलीविजन चैनलों पर जिस तरह का समाज दिखाया जाता है, वह समाज दरअसल समाज है ही नहीं। सामूहिकताविहीन समाज हर घर में देखा जाता है। पूंजी का असर सामने आता है। मैं तो गांव का आदमी हूं। मेरे गांव में कोई ऐसा पर्व नहीं होता था, जिसमें सामूहिकता नहीं होती थी। यहां तक कि शादी और गमी के मौके पर भी लोग एक-दूसरे का साथ नहीं छोड़ते थे। भोज आदि में हलवाई रखे जाने की बात तो एकदम हाल की है। पहले तो गांव के लोग ही मिलकर अपने लिए खाना पकाते थे। गांव की महिलाएं मिल-जुलकर करमा, जीतिया और तीज आदि त्यौहार मनातीं। कोई अंतर नहीं होता था कि कौन किस जाति की हैं। उनके बीच वर्ग का अंतर तो था ही नहीं।
गंगा में लाशों का मंजर और हुकूमत का सच (डायरी 17 दिसंबर, 2021)
अब सब तरह का अंतर है। जीतनराम मांझी ने जिस दर्द की अभिव्यक्ति की है, उसे समझा जाना चाहिए। मैं तो इसी तरह की घटना उत्तराखंड के चंपावत जिले में देख रहा हूं जहां सवर्ण बच्चों ने एक दलित महिला रसाेइया के हाथों का पका खाना खाने से इंकार कर दिया और राज्य सरकार का हाल देखिए कि उसने उस महिला रसोइया को काम से हटा दिया है। काम से हटाने की वजह राज्य सरकार के अधिकारी ने उसकी नियुक्ति में गड़बड़ी बताई है।
खैर, हम कैसा समाज चाहते हैं और हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, हमें खुद विचार करना चाहिए। फिलहाल तो मैं यह देख रहा हूं कि आदमी सामाजिक नहीं, आर्थिक प्राणी बनता जा रहा है।
ओह, फिर से बचपन याद आ गया।
तब घरौंदा होता था आंगन में
होते थे उसमें कुछ कमरे
कुछ खिड़कियां
और एक दस-बीस अंगुल की सीढ़ी
जिसपर ऊंगलियों के सहारे
कोठे पर जाना होता था।
अब एक इमारत है
बड़े-बड़े दरवाजे
और छोटी-बड़ी कई खिड़कियां हैं।
लेकिन
सब बेकार।
नवल किशोर कुमार फॉरवर्ड प्रेस में संपादक हैं।




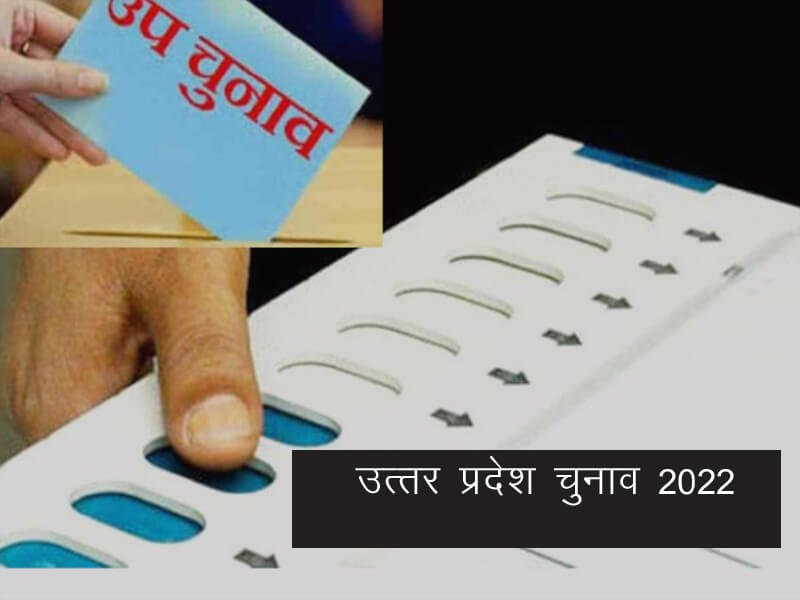

[…] आदमी अब सामाजिक नहीं, आर्थिक प्राणी है… […]