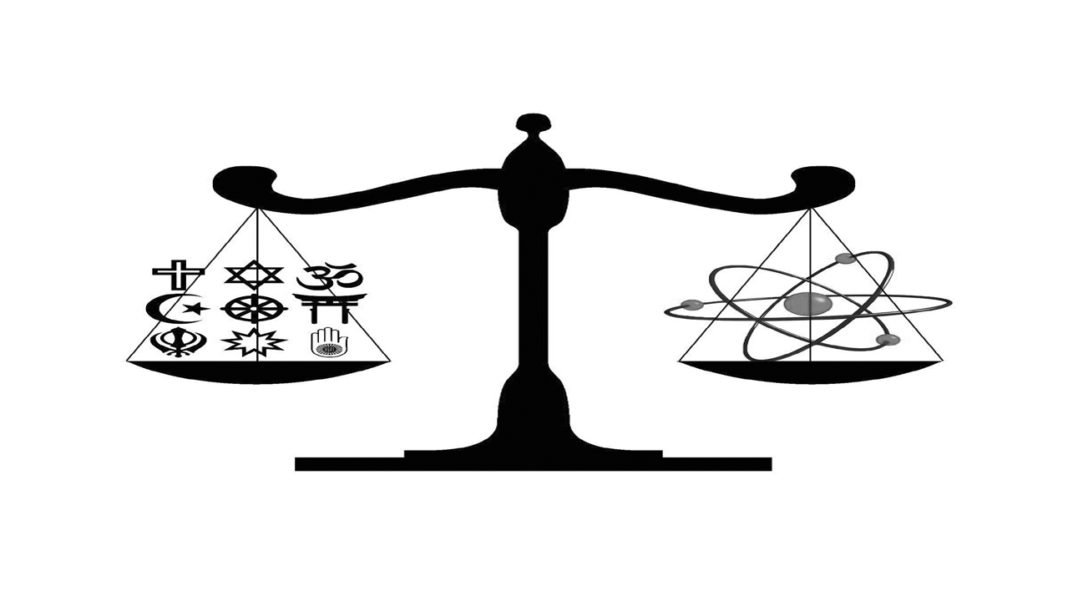मेरा जन्म महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के मालवण तालुका के कांदलगाँव में 12 जुलाई 1958 को हुआ। हमारे माता-पिता की चार सन्तानें हैं। मेरे एक बड़े भाई जो अध्यापक थे और अब चौरासी साल के हैं। मैं चौथे नंबर की हूँ। इस तरह मेरे बड़े भाई और मुझमें बीस साल का फासला है।
यह गाँव कोंकण क्षेत्र में पड़ता है। जब मैंने होश संभाला तो देखा कि इस गाँव में हमारे लोगों में एक अलग तरह की संचेतना का विकास हो रहा है। यह संचेतना बाबा साहब की धम्मक्रांति के बाद फैली। 1956 में उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि अपना पुराना स्थान छोड़ दो तभी प्रगति करोगे। लोगों ने इस बात को माना और उन्होंने हिन्दू धर्म छोड़ दिया और अछूतपन और भेदभाव से निजात पाने के लिए बौद्ध हो गए। मेरे जन्म के पहले ही यह परिघटना हो चुकी थी।
मेरी यादें तभी की हैं। बाबा साहब ने जब गाँव-देहात में धम्म क्रांति का ऐलान किया तो इस गाँव के लोगों का जीवन रातों-रात बदल गया ऐसा नहीं था। लेकिन धीरे-धीरे बदलाव आया। मैंने बचपन में अपना जो गाँव देखा उसमें छुआछूत के आधार पर विभाजन था। हमारी बस्ती गाँव के बाहर थी। उसे अस्पृश्य बस्ती के रूप में देखा जाता था। लेकिन धम्म क्रांति के बाद उसे बौद्ध बस्ती कहा जाने लगा। मेरे गाँव के लोगों को प्रगति की दिशा में ले जानेवाला बौद्ध धम्म ही है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि लोगों ने उसे स्वीकारा और तुरंत ही उनके जीवन में बदलाव दिखाई देने लगा। इसमें एक लंबा समय लगा।

जाति और गरीबी के दोहरे पाटों तले दबा समाज
हमारी अस्पृश्य बस्ती केवल छुआछूत का शिकार नहीं थी बल्कि वहाँ गरीबी और दरिद्रता का बोलबाला भी था। हमारे गाँव में ब्राह्मण का एक घर था। वह खेती करता था। इसके बावजूद उसको बहुत सम्मानित माना जाता था। बाकी के लोगों में तेली, कुनबी, भंडारी आदि ओबीसी जातियाँ थीं। मराठा लोग थे। उन सबके पास बहुत ज्यादा ज़मीनें थीं। इसलिए वे लोग शावकार अथवा महाजन कहे जाते थे। वे ऊंची जाति के माने जाते थे। लेकिन बौद्ध बस्ती में कोई भी ऐसा सम्पन्न नहीं था। किसी के पास भी ज़मीन नहीं थी। इसका कारण सबको मालूम है कि दलितों की आजीविका के साधन यहाँ की सामाजिक व्यवस्था ने पूरी तरह नष्ट कर दिया था।
अपनी ज़मीन न होने कारण कारण दलित दूसरे के खेतों में मजदूरी करते थे। ज़्यादातर मराठों के खेत में क्योंकि वे ही सबसे अधिक अमीर थे। अस्पृश्यता के कारण दलितों के साथ वे बुरा व्यवहार करते थे। बेगार, कम मजदूरी, गाली-गलौज और हिंसा के माध्यम से उनका शोषण होता रहता। तो मैंने जाति और गरीबी के कारण अपने लोगों का शोषण और दमन देखा। लेकिन यह दलितों के साथ ही था, क्योंकि हमारे गाँव का ब्राह्मण गरीब था फिर भी उसको सम्मान मिलता था। लेकिन वैसे ही गरीब दलित को कोई सम्मान नहीं था। उनको मंदिरों में जाने पर रोक थी।
जब मैं छोटी थी तब दूध लेने के लिए जाती थी। एक-दो घर ओबीसी समुदाय के लोग थे जो गाय-भैंस पालते थे और दूध बेचते थे। वे लोग दूध ऊपर से डालते थे। उनके मन में हम जैसे ग्राहकों के लिए कोई सम्मान नहीं था बल्कि कहीं वे हमसे छू न जाएँ इस बात का डर था। कहने का मतलब कि हमारा गाँव जातिवाद से भरा हुआ था। हमारी बस्ती में दो अध्यापक थे। एक डी डी कदम थे। उनको लोग मास्टर कहते थे। उनके घर में हम त्रिशरण-पंचशील के लिए जाते थे। उस समय हम इसको प्रार्थना कहते थे। हमको इतना ही समझ आता था कि यह प्रार्थना है।
मेरे माता-पिता
मेरे-माता-पिता का घर छोटा सा था। झोपड़ी। घर में बहुत गरीबी थी। पिता मजदूरी करते थे। माँ ने हमें पालने के लिए बाँस की टोकरियाँ बनाई। यह काम माँ ने सीख लिया था। इसलिए उसने कठिन समय में घर को भुखमरी से बचाया। माँ का मायका सम्पन्न था। अच्छा जीवन स्तर था, क्योंकि माँ के चाचा सेना में नौकरी करते थे। उनके पिता भी म्युनिसिपलिटी में नौकरी करते थे। इसलिए उनके पास थोड़ी ज़मीन भी थी।
मेरे पिता से शादी हो गई। पिताजी का घर गरीबी में था। इसलिए माँ को उसका सामना करना पड़ा। माँ-पिता की शादी का किस्सा यूं है कि उन दिनों छोटी उम्र में शादियाँ होती थीं। माँ की उम्र उस समय चौदह साल की थी। मेरे पिताजी को देखने के नाना लोग गए। लेकिन नाना को जमा नहीं। इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया।
लेकिन मेरी ददिहाल के लोगों ने नानाजी को डराया कि अगर तुमने हमारे बेटे से अपनी बेटी की शादी नहीं की तो किसी भी दूसरी जगह शादी नहीं कर पाओगे। कहीं और शादी करोगे तो तुम्हारी बेटी कैसे सुखी रहेगी। उस समय कांदलगाँव में रामेश्वर भगवान का भय दिखाया कि तुम्हारी बेटी कहीं और कैसे सुखी रहेगी। यह एक ऐसा भय था जिसका आगे मेरे नाना ने हार मान ली और इस तरह मेरे माता-पिता की शादी हो गई। लेकिन एक बात देखिये कि दलितों में धम्म क्रांति हो गई। उन्होंने बौद्ध धम्म अपना लिया फिर भी अपने स्वार्थ के लिए कैसे अपनी पुरानी मान्यताओं को ओढ़ लिया।

यह बात मेरे माता-पिता की है जब पुराने विचारों के असर में एक सम्पन्न घर की लड़की गरीब लड़के के साथ ब्याह दी गई। यह सब भगवान का डर पैदा करके किया गया। उनके पहले हमारी न जाने कितनी पीढ़ियाँ हैं जो इस डर का शिकार बनाई जाती रही हैं।
वतनदारी की घृणित प्रथा के शिकार
हालांकि जब बाबा साहब ने उनकी पहचान बौद्ध धम्म से करा दी तब धीरे-धीरे बदलाव आने लगा। लोग पुराने रीति-रिवाज से बाहर निकले। अस्पृश्यता का जो रीति-रिवाज था उसे हमारे यहाँ वतनदारी कहते थे। इस प्रथा के अंतर्गत जो ऊंची जाति के लोग थे उनके कुछ घर महार जाति के लोगों को काम करने के लिए दिये जाते थे। महार लोग उस घर में जो काम होता था उसे करते थे। घर वालों के मन में आया तो मजदूरी के नाम पर महारों को कुछ दे देंगे। इनकी जिंदगी दरअसल उनकी कृपा पर निर्भर थी।
हमारे लोगों ने जब बौद्ध धम्म स्वीकार किया तब वतनदारी पद्धति बंद कर दी। हमारी बस्ती के पच्चीस-तीस घरों में से चार घर ही ऐसे थे जिन्होंने पुराना हिन्दू धर्म नहीं छोड़ा था। इसलिए वे लोग वतनदारी का काम करते थे। मेरे नजदीक एक घर था। उस समय मैं छोटी थी। तब देखती थी कि उनके घर में कभी-कभी नई कुर्सी दिखाई देती थी। यह अचरज की बात थी क्योंकि बौद्ध बस्ती में अभी तक किसी के घर में कुर्सी नहीं थी। मुझे यह बहुत बड़ी बात लगती थी। लोग इतने गरीब थे कि किसी के घर में कुर्सी हो इसका खयाल भी नहीं हो सकता था।
इसलिए मैं सोचती थी कि वतनदारी करनेवाले के घर में यह कुर्सी कहाँ से आई? मेरी सहेलियाँ बोलती थीं कि गाँव में वह मर गया तो इस कुर्सी पर उसका प्रेत उठाकर श्मशान में ले गए थे। वही कुर्सी इनको मिली। यह उनकी कृपा थी। यह तो अपमान है न कि मुर्दे की कुर्सी दलित को दे रहे हैं। यह स्वाभिमान तो नहीं है किसी का प्रेत लेकर गए थे और वह कुर्सी दलित को दे रहे हैं। किसी की शादी हो रही है तो जब हल्दी डालते हैं , स्नान कराते हैं उस समय जो भी साड़ी या कपड़ा उतरता है वह साड़ी इन लोगों को दे देते थे। उसे कोंकणी में निंबाची साड़ी कहते थे। ऐसी थी वतनदारी प्रथा।
लेकिन बचपन में यह नहीं समझ में आता था कि उसमें गलत क्या है और सही क्या है। सिर्फ इतना समझ में आता था कि उनके घर में जो साड़ी आती थी वह मेरे घर में नहीं आती। लेकिन मेरे घर में नहीं आती है मेरे मन में इसकी कोई शिकायत नहीं थी। फिर भी जिंदगी जीने का डिफरेंस मन में आने लगा था। मैंने बताया कि छोटी ही उम्र से मैं त्रिशरण-पंचशील में जाती थी तभी मेरे मन यह फर्क आने लगा था कि जिन्होंने बौद्ध धम्म अपनाया और जिन्होंने नहीं अपनाया उनके जीने में कुछ तो अलग हो रहा है लेकिन एकदम से स्पष्ट कुछ भी नहीं था।

एक ऐसा परिवार था जिसका पुरुष सुबह-सुबह गाँव के मंदिर में ढोल बजाने जाता था। मेरे मन में वह भी डिफरेंस समझ में आता था। उसको भी कृपा करके कुछ आता था। मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में क्या फर्क था। जिन लोगों ने बौद्ध धम्म अपनाया था उनके घर में मुर्दे की कुर्सी नहीं आई। निंबाची साड़ी नहीं आई। लेकिन उनके घर में बाबा साहब का दिया हुआ स्वाभिमान आया। उस स्वाभिमान की वजह से शिक्षा आई। झोपड़ी में रहने और गरीबी में जीने के बावजूद बदलाव आने लगा। हर घर से बच्चे स्कूल भेजे जाने लगे। लेकिन जो वतनदारी निभा रहे थे वे ऊंची जाति का उतरन पहनकर और मुर्दे की कुर्सी पर बैठकर खुश थे।
कई मोर्चों पर संघर्ष चलता रहा
वह गाँव क्या था? कुछ लोग बहुत सम्पन्न थे और वे बहुत रुआब से चलते थे। चार घर छोड़कर हमारे लोग अब अपने को उनकी वतनदारी से मुक्त कर चुके थे इसलिए उनमें हमारे लिए ईर्ष्या-द्वेष भरा था। एक बार जब बाबा साहब की जयंती पर कार्यक्रम हुआ और रात को नाटक का मंचन हो रहा था तो उधर से पत्थरबाजी होने लगी।
लेकिन हमारे लोगों में थोड़ी जागृति आना शुरू हो गई थी। हमारे समाज का एक लड़का था जो वकीली की पढ़ाई कर रहा था। उसके पिता तलाठी में नौकरी करते थे इसलिए उनका खानपान और रहन-सहन अच्छा था। वह शहर में रहकर पढ़ाई कर रहा था और उसमें व्यक्ति के अधिकारों की चेतना आ गई थी। एक बार की बात है कि उसने मंदिर में प्रवेश करने का प्रयास किया। इस पर गाँव के अनेक लोगों ने विरोध किया। एक दिन उसी लड़के ने देखा कि सरकार द्वारा बनाए गए हमारे कुएं की जगत पर अपने को ऊंची जाति का समझने वाला एक आदमी बैठा था और कुएं में थूक रहा था। वह देउली समाज का आदमी था। देउली समाज मध्यवर्ती जाति होती है। दलितों से थोड़ा ऊपर और सवर्ण मराठा लोगों से बहुत नीचे। लेकिन घमंड यह था कि मैं ऊंची जाति का हूँ। मैं उसका नाम नहीं ले रही हूँ। उस दिन वह बात करता जाता था और कुएं में थूकता जाता था।
इस बात को इस युवक ने देखा। उसको बहुत गुस्सा आया। उसने वहाँ खेल रहे छोटे बच्चों को वहाँ से घर जाने को कहा और अकेले कुएँ पर पहुँचा। फिर उस आदमी को कुएं में थूकने के अपराध में मारा। कई तमाचे और घूंसे मारे। हमारे गाँव के लोग अभी भी वह किस्सा बताते हैं।

उस आदमी का देसी दारू का धंधा था। उसके ग्राहक सभी गरीब लोग थे। वकील युवक द्वारा मार खाने की प्रतिक्रिया में उसने हमारे कुएं के सामने की एक जगह पर दारू की दुकान खुलवाने की कोशिश की। जब वह दुकान वहाँ बनवा रहा था तब हमारी बस्ती को ध्यान आया कि यह तो बहुत बुरा होने जा रहा है। यह हमारी बस्ती का मुख्य रास्ता था। अगर दारू की दुकान खुल जाएगी तो शाम को काम से लौटनेवाले लोग अपनी कमाई से जरूर दारू पिएंगे। और फिर घर कैसे चलेगा?
दूसरे वहाँ लोग बैठ कर दारू पिएंगे और हुड़दंग मचाएंगे। हमारी बस्ती की औरतें उधर से निकलेंगी या कुएं से पानी भरने के लिए आएंगी दारू पिनेवाले लोग छींटाकशी और छेड़छाड़ करेंगे। यह तो अच्छा नहीं होगा। बच्चे भी स्कूल में नहीं जा पाएंगे। तब बस्ती की महिलाओं ने दुकान उजाड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने का दुकान का ‘जांभा-दगड़’ (स्थानीय शब्द जिसे पूर्वाञ्चल में पाया और थून्ह-बड़ेरा कहते हैं।) उखाड़ दिया।
ये सब पढ़ी-लिखी औरतें नहीं थीं लेकिन उनमें अपने भले की समझ थी। इसलिए उन्होंने उस आदमी से पंगा लिया। उन्होंने सबसे पहले ग्राम पंचायत में मोर्चा निकाला कि इधर यह दुकान नहीं चाहिए। तब भी वह आदमी मान नहीं रहा था। तब सभी औरतों ने मिलकर उस बनती हुई दुकान को तोड़ डाला।
इस पर उसे बहुत गुस्सा आया और एक दिन हमारी बस्ती में वह वकीली पढ़ने वाले लड़के को मारने के लिए घुसा। वह लड़का उस समय घर पर नहीं था। तब उसकी माँ ने अपने नेतृत्व में सारी औरतों को लेकर उस आदमी को पकड़ा और उसको अच्छी तरह धुनकर रख दिया। फिर लकड़ी के खंभे से उसे रस्सी में बांधा और पुलिस में शिकायत की। कोर्ट में बहुत सालों तक यह मुकदमा चला। यहाँ तक कि लड़ते-लड़ते वह भी थक गया तो बाद में उसने कंप्रोमाइज़ करके केस उठा लिया।
बरसों के अंतराल के बाद बहुत कुछ बदल गया है। हमारी बस्ती के लोग पढ़-लिखकर इतना आगे बढ़ चुके हैं कि लोग अब उनसे सलाह लेने आते हैं। जिस जगह दारू की दुकान खुल रही थी वहाँ अब बौद्ध विहार है और असल में विहार शिक्षा का केंद्र बन गया है। बेशक इसके लिए बहुत संघर्ष हुआ है। मैंने इस पर विहार नाम से एक कहानी लिखी है।

नई पीढ़ी के लिए मेरी माँ का संघर्ष
मैं अपनी माँ की बात कहना चाहती हूँ जो खाते-पीते घर से थीं लेकिन भगवान के डर से दरिद्र घर में ब्याह दी गई थीं। यहाँ रहने के लिए घर भी नहीं था। खाने के लिए अन्न नहीं था। ऐसी स्थिति में भी मेरी माँ ने किसी भी भगवान की तस्वीर नहीं रखी थी। जब से मुझे समझ आने लगा तभी से मैं देखती आई कि मेरे घर में बुद्ध, बाबा साहब अंबेडकर और जोतीराव फुले जी की तस्वीरें हैं। दीवार टूटी-फूटी थी लेकिन इन तसवीरों के कारण बहुत सुंदर लगती थी। मैं रोज शाम को इस दीवार के सामने हाथ जोड़कर अपनी माँ के साथ खड़ी रहती थी।
माँ पढ़ी-लिखी नहीं थी इसलिए वह बौद्ध धम्म का तत्व ज्ञान नहीं मालूम था लेकिन वह सच्ची भावना से जुड़ी हुई थी। उनको बाबा साहब पर आस्था थी और बाबा साहब ने जो सीख दी थी उसे वह मानती थी। वहीं सीख हमें देने के लिए वह प्रयत्नशील थी। आज मुझे लगता है कि उसी सीख से मेरी उस छोटी सी झोपड़ी में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ। मैं जब यह बोलती तब मुझे रोना आता है। मैंने वह दरिद्रता देखी है। अपनी माँ के कष्ट देखे हैं। लेकिन पचास साल के बाद आज उस झोपड़ी को कोठी में बदलते भी देख रही हूँ। पूरा कायापलट हुआ है।
बचपन में मुझे पैरों के लिए चप्पल नहीं होती थी लेकिन अब जब कभी मैं अपने मायके जाती हूँ तब मेरे पाँव में वहाँ की धूल भी नहीं लगनी चाहिए। मेरे भतीजे इतना खयाल रखते हैं। मुझे लेने के लिए स्टेशन पर उतरने से पहले गाड़ी आती है। इस परिवर्तन के जो रूट्स हैं उसे बाबा साहब अंबेडकर ने दिया है। उन्होंने हमें गुलामी से मुक्ति का रास्ता दिया। उन्होंने ही यह सीख दी कि किसी को मुर्दे की कुर्सी के मोह में नहीं पड़ना चाहिए। इसी सीख की वजह से यह परिवर्तन हुआ।
मेरे भाई में स्कूल जाने की इच्छा नहीं थी। वह जाने से बचता था। एक प्रसंग याद आता है कि मेरी माँ ने एक दिन उसका कंधा पकड़ा और पिताजी से कहा पैर पकड़िए। वह रो रहा था और अपने को छुड़ा रहा था लेकिन माँ-पिताजी उसको लेकर स्कूल गए। अध्यापक से कहा कि इस बच्चे को स्कूल में होना चाहिए। इसको पढ़ते हुये आप दंडित करेंगे तब भी कोई चिंता नहीं है। इस घटना के बाद मेरा भाई कभी स्कूल से अनुपस्थित नहीं रहा। आगे चलकर वह अध्यापक हुआ। यह माँ के कारण संभव हुआ क्योंकि उन्होंने बाबा साहब की सीख को गाँठ बांध ली थी।
मैंने अपनी माँ का उदाहरण दिया लेकिन बौद्ध बस्ती के हर घर में ऐसी माँ थी। इसलिए सबने शिक्षा का मार्ग पकड़ा और गुलामी से निकलने की हिम्मत की। अब उन झोपड़ियों की जगह सबके पक्के घर बन चुके हैं। हर घर के सामने गाड़ी खड़ी है। वहाँ एक भी झोपड़ी नहीं दिखाई देती।
अब कांदलगाँव का रूप ऐसा दिखता है कि बौद्ध बस्ती के लोग जिनके खेतों में काम करते थे, वे आज भी वहीं के वहीं हैं। उनकी स्थिति जैसी थी वैसी ही है लेकिन बौद्ध बस्ती की तीसरी पीढ़ी में भारी परिवर्तन हो चुका है। बहुत से बच्चे पढ़ाई के लिए विदेशों में जा रहे हैं। कम से कम दस बारह बच्चे विदेश में हैं। मेरी बहन का बेटा आस्ट्रेलिया में स्थायी तौर पर सेटल्ड है। मेरी बेटी लंदन में पढ़कर आई। कांदलगाँव की और एक बेटी अमेरिका में है। एक कैलिफोर्निया में पढ़ाई कर रही है। एक ज़माना था जब हमारे परिवार को न जाने कितनी बार खाली पेट सोना पड़ता था। लेकिन अब सबकुछ बदल चुका है।
एक ज़माना था कि मेरी माँ रात-रात भर जागकर आयदान बनाती थी और सुबह उसे बाज़ार में बेचकर आती तो खाने का सामान लाती तब घर में चूल्हा जलता था। तब हम खाते थे लेकिन अब यह जो तीसरी पीढ़ी है वह अच्छी तरह जीवन जी रही है।
मैंने एम ए तक की पढ़ाई गाँव से ही की थी और वहीं अध्यापिका हो गई। उन्नीस सौ नब्बे में मैं मुंबई आई। मुंबई आने के पहले मैं राष्ट्र सेवा दल में काम करती थी। 1980 से ही मैं सामाजिक आंदोलनों से जुड़ने लगी। जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि अगर बाबा साहब के मूवमेंट से इतना परिवर्तन आ सकता है तो अगर मैं मूवमेंट में काम करूँ तो मुझे इसी में काम करना चाहिए। इसी प्रक्रिया में मैंने मंचों से बोलना शुरू किया। मैं आगे चलकर लिखने लगी।