बातचीत का चौथा हिस्सा
जब आप कहानी लिखती हैं तो मन:स्थिति कैसी होती है। थोड़ा रचनाप्रक्रिया पर भी प्रकाश डालें?
शुरू के दो तीन सालों को छोड़कर मैंने रुटीन बनाकर नियमित लेखन नहीं किया। जो कुछ भी लिखा गया, भीतरी खलबली और बेचैनी के तहत ही लिखा गया। जितना अब तक लिखा है, लगभग उतना ही अधूरा लिखा रखा है। कभी कोई रचना भीतर से विस्फोट के तहत शुरू तो हो जाती है, पर अधरस्ते लिखते हुए सांस फूलने लगती है और उस कहानी को पूरा करना असंभव सा लगने लगता है। वैसी मारक सज़ा आप अपने को देना नहीं चाहते तो वह रचना अधूरी छूट जाती है।
हां, कुछ रचनाएं एक रौ में लिख ली जाती हैं। जो अपने प्रत्यक्ष अनुभव के दायरे में आती हैं, उन्हें लिखना अपेक्षाकृत आसान होता है। जैसे दंगों के दौरान लिखी काला शुक्रवार या ताज़ा कहानी पीले पत्ते– जो शुरु से आखिर तक एक संस्मरण ही है। यह भी है कि अक्सर कहानी का अंत मेरे दिमाग़ में पहले दर्ज़ होता है, शुरु का हिस्सा बाद में जुड़ता है। पीले पत्ते कहानी का अंत अगर यथार्थ में उस तरह से घटित न हुआ होता तो पार्क में मिली उस बुज़ुर्ग महिला पर कहानी लिखी ही नहीं जाती।
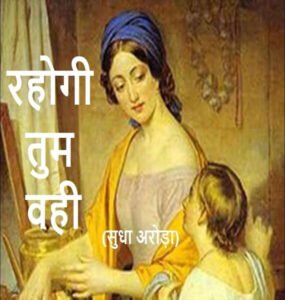 कई बार अलग-अलग समय में घटित हुए प्रसंग भी एकसाथ जुड़ कर किसी कथा की रचना करते हैं। शुक्रवार के जनवरी 2012 वार्षिकांक में मेरी जो नयी कहानी कांच के इधर–उघर आई है, उसमें भी कहानी का आखिरी हिस्सा हाल ही की घटना है जबकि उसमें कामगार के बच्चों के मोबाइल क्रेश और मजदूर के साथ घटी दुर्घटना वाला प्रसंग ग्यारह साल पुराना है लेकिन मधुमक्खी के छत्ते टूटने की घटना अपने सामने इस तरह से न हुई होती तो दोनों घटनायें आपस में जुड़ती नहीं और कहानी बनती नहीं।
कई बार अलग-अलग समय में घटित हुए प्रसंग भी एकसाथ जुड़ कर किसी कथा की रचना करते हैं। शुक्रवार के जनवरी 2012 वार्षिकांक में मेरी जो नयी कहानी कांच के इधर–उघर आई है, उसमें भी कहानी का आखिरी हिस्सा हाल ही की घटना है जबकि उसमें कामगार के बच्चों के मोबाइल क्रेश और मजदूर के साथ घटी दुर्घटना वाला प्रसंग ग्यारह साल पुराना है लेकिन मधुमक्खी के छत्ते टूटने की घटना अपने सामने इस तरह से न हुई होती तो दोनों घटनायें आपस में जुड़ती नहीं और कहानी बनती नहीं।
कुछेक छोटी कहानियां एक बैठक में लिख ली जाती हैं जैसे रहोगी तुम वही और सत्ता संवाद। पर कुछ छोटी कहानियों को लिखने में कई बार एक बड़ी कहानी से ज़्यादा बहुत मेहनत करनी पड़ती है– जैसे डेज़र्ट फोबिया उर्फ समुद्र में रेगिस्तान या एक औरत: तीन बटा चार ।
कथा साहित्य आपके सृजन के केंद्र में रहा है फिर भी उपन्यास की अपेक्षा आप कहानी लेखन के क्षेत्र् में अधिक सक्रिय दिखाई देती हैं ! क्या उपन्यास देर से लिखने का कारण अधिक आत्मविश्वास और अनुभव की ज़रूरत है ? क्यों ?
उपन्यास लिखने के लिये जिस एकाग्रता और फुरसत की ज़रूरत होती है, ज़िन्दगी ने उसके लिये मोहलत नहीं दी। वैसा माहौल और मन:स्थिति बन ही नहीं पाई। दो अधूरे उपन्यास लिखे जो एक जिल्द में हैं–यहीं कहीं था घर पर चूंकि उसका हर अध्याय एक स्वतंत्र् कहानी के शिल्प में है इसलिये वे अधूरे लगते नहीं।

लिखने के कारण आपको किसी विषम परिस्थिति का सामना तो नहीं करना पड़ा ? परिवार में या बाहर?
ऐसा मैंने कुछ लिखा नहीं कि परिवार से कोई आपत्ति करे। माता-पिता खुद साहित्य प्रेमी थे। उन्हें मेरा लिखना अच्छा लगता था। एक दिलचस्प घटना याद आ रही है। इधर अपने पिता पर आठ दस पृष्ठों का एक संस्मरण लिखा जिसमें अधिकांश में उनकी प्रशंसा ही थी, सिर्फ़ दो पैराग्राफ में यह था–’दूसरा बदलाव उनमें यह आया कि वह पापा, जो बच्चों की उपस्थिति का ख़याल किये बिना, बीजी को हमेशा बड़े प्यार भरे सम्बोधनों से बुलाया करते थे, अचानक उनके प्रति बड़े रूखे और साफ़ शब्दों में कहें तो ‘जालिम’ हो उठे। यह शायद वह ज़माना था, जब अपनी पत्नी की सलाह मानना मध्यवर्गीय पुरुष को अपनी शान के खिलाफ़ लगता था। उठते–बैठते, हर जगह, हर किसी के सामने बीजी को अपना मुंह खोलते ही इस तरह के वाक्य सुनने पड़ते-
‘तुमसे चुप क्यों नहीं रहा जाता ?’
‘तुम बेवकूफ़ी की बातें मत करो। किसी बात की समझ न हो तो मत बोला करो। बिजनेस की बातों में टांग मत अड़ाया करो।’
’तुम्हें तो अक्ल ही नहींं है। रसोई से बाहर की बातों में दखल मत दिया करो।’
‘अपनी अक्ल बस रसोई में ही चलाया करो !’
[bs-quote quote=”महिला रचनाकार तो पहले से ही सेल्फ सेंसरशिप की स्कैनिंग के बाद ही किसी रचना को प्रकाशन के लिये भेजती हैं। सबसे बड़ा प्रतिबंध तो उसका अपना ही होता है क्योंकि घर परिवार उसके लिये हमेशा पहली प्राथमिकता रहता है।” style=”style-2″ align=”center” color=”” author_name=”” author_job=”” author_avatar=”” author_link=””][/bs-quote]
रोज दर रोज कम अक्ल और बेवकूफ़ होने के तमगे अपनी पोशाक पर टांकते हुए बीजी लगातार चुप होती चली गयीं। अब पापा के सामने वह सिर्फ़ एक श्रोता की भूमिका अदा करतीं। पापा अपने व्यवसाय की समस्याओं के बारे में बताते और वह बग़ैर अपनी राय दिये चुपचाप सुनतीं और वहां भी इस समझदारी के साथ कि तुम्हारे पापा के पास और कोई है भी तो नहीं जिससे वह अपने मन की बात कह सकें। सबसे बड़ी होने के नाते मां का यह दर्द सबसे ज्यादा मेरे हिस्से में आया। अपने पति और बच्चों द्वारा बेशक वह घर संभालने और खाना पकाने वाली एक नौकरानी की तरह ट्रीट की जातीं, पर बिना किसी गिले–शिकवे के हम सब को खुश रखना उनका एकमात्र सरोकार होता। पापा को खाना खिलाते वक्त वह इतनी सतर्क रहतीं कि खाना बिल्कुल वैसा बना हो जैसा पापा को पसंद है–भिंडी–न ज्यादा भुनी न हरी, बैगन का भुरता ठीक बराबर के प्याज–टमाटर के अनुपात के साथ, दाल ऐसी जो उंगली पर चढ़े, घी बराबर उतना ही जितना दाल में होना चाहिये, और खाते वक्त एक फुलका ख़त्म हो, तभी दूसरा गरम फुल्का उनकी प्लेट में आये।
इसे पढ़कर मेरे पिता नाराज़ हो गये। पुरुष–चाहे वह पिता हो, पति या बेटा–बेहद असहनशील होता है। उसका अहंकार उसे सच सुनने की ताब नहीं देता।
एकबार सहारा समय में ‘रहन–सहन’ स्तंभ में अपनी दिनचर्या में मैंने यह बता दिया कि मेरे पति नाश्ते में क्या खाते हैं। इस बात को लेकर पति नाराज़ हो गये कि–अपने बारे में जो लिखना हो, लिखो पर मेरे बारे में कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं। बहरहाल, महिला रचनाकार तो पहले से ही सेल्फ सेंसरशिप की स्कैनिंग के बाद ही किसी रचना को प्रकाशन के लिये भेजती हैं। सबसे बड़ा प्रतिबंध तो उसका अपना ही होता है क्योंकि घर परिवार उसके लिये हमेशा पहली प्राथमिकता रहता है।
औरत की दुनिया स्तंभ के लिये एक दो बार कुछ अवांछित प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ा पर सच बोलने और लिखने की वैसी कीमत तो हर रचनाकार को चुकानी पड़ती है। उसमें कोई खास बात नहीं है! अब उससे डर नहीं लगता।
आपकी कसौटी क्या है सार्थक–सफल कहानी की?
ऐसी कहानी जो दुपहर की फुर्सत में नींद दिलाने के लिए नहीं, नींद से जगाने के लिए लिखी जाए। कुछ सोचने पर मजबूर करे और याद रह जाए।
आर्थिक स्वतंत्रता को स्त्रियों की मुक्ति की पहली शर्त मानती हैं आप, कितना ठीक है यह?
आर्थिक आज़ादी ने औरत को एक सक्षम नागरिक बनाया है, समाज के हर क्षेत्र में उसकी सहभागिता बढ़ी है। पर अफसोस कि आर्थिक आजादी भी औरतों को बराबरी का दर्जा या घरेलू हिंसा से निज़ात नहीं दिला पाती।
आर्थिक आज़ादी स्त्री मुक्ति नहीं, पुरुष मुक्ति का दरवाज़ा है। भारतीय समाज के मध्यवर्गीय ढांचे में हमने औरत को आधुनिक और आत्मनिर्भर तो बनाया पर उसे वह माहौल देने में असमर्थ रहे जहां यह आत्मनिर्भरता उसे बराबर का हक या सम्मान दिला पाती।
[bs-quote quote=”दमयंती जोशी, सोनल मानसिंह, तीजन बाई जैसे सैकड़ों उदाहरण हैं, जहां उनके पतियों ने उनकी कला पर रीझकर उनसे शादी की और शादी के बाद कला को ही तिलांजलि देने का आदेश दिया। जिन पत्नियों ने इस आदेश का पालन किया, वे शादियां टिकी रहीं, बाकी टूट गईं। यह भी देखा गया है कि अधिकांश महिला कलाकारों ने अपने असहयोगी पतियों से अलग होने के बाद ही अपनी कला को बुलंदियों तक पहुंचाने में महारत हासिल की।” style=”style-2″ align=”center” color=”” author_name=”” author_job=”” author_avatar=”” author_link=””][/bs-quote]
अर्थसत्ता या मनीपॉवर से इनकार नहीं किया जा सकता पर वही अर्थ जब पुरुष कमा कर लाता है तो वह गृहस्वामी है, घर का सर्वेसर्वा है, आदर का पात्र है। उसके घर में घुसते ही पत्नी या बहन को पंखे का स्विच आन कर देना चाहिए, चाय का कप या शरबत का गिलास लेकर खड़े हो जाना चाहिए और वही अर्थ जब औरत कमाकर लाए तो कितने घरों में उसके ससुराल वाले पलक पांवडें बिछाए खड़े रहते हैं ?
दुहरी जिम्मेदारियों के बोझ से लदी औरत के लिए मुंबई महानगर में जैसे लोकल टिकट की क्यू या राशन की लाइन में कोई रियायत नहीं है, वैसे ही एक संयुक्त परिवार में कामकाजी औरत के लिए घरेलू फ्रंट पर कोई कटौती नहीं है ।
पति–पत्नी काम से साथ–साथ लौटेंगे तो पति अखबार लेकर या टीवी खोल कर बैठ सकता है, चाय पत्नी को ही बनानी पड़ेगी।
‘पति–पुरुष की अधीनता में ही सुख है।’ इस मूल–मंत्र को सत्य मानते हुए आपसी अनबन या मनमुटाव का पहला और अहम कारण जरुरी तौर पर लड़की का आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना मान लिया गया है। आत्मनिर्भर होना या घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में सहायक होना उसे आत्मसम्मान से जीना और अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखना भी सिखाता है, पर ससुराल वाले आम तौर पर इसे उसका गुमान मान लेते हैं और ‘चार पैसे घर क्या ले आती है, दिमाग सातवें आसमान पर चढ़ा रहता है’ जैसे वाक्यों के तमगे उसकी पोशाक पर जब–तब टांकते रहते हैं। इन ‘चार पैसों’ की बदौलत उसके साथ कोई रियायत भी बरती नहीं जाती। दिन की रसोई सास या ननद ने संभाल भी ली तो रात का चूल्हा–चौका उसे नौकरी से लौटकर संभालना ही पड़ता है।
आमतौर पर घर में रहनेवाली पत्नी या गृहस्थी संभालने वाली घरेलू औरत ही कमा पति की हिंसा का शिकार होती है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि कामकाजी पत्नी को उनके पति उसकी कड़ी मेहनत की कमाई के एवज सर–आंखों पर बिठाकर रखते हैं। बाहर का ‘वर्क–लोड’ उस पर जितना भी हो, घर पहुंचकर उसे वही रोल अदा करना पड़ेगा जो एक अशिक्षित या अर्द्धशिक्षित घरेलू महिला करेगी। रसोई का पूरा कार्यक्षेत्र पत्नी के जिम्मे है, पति अगर अपने हाथ से एक कप चाय बनाकर पी भी लेता है तो देर–सवेर उस चाय को लेकर अपने तरक’ में से एकाध व्यंगबाण छोड़े बिना वह नहीं रहेगा। यहां आपसी कलह का कारण घर या बच्चे नहीं होंगे, आपसी कैरियर होगा।

आज भी मध्यवर्गीय कस्बई मानसिकता के पास इन समस्याओं का हल एक ही हैं–लड़की को इतना आगे मत पढ़ाओ कि वह सवाल करने लगे या ससुराल में अपनी बेकद्री और अपमान को पहचानने लगे। यह ‘पहचान’ देना गलत है–आज भी इसके पक्ष में बोलने वाले कस्बों में क्या, महानगर की घनी बस्तियों में भी बहुतेरे मिल जाएंगे।
आर्थिक आज़ादी ने औरत को दोहरी तिहरी जिम्मेदारी में जकड़ दिया है और पुरुष औरत की आर्थिक आज़ादी से चुनौती पाकर, अपनी असुरक्षा को ढांपने के लिए न सिर्फ गैर जिम्मेदार हो जाता है बल्कि उसके भीतर पत्नी के लिए शक का फन फुंफकारता हुआ उसे हिंसक भी बना देता है। प्रताड़ना का स्तर यहां भी है। काम से लौटने में देर हो गई तो परिवार में बवाल उठ खड़ा होता है। पत्नी को नौकरी में अगर प्रमोशन मिलता है तो पति इसका श्रेय उसकी काबिलियत को न मानकर बॉस को खुश रखने के इतर करणों में ढूंढता है। यह शक की लाइलाज बीमारी हर वर्ग के पुरुष में है बिल्कुल निचले तबके से लेकर उच्च वर्ग के पुरुष तक इससे कतई मुक्त नही है। 15 वीं शताब्दी का ‘ओथेलो’ सिर्फ़ शेक्सपीयर के समय का यथार्थ नहीं है, आज की इक्कीसवीं शताब्दी के पुरुष में भी ओथेलो मौजूद है और यह कस्बे के अर्द्ध शिक्षित ओंकारा में ही नहीं, विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलरों और करोड़पति उद्योगपतियों तक में फैला हुआ है। इनकी निरीह डेस्डिमोनाएं बेचारी समझ ही नहीं पातीं कि उनका आकर्षक व्यक्तित्व और मिलनसार स्वभाव उनके समर्पण के विपरीत जाकर बेवजह ही उनके जीवन का अभिशाप कैसे बन जाता है।
भारतीय समाज में पुरुषवर्चस्व की जड़ें इतनी दूर तक और इतने गहरी पसरी हुई हैं कि अपने अगल बगल, दाएं-बाएं, गली नुक्कड़, जहां नज़र दौड़ाएं, आपको हर औरत में इस पितसत्तात्मक समाज से मिले अवांछित दबाव की अलग अलग किस्में नज़र आएंगी। एक औसत पति अपनी पत्नी को अपने बराबर की जगह पर भी देखना नहीं चाहता। वह अगर एक सीढ़ी भी ऊपर दिखती है तो वह उसे काट छील कर अपने से नीचे लाने की कोशिश में सतत जुटा रहता है। दमयंती जोशी, सोनल मानसिंह, तीजन बाई जैसे सैकड़ों उदाहरण हैं, जहां उनके पतियों ने उनकी कला पर रीझकर उनसे शादी की और शादी के बाद कला को ही तिलांजलि देने का आदेश दिया। जिन पत्नियों ने इस आदेश का पालन किया, वे शादियां टिकी रहीं, बाकी टूट गईं। यह भी देखा गया है कि अधिकांश महिला कलाकारों ने अपने असहयोगी पतियों से अलग होने के बाद ही अपनी कला को बुलंदियों तक पहुंचाने में महारत हासिल की।
हां, आर्थिक रूप से सक्षम होने का, एक मध्यवर्गीय औरत को जो लाभ मिलता है, वह यही है कि गैर बराबरी, घरेलू हिंसा से पैदा होती भीषण स्थितियों से जूझना उसके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है, जो आर्थिक रूप से पूरी तरह पति की कमाई पर आश्रित गृहिणी के लिए संभव ही नहीं है। जहां एक आम गृहिणी वैवाहिक जटिलताओं या आर्थिक रूप से पराश्रित होने के कारण उपजी स्थितियों से पूरी तरह ढह जाती है और अपने को समेट पाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, वहीं आर्थिक आज़ादी के बूते पर, आत्मनिर्भर स्त्री के लिए, हिंसा या पति के इतर सम्बन्धों से उपजी जटिल स्थितियों के भीषण स्वरूप की तीव्रता कम हो जाती है और वह अपने जीवन के नक्शे को फिर से अपने सामने फैलाकर सुनियोजित कर सकती है और मानसिक गुलामी से बाहर आना उसके लिए अपेक्षाकृत आसान होता है। उसके सामने चुनाव की सुविधाएं और जीने के विकल्प अधिक होते हैं ।

पल्लव जाने-माने युवा आलोचक और बनास जन पत्रिका के संपादक हैं। फिलहाल वे हिन्दू कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं।





[…] […]