आपके ज़माने में एक ऐसा तक़्क़ीपसंद नज़रिया भी राइज था, जिसमें इतनी भी ‘सहूलियत’ बर्दाश्त नहीं की जा पाती थी, जैसा कि नैरेटर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था । असली सवाल तो ये था कि रमेश की सहूलियतों से भरी इस ‘नयी ज़िंदगी’ की शुरूआत का करिश्मा हुआ कैसे ? इन दो वाक़ियों के बीच में ख़ाली जगहें काफ़ी रह गयी हैं, जो drama को melodrama में तब्दील कर गयीं ।
नयी ज़िंदगी में भी मौज़ू तो self analysis जैसा संजीदा ही है, मगर ये ‘क्लॉड ईथरली’ या ‘पक्षी और दीमक’ जैसी कहानियों जितनी ऊँचाई तक भी नहीं पहुँचा, ‘अँधेरे में’ या ‘ब्रह्मराक्षस’ जैसी कविताओं की ऊँचाई तक पहुँचना तो दूर की बात है।
‘प्रश्न’ का प्रश्न है, ‘माँ, तुम पवित्र हो ? तुम पवित्र हो, न ?’ ( वही, पे. 109 )
जिसकी वजह से नरेंद्र के मन में ‘प्रश्न’ उठता है वो ‘काका’ हैं, जिनके लड़के का नाम सुधीर है। उनकी बीवी का इंतक़ाल हो चुका है । इंतक़ाल सुशीला के शौहर का भी हो चुका है । अब काका सुधीर सुशीला और नरेंद्र साथ रहने लगे।’ ( वही. पे. 112 ) ‘उन दोनों का घर एक हो गया ।’ (वही. पे.112)
एक बार सुशीला जब काका के ‘विह्ववल आलिंगन में बिंध गयी’ तो उसे अपने पतिदेव का ख़्याल आया । उनका स्नेहाकुल मुख कह रहा था, ‘तुमको सलोना युवक चाहिए था ।’ (वही, पे. 112 ) “ उस वक़्त सुशीला ने कहा था, ‘नहीं – नहीं ।’ पर आज वह कह रही थी, ‘हाँ, हाँ ।’ ” ( वही, पे. 112 )
काका को देखकर ‘नरेंद्र सोच रहा था कि वह उन्हें मार डालेगा । पर वह चले गये, तो आत्महत्या करने की सोचने लगा।’ (वही, पे. 113 )
“सुशीला ने डरते-डरते पूछा, ‘तुम उनको, ‘काका’ को, ग़ैर समझते हो ? साफ़ कहो। ” ( वही, पे. 113 )
‘‘नरेंद्र ने सोचा, कहा, ‘नहीं।’ ’’ ( वही, पे. 114 )
सुशीला ने रोते हुए कहा, ‘तुम कभी उनको तकलीफ़ मत देना। – – – अँ ।’ ( वही, पे. 114 )
मारे भावुकता के जो प्रश्न पैदा हुआ था, मारे भावुकता के मर भी गया। सुशीला तीव्र होकर बोली, ‘तो मैं अपवित्र कैसे हुई ?’ (वही, पे. 114 ) नरेंद्र ने कहा, ‘लोग कहते हैं।’ ( वही, पे. 114 ) सुशीला बोली, ‘तो तुम उनको जाकर क्यों नहीं कहते, बुलंद आवाज़ में कि मेरी माँ ऐसी नहीं है ।’ (वही, पे. 114 ) नरेंद्र ने कहा, ‘वे मुझे छेड़ते हैं, मुझे तंग करते हैं, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा।’ ( वही, पे. 114 ) सुशीला कहती है, ‘तुम बुज़दिल हो।’ (वही, पे. 114 )
‘और यह शब्द नरेंद्र के हृदय में तीक्ष्ण पत्थर के समान जा लगा। वह बच्चा तो था, लेकिन तिलमिला उठा । उसे भूला नहीं । अमूल्य निधि की भाँति उस घाव के सत्य को उसने छुपा रखा।’ ( वही, पे. 114 )
इसके बाद नैरेटर ने इतना ही नहीं बताया कि ‘… नरेंद्र कुमार एक कलाकार हो गया।’ ( वही, पे. 114 ) बल्कि ये भी बता दिया, ‘पर मैं यहीं दुनिया के आस्मान में एक कृपाण की भाँति तेजस्वी उल्का का प्रकाश छाया हुआ देख रहा हूँ, जिसकी पूजा सब लोग कर रहे हैं। मुझे बाद में मालूम हुआ कि यह नरेंद्र कुमार का प्रकाश है। सुशीला की जन्मभूमि, हमारा गाँव, धन्य है !’ ( वही, पे. 114 )
ये ‘प्रश्न’ तो उतना ‘धन्य’ नहीं है, क्योंकि लोगों के ज़रिये ये पैदा किया जा सकता है, लेकिन इसका समाधान ज़रूर ‘धन्य’ है, क्योंकि उसका वाक़ियों से कोई रिश्ता जोड़ पाना मुमकिन नहीं है।
आपकी कहानी ‘ब्रह्मराक्षस का शिष्य’ के सिलसिले में अपनी कहानी ‘ ब्रह्मराक्षस की मुक्ति’ का हवाला देने के लिए ही नहीं, बल्कि पहले कही गयी अपनी बात को देहराने के लिए भी मुआफ़ी का तलबग़ार हूँ। महावीर अग्रवाल के ज़रिये सवाल ये किया गया था, ‘मुक्तिबोध की कहानियों में कौन-सी कहानी आपको तत्काल याद आती है?’ मेरा जवाब था, “इसके जवाब में अगर मैं ‘ब्रह्मराक्षस का शिष्य’ का नाम न लूँ , तो अपने साथ नाइंसाफ़ी कर जाऊँगा, क्योंकि इसी को मैंने ‘ब्रह्मराक्षस की मुक्ति’ के नाम से आगे बढ़ाया है। मेरी कहानी दरअसल कहानी कम मुक्तिबोध की कहानी की आलोचना ज़्यादा है। ‘ब्रह्मराक्षस का शिष्य’ कहानी हमें इस मक़सद तक ले जाती है, ‘जब तक मेरा दिया ( ज्ञान ) तुम किसी और से न दोगे, तब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं।’ ( मुक्तिबोध रचनावली : तीन – नेमिचंद्र जैन, पे. 120 )
ये ‘ज्ञान’ तब्क़ों की लड़ाई की पेचीदगियों से भरे माहौल से बेख़बर रहकर भी हासिल किया और दिया जा सकता है। इस हिसाब से ये कहानी इतनी आसान हो जाती है कि जैसे सह्लपसंद हो गयी हो । मेरी कहानी ‘ब्रह्मराक्षस की मुक्ति’ का नया शिष्य अपने गुरु ‘वणिकराक्षस’ बनाम ‘ब्रह्मराक्षस’ के सामने जब ये सवाल खड़ा करता है कि ..‘आप जैसे अकेले आदमी को यह आठ मंज़िला भव्य भवन क्यों मिला हुआ है ? यह सिंह द्वार, विशाल आँगन, बरामदे, फ़ानूस, तबला, सितार, दरी, तैलचित्र, व्याघ्रासन, मृगासन, कश्मीर का यह क़ीमती शाल मिलने का रहस्य क्या है? आपके हाथों को वह शक्ति कौन देता है कि आप एक कक्ष में बैठकर किसी अन्य कक्ष से घी का लुटिया उठा लेते हैं? ( कथादेश, दिसम्बर 2000, पे. 47) तब ‘.. गुरु को इतना आतप्त ज्ञान प्राप्त हुआ कि वह तत्काल निरोधान हो गया।’( वही. पे. 47)
[bs-quote quote=”‘मेहनत की हिमायत’ आपकी ख़ूबियों में से एक है। ये भी करुणा में से ही पैदा होती है। ‘ब्रह्मराक्षस का शिष्य’ बड़ी मेहनत करता है। क्या हासिल करता है? ‘ज्ञान’। इधर ये सुनने में आने लगा है कि ‘ब्रह्मराक्षस’ लफ़्ज का इस्तेमाल करते ही आदमी ‘अंधविश्वास’ का हिमायती हो जाता है। अरे हाँ, ‘मिथ’ के इस्तेमाल की वजह से भी आपको ‘अंधविश्वास’ का हिमायती गिनाया जा सकता है। इस तरह की ‘इंकलाबी लफ़्फ़ाज़ी’ ये भी नहीं देखती है जिसका मक़सद ये हो, ‘समस्या एक मेरे सभ्य नगरों और ग्रामों में / सभी मानव सुखी, सुंदर व शोषण-मुक्त कब होंगे!’” style=”style-2″ align=”center” color=”” author_name=”” author_job=”” author_avatar=”” author_link=””][/bs-quote]
ज़ाहिर है कि अगर मैं तत्काल याद आनेवाली एक कहानी के तौर पर ‘ब्रह्मराक्षस का शिष्य’ का ज़िक्र करके ठहर जाता हूँ, तो ये मुक्तिबोध के साथ नाइंसाफ़ी होगी। समझौता, पक्षी और दीमक क्लॉड ईथरली और जंक्शन साफ़ तौर पर ‘ब्रह्मराक्षस का शिष्य’ से आगे बढ़ी हुई कहानियाँ हैं। ‘विपात्र’ को जब ज़्यादातर लोगों ने उपन्यास मान लिया है, तो मैं उसे कहानी मानकर अपने लिए उलझन खड़ी क्यों करूँ? ये तो इतना अहम है कि इसका ज़िक्र अलग से ही होना चाहिए।’ (सापेक्ष : 55 – मुक्तिबोध विशेषांक) – सं. महावीर अग्रवाल, पे. 668)
‘मेहनत की हिमायत’ आपकी ख़ूबियों में से एक है। ये भी करुणा में से ही पैदा होती है। ‘ब्रह्मराक्षस का शिष्य’ बड़ी मेहनत करता है। क्या हासिल करता है? ‘ज्ञान’। इधर ये सुनने में आने लगा है कि ‘ब्रह्मराक्षस’ लफ़्ज का इस्तेमाल करते ही आदमी ‘अंधविश्वास’ का हिमायती हो जाता है। अरे हाँ, ‘मिथ’ के इस्तेमाल की वजह से भी आपको ‘अंधविश्वास’ का हिमायती गिनाया जा सकता है। इस तरह की ‘इंकलाबी लफ़्फ़ाज़ी’ ये भी नहीं देखती है जिसका मक़सद ये हो, ‘समस्या एक मेरे सभ्य नगरों और ग्रामों में / सभी मानव सुखी, सुंदर व शोषण-मुक्त कब होंगे!’ ( मुक्तिबोध रचनावली : दो –सं. नेमिचंद जैन, पे. 243 ) वो अंधविश्वास का हिमायती कैसे हो सकता है?
आपकी कहानी दो चेहरे का ‘प्लॉट’ अकबर की जगह किसी और बादशाह के नाम पर मैं पहले ही सुन चुका था। मज़े की बात ये है कि इसमें आपने कोई ख़ास इज़ाफ़ा भी नहीं किया। उसी ‘प्लॉट’ को आपने अपने लफ़्जों में दोहरा भर दिया है।
एक दिन अकबर बादशाह एक पेड़ के साये में नमाज़ पढ़ते वक़्त जब सज्दे में था, तो राह चलते एक प्रेमी जोड़े के पैर की उसे ठोकर लग गयी। उसने बेहद नाराज़ होकर जब ठोकर के लिए डाँट पिलायी, तो वो भौंचक्के रह गये कि मुहब्बत की बातों में मशग़ूल ‘… उन्हें मालूम ही न हो सका कि रास्ते चलते उन्होंने एक ठोकर मार दी है।’ ( मुक्तिबोध रचनावली : तीन – नेमिचंद्र जैन, पे. 122 ) फिर वो दुआ माँगने लगा, ‘या परवरदिगार, वे दोनों इश्क़ में इतने डूबे हुए हैं कि वे इस दुनिया में ही नहीं रहे । लेकिन अभागा मैं तेरी इबादत में होते हुए भी तेरा ध्यान करते हुए भी, दुनिया में जमा रहा, मैं अपने को भूल न सका, ख़ुदा मुझे माफ़ कर।’ ( वही, पे. 122 )
[bs-quote quote=”अगर आपका किरदार ‘गणित के नशे में रहता है।’ तो आख़िर उसका किस ‘वस्तुगत संदर्भ’ में इस्तेमाल करता है कि आज की सरमायेदारी से उसका मेल बैठ नहीं पाता? मैथेमेटिक्स तो एसा मौज़ू है कि उसके इस्तेमाल से मुनाफ़ा कमाने की भरपूर गुंजाइश है।” style=”style-2″ align=”center” color=”” author_name=”” author_job=”” author_avatar=”” author_link=””][/bs-quote]
इस कहानी की अगर कोई ख़ूबी गिनायी जा सकती है, तो वो ये है कि इसमें आपकी उस ‘धुन’ का ज़िक्र है, जिसके बारे में आपने ‘एक लंबी कविता का अंत’ में कहा था ‘लेकिन क्या बताऊँ कि एक चीज़ है, जिसका नाम है धुन जिसका नाम है लौ। ये शब्द ‘आधुनिक’ नहीं हैं, फिर भी उनके अर्थ का अस्तित्व आज भी विराजमान है। वह मुझे कविता की ओर ही ले जाती है। लेकिन मैं वचन देता हूँ कि मैं कविता नहीं, बल्कि गद्य लिखूँगा। इससे मुझे आमदनी भी हो जायेगी और कुछ यश भी बढ़ेगा ।”( मुक्तिबोध रचनावली : चार – सं. नेमिचंद्र जैन, पे. 153 )
आपकी कहानियों में ‘धुन’ पर बहुत ज़ोर है। आपकी कविताएँ हों या कहानियाँ, यहाँ तक कि आलोचनाएँ भी, बिना ‘धुन’ के लिखी नहीं जा सकती थीं। इसी ‘धुन’ की कहानी ‘दो चेहरे’ आपकी अच्छी कहानियों में नहीं गिनी जायेगी।
‘धुन’ से किये गये काम की ख़ूबी ये होती है कि उसमें गहराई और ख़ूबसूरती जैसी चीज़ें आ जाती हैं। ये चीज़ें ज़िंदगी को ख़ूबसूरत बनाने में मदद करती हैं। लेकिन यहीं ग़ौर कर लिया जाना चाहिए कि बिना ‘धुन’ के किये गये काम भी जीने में मदद करते हैं। सारे मज़दूरों पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो ‘धुन’ से काम नहीं करते, लेकिन कभी उनका कोई काम सरमायेदार करना शुरू नहीं कर देता। बिना ‘धुन’ के यानी पूरे alienation के साथ किये गये मज़दूरों के काम में भी ज़िंदगी की ज़रूरतों और उसकी ख़ूबसूरती की ख़ूबियाँ बरक़रार रहती हैं। बिना ‘धुन’ के किये गये उनके काम की वजह से उनकी ज़िंदगी जलती रहती है। और ये ‘जलना’ उनके भीतर ‘तेज़ाबी काला गटर’ बहाने लगता है। इस alienation की कहानी आपकी कविता ‘मुझे याद आते हैं’ में कहीं बेहतर ढंग से पेश की गयी है, जिसमें बताया गया है, ‘मात्र अस्तित्व ही की रक्षा में व्यतीत हुए दिन की / कि फलहीन दिवस की / निरर्थकता की ठसक को देखकर / श्रद्धा भी भर्त्सना की मार सह लेती है / झुकाती है लज्जा से देवोपम ग्रीव निज / ग्लानि से निष्ठा का जी धँस जाता है।’ ( मुक्तिबोध रचनावली : एक – सं. नेमिचंद्र जैन, पे. 239 )
आपकी कविताओं की बहुत बड़ी कशिश यही नहीं है कि वो ‘क्षणिक उच्छवासों की’ नहीं होतीं, बल्कि ये भी होती है कि तमाम फ़ैंटेसियों के इस्तेमाल के बावजूद उनका ‘वस्तुगत संदर्भ’ बिल्कुल साफ़ होता है। ‘भूत का उपचार’ कहानी में वो धुँधला रह गया है।
आपके नैरेटर ने कहा, ‘और मैंने एक चित्र बनाना चाहा। एक ऐसा व्यक्ति, जो द्विधाग्रस्त है, द्विधापन्न है।’( मुक्तिबोध रचनावली : तीन – नेमिचंद्र जैन, पे. 123 ) द्विधा क्या है ? ‘एक तरफ़ वह इतना बहिर्मुख, सचेत और मुस्तैद बनना चाहता है, इतना कार्यकुशल और दुनियादार होना चाहता है..’ ( वही. पे. 124 ) दूसरी तरफ़ ‘उसकी भीतरी मानवीय, सहज-संवेदनशील अंतर्मुख आत्मा में एक अक्षम, नाज़ुक किंतु वांछनीय ,परम-श्लाध्य पराजय छिपी हुई है।’ ( वही. पे. 124 )
साफ़ ज़ाहिर है कि नैरेटर का झुकाव दूसरी तरफ़ ही है। पहला पहलू ‘सफलता’ का है और दूसरा पहलू ‘सार्थकता’ का है । आपको ‘सफलता’ में दिलचस्पी नहीं थी। नैरेटर के उस किरदार में भी ऐसी कोई दिलचस्पी नज़र नहीं आयी। फिर ‘द्विधा’ क्या हुई ? ‘द्विधा’ तब होती, जब उसका झुकाव ‘सफलता’ की तरफ़ भी होता।
आपके नैरेटर ने जो अपने किरदार के बारे में बताया, ‘वह इस पराजय पर पछताता है, क्योंकि उसको भ्रम है कि यदि उसकी विजय होती तो ख़ूब अच्छा होता। दूसरे शब्दों में – – उसका अभिप्राय है – बुलबुल को यह शिकायत कि हम उल्लू न हुए।’ ( वही. पे. 124 ) इसमें भी ‘द्विधा’ कहाँ है? क्या वो एक ‘नाकाम बुलबुल’ की बनिस्बत एक ‘कामयाब उल्लू’ को पसंद कर सकता था ? क्या उसका किरदार भी ऐसा कर सकता था? फिर वो कौन हैं, जो ‘नाकाम बुलबुल’ की बनिस्बत ‘कामयाब उल्लू’ को पसंद करते हैं? ये वो ‘दुनियादार’ दुनिया है, जो इस कहानी में ‘वस्तुगत संदर्भ’ की तरह पेश नहीं हो पायी। ‘वस्तुगत संदर्भ’ की कमी इससे भी ज़ाहिर होती है कि आपकी कहानी का नैरेटर और उसका किरदार दोनों एक ही पहलू के नुमाइंदे नज़र आते हैं । यानी उनका मुख़ालिफ़ पहलू ठीक-ठीक सामने नहीं आ पाता।
[bs-quote quote=”आपकी कहानी एक दाख़िल-दफ़्तर साँझ में ऐसे सवाल का ख़ाका बड़ी बारीकी से खींचा गया है। कभी-कभी लगता है कि जैसे ‘एक दाख़िल-दफ़्तर साँझ’ बुनियादी तौर पर ‘वाच्यार्थ’ है, तो समझौता कहानी का रीछ और शेरवाला हिस्सा उसका ‘व्यंग्यार्थ’ है। यहीं ये भी बता दूँ कि ये कहानी मैं आपकी कहानी पढ़ने से पहले सुन चुका था । इससे कोई फ़र्क़ इसलिए नहीं पड़ता कि मेहरबान सिंह ने बता ही दिया था, ‘यह एक लोककथा है।’” style=”style-2″ align=”center” color=”” author_name=”” author_job=”” author_avatar=”” author_link=””][/bs-quote]
आपके नैरेटर ने अपने किरदार के बारे में बताया,‘वह एक गणित के नशे में रहता है। – – बेवक़ूफ़ है वह, जो साहित्य, संगीत और गणित की दुनिया में पड़ा हुआ है। वह न साहित्यज्ञ है, न संगीतज्ञ, न गणितज्ञ। इन सबमें पारंगत होने का अवसर नहीं मिला, .. ’ ( वही. पे. 125 )
साहित्य हो या संगीत हो या गणित, अगर सरमायेदारों की ख़िदमत में लगा दिये जाते हैं, तो ‘कामयाब’ होने के दरवाज़े ख़ुल जाते हैं, अगर इनकी सेवा में नहीं लगाये जाते, तो ‘कामयाब’ नहीं हो पाते। हाँ कार्ल मार्क्स ने ये ज़रूर बताया था कि कुछ कलाओं से सरमायेदार दुनिया को बड़ी दुश्मनी है। उन्हीं के लफ़्ज़ों में सुन लें, ‘ .. पूँजीवादी उत्पादन का आत्मिक सृजन की कतिपय शाखाओं के साथ, जैसे कला तथा काव्य के साथ वैमनस्य है।’ ( साहित्य तथा कला – मार्क्स – एंगेल्स, पे. 164 )
अगर आपका किरदार ‘गणित के नशे में रहता है।’ तो आख़िर उसका किस ‘वस्तुगत संदर्भ’ में इस्तेमाल करता है कि आज की सरमायेदारी से उसका मेल बैठ नहीं पाता? मैथेमेटिक्स तो एसा मौज़ू है कि उसके इस्तेमाल से मुनाफ़ा कमाने की भरपूर गुंजाइश है।
ऐसा नहीं कि ‘गणित की दुनिया’ में रहकर कोई नाकाम नहीं हो सकता, लेकिन उसका ‘वस्तुगत संर्दभ’ साफ़ दिखाया जाना क़तई ज़रूरी है।
उसे ‘साहित्य, संगीत और गणित’ में ‘पारंगत’ होने का अवसर क्यों न मिल सका, इसकी एक abstract वजह ‘प्रतिकूलता’ बता दी गयी, लेकिन उसपर रौशनी नहीं डाली गयी।
हम चाहें तो आपके नैरेटर के किरदार का ‘वस्तुगत संदर्भ’ इसे कह सकते हैं, ‘जेब में धेला नहीं। कल क्या होगा मालूम नहीं। बच्चों के पास कपड़े नहीं। ओढ़ने-बिछाने की तकलीफ़ ।’ ( वही. पे. 125)
‘गणित के नशे’ की वजह से बहुत सारे साइंसदाँ तकलीफ़ उठाते हुए दिखायी देते हैं, मगर अस्ल में ‘गणित के नशे’ की वजह से नहीं, बल्कि ‘समाज’ की, और ख़ास तौर पर ‘हाकिमों’ की आलोचना की वजह से तकलीफ़ उठाते हैं ।
आपके नैरेटर ने अपने किरदार को ‘गणित का नशा’ तो दिया, लेकिन ‘समाज की आलोचना’ का तत्व नहीं दे सका। इसीलिए अपने तमाम ड्रामे के एलीमेंट के बावजूद ये कहानी पुरकशिश न बन सकी।
सवाल ये है कि वो अपने ‘गणित के नशे’ से क्या हासिल करना चाहता है कि पेट भरने के सवाल को वो ‘भाड़े पर बिक’ जाना समझता है। और अगर वो ऐसा ही समझता है, तो उसके मुँह पर ऐसे जुमले नहीं जँचते, 1 – ‘मैंने भी एक नया धंधा सीख लिया है।’ ( वही, पे. 125 ) 2 – ‘ – – – मेरे डायरेक्टर इसलिए ख़ुश हैं कि मैं एक अच्छा गणितज्ञ होने के साथ ही ख़ासा पोलिटिकल आदमी भी हूँ।’ ( वही, पे. 126 ) 3 – ‘… मैंने दो अख़बारों पर मुक़दमा चला दिया है।’ ( वही, पे. 126 )
इतनी ‘दुनियादारी’ दिखाने के बाद वो किरदार कहता है, ‘ …. मैं इस बात का विरोध करता हूँ कि आप निम्न-मध्यवर्गीय कहकर मुझे ज़लील करें , मेरे फटेहाल कपड़ों की तरफ़ जान-बूझकर लोगों का ध्यान इस उद्देश्य से खिंचवायें कि वे मुझपर दया करें। उन सालों की ऐसी की तैसी।’ ( वही, पे. 129 ) जब ‘निम्न-मध्यमवर्गीय’ कहने पर ज़लालत महसूस होती है, तो ‘सर्वहारा’ दिखाने पर क्या हालत होगी? ऐसे व्यक्ति के लिए ‘डी-क्लास’ होने के सिलसिले का मतलब क्या होगा? ‘इस भूत को मार भगाया जाये !’ तो भी क्या उसके ‘डी-क्लास’ होने का सिलसिला शुरू हो पायेगा?
समझौता पर बात शुरू करने से पहले मैं उसको लेकर कही हुई अपनी दो बातें दोहरा दूँ। पहली समझौता, पक्षी और दीमक, क्लॉड ईथरली और जंक्शन साफ़ तौर पर ब्रह्मराक्षस का शिष्य से आगे बढ़ी हुई कहानियाँ नज़र आती हैं। (सापेक्ष : 55 – मुक्तिबोध विशेषांक – सं. महावीर अग्रवाल, पे. 668 )
दूसरी “ समझौता में ‘मेहरबान सिंह’’ और ‘मैं’ की कहानी उसी तरह कचहरियों में फैली नाइंसाफ़ियों का बयान करती है, जैसी ‘एक दाख़िल-दफ़्तर साँझ’ में भी देखी जा सकती है। मगर उसके बीच आयी हुई रीछ और शेर की नीतिकथा इस कहानी को ज़्यादा मानीख़ेज बना देती है। यहाँ मुक्तिबोध ने एक लतीफ़े को डरावने माहौल की अक्कासी का औज़ार बना दिया है । एक सर्कस का शेर जब रीछ पर हमला करता है, तो रीछ ‘मरा-मरा’ पुकार उठता है, तब शेर उससे कहता है, ‘अबे डरता क्या है, मैं भी तेरे ही सरीखा हूँ, मुझे भी पशु बनाया गया है, सिर्फ़ मैं शेर की खाल पहने हूँ, तू रीछ की !’ (मुक्तिबोध रचनावली : तीन, पे. 139 ) मगर ये कहानी उतनी मानीख़ेज़ भी नहीं है, जितनी ‘पक्षी और दीमक’ है।” ( सापेक्ष : 55 – मुक्तिबोध विशेषांक – सं. महावीर अग्रवाल, पे. 669 )
आपकी कहानी के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा नैरेटर और मेहरबान सिंह की कहानी का, जिसे ‘वाच्यार्थ’ भी कह सकते हैं। इसे हम symbol की कहानी न कहकर metaphor की कहानी कह सकते हैं। नैरेटर और मेहरबान सिंह की कहानी ‘उपमेय’ है, तो रीछ और शेर की कहानी ‘उपमान’। दोनों के एक साथ होने की वजह से metaphor बन जाता है।
नैरेटर और मेहरबान सिंह की कहानी ‘उपमेय’ होते हुए भी कमज़ोर इसलिए रह जाती है कि उनकी कहानी की वजहें पूरी तरह से खुल नहीं पातीं। उसका ये हिस्सा तो बहुत ही धुँधला है, “ ‘नियम के विरुद्ध मैं नहीं था, वह था। लेकिन, मुझे जब डाँटकर कहा तो मैंने पहले अदब से, फिर ठंडक से, फिर और ठंडक से, फिर खीझकर एक ज़ोरदार जवाब दिया। उस जवाब में ‘नासमझ’ और ‘नाख़्वांद’ जैसे शब्द ज़रूर थे। लेकिन, साइंटिफ़िकली, ग़लती उसकी थी, मेरी नहीं। फिर ग़ुस्से में मैं नहीं था, वह था। एक जूनियर आदमी मेरे सर पर बैठा दिया गया, ज़रा देखो तो ! इसीलिए कि वह फ़लाँ-फ़लाँ का ख़ास आदमी, वह ‘ख़ास-खास’ काम करता है। उस शख़्स के साथ मेरी ‘ह्यूमन डिफ़िकल्टी’ थी !”
( मुक्तिबोध रचनावली : तीन – सं. नेमिचंद्र जैन, पे. 132 )
इसके किरदार ‘वह’ और ‘फ़लाँ’ ही नहीं, बल्कि ‘ख़ास-ख़ास काम’ के भी ख़ाके ठीक से पेश नहीं किये जा सके हैं। हम इसपर सवाल इसलिए नहीं उठाते कि दफ़्तरों में इस तरह के सवाल तो उठते ही रहते हैं। मगर आपकी कहानी एक दाख़िल-दफ़्तर साँझ में ऐसे सवाल का ख़ाका बड़ी बारीकी से खींचा गया है। कभी-कभी लगता है कि जैसे ‘एक दाख़िल-दफ़्तर साँझ’ बुनियादी तौर पर ‘वाच्यार्थ’ है, तो समझौता कहानी का रीछ और शेरवाला हिस्सा उसका ‘व्यंग्यार्थ’ है। यहीं ये भी बता दूँ कि ये कहानी मैं आपकी कहानी पढ़ने से पहले सुन चुका था । इससे कोई फ़र्क़ इसलिए नहीं पड़ता कि मेहरबान सिंह ने बता ही दिया था, ‘यह एक लोककथा है।’ ( वही, पे. 140 )
‘समझौता’ कहानी का ज़िक्र करते हुए मैंने कहा था, “मगर ये कहानी उतनी मानीख़ेज़ भी नहीं है, जितनी ‘पक्षी और दीमक’ है।” ( सापेक्ष : 55 – मुक्तिबोध विशेषांक – सं. महावीर अग्रवाल, पे. 669 )
उससे आगे की बात भी दोहरानी ज़रूरी है –
“ पक्षी और दीमक की ‘नीति-कथा’ का मुख़्तसर बयान यों किया जा सकता है — एक गाड़ीवाला चिल्ला-चिल्लाकर कहता है, ‘दो दीमकें लो, एक पंख दो।’ उसकी आवाज़ सुनकर एक नौजवान पक्षी को लगा कि यह बहुत बड़ी सुविधा है — वह रोज़ तीसरे पहर नीचे उतरता और गाड़ीवाले को एक पंख देकर, दो दीमकें ख़रीद लेता। — उसके पंखों की संख्या लगातार घटती गयी। – – फिर, एक दिन उस पक्षी के जी में न मालूम क्या आया। वह ख़ूब मेहनत से ज़मीन में से दीमकें चुन-चुनकर, खाने के बजाय उन्हें इकट्ठा करने लगा। अब उनके पास दीमकों के ढेर हो गये। – – उसने गाड़ीवाले से कहा – – ‘ये मेरी दीमकें ले लो और मेरे पंख मुझे वापस कर दो।’ – – गाड़ीवाला ठठाकर हँस पड़ा। उसने कहा, ‘बेवक़ूफ़, मैं दीमक के बदले पंख लेता हूँ, पंख के बदले दीमक नहीं।’
क्या ऐसा कोई गाड़ीवाला था? क्या ऐसी दीमकें थीं? क्या ऐसा कोई ‘नौजवान पक्षी’ था? सारी बेमतलब की बातें हैं। मगर जितनी बेमतलब उतनी ही मानीख़ेज़।” ( वही, पे. 669 )
इस कहानी का पक्षी नैरेटर का उपमान है, तो गाड़ीवाला ‘भगवे खद्दर-कुरतेवाले’ का। पक्षी दीमकों के बदले अपने पंख देता है, तो नैरेटर ‘भगवे खद्दर-कुरतेवाले’ से मिलनेवाली सहूलतों के बदले अपनी आज़ादी खोता है । वो छटपटाता चाहे जितना हो, ‘उस भगवे खद्दर-कुरतेवाले से छुटकारा कब होगा !’ ( मुक्तिबोध रचनावली : तीन – सं. नेमिचंद्र जैन, पे. 145 ), लेकिन उसकी अस्ली हालत उसके सामने अयाँ है, ‘साफ़ है कि उस भगवे खद्दर कुरतेवाले से मैं दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता। मैं उसके प्रति वफ़ादार रहूँगा, क्योंकि मैं उसका आदमी हूँ। भले ही वह बुरा हो, भ्रष्टाचारी हो, किंतु उसी के कारण मेरी आमदनी के ज़रिये बने हुए हैं। व्यक्ति-निष्ठा भी कोई चीज़ है, उसके कारण ही मैं विश्वास-योग्य माना गया हूँ। इसीलिए, मैं कई महत्वपूर्ण कमेटियों का सदस्य हूँ।’ ( वही, पे. 148 )
नैरेटर को सहूलतें देने और उसकी आज़ादी ख़रीद लेने का ‘भगवे खद्दर-कुरतेवाले’ का मक़सद क्या है, उसकी भी एक ठोस मिसाल इस कहानी में है, “किसी ख़ास जाँच के ऐन मौक़े पर किसी दूसरे शहर की – – संस्था से उधार लेकर सूक्ष्मदर्शी यंत्र हाज़िर। सब चीज़ें मौजूद हैं। आइए, देख जाइए। जी हाँ, ये तो हैं सामने। लेकिन जाँच ख़त्म होने पर सब ग़ायब, सब अंतर्धान। कैसा जादू है ! ख़र्च का आँकड़ा ख़ूब फुलाकर रखिए। सरकार के पास काग़ज़ात भेज दीजिए। ख़ास मौक़ों पर ऑफ़िसों के धुँधले गलियारों और होटलों के कोनों में मुट्ठियाँ गरम कीजिए । सरकारी ‘ग्रांट’ मंज़ूर! और, उसका न जाने कितना बड़ा हिस्सा, बड़े ही तरीक़े से संचालकों की जेब में। जी!” ( वही, पे. 145 )
मगर गाड़ीवाले का मक़सद क्या है कि वो पक्षी को दो दीमकें देकर एक पर ख़रीदता है ? ऐसा तो किसी कोने से नहीं लगता कि वो ‘काली बिल्ली’ का ‘एजेंट’ था ! कहानी के आख़िर में हुआ तो ये ज़रूर था, ‘एक दिन एक काली बिल्ली आयी और अपने मुँह में उसे दबाकर चली गयी।’ ( वही, पे. 150 )
गाड़ीवाले का मक़सद आपने अनकहा छोड़ दिया, इससे इस नीति-कथा की ताक़त में कोई कमी नहीं आयी। किसी कहानी के लिए उपमान का तमाम दलीलों पर खरा उतरना बहुत ज़रूरी भी नहीं है । ज़रूरी है उसका पुरअसर होना। आख़िर नैरेटर की कहानी से कहीं ज़्यादा ‘पक्षी और दीमक’वाली नीति-कथा ही ज़ेहन में जगह बनाती है।
पक्षी और दीमक से भी ज़्यादा बेमतलब और उससे कहीं बढ़कर मानीख़ेज़ कहानी है ‘क्लॉड ईथरली’। मुक्तिबोध की दिलचस्पी की सारी चीज़ें इसमें इकट्ठी मिल जायेंगी, जैसे उनकी ‘अँधेरे में’ नाम की कविता में। इस हिसाब से यही उनकी सबसे अहम कहानी गिनी जायेगी। ‘क्लॉड ईथरली’ के किसी किरदार, किसी वाक़िये का हक़ीक़त से बहुत वास्ता नहीं है और इस कहानी के हर्फ़-हर्फ़ में हक़ीक़त कूट-कूटकर भरी हुई है। इस बात को समझने के लिए प्रेमचंद के इस जुमले को याद किया जा सकता है, ‘एक आलोचक ने लिखा है कि इतिहास में सब कुछ यथार्थ होते हुए भी वह असत्य है, और कथा-साहित्य में सब कुछ काल्पनिक होते हुए भी वह सत्य है।’ ( साहित्य का उद्देश्य – प्रेमचंद, पे. 46 )
क्रमशः ….
सुल्तान अहमद जाने-माने ग़ज़लकार हैं ।


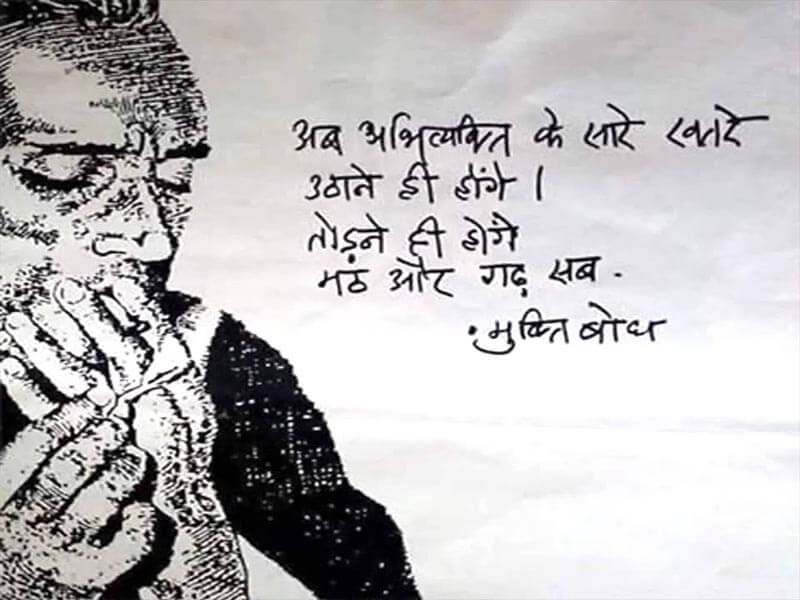


[…] मुक्तिबोध को एक ग़ज़लकार की चिट्ठी – 2 […]