दो अक्टूबर, 2017 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ओबीसी की केंद्रीय सूची के वर्गीकरण के लिये आयोग बनाने के फैसले को मंज़ूरी दी है। यानी इस वर्ग में भी पिछड़ेपन की सीमा के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो एक तरह से यह कोटे के अंदर कोटा होगा। सरकार के राजनैतिक उद्देश्यों से परे हटकर विचार करें तो सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में यह एक महत्त्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। इस लेख में हम ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण, सरकार के इस प्रयास के निहितार्थों एवं संभावित प्रभावों तथा इसकी ज़रूरतों के बारे में चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2017 में दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रोहिणी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ओबीसी उपवर्गीकरण जाँच आयोग का गठन किया गया। जिसको 13वां विस्तार देते हुए 31 जनवरी, 2023 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी है।
ओबीसी आरक्षण की पृष्ठभूमि
मंडल आयोग का गठन 1 अप्रैल, 1979 में सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान के उद्देश्य से किया गया था। इस आयोग का नेतृत्व भारतीय सांसद बी.पी. मंडल द्वारा किया गया था।
जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिये आरक्षण एवं कोटा निर्धारण की व्यवस्था की गई। लेकिन सवाल यह था कि किन समूहों को यह लाभ दिया जाए अर्थात समूहों के पिछड़ेपन का निर्धारण कैसे हो। गौरतलब है कि समूहों के पिछड़ेपन का निर्धारण करने के लिये मंडल आयोग द्वारा ग्यारह सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक संकेतकों का इस्तेमाल किया गया। वर्ष 1980 में मंडल आयोग की रिपोर्ट में पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 27 फीसदी आरक्षण की सिफारिश की गई।
[bs-quote quote=”ओबीसी वर्ग के अंतर्गत ही कुछ ऐसी जातियाँ हैं जो इसी वर्ग से संबंध रखने वाली अन्य जातियों के उत्पीड़न में शामिल हैं। ऐसे में ओबीसी आरक्षण का लाभ कुछ सीमित समूहों तक ही सीमित हो जाना लाज़मी है। ऐसे में सरकार का यह कदम स्वागत योग्य है, क्योंकि ओबीसी आरक्षण कोटे में एक कोटा बनाकर इस आरक्षण वर्ग में लाभ से वंचित अन्य जातियों को राहत दी जा सकती है।” style=”style-2″ align=”center” color=”” author_name=”” author_job=”” author_avatar=”” author_link=””][/bs-quote]
मंडल आयोग ने यह भी सिफारिश की कि केंद्र और राज्य सरकारों के अधीन चलने वाली वैज्ञानिक, तकनीकी तथा प्रोफेशनल शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिये ओबीसी वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिये 27% आरक्षण लागू किया जाए।
वर्ष 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों को सरकार द्वारा लागू किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय राजनीति में व्यापक बदलाव आया। हालांकि कई जगह व्यापक विरोध भी देखने को मिला, लेकिन इंद्रा साहनी बनाम भारत सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले पर 16 नवम्बर, 1992 को मुहर लगा दी।
विदित हो कि इंद्रा साहनी मामले में ही सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी थी कि पिछड़े वर्गों को पिछड़ा या अति-पिछड़ा के रूप में श्रेणीबद्ध करने में कोई संवैधानिक या कानूनी बाधा नहीं है। अतः राज्य सरकारें ऐसा करना चाहें तो कर सकती हैं।
तब से भारतीय राजनीति में आरक्षण इतना महत्त्वपूर्ण हो गया है कि इसके जिक्र मात्र से सरकारे बन और बिगड़ जाती हैं।
क्या है ओबीसी में वर्गीकरण का मामला
भारतीय सामाजिक व्यवस्था कुछ ऐसी है कि ओबीसी में आने वाली कुछ जातियाँ ओबीसी में ही शामिल कुछ अन्य जातियों से सामाजिक और आर्थिक दोनों ही रूपों में बेहतर स्थिति में हैं। दरअसल, मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था तो कर दी गई, लेकिन ओबीसी में ही अत्यधिक कमज़ोर वर्ग के लिये कुछ विशेष नहीं किया गया। यही कारण है कि ओबीसी आरक्षण का लाभ भी ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखने वाली कुछ ताकतवर जातियों के हाथों में ही सिमटकर रह गया है। आज के दौर में यादव, कुर्मी, कोयरी, जाट, थेवर, कु
यह भी पढ़ें…
बनारस के उजड़ते बुनकरों के सामने आजीविका का संकट गहराता जा रहा है
ऐसे में ओबीसी वर्ग के अंदर ही वर्गीकरण की माँग लगातार की जाती रही है और अब तक 11 राज्यों-आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुंडूचेरी, कर्नाटक, हरियाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, केरल, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु ने पहले ही ओबीसी वर्गीकरण को लागू कर दिया है।
ओबीसी आरक्षण से संबंधित केन्द्रीय सूची में इस प्रकार के वर्गीकरण की व्यवस्था नहीं की गई है।
हालांकि पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्ज़ा देने का फैसला कर चुकी सरकार ने अब ओबीसी कोटे के अंदर कोटे की व्यवस्था कर उन पिछड़ी जातियों को राहत देने की तैयारी की है, जिन्हें आरक्षण का समुचित लाभ नहीं मिल पाता है।
केन्द्रीय ओबीसी सूची वर्गीकरण आयोग का कार्य
इस आयोग का नाम अन्य पिछड़ा वर्ग उप-वर्गीकरण जाँच आयोग रखा गया है। यह ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल जातियों को आरक्षण के लाभ के असमान वितरण की जाँच करेगा। साथ ही असमानता दूर करने के तौर-तरीके और प्रक्रिया भी तय करेगा। यह ओबीसी के भीतर उप-वर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक और उचित दृष्टिकोण पर आधारित व्यवस्थात्मक मानदंडों के निर्माण का कार्य भी करेगा। गठन के समय अक्टूबर, 2017 में तय किया गया कि यह आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति की तारीख से 12 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।दरअसल, पिछड़ा वर्ग आयोग ने तीन वर्गों में वर्गीकरण का सुझाव दिया था- पिछड़ा वर्ग, अधिक पिछड़ा वर्ग और अति-पिछड़ा वर्ग। यह आयोग उन जातियों की संख्या और पिछड़ेपन को ध्यान में रखकर नई सूची तैयार करेगा। लेकिन इस आयोग का कार्यकाल बढ़ते बढ़ते 31 जनवरी, 2023 तक बढ़ा दिया गया है।
यह भी पढ़ें…
अर्थव्यवस्था के कुठाराघात ने बनारस में खिलौना बनानेवालों को तबाही के कगार पर ला खड़ा किया है
क्या होगी आगे की राह
यदि सच में हम हाशिए पर ठेल दिए गए समूहों के जीवन में आरक्षण के ज़रिये महत्त्वपूर्ण बदलाव लाना चाहते हैं, तो हमारे पास केवल दो विकल्प हैं-या तो सरकार को सरकारी नौकरियों और विश्वविद्यालयों में सीटों की उपलब्धता में व्यापक रूप से वृद्धि करनी चाहिये या फिर इन लाभों को प्राप्त करने योग्य आबादी का आकार कम करना चाहिए।
इन दो विकल्पों में से सबसे व्यवहार्य विकल्प दूसरा है। लेकिन इसके लिए हमें ज़रूरत है जाति संबंधित मानद आँकड़ों की। जातिगत जनगणना के सम्बंध में हमारे पास आंकड़ों का अभाव है, अब जबकि वर्ष 2021 की जनगणना की तैयारियाँ चल रही हैं तो जातिगत के आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए अब एक विशेषज्ञ समूह बनाने का समय है। बिना इन आंकड़ों के यह आयोग अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में उतना सफल नहीं रहेगा।
यह भी पढ़ें…
खिलौना रंगने वाली औरत की साठ रुपये रोज पर कैसे गुजर होती होगी?
इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत की जातीय और सामाजिक व्यवस्था काफी जटिल है। ओबीसी वर्ग के अंतर्गत ही कुछ ऐसी जातियाँ हैं जो इसी वर्ग से संबंध रखने वाली अन्य जातियों के उत्पीड़न में शामिल हैं। ऐसे में ओबीसी आरक्षण का लाभ कुछ सीमित समूहों तक ही सीमित हो जाना लाज़मी है। ऐसे में सरकार का यह कदम स्वागत योग्य है, क्योंकि ओबीसी आरक्षण कोटे में एक कोटा बनाकर इस आरक्षण वर्ग में लाभ से वंचित अन्य जातियों को राहत दी जा सकती है। दरअसल, मंडल आयोग की सिफारिशों का उद्देश्य आरक्षण के ज़रिये सामाजिक न्याय के लक्ष्य को पूरा करना था, लेकिन पिछले कुछ समय से इस व्यवस्था को इस रूप में देखा जाने लगा है जैसे यह सरकारी नौकरियाँ हासिल करने का आसान ज़रिया हो। यही कारण है कि वोट बैंक के लालच में कई राज्यों ने ओबीसी वर्ग के अन्दर वर्गीकरण करते हुए 50 प्रतिशत की तय सीमा से आगे जाकर भी आरक्षण की व्यवस्था की, जिसे सुप्रीम कोर्ट को खारिज़ करना पड़ा। इस आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद वर्गीकरण की एक केन्द्रीय सूची मिल जाएगी, जिससे आरक्षण के नाम पर आए दिन होने वाले दंगा-फसादों से मुक्ति मिल सकती है।

चौ. लौटनराम निषाद सामाजिक न्याय चिंतक व भारतीय ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं।



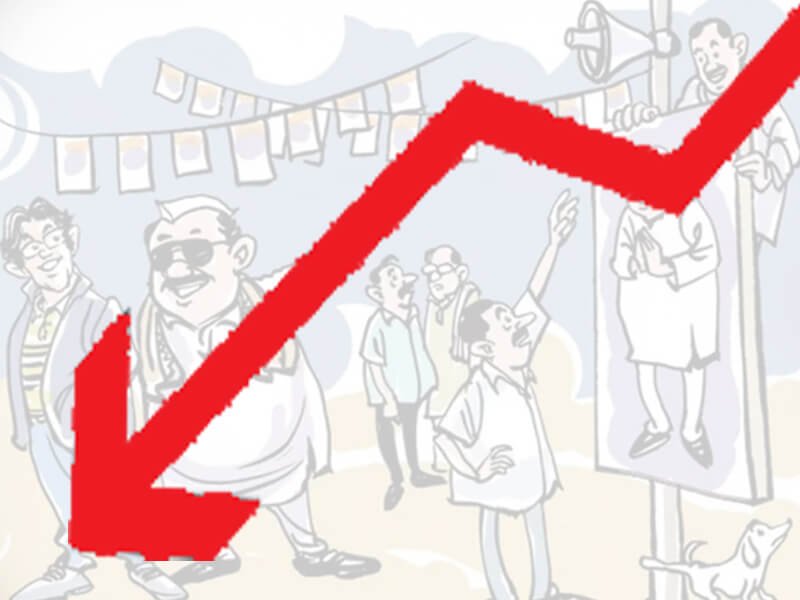

[…] ओबीसी वर्गीकरण का औचित्य कितना उचित? […]