बातचीत का पहला हिस्सा
कुछ साल पहले आपका एक उपन्यास प्रकाशित हुआ था ‘नरक मसीहा’ जिसकी काफी चर्चा रही है। यह उपन्यास एनजीओ की भीतरी दुनिया के जाल-फरेब, जमीन मालिक से भूमिहीन होते किसानों और तमाशाई मीडिया की भी खबर लेता है। चर्चा केवल एनजीओ को केंद्र में रखकर की जा रही है, क्या इससे आप संतुष्ट हैं?
नहीं, एनजीओ संस्कृति तो केवल एक कथावस्तु है जिसको उसकी अनेक कथा-उपकथाएं एक बड़ी नदी का रूप प्रदान करती हैं। मेरी दृष्टि में इस उपन्यास को लेकर जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वे तात्कालिक प्रतिक्रियाएं हैं। असल मुद्दा यह है कि इस संस्कृति के पनपने से हमारे सांस्कृतिक, राजनैतिक और आर्थिक पक्षों पर क्या असर हो रहा है। हमें देखना यह है कि इस संस्कृति के हावी होने से हमारी वैचारिक प्रतिबद्धता का कितना क्षरण हुआ है। इसके पनपने से हमारे जनांदोलनों को कितना नुकसान हुआ है और सबसे बड़ी बात, नव साम्राज्यवादी मानसिकता को अन्दर ही अन्दर पोषित करने वाले नरक मसीहाओं द्वारा किस तरह ग़रीबी का बाई-प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। हिंदी पट्टी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि यहाँ हर विषय का सरलीकरण कर दिया जाता है। रचना की आंतरिक परतों में घुसने का साहस और रिवाज लगभग समाप्त हो चुका है। जैसाकि आपने अपने सवाल में खुद एनजीओ की भीतरी दुनिया के जाल-फरेब, जमीन मालिक से भूमिहीन होते किसानों और तमाशाई मीडिया की खबर लेने की बात की है। तो क्या एनजीओ के बहाने ऐसे गंभीर मुद्दों पर बात नहीं होनी चाहिए? मेरा मानना है कि लेखक से बड़ी ज़िम्मेदारी और तैयारी आलोचक की होनी चाहिए मगर हिंदी में अब ऐसा नहीं होता ।
‘नरक मसीहा’ में आपने तथाकथित गांधीवादियों, वामपंथियों, अम्बेडकरवादियों, नारीवादियों आदि को पतनशील कार्यों में लिप्त दिखाया है। एक तरह से उपन्यास यह संदेश देता है कि आचरण के स्तर पर युवाओं के लिए मूल्य, संस्कार और विचारधारा का खास मायने नहीं रह गया है। इसके पीछे आप कौन से कारक जिम्मेदार मानते हैं?
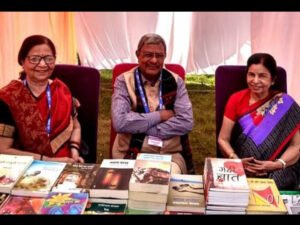
यह आप कह सकते हैं कि उपन्यास में गांधीवादियों, वामपंथियों, अम्बेडकरवादियों, नारीवादियों आदि को पतनशील कार्यों में लिप्त दिखाया है। दरअसल, काम कोई भी पतनशील नहीं होता. पतनशीलता हमारी मानसिकता, नीयत और सोच में होती है वरना जिस कल्याण की भावना को गांधी जी एक मिशन कहा करते थे वह पिछले तीन दशकों में बड़ी तेज़ी से ‘व्यवसाय’ में कैसे तब्दील हो गया? मेरा मानना है कि इस कल्याणकारी भावना को सबसे ज्यादा चोट हमारी तथाकथित वैचारिक प्रतिबद्धता, चाहे वह गांधीवादी रही हो या वामपंथी, अम्बेडकरवादी रही हो या नारीवादी, ने की है। वैचारिकता तो आज के समय में एक लिबास का काम करने लगी है जो सुविधा, समय और ज़रूरत के हिसाब से बदल जाती है। आपने उपन्यास के उस मूल स्वर को पकड़ लिया है कि आचरण के स्तर पर युवाओं के लिए मूल्य, संस्कार और विचारधारा का खास मायने नहीं रह गया है। रही बात इसके पीछे के कारकों की तो मुझे लगता है कि प्रतिबद्धता का सीधा संबंध हमारे जीवन-मूल्यों और जीवन-संघर्षों से होता है। ज्यादातर भारतीय उपमहाद्वीप खासकर दक्षिण एशियाई निम्न-मध्यवर्गीय समाज से आते हैं। ऐसे निम्न-मध्यवर्गीय समाज से जिसका बचपन से लेकर युवावस्था का समय अभावों में गुज़रा हुआ होता है। एक तरह से हम अपने अभावों को अभिशाप की तरह ढोते हैं। जैसे ही हमें कुछ करने के नाम पर कहीं से आर्थिक मदद के नाम पर धन उपलब्ध होने लगता है हमारी यह प्रतिबद्धता डगमगाने लगती है जिसकी परिणिति पतन पर जाकर ठहरती है। सच तो यह है कि हमारे समाज से शुचितावादी राजनीतिक, सामाजिक और कल्याणकारी प्रशिक्षण की भावना समाप्त होती जा रही, यह पतनशीलता उसी का परिणाम है। हमारी इसी पतनशील कमज़ोरी का वे साम्राज्यवादी संस्थाएं फायदा उठा रही हैं जो हमारी ग़रीबी दूर करने के लिए विदेशी अनुदान प्रदान करती हैं। वास्तव में इस अनुदान के पीछे एक समानांतर व्यवस्था चलाने की योजना काम करती है। इससे उन साम्राज्यवादी ताकतों को अपने लिए एक तरह से सस्ते अनुयायी मिल जाते हैं, जो अपनी ग़रीबी दूर करने के नाम पर ऐसे-ऐसे आंकड़े उपलब्ध कराते हैं जो हमें ही नुकसान पहुंचाते हैं।
आपने अपनी फेसबुक वाल पर हाल में इंटेलीजेंस ब्यूरो (आईबी) की भारत में तेज़ी से पनपती एनजीओ संस्कृति और विदेशी फंड प्राप्त करने को लेकर आई एक रिपोर्ट का उल्लेख किया है। इस रिपोर्ट में एनजीओ के क्रियाकलापों को लेकर कई गंभीर सवाल उठाये गए हैं, जबकि इन्हीं गंभीर सवालों से ‘नरक मसीहा‘ दो-चार होता है। मैं इस रिपोर्ट के तथ्यों और उपन्यास व उपन्यासकार के रचनात्मक कौशल तथा उसकी दृष्टि के संदर्भ में यह जानना चाहता हूँ कि तथ्यों और रचनात्मक कौशल को आप किस तरह साधते हैं?

एक लेखक के रूप में मेरा मानना है कि किसी भी रचना की सामयिकता और उसकी रचना मूल्यता का आधार यथार्थ और कल्पना का वह सम्मिश्रण है जो उसे विश्वसनीय और प्रामाणिक बनाता है। दरअसल, रचनाकार यथार्थ से इतर अपने लोक के उन सूक्ष्म स्रंध्रों के भीतरी अवयवों को पहले ही जान लेता है जिसे आम व्यक्ति आसानी से नहीं जान पाता। ‘नरक मसीहा’ के कबीर, सानिया, बहन भाग्यवती, टीना डालमिया, डॉ. वंदना राव, गंगाधर आचार्य, सुमन भारती, सरला बजाज, अमीना खान जैसों से एनजीओ की यह दुनिया अटी पड़ी है। दरअसल, ये मात्र पात्र भर नहीं हैं बल्कि एनजीओ जगत की पहचान इन्हीं से है। इन नरक मसीहाओं के लिए बकौल मदर टेरेसा की उत्तराधिकारी सिस्टर निर्मला ग़रीबी ईश्वर का वह उपहार है जो हमेशा बनी रहेगी। अगर दुनिया से ग़रीबी खत्म हो जाए तो ये बेरोजगार हो जाएंगे। ‘नरक मसीहा’ आज़ादी के बाद के वैचारिक-सामाजिक प्रतिबद्धताओं के सत्व के क्षरण की गाथा है। अब यह लेखक के कौशल पर निर्भर करता है कि वह इन दोनों तत्वों यानी यथार्थ और कल्पना को किस हद तक प्रामाणिक और विश्वसनीय बनाने में कामयाब होता है।
लाभ और लूट की संस्कृति वाले इस समय में व्यक्तिगत लाभ और हानि से ही संबंध तय हो रहे हैं। इसके साथ ही भाई-भतीजावाद, क्षेत्रवाद और जातिवाद भी बहुत कुछ तय कर रहा है, लेकिन आपने ‘नरक मसीहा’ में जातिवाद केवल दलितों में दिखाया है, जबकि यह तो बड़ी समस्या है और इससे शायद ही कोई जाति छूटी हो? क्या यह आपको न्यायसंगत लगता है?
इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि लाभ और लूट की संस्कृति वाले इस समय में व्यक्तिगत लाभ और हानि से ही संबंध तय हो रहे हैं। इस सच्चाई से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि भाई-भतीजावाद, क्षेत्रवाद और जातिवाद इन संबंधों को और मजबूती प्रदान करते हैं। आपने जैसा कहा है कि ‘नरक मसीहा’ में जातिवाद केवल दलितों में दिखाया गया है, ऐसा लगता है लेकिन अगर हम इसकी गहराई में जाएँ तो ऐसा नहीं है। यह बड़ा विचित्र है कि दलितों का भाई-भतीजावाद, क्षेत्रवाद या जातिवाद हमें तुरंत नज़र आ जाता है लेकिन सदियों से वर्ण-व्यवस्था के पोषकों (विभिन्न विचारधाराओं के होने के बावजूद) का भाई-भतीजावाद, क्षेत्रवाद या जातिवाद हमें नज़र नहीं आता है।
[bs-quote quote=”विधायिका में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का मामला सदन में अगर आज तक, बकौल इस लेखिका मेहनत पर जीने वाली सिविल सोसाइटी और आए दिन जंतर मंतर या इंडिया गेट पर चिल्लाने के बावजूद, पास नहीं हो पाया है तो उसका कारण भी यही है। यानी इनका यह शोर दिन भर खेत-खलिहानों, ईंट-भट्टों पर काम करने वाली, सड़क किनारे मिट्टी ढोने वाली मेहनतकश स्त्री के हिस्से पर कब्ज़ा करने को लेकर ही है।” style=”style-2″ align=”center” color=”” author_name=”” author_job=”” author_avatar=”” author_link=””][/bs-quote]
मान लीजिए ‘नरक मसीहा’ के अनुसार जातिवाद केवल दलितों में ही है, तो इसमें बुराई क्या है? विचारणीय यह है कि ये व्याधियां आई किस समाज से हैं। स्वाभाविक है ये वर्ण-व्यवस्था के पोषक उस समाज से आई हैं जो सदियों से दलितों-पिछड़ों का सामाजिक-आर्थिक शोषण करते आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि भाई-भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद या सांप्रदायिकता आज ख़त्म हो गया है, नहीं। बल्कि आज समाज में ये विकार, खासकर छोटे शहरों, कस्बों और गाँव-देहातों में पहले की अपेक्षा ज्यादा बढ़ा है। यह भाई-भतीजावाद, क्षेत्रवाद और जातिवाद अकेले कुछ ही क्षेत्रों में है, ऐसा नहीं है बल्कि हिंदी साहित्य में तो इसका रूप और भी विकराल है. यह विकरालता यदि देखनी है तो आप फेसबुक पर जाइए. आपको पता चल जाएगा कैसे एक राज्य, जिले और अपनी जाति के लेखकों को, जहां जिसे मौका मिलता है, चाहे वह किसी प्रकाशन गृह में कार्यरत है या किसी पत्र-पत्रिका में, बढ़ावा दे रहा है। बल्कि हिंदी साहित्य और विश्वविद्यालयों के हिंदी विभागों में नियुक्ति के लिए तो यह एक तरह की अनिवार्य शर्त बन गई है कि अगर आप पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से नहीं हैं तो आप उसी उपेक्षा की नज़र से देखे जाएंगे, जैसे समाज में किसी दलित-आदिवासी या फिर किसी अति पिछड़ी जाति के लोगों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता है।मैं इसी को साहित्य का ‘नया सवर्णवाद’ कहता हूँ। हमें इन कारणों का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन करना चाहिए कि क्यों हिंदी साहित्य से आज तक पूरा पश्चिमी भारत (पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पूर्वी पंजाब और एक हद तक मध्य प्रदेश का बड़ा हिस्सा ) बेदखल है? अगर बहन भाग्यवती, सुमन भारती, मिसेज मौर्य की जगह कोई सवर्ण पात्र होते तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये भी पढ़ें :
पुरुषों के पेटूपन और भकोसने की आदत ने औरतों को नारकीय जीवन दिया है !
वैसे भी घुटने तो पेट की तरफ़ ही मुड़ेंगे। अगर सदियों से शोषित समाज के लोग अवसर मिलने पर अपने लोगों को सत्ता के विभिन्न क्षेत्रों में उनको उनका हक़ दिला रहे हैं, तो मैं न तो इसे बुरा मानता हूँ न अनैतिक। यह तो महज एक संयोग है कि तीनों पात्र दलित हैं। चलो, थोड़ी देर के लिए हम इसे लेखक का पूर्वाग्रह मान भी लें लेकिन है तो यह एक सत्य कि हम भले ही अपने आपको कितने भी प्रगतिशील बल्कि कहिये कम्युनिस्ट कह लें, कितना भी अपने आपको गांधीवादी मानने का भ्रम पाल लें, कितना भी अपने आपको अंबेडकरवादी घोषित कर लें मगर इस देश में ‘जातिवाद’ और ‘वर्ण-व्यवस्था’ जैसी सच्चाई को भी हम नहीं झुठला सकते। वरना क्या कारण हैं कि लाख कम्युनिस्ट, प्रगतिशील या गांधीवादी होने के बावजूद हमारी मानसिकता उन्हीं पूर्वाग्रहों, दुराग्रहों की बंधक है, जिससे हम मुक्त होने का प्रपंच रच रहे होते हैं। सच तो यह है कि हमारी रगों में जातिवाद, साम्प्रदायिकता, क्षेत्रवाद का खून कहीं ज्यादा गाढ़ा हुआ है। आचरण और विचारधारा का आपस में कोई मेल नहीं है। आपकी असली पहचान विचारधारा से नहीं आचरण से होती है। विचारधारा आवरण है और आचरण हमारी पहचान। जैसे-जैसे कुछ जातियों की सत्ता में हिस्सेदारी बढ़ी है यह और ज्यादा गाढ़ा होता गया है। मैं तो इस बात को बार-बार कहता हूँ कि आज़ादी के बाद के जो कुछ झूठ हैं सामाजिक न्याय, बहुजन, समरसता, समाजवाद जैसे भ्रामक शब्द भी उनमें शामिल हैं। वास्तव में इनका सीधा संबंध सत्ता में भागीदारी से है. शायद यही वजह है कि जिस ‘बहुजन’ समाज की जो परिकल्पना थी उसका क्या हुआ? इसकी ज़द में ज़्यादातर वही जातियां हैं जिनकी राजनीतिक हिस्सेदारी ज्यादा मजबूत हुई है और जो जातियां, विशेषकर ऐसी कुछ अति पिछड़ी जातियां (कुम्हार, तेली, नाई, माली आदि ) जिनके अधिकारों और हिस्से को दूसरी दबंग ‘तथाकथित’ पिछड़ी जातियों ने लगभग हड़प लिया है, ऐसी जातियों का आज समाजवाद, सामाजिक न्याय और बहुजन से लगभग भरोसा और मोह ख़त्म हो गया है। दरअसल, ‘बहुजन’ की परिभाषा भी अब सुविधा-असुविधा के अनुसार तय होने लगी है। ऐसे में कोई यह कहे कि मैंने जातिवाद केवल दलितों में ही दिखाया है मुझे न यह तर्क संगत लगता है न न्याय संगत।
मेरे प्रश्न का आशय था कि दलितों से अधिक जातिवाद तो सवर्णों में है। वहीं से यह बीमारी दलितों और पिछड़ों में आई है। ऐसे में केवल दलितों में जातिवाद दिखाना कहाँ तक जायज है?
आपका आशय अपनी जगह बिलकुल सही है। दरअसल यह अवसर, मानसिकता और उस परंपरा से जुड़ा मामला है जो एक दूसरे की देखा-देखी आपस में हस्तांतरित होता है। ‘दलित’ तो यहाँ महज रूपक है जो इस मानसिकता को इंगित करता है कि अवसर आने पर व्यक्ति ‘अपने’ को ही उपकृत करने का प्रयास करता है, जो मनुष्य की एक स्वाभाविक और सहज प्रवृत्ति है। क्या हम इस सच्चाई से इनकार कर सकते हैं कि जब हम किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले जो स्वाभाविक जिज्ञासा पैदा होती है वह यह होती है कि सामने वाले की जाति क्या है। अगर वह सजातीय हुआ तो हम अपने आपको कितना सहज और सुविधाजनक पाते हैं, बताने की ज़रुरत नहीं है। दरअसल, यह मानव स्वभाव जो आज एक व्याधि का रूप ले चुकी है हमें सभी समाजों में देखने को मिल जायेगी।
‘नरक मसीहा’ को जहां समीक्षकों ने सराहा है वहीं लखनऊ की एक लेखिका ने उसकी मुखर आलोचना की है। उनका कहना है कि लेखक ने अभी तक अपनी मेहनत पर जीने वाली स्त्री नहीं देखी तभी तो उन्हें सारी औरतें गड़बड़ नजर आती हैं। क्या आप उनके तर्क से सहमत हैं?

जैसा कि उस लेखिका (जिसने स्वयं दो-तीन उपन्यास लिखे हैं) का कहना है कि लेखक ने अपनी मेहनत पर जीने वाली स्त्री नहीं देखी है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि इस लेखिका की नज़र में आखिर ‘अपनी मेहनत पर जीने वाली स्त्री’ से क्या अभिप्राय है, उसकी परिभाषा क्या है। वह जो धूल और धूप में दिन भर खेत-खलिहानों, ईंट-भट्टों पर पर काम करने वाली, सड़क किनारे मिट्टी ढोने वाली मेहनतकश स्त्री है या खाई-पी और एक हद तक अघाई हुई लेखन जैसे कर्म को विमर्श के नाम करियर के रूप में इस्तेमाल करने वाली उस स्त्री से है, जो वातानुकूलित कमरों में बैठ कर मेहनतकश स्त्रियों की झूठी मुक्ति का शोर मचाती है? दुर्भाग्य से हमें स्त्री के पक्ष में ऐसी ही विमर्शकार सबसे अधिक शोर मचाती नज़र आएँगी और उनकी मेहनत और ग़रीबी का सबसे अधिक अपने लेखन के लिए कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करती हैं। दरअसल जिसे आप ‘नरक मसीहा’ के स्त्री-पात्रों को लेकर मुखर आलोचना कह रहे हैं वह आलोचना नहीं एक अघाई कुंठा और ईर्ष्या है। दूसरी यह कोई आलोचकीय दृष्टि और परंपरा नहीं है कि आप रचना की समग्रता में न जाकर उसकी ऐसी आलोचना करते हैं, जो आलोचना न होकर आपकी कुंठा को जाहिर करे। दुर्भाग्य से हिंदी साहित्य में ऐसी कुंठाओं का तेज़ी से प्रवेश हुआ है। उनकी पीड़ा को आप भी समझ सकते हैं।
वास्तव में अपनी मेहनत पर जीने वाली जिस स्त्री की ये बात कर रही हैं ये ऐसी ही स्त्रियाँ है जो सिविल सोसाइटी का हिस्सा बन, क्रांति की मोमबत्ती लिए आये दिन आपको जंतर मंतर, इंडिया गेट और अब बापू की समाधि पर प्राय: नज़र आ जाएँगी। सिविल सोसाइटी का हिस्सा बनना और क्रांति की मोमबत्ती हाथ में लिए जंतर मंतर, इंडिया गेट पर जाना इनके लिए पिकनिक और मौज-मस्ती से ज्यादा कुछ नहीं है। मुट्ठी भर ये क्रांतिकारी अपने आपको पूरी स्त्री-जाति की भाग्य-विधाता मानने का भ्रम पाले हुए हैं। अगर इनकी नज़र में मेहनत पर जीने वाली स्त्री यही है और अगर इन्हें इनकी आलोचना बर्दाश्त नहीं है, तो अपनी ऐसी ‘गड़बड़’ पर मुझे ख़ुशी है। विधायिका में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का मामला सदन में अगर आज तक, बकौल इस लेखिका मेहनत पर जीने वाली सिविल सोसाइटी और आए दिन जंतर मंतर या इंडिया गेट पर चिल्लाने के बावजूद, पास नहीं हो पाया है तो उसका कारण भी यही है। यानी इनका यह शोर दिन भर खेत-खलिहानों, ईंट-भट्टों पर काम करने वाली, सड़क किनारे मिट्टी ढोने वाली मेहनतकश स्त्री के हिस्से पर कब्ज़ा करने को लेकर ही है। अगर इस तथाकथित सिविल सोसाइटी और बात-बात पर मोमबत्ती लेकर सड़कों पर उतरने वाली अपनी मेहनत पर जीने वाली ‘स्त्री’ की इतनी ही चिंता है, तो क्यों नहीं इस 33 प्रतिशत महिला आरक्षण में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए अलग से आरक्षण की मांग करतीं? दरअसल, ‘नरक मसीहा’ ऐसी ही तथाकथित वर्चस्ववादी मानसिकता को उद्घाटित करता है। दूसरी बात यह कि किसी भी रचना का पाठ पाठक के विवेक और आस्वाद पर निर्भर करता है। हरेक पाठक के लिए उसका अंतर्पाठ अलग होता है।
अटल तिवारी पत्रकारिता के प्राध्यापक हैं और दिल्ली में रहते हैं
बातचीत क्रमशः




