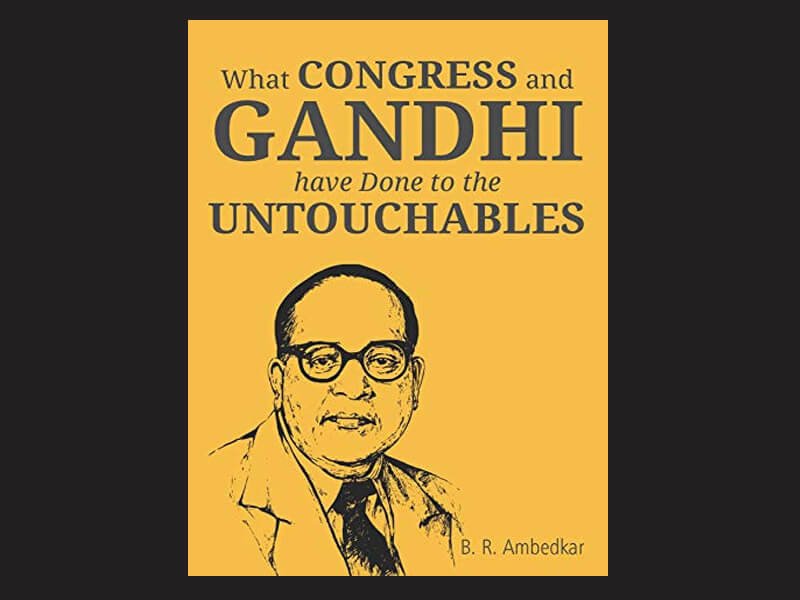दूसरा और अंतिम भाग
भारतीय सवर्ण समाज का अपने जातीय श्रेष्ठता के भावबोध से न उबर पाना उतना बुरा नहीं है जितना बुरा अपने से निम्न जाति के लोगों को आगे बढ़ने से रोकने की मानसिकता से पीड़ित होना है। बाबा साहेब इस बीमारी को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने इसके इलाज का सार्थक नुस्खा भी सुझाया था लेकिन वह यह भी जानते थे कि संकीर्ण सोच वाला भारतीय सवर्ण समाज इस रोग से छुटकारा पाना ही नहीं चाहता। यदि हम इतिहास के पन्ने कुरेदें तो यही पाएंगे कि दलितों के उत्थान में दलित के सबसे बड़े खैरख्वाह माने जाने वाले महात्मा गाँधी सबसे बड़े अवरोधक के रूप में सामने आते हैं।
अपने आमरण अनशन के हथियार से गाँधी ने जिस प्रकार कम्युनल अवार्ड की हत्या करके पूना समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिये डॉ. अम्बेडकर को बाध्य किया था उससे एक बात तो स्पष्ट हो गयी थी कि गाँधी दलितों को हिन्दुओं के चंगुल से छुटकारा दिलाने नहीं जा रहे हैं। हिन्दुओं के चंगुल में फंसे रहने का सीधा अर्थ यही है कि दलित यथास्थितिवाद के शिकार अर्थात् हिन्दुओं के जरखरीद गुलाम बने रहें । अब किसी गुलाम को पढ़ाई-लिखाई से क्या काम ! अम्बेडकर को उद्धृत करने से पहले मैं गाँधी को उद्धृत करना ज्यादा समीचीन समझता हूँ।
इसमें कोई विवाद नहीं है कि गाँधी ने दलितों के उत्थान के लिये शिक्षा समेत अनेकानेक योजनाओं की शुरुआत की थी। यदि इन सभी योजनाओं का अध्ययन किया जाये तो गाँधी को दलितों का सबसे बड़ा मसीहा कहने में देर नहीं लगेगी। लेकिन अपनी ही योजनाओं को कार्यान्वित करने में उन्होंने जो उदासीनता दिखाई और कभी परोक्ष तो कभी प्रत्यक्ष रूप से जो अड़ंगे लगाये वे हैरतअंगेज हैं। दलितोत्थान के नाम पर चलायी गयीं उनकी सारी योजनाएँ कभी भी अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर सकीं। उन्होंने कभी भी दलितों को उन स्कूलों में पढ़ने की पैरोकारी नहीं की जिनमें सवर्ण हिन्दुओं के भी बच्चे पढ़ते थे।
उन्होंने सवर्ण हिन्दुओं की इच्छाओं के आगे हमेशा घुटने टेके हैं। दलित बच्चों के लिये अलग से स्कूल खोलने और उन्हीं में उनकी पढ़ाई के पक्षधर रहे हैं। हम आज इतिहास के विरूपीकरण का बड़े जोर-शोर से रोना रोते हैं लेकिन गाँधी की छवि को चमकाने के लिये उनके बारे में लिखे गये इतिहास का जो विरूपीकरण किया गया है, उस पर कभी भी चर्चा नहीं करते। गाँधी की शिक्षा नीति का आधारभूत तत्व रामराज्य की स्थापना थी। रामराज्य में दलितों की शिक्षा पर एक तो धार्मिक निषेध है और दूसरे यदि किसी ने पढ़ने का दुस्साहस किया भी तो राम स्वयं उसकी हत्या कर देंगे।
कहना अन्यथा न होगा कि वर्तमान मोदी सरकार गाँधी के ही रास्तों का अनुसरण करते हुए रामराज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर रही है और ऐसी व्यवस्था कर रही है जो दलितों की शिक्षा के सारे रास्ते बन्द कर देगी।
वृहत प्रचार के आडम्बर पर टिकी गाँधी की दलितोत्थान की सारी योजनाएँ मात्र कागजों पर ही सिमट कर रह गयी थीं और शिक्षा कोई अपवाद नहीं है। गाँधी के मन का भेद पाने को व्यग्र पाठकों को चाहिए कि वे डॉ. अम्बेडकार की पुस्तक व्हाट कांग्रेस ऐंड गाँधी हैव डन टु द अनटचेबुल्स का अध्ययन करें। इसी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 264 से 266 पर वर्णित एक घटना का सार मैं यहाँ पर उद्धृत कर रहा हूँ ।
घटना सन् 1935 की है। गुजरात के अहमदाबाद जनपद के एक गाँव ‘कविता’ के दलितों ने वहाँ के सवर्ण हिन्दुओं से यह माँग की कि वे अपने बच्चों के साथ उसी स्कूल में उनके बच्चों को भी पढ़ने की अनुमति दें। सवर्ण हिन्दुओं ने उनकी बात तो नहीं मानी उलटे उन्हें इतना प्रताड़ित किया कि दलितों ने गाँव छोड़ने का मन बना लिया। मामला गाँधी तक पहुँचा लेकिन दलितों के पक्ष में खड़े होने के स्थान पर सवर्ण हिन्दुओं का पक्ष लिया और उन्हें गाँव छोड़ कर चले जाने की सलाह दे दी।
गाँधी का यही वास्तविक चेहरा था। दलितों की बेहतरी की बात उनके मन में दूर-दूर तक नहीं थी। गाँधी के रामराज्य की स्थापना के आध्यात्मिक पैरोकार और गाँधी समेत पूरे भारतीय सवर्ण समाज के आदर्श तुलसीदास दलितों की शिक्षा को लेकर कितने घृणित विचार रखते हैं, इसे वह बिना किसी झिझक के निम्न पंक्तियों में उजागर कर देते हैं:
अधम जाति मैं बिद्या पाएँ । भयउँ जथा अहि दूध पिआएँ ।।
ये पंक्तियाँ रामचरितमानस के उत्तरकाण्ड के दोहा सख्या 106 क की चैपाई संख्या तीन में वर्णित हैं। सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि नीच जाति के लोगों को शिक्षा देकर कौन मूर्ख उन्हें साँप बनाने का खतरा मोल लेना चाहेगा ?
यह भी पढ़ें :
: https://gaonkelog.com/myth-of-merit-an…ducation-for-all/
डॉ अंबेडकर का योगदान
गाँधी के विपरीत डॉ. अम्बेडकर सारी उम्र दलितों की बेहतरी के लिये लड़ते रहे। दलितों को जो कुछ भी मिला है वह केवल उन्हीं के अथक संघर्षों की बदौलत ही मिला है। गाँधी की यूटोपियाई सोच के बरक्स डॉ. अम्बेडकर की शिक्षा नीति उनके ‘स्वतंत्रता, समता और बंधुता’ तथा ‘शिक्षित करो, आंदोलित करो, संगठित करो’ के व्यावहारिक सिद्धान्त पर आधारित है। अम्बेडकर ने इन दोनों ही सिद्धान्तों को भारत के संविधान का हिस्सा तो बनाया ही दूसरे सिद्धान्त को साकार करने का उत्तरदायित्व दलित समाज के सक्षम व्यक्तियों के कंधे पर भी डाला।
यदि दलित समाज का सक्षम तबका वास्तव में अम्बेडकरवादी होता तो वह अपने समाज को शिक्षित करने में स्वयं आगे आता और इसके लिये समाज को सरकार का मुखापेक्षी न होना पड़ता और तब शायद सरकार भी अपने दायित्वों से विमुख होने का साहस न कर पाती क्योंकि उस स्थिति में पूरा दलित समाज एक चेन की शकल में संगठित होता और उसके पास संगठन की अपार शक्ति होती। लेकिन मुझे यह लिखते हुए लेशमात्र भी संकोच नहीं है कि इन सक्षम दलितों ने डॉ. अम्बेडकर के सपनों की निर्मम हत्या कर दी।
मैं अपने इस कथन को कुछ दृष्टान्त देकर सिद्ध करना चाहूँगा क्योंकि यह समय सरकार या गाँधी की आलोचना का समय नहीं है। गाँधी सनातनी हिन्दू विचारधारा से ओतप्रोत व्यक्ति थे तो वर्तमान सरकार हिन्दू धर्म और शास्त्रसम्मत शासन और न्याय व्यवस्था की स्थापना की ओर अग्रसर है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि वर्तमान सरकार की नीतियाँ गाँधी की ही बौद्धिक सोच का व्यावहारिक विस्तार हैं। निश्चित है कि दलितों की कहीं कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। ऐसे में यदि दलित डॉ. अम्बेडकर की ओर उन्मुख नहीं होते हैं तो उनके बौद्धिक विनाश को कोई रोक नहीं सकता। मेरे इस कथन में पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और स्त्रियों को भी शामिल किया जा सकता है क्योंकि वे भी हिन्दू धर्म के ही मारे हुए हैं।
स्वतंत्रता के बाद संविधान को अंगीकृत जरूर किया गया लेकिन इसे पूरी ईमानदारी से लागू करने की कोशिश कभी भी नहीं की गयी। लोकतंत्र की नैतिक गरिमा बनाये रखने के लिये शासन, प्रशासन, विधायिका, न्यायपालिका, संचार माध्यमों अर्थात् देश के सभी कार्य-व्यापार में सभी जाति,धर्म और समुदाय के व्यक्तियों का समुचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ताकि हर एक नागरिक के हित सुरक्षित हो सकें। लेकिन हुआ इसका उल्टा। आजादी से लेकर आज तक इन सभी स्थानों पर वही लोग काबिज रहे जो शासक समूह से आते हैं।
इसलिये आजादी के बाद का उत्साह बहुत दिनों तक टिक नहीं पाया और नीति निर्माण की प्रक्रिया में धीरे-धीरे वे सभी लोग उपेक्षित होते गये जो शासित समूह से आते थे तथा जिन्हें संविधान ने आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया था। इसके लिये निजीकरण सबसे आसान तरीका था और इसी को आजमाया भी गया। सरकार अपने मूलभूत कल्याणकारी सामाजिक दायित्वों से विमुख होकर पूँजीपतियों की गोद में बैठ गई। शिक्षा का भी यही हश्र हुआ।
व्यवसायीकरण और निजीकरण
किसी भी समुदाय अथवा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास और अपने अधिकारों के प्रति सजग होने के लिये शिक्षा अनिवार्य शर्त है। बाबा साहब इस बुनियादी जरूरत से भलीभांति भिज्ञ थे इसलिए इसकी जिम्मेदारी उन्होंने समाज पर डाली थी क्योंकि अपने अनुभव के आधार पर उन्हें पता था कि आजादी के बाद देश की बागडोर इन्हीं शासक समूह के हाथों में रहेगी और ऐसी सरकार दलितों को गुलाम ही बना कर रखने के लिये सौ-सौ उपाय करेगी। और वही हुआ भी। सरकार चुपचाप अपना काम करती रही और दलित समाज केवल अम्बेडकर की माला जपता रहा। अम्बेडकर की बौद्धिक सम्पदा तो बिखरती ही रही और अब समाज भी गर्त के कगार पर पहुँचने वाला है।
शिक्षा के व्यावसायीकरण के मुद्दे को केन्द्र में रखकर द्विमासिक पत्रिका कॉम्बैट लॉ हिंदी ने अपने फरवरी-मार्च 2006 में काफी सूचनापरक सामग्री प्रकाशित की है। इसी पत्रिका के आधार पर मैं कुछ चीजें इस लेख के पाठकों को आगाह करने के उद्देश्य से उनके साथ शेयर कर रहा हूँ।
सर्वोच्च न्यायलय ने अपने एक निर्णय के द्वारा गैर-सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों को इस आधार पर आरक्षण व्यवस्था से मुक्त कर दिया था कि जहाँ सरकारी धन न लगा हो वहाँ राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इस आदेश को केन्द्र सरकार ने 104वें संविधान संशोधन के द्वारा निष्प्रभावी कर दिया था। सभी दलों के समर्थन के कारण यह संशोधन विधेयक दोनों सदनों में भारी बहुमत से पास हो गया था। यद्यपि इस समर्थन के पीछे सभी दलों के अपने राजनैतिक हित थे फिर भी इस संशोधन से दलित बच्चों के लिये ऐसे शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के दरवाजे तो खुल ही गये थे। लेकिन हुआ क्या ?
इसके उत्तर में उल्लिखित पत्रिका में शिक्षा का निजीकरण: विश्व बाजार का एजेंडा शीर्षक से प्रकाशित अनिल सद्गोपाल के लेख का यह अंश उद्धृत किया जा रहा है-‘‘समूची संसदीय बहस और उसके बाद मीडिया की टिप्पणियों – चाहे समर्थन में हों या विरोध में – में यह चिंता सिरे से गायब थी कि अधिकांश अनुसूचित जाति/जनजाति के लोग कभी आरक्षण पाने के योग्य रहे ही नहीं। वजह यह है कि आधे से अधिक दलित और आदिवासी बच्चे बुनियादी शिक्षा ( आठवीं कक्षा तक ) से भी वंचित हैं और अनुसूचित जाति-जनजाति की 80-90 प्रतिशत लड़कियाँ कक्षा दस तक नहीं पहुँच पातीं । ( यही स्थिति मुसलमान बच्चों के बारे में भी कही जा सकती है )। मगर यह शर्मनाक स्थिति किसी भी पार्टी के लिये संसद में कोई काम रोको प्रस्ताव लाने या वॉकआउट करने या फिर कोई राजनैतिक आन्दोलन का विषय नहीं बन सकी। उन पार्टियों के लिये भी नहीं, जो इन्हीं के नाम पर वोट पाती हैं। किसी राजनैतिक दल ने इस दलील को आगे नहीं बढ़ाया कि आरक्षण के लाभ मुट्ठी भर सुविधा सम्पन्न अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के लोगों तक ही सीमित हैं क्योंकि कम से कम उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पाये बिना ये लाभ नहीं प्राप्त किये जा सकते।’’ ( पृष्ठ 6 ) इसके आगे मैं यह जोड़ना चाहता हूँ कि यदि डॉ. अम्बेडकर की इच्छा के अनुरूप इन बच्चों की बुनियादी शिक्षा की व्यवस्था की जिम्मेदारी समाज उठा लेता तो इस संशोधन का लाभ लेने के लिये बच्चों की कमी न होती।
सर्वोच्च न्यायालय का वह फैसला जिसे केन्द्र सरकार 104वें संविधान संशोधन से निष्प्रभावी करने का नाटक किया था, इस देश के न्यायालयों के सामाजिक सरोकारों के प्रति बढ़ती हुई उदासीनता का भी द्योतक है। सर्वोच्च न्यायालय के ही जस्टिस उन्नीकृष्णन ने 1993 में संविधान के अनुच्छेद 45 ( भाग 4 ) को अनुच्छेद 21 ( भाग 3 ) के साथ पढ़ने की आवश्यकता पर जोर देते हुए यह फैसला सुनाया था कि चूँकि शिक्षा के बिना जीने का अधिकार बेमानी है इसलिए शिक्षा हमेशा ही बुनियादी अधिकार है। ( पृष्ठ 6 ) निश्चित रूप से बाद वाले फैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ही निर्णय का गला घोंट कर स्वयं को बाजारोन्मुखी निजीकरण की व्यवस्था का पोषक ही सिद्ध किया है। जब न्यायालय ही साधनहीनों के विरोध में फैसले सुनाने लगेंगे तो इन लोगों के सामने मौत को गले लगाने के सिवा और कोई चारा नहीं रह जायेगा । और अब तो ऐसी सरकार सत्तारूढ़ हो गयी है जिसके अंदर इन विपन्न लोगों के लिये कोई स्थान ही नहीं है और न्यायालय पूरी तरह मनमानी पर उतर आये हैं । इस सम्बन्ध में पत्रिका के सम्पादकीय का यह अंश देखा जा सकता है-‘‘विदेशी ताकतों के घुसपैठ के सन्दर्भ में निर्णय लेते समय सरकार हो या न्यायालय एक साथ स्वागत में खड़े हो जाते हैं । सर्वोच्च न्यायालय ने हाल के दिनों में कई ऐसे फैसले दिये हैं जो बेरहमी से निजीकरण के पक्ष में जाते हैं।’’
आजादी के बाद सरकार ने जिस सार्वजानिक शिक्षा प्रणाली को अपनाया था और मेरे समेत अनेक पीढियाँ जिस प्रणाली की उपज हैं, उसे सरकार ने स्वयं तहस-नहस कर दिया है । यह बिल्कुल उसी तरह है जैसे कोई माँ अपने होनहार बच्चे की हत्या मात्र इसलिए कर दे क्योंकि उसे किसी धनाढ्य व्यक्ति से इश्क हो गया है। भारत की सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था की प्रशंसा विश्व के अनेक देशों द्वारा की गयी थी। इसी व्यवस्था ने देश को अनेक विभूतियों से नवाजा था। लेकिन इसे पूँजीपतियों की धनलिप्सा कहें अथवा सरकार की कोई गर्हित योजना, जिसने इस समाज-विध्वंसक और देश-विनाशक पैचाशिक सोच को जन्म दिया।
शिक्षा व्यवस्था की दयनीय स्थिति पर दिल दहलाने वाली जो टिप्पणी की गयी है इस सम्पादकीय में वह इस प्रकार है-‘‘यह शिक्षा पर हमला नहीं, देश की रीढ़ पर हमला है। आज भी विकासशील देश के दस करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं और लगभग अट्ठासी करोड़ लोग निरक्षर हैं जिन्हें शिक्षित करने में अनुमानतः दस बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च आने का अनुमान है। अमेरिका कहता है यह खर्च तो अमेरिकियों द्वारा प्रत्येक वर्ष आइस्क्रीम खाने पर आने वाले खर्च का आधा है, वह 2015 तक सभी को शिक्षित कर देगा। सरकार इस दंभ से अभिभूत नजर आती है। सवाल है कि इस दंभ पर शर्मनाक तरीके से अभिभूत हो जाने से क्या शिक्षा के शत-प्रतिशत आँकड़े को छुआ जा सकता है ? सरकार को यह भी जानना चाहिए कि खुद अमेरिका में एक करोड़ दस लाख लोग अंग्रेजी पढ़ना-लिखना नहीं जानते। एक सर्वे के अनुसार 1992 से 2003 के बीच यानी कि हाल के दिनों में अमेरिका में अशिक्षा का माहौल इतना भयानक रूप ले चुका है कि हर तीसवें अमेरिकी के लिये छोटी-मोटी जानकारी भी पढ़ना मुश्किल हो गया है । हिसाब भी बस उतना ही जानते हैं कि टैक्स फॉर्म पर अंकों को किसी तरह जोड़ घटा भर कर सकते हैं ।’’ और आज 2018 में जब मैं इस लेख को लिख रहा हूँ आँकड़े बद से बदतर ही हुए होंगे। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए।
सरकारी स्कूली व्यवस्था को चौपट करने के पीछे सरकार की क्या मंशा है इसका खुलासा उक्त शीर्षक लेख में इन शब्दों में किया गया है – ‘‘..1991 में नई आर्थिक नीति की घोषणा के समय से शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत खर्च घटना शुरू हो गया और यही प्रवृत्ति लगभग 1990 के दशक में जारी रही, जबकि प्राथमिक शिक्षा में बाहरी मदद पर निर्भरता बढ़ती गयी है । इसी दौरान विश्व बैंक प्रायोजित परियोजनाओं और योजनाओं ( डीपीईपी ) ने गरीबों के लिये कई तरह की समांतर शिक्षा सुविधाओं को आगे बढ़ाया। मसलन, वैकल्पिक स्कूल, शिक्षा गारंटी केन्द्र और शिक्षा केन्द्र। 1986 की नीति में हर प्राथमिक विद्यालय में तीन अध्यापक मुहैया कराने के वादे को बदलकर विविध स्तरीय अध्यापन व्यवस्था की गयी और वह भी कमतर, अप्रशिक्षित और कम वेतन वाले अल्पकालिक स्तर पर नियुक्त ‘पैरा अध्यापकों’ के साथ । सरकारी व्यवस्था में शिक्षा की गुणवत्ता में लगातार गिरावट से इन स्कूलों से गरीब बच्चे भी हटा लिये गये और ग्रामीण इलाकों तथा शहरी-झुग्गी बस्तियों में फीस लेकर घटिया स्तर की शिक्षा देने वाले निजी स्कूलों की संख्या में भारी इजाफा हुआ। संरचनात्मक समायोजन की वजह से आयी नीतियों में इन गिरावटों को अब बहुप्रचारित सर्वशिक्षा अभियान ( एसएसए ) के सुन्दर नाम से ढँक दिया गया है। यूनेस्को की विश्व निगरानी रपट ( ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट ) के मुताबिक अविचारित सर्वशिक्षा अभियान 2015 तक भी अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर सकता। सर्वशिक्षा अभियान के धराशायी होने से घटिया स्तर की निजी शिक्षा की ‘दुकानों’ की और बाढ़ आ जायेगी। यह भारत में स्कूली शिक्षा को बिक्री की वस्तु बनाने के नव उदारवादी एजेण्डे की एक हल्की झलक भर है जबकि भारत नई आर्थिक नीतियों के पहले तक अपने विशाल और शक्तिशाली सरकारी स्कूली व्यवस्था के लिये जाना जाता रहा है।
सरकारी स्कूलों की भौतिक संपदाएँ हड़पने के षड्यंत्र
सरकारी स्कूलों का बन्द होना और उनकी कीमती जायदाद की बिक्री, खासकर शहरी इलाकों में, अब देशव्यापी मामला बन गया है। यह सरकारी स्कूली व्यवस्था को अपनी मौत मर जाने देने और निजी स्कूलों को प्रश्रय देने की सुविचारित, सोची-समझी नीति का ही परिणाम है । असल में, ताकतवर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं और कर्ज देने वाली एजेंसियों की अगुआई में विश्व बाजार की ताकतें ठीक इसी दिशा में ले जाने को सक्रिय हैं।
राज्य एक तरफ अपने संवैधानिक दायित्वों से मुँह मोड़ता जा रहा है और साथ ही साथ एक ऊर्ध्वगामी अल्पसंख्यक जमात के लाभ के लिये स्कूली शिक्षा के निजीकरण और व्यावसायीकरण को भी प्रश्रय दे रहा है। इसके लिये वह धनी और उच्च मध्य वर्ग के लाभ के लिये तथाकथित निजी गैर-सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को सब्सिडी भी निम्न तरीकों से मुहैय्या करा रहा है- ( क ) शहरी इलाकों में बेहद रियायती दर पर मौके की जमीन उपलब्ध कराना, ( ख ) उनकी आमदनी के साथ-साथ उनके ट्रस्ट, सोसाइटी को मिले दान को आयकर कानून के तहत छूट मुहैया कराना, ( ग ) मुफ्त में पेशेवर प्रशिक्षित अध्यापकों को मुहैया कराना, जो सरकारी रियायती अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों से डिप्लोमा, डिग्री पा चुके हैं, और ( घ ) सरकार समर्थित सीबीएसई या राज्य शिक्षा बोर्डों से उनके संस्थानों और परीक्षाओं को मान्यता दिलाना। मानव संसाधन मंत्रालय की पिछले साल एक रिपोर्ट में ये आँकड़े जुटाए गए हैं कि कैसे निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल पैसा बना रहे हैं, रकम का दुरुपयोग कर रहे हैं और कर देने से बच रहे हैं, इस तरह सरकारी खजाने को भारी चपत लगा रहे हैं। विडम्बना देखिये कि शिक्षा के अधिकार विधेयक, 2005 के मसौदे में प्रस्ताव है कि ऐसे ‘गैर-सहायताप्राप्त’ स्कूलों को किसी न किसी बहाने सरकारी अनुदान मुहैया कराया जाये और उन्हें गैर-सहायताप्राप्त श्रेणी में ही गिना जाये। लेकिन मसौदे में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि राज्य सरकार इन संस्थानों की निगरानी करें।
ऐसी सरकारी रियायत पाये निजी स्कूलों से यह उम्मीद नहीं की गयी है कि वे देश की भावी पीढ़ियों को समान शिक्ष मुफ्त देने के संवैधानिक दायित्व का निर्वाह करें। ऐसे कुछेक निजी स्कूलों द्वारा मुट्ठी भर वंचित समुदाय के बच्चों को सहूलियत देने के हाल के रुझान से नीतियों के मामले में कोई फेरबदल नहीं मानं लेना चाहिए। इसके विपरीत, राज्य बाहरी मदद में इजाफा हुए बिना अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने में संसाधनों की कमी का रोना रोता है। वह यह भूल जाता है कि भारत की शिक्षा नीति और उसका एजेंडा पहले ही भूमंडलीकरण से दब गया है।’’ ( पृष्ठ 6-7 )
सरकारी शिक्षा व्यवस्था को हतोत्साहित करके सरकार ने जिस भी शिक्षा व्यवस्था को लागू किया उन सब से सरकारी शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता और पब्लिक में इसकी विश्वसनीयता का क्षरण तो हुआ ही भेदभाव की युगों पुरानी मानसिकता भी नये स्वरूप में आकार ग्रहण करने लगी। वह चाहे विश्व बैंक पोषित जनपदीय प्राइमरी शिक्षा कार्यक्रम ( 1993-2002 ) हो, चाहे सर्व शिक्षा अभियान ( 2000-2010 ) हो, चाहे शिक्षा का अधिकार अधिनियम ही क्यों न हो। अनिल सद्गोपाल ने अपने एक लेख के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निजी स्कूली शिक्षा व्यवस्था के पक्ष में दिये गये निर्णय में तमाम खामियों को इंगित किया है। ये खामियाँ जिनकी ओर न तो सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं संज्ञान लिया और न ही किसी अन्य के द्वारा न्यायालय को बताने का प्रयास किया गया, वास्तव में बहुत ही गम्भीर हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम से मात्र मुट्ठी भर बच्चे ही समावेशी शिक्षा व्यवस्था के नाम पर लाभान्वित होंगे जबकि एक बड़ी संख्या में बच्चे शिक्षित होने से वंचित रह जायेंगे। इन खामियों को निम्नवत् उद्धृत किया जा रहा है;
- यह सरलीकृत व्यवस्था संविधान की उद्देशिका के सामाजिक,आर्थिक और राजनैतिक न्याय और अवसर की समानता प्रदान किये जाने के सरकारी दायित्व का खुला उल्लंघन है।
- इससे संविधान के अनुच्छेद 14 जो कानून के सामने सब को बराबर होने का अधिकार देता है, अनुच्छेद 15 जो सरकार को निर्देशित करता है कि वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी, अनुच्छेद 16 जो सार्वजानिक सेवायोजन में समान अवसर की गारंटी देता है और अनुच्छेद 21 जो सब को गरिमामय जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता हैं, का उल्लंघन होता है।
- शिक्षा का अधिकार अधिनयम यह प्रावधान करता है कि निजी स्कूल सरकारी स्कूलों की तुलना में न केवल वर्तमान में बेहतर गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं बल्कि भविष्य में भी इसे बनाये रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने आँख मूँदकर इसे क्यों स्वीकार कर लिया जबकि वास्तविकता यह है कि वार्षिक परीक्षा परिणामों में निजी स्कूल हमेशा तीसरे स्थान पर रहते हैं और प्रथम तथा द्वितीय स्थान पर या तो केन्द्रीय विद्यालय रहते हैं या नवोदय विद्यालय। इसलिए निजी स्कूलों के पक्ष में निर्णय देने की बजाय सरकार से यह पूछा जाना चाहिए था कि वह निजी स्कूलों की तुलना में सरकारी स्कूलों में बेहतर गुणवत्ता की शिक्षा देने की व्यवस्था क्यों नहीं कर सकती ?
- सरकार हमेशा संसाधनों की कमी का रोना रोकर अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने से पल्ला झाड़ लेती है। इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिये सरकार से तार्किक उत्तर माँगा जाना चाहिए था।
- सरकार से यह भी पूछा जाना चाहिए था कि इस अधिनियम के द्वारा कुल बच्चों के कितने प्रतिशत बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करायी जा सकती है ( और शेष बचे बच्चों को शिक्षित करने के लिये सरकार के पास कौन सी योजना अथवा परियोजना है ) ?
- सरकार से यह भी पूछा जाना चाहिए था कि व्यय प्रतिपूर्ति के नाम पर सरकारी कोष से जो हजारों करोड़ रुपये निजी स्कूलों को दिये गये उनका इस्तेमाल सरकारी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिये क्यों नहीं किया जा सकता ? आखिरकार सरकारी कोष में जमा धन तो पब्लिक का ही होता है।
- सरकार से यह स्पष्ट कराना चाहिए था कि वह भेदभाव की जनक बहुस्तरीय शिक्षा व्यवस्था को क्यों बनाये रखना चाहती है ? यहाँ यह भी सवाल पैदा होता है कि देश की शिक्षा व्यवस्था में किसे शामिल करना है और किसे बाहर रखना है, इसे तय करने के लिये क्या सरकार अन्तिम रूप से अधिकृत है ?
भविष्य को अंधकार में ढकेलकर झूठे आश्वासन देना पतन के गर्त में ढकेलना है
इन सवालों से गुजरते हुए मेरे मस्तिष्क में जो विचार पैदा होते हैं वे यही हैं कि सरकार मात्र पूँजीपतियों को खुश करने के लिये औने-पौने दामों में उन्हें सरकारी सम्पत्तियाँ बेचकर अपने संवैधानिक दायित्वों से मुक्त हो रही है और एक सुनियोजित षड्यन्त्र के द्वारा भारतीय सामाजिक वर्ण व्यवस्था को पुनः जीवित करने की ओर अग्रसर है। उसे इस बात की कतई चिंता नहीं नही है कि उसके इस कृत्य से देश अशिक्षा, भूख, बेरोजगारी के भयंकर अँधेरे गर्त में डूब जायेगा। अशिक्षित और अज्ञानी जनता को खुश करने के लिये जातियों, धर्मों और सम्प्रदायों के बीच लगातार दंगों का प्रयोजन कराके सरकार अपने विरुद्ध होने वाले किसी भी विद्रोह को रोकने में सफल भी हो रही है। कहते हैं कि क्रांतियाँ भूखे पेट से पैदा होती हैं लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में यह कहावत कभी चरितार्थ हुई हो, मुझे नहीं पता।
लेख के अन्त में मैं ‘क्रेडिट सुइसे’ की रिपोर्ट के हवाले से यह बताना चाहूँगा कि सन् 2015 में भारत की टॉप की दस प्रतिशत आबादी के पास 81ः धन है जबकि नीचे की पचास प्रतिशत आबादी मात्र 4.1ः धन पर ही गुजर-बसर करने पर विवश है। सन् 2018 में यह स्थिति और भी भयावह हुई है। यह निश्चित है कि नीचे की पचास प्रतिशत आबादी में दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय के ही लोग आते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक तरफ दिनोंदिन महँगी होती हुई शिक्षा व्यवस्था, साल दर साल बजट में घटती हुई धनराशि का प्रावधान है और दूसरी तरफ दो जून की रोटी के लिये तरसता हुआ दलित, आदिवासी, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज। मुझे नहीं सूझ रहा है कि इतनी विकट और विषम परिस्थितियों, जिन्हें सरकार और भी दुरूह बनाती जा रही है, के होते हुए यह समाज किस प्रकार शिक्षित होकर अपने पैरों पर खड़ा हो पायेगा ? समान शिक्षा की कौन कहे, इनके लिये तो शिक्षा पाना ही सपना है!
मूलचन्द सोनकर हिन्दी के महत्वपूर्ण दलित कवि-गजलकार और आलोचक थे । विभिन्न विधाओं में उनकी तेरह प्रकाशित पुस्तकें हैं 19 मार्च 2019 को उन्होंने इस संसार को अलविदा कहा ।