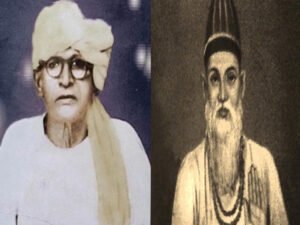कल एक गुजरात निवासी सज्जन मिलने आये। यह उनसे मेरी पहली मुलाकात थी। गुजरात को लेकर शुरू हुई बातचीत शब्दों के विभिन्न आयामों तक पहुंची। उनका कहना था कि कोई भी शब्द केवल वर्णों का मेल मात्र है। उसका अर्थ समाज तय करता है। जाहिर तौर पर उनका यह कहना गलत नहीं है। वैसे भी वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। आप चाहें तो सार्थक शब्द के बदले कुछ और भी कह सकते हैं। जैसे यह कि वर्णों का वह मेल, जिससे कोई मतलब निकलता हो, शब्द कहलाता है। तो कुल मिलाकर यह कि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिन्हें ब्राह्मणों द्वारा ईजाद किया गया है और गुजरात निवासी सज्जन का प्रस्ताव रहा कि हमें ऐसे शब्दों का उपयोग करना छोड़ देना चाहिए।
जाहिर तौर पर यह कठिन काम है। वजह यह कि जो शब्द चलन में आ चुके हैं, अब उनके बदले एकदम से नया शब्द लाना तभी मुमकिन हो सकता है, जब इसके लिए सामूहिक प्रयास हों। यदि ऐसा नहीं होगा तो यह बेहद मुश्किल काम है। लेकिन यह काम बड़ा दिलचस्प होगा। मैं तो इसकी कल्पना मात्र से रोमांचित हो रहा हूं कि हमारे पास ऐसे शब्द भंडार हों, जो हमारे अपने हों।
[bs-quote quote=”यह साहित्य बुद्ध का साहित्य भी नहीं है। आजीवक बुद्ध से पहले हुए और मक्खलि गोसाल सहित जिन पांच आजीवकों काे हम मानते हैं कि उन्होंने ब्राह्मणों के साहित्य-दर्शन को सबसे पहले चुनौती दी, वे सब ओबीसी जातियों के लोग थे। कोई नाई थे तो कोई यादव। वे सब श्रमण परंपरा के लोग थे।” style=”style-2″ align=”center” color=”” author_name=”” author_job=”” author_avatar=”” author_link=””][/bs-quote]
हमारे शब्दों से मेरा आशय वे शब्द हैं, जिनका इस्तेमाल हमारे लोग करते रहे हैं। दिलचस्प यह कि इन शब्दों का सरल विकल्प अन्य भाषाओं में नहीं। अब एक उदाहरण देखिए। आज मैं देर से जगा। सामान्यत: मैं छह से सात घंटे की नींद पूरी करता ही हूं। लेकिन आज मैंने इसे बढ़ाकर साढ़े आठ घंटे कर दिया। आंख भी तब खुली जब बगल में रहनेवाले एक मासूम की मासूम आवाज सुनायी दी। थोड़ी ही देर बाद घर से परिजनों का वीडियो कॉल आया तो मोबाइल में अपना चेहरा दिखा। अब हुआ यह कि मेरी पत्नी ने कहा कि चेहरा “भकुआएल” क्यों है।
अब यह “भकुआएल” शब्द कितना खास है। अब हिंदी में इसके विकल्प के बारे में सोचें तो हम यह कह सकते हैं कि उदास चेहरा, खींचा-खींचा सा चेहरा, भर्राया हुआ चेहरा आदि कह सकते हैं। लेकिन “भकुआएल” शब्द का अपना ही सौंदर्य है। यही खासियत है हमारे शब्दों की और इसी तरह की खासियत है हमारे साहित्य की।
जब हम साहित्य की बात करते हैं तो इसका सौंदर्य शास्त्र भी गजब का होता है। मसलन, ब्राह्मणों के हिंदी साहित्य का सौंदर्य बिल्कुल अलग है, दलितों-आदिवासियों-ओबसी के साहित्य से। अब तो महिलाओं के साहित्य को भी पृथक साहित्य के रूप में मान्यता दी जा चुकी है। लेकिन नारी साहित्य में भी उसी तरह का भेद है जिस तरह का भेद समाज में है। मसलन कुलीन घरों की महिलाओं का साहित्य अलग और जो कुलीन नहीं हैं, उनका साहित्य अलग।
[bs-quote quote=”ओबीसी साहित्य के मूल में ही सवाल उठाना है। आजीवकों की बात छोड़ते हैं। भारत के आजाद होने के पहले और उसके बाद की बात करते हैं। गुलामगिरी के रचनाकार जोतीराव फुले को याद करते हैं। उनके बाद के भिखारी ठाकुर ओबीसी साहित्यकार-कलाकार थे। वे नाई जाति के थे। उन्होंने जितनी रचनाएं रचीं, फिर चाहे वह ‘गबरघिचोर’ हो, ‘बेटीबेचवा’ हो या फिर ‘बिदेसिया’ हो, सवाल ही तो खड़ा करते हैं। हर बार वह उनलोगों से पूछते हैं जो खुद को शासक वर्ग का मानते हैं कि यदि तुम अपनी बेटी बेचते हो, तो तुम्हारी श्रेष्ठता कैसी है और कहां है?” style=”style-2″ align=”center” color=”” author_name=”” author_job=”” author_avatar=”” author_link=””][/bs-quote]
खैर, आज मैं ओबीसी साहित्य के बारे में ही सोच रहा हूं। एक साहब हैं जो खुद को ओबीसी साहित्य का बाप बताते हैं। वे कहीं प्रोफेसर भी हुआ करते हैं और दर्जन भर से अधिक किताबें उनके नाम से हैं। लेकिन जब वे खुद को ओबीसी साहित्य का बाप कहते व कहलवाते हैं तो वे यह भूल जाते हैं कि यह साहित्य आजीवकों का लोकायतिक साहित्य है। यह साहित्य बुद्ध का साहित्य भी नहीं है। आजीवक बुद्ध से पहले हुए और मक्खलि गोसाल सहित जिन पांच आजीवकों काे हम मानते हैं कि उन्होंने ब्राह्मणों के साहित्य-दर्शन को सबसे पहले चुनौती दी, वे सब ओबीसी जातियों के लोग थे। कोई नाई थे तो कोई यादव। वे सब श्रमण परंपरा के लोग थे। वे बुद्ध और महावीर की तरह राजकुमार नहीं थे।
मैं बुद्ध और महावीर पर यह आरोप नहीं लगा रहा कि इन दोनों ने आजीवकों के विचारों काे हाईजैक किया और उसपर अपनी मोहर लगा दी। लेकिन सवाल तो उठने ही चाहिए। ओबीसी साहित्य के मूल में ही सवाल उठाना है। आजीवकों की बात छोड़ते हैं। भारत के आजाद होने के पहले और उसके बाद की बात करते हैं। गुलामगिरी के रचनाकार जोतीराव फुले को याद करते हैं। उनके बाद के भिखारी ठाकुर ओबीसी साहित्यकार-कलाकार थे। वे नाई जाति के थे। उन्होंने जितनी रचनाएं रचीं, फिर चाहे वह ‘गबरघिचोर’ हो, ‘बेटीबेचवा’ हो या फिर ‘बिदेसिया’ हो, सवाल ही तो खड़ा करते हैं। हर बार वह उनलोगों से पूछते हैं जो खुद को शासक वर्ग का मानते हैं कि यदि तुम अपनी बेटी बेचते हो, तो तुम्हारी श्रेष्ठता कैसी है और कहां है? वह गबरघिचोर में एक महिला के हवाले से यह सवाल खड़ा करते हैं कि जब बच्चे को गर्भ में पालने से लेकर उसे जन्म देते समय मृत्यु तक को पराजित करने की जिम्मेदारी महिला की है तो यह तय करने का अधिकार पुरुषों को किसने दिया कि बच्चा किसका है?
[bs-quote quote=”आज मैं देर से जगा। सामान्यत: मैं छह से सात घंटे की नींद पूरी करता ही हूं। लेकिन आज मैंने इसे बढ़ाकर साढ़े आठ घंटे कर दिया। आंख भी तब खुली जब बगल में रहनेवाले एक मासूम की मासूम आवाज सुनायी दी। थोड़ी ही देर बाद घर से परिजनों का वीडियो कॉल आया तो मोबाइल में अपना चेहरा दिखा। अब हुआ यह कि मेरी पत्नी ने कहा कि चेहरा “भकुआएल” क्यों है।” style=”style-2″ align=”center” color=”” author_name=”” author_job=”” author_avatar=”” author_link=””][/bs-quote]
ओबीसी साहित्यकारों की यही खासियत रही है। वे डंके की चोट पर अपनी बात कहते हैं। वे दलित साहित्यकाराें के जैसे आत्मकथाओं के माध्यम से अपनी पीड़ा का बखान नहीं करते। हालांकि पीड़ा का भी अपना सौंदर्य शास्त्र औ प्रभाव होता है। जैसे कि ओमप्रकाश वाल्मीकि का ‘जूठन’ बेहद उम्दा साहित्य है क्योंकि इसमें वह सवाल पूछते हैं। वह केवल अपने साथ हुए जातिगत भेदभाव का बखान एक पीड़ित के रूप में नहीं करते। खैर कुछ और लोगों ने भी अपनी आत्मकथाओं का सृजन किया है, जिनके बारे में मेरी एकदम दूसरी है।
ओबीसी साहित्यकारों ने आत्मकथाएं नहीं लिखीं। मसलन, फणीश्वरनाथ रेणु ने नहीं लिखी। उन्होंने साहित्य रचा और सवाल पूछा। राजेंद्र यादव ने भी साहित्य रचा और सत्ता के मठाधीशों की आंखों में आंख डालकर सवाल पूछा।
बहरहाल, मौजूदा दौर में ओबीसी साहित्य गर्त में है। वजह यह कि यह समाज ही चेतनशील नहीं रह गया है। इसकी चेतना को राजनीति ने कुंद कर दिया है। एक उदाहरण मेरे ससुर राजभवन सिंह हैं। इन्होंने भी साहित्य रचा है। लेकिन इन्होंने जो रचा है, वह ब्राह्मणों का साहित्य है। मतलब यह कि उन्होंने हिंदू धर्म के मिथकों के आधार पर खंड काव्य लिखा है। मेरा मानना है कि यदि आप वही लिखेंगे जो कि ब्राह्मण लिखते रहे हैं तो आपको ओबीसी साहित्यकार नहीं माना जाएगा और ब्राह्मण साहित्यकार का तमगा आपको वैसे भी ब्राह्मण नहीं देने जा रहे।
सनद रहे कि ओबीसी साहित्य का अपना महत्व है। इसमें सामूहिकता है। यह साहित्य दलितों को नहीं अलगाता, आदिवासियों को नहीं अलगाता, महिलाओं को नहीं अलगाता। लेकिन चूंकि आज के ओबीसी बुद्धिजीवियों में ब्राह्मण बनने का होड़ है तो उनके अंदर खामियां भी बढ़ी हैं। नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक सीमित सूची है ऐसे स्वनामधन्य ओबीसी लेखकों की।
खैर, कल एक सवर्ण साथी डेमोक्रेसी की बुराइयों का जिक्र कर रहे थे। वैसे वह स्वयं को वामपंथी भी मानते रहते हैं। उनसे हुई बातचीत का असर मेरी जेहन पर पड़ा। एक कविता सूझी–
मैं यह मान लेता हूं कि
डेमोक्रेसी में अनेक खामियां हैं
और यह कि
सारे डेमोक्रेटिक असल में
डेमोक्रेटिक नहीं होते।
बाजदफा वह
नवउदारवाद का ढोल
गले में लटकाकर बजाते हैं
और संसद में
पूंजीवाद के विरोध का ढोंग करते हैं।
लेकिन मैं यह नहीं मान सकता कि
डेमोक्रेसी का विकल्प राजतंत्र है
या फिर यह कि
कोई तानाशाह करे हुकूमत
और देश में आग लगा दे।
हां, डेमोक्रेसी हर हाल में जरूरी है ताकि
फिर से कोई ब्रह्मा
औरतों के बदले
बच्चे ना पैदा करने लगे
और कोई राम
किसी शंबूक की तरफ
आंख उठाने से पहले
पैंट में पेशाब कर दे।
![]()
नवल किशोर कुमार फ़ॉरवर्ड प्रेस में संपादक हैं।