महाराष्ट्र में पंचायती राज अधिनियम के तहत स्थानीय निकायों के चुनाव होने हैं। इसकी अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है। लेकिन इसके क्रियान्वयन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी थी। कल सुप्रीम कोर्ट ने इस रोक को हटा लिया है और राज्य सरकार को चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है।
दरअसल, यह मामला सुप्रीम कोर्ट इस कारण पहुंचा क्योंकि महराष्ट्र सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में 27 फीसदी सीटें ओबीसी को देने का फैसला किया था और वहां के ऊंची जातियों के लोगों को यह पसंद नहीं था। इसलिए पहले यह मामला बंबई हाई कोर्ट पहुंचा और बाद में दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में।
कल सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की खंडपीठ ने अपने फैसले में महाराष्ट्र सरकार के फैसले को रद्द करते हुए ओबीसी के लिए आरक्षित व अधिसूचित 27 प्रतिशत सीटों को सामान्य श्रेणी के सीटों में बदलने का निर्देश दिया। इसके लिए खंडपीठ ने मुख्य रूप से दो तरह के तर्क रखे हैं।
पहला तो यही कि आरक्षण की सीमा 50 फीसदी के उपर नहीं होनी चाहिए और दूसरा यह कि महाराष्ट्र सरकार ने पंचायती व स्थानीय निकायों में ओबीसी के आरक्षण हेतु कोई विश्वसनीय आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया है।
खंडपीठ की दोनों बातें अहम हैं। इसे हम चाहें तो आसानी से यह कहते हुए खारिज कर सकते हैं कि यदि 50 फीसदी की सीमा ही अधिकतम सीमा है तो ईडब्ल्यूएस यानी गरीब सवर्णों के लिए दस फीसदी आरक्षण भी अवैध है क्योंकि इसे जोड़ देने के बाद आरक्षण 60 फीसदी हो जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को खारिज नहीं किया है।
अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों नहीं किया है, यह एक दूसरा सवाल है। सवाल यह कि क्या ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को अदालतों में चुनौती दी गयी है? इसका जवाब सकारात्मक है। लेकिन अदालतों ने इस मामले में अबतक क्या किया है, यह विचारने योग्य सवाल है।
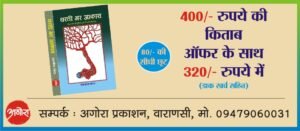
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में ही मेरी जानकारी के अनुसार 13 याचिकाकर्ताओं ने ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को चुनौती दी है और अधिकांश की चुनौती का आधार यही है कि संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। भारत सरकार ने इसमें आर्थिक पहलू को शामिल कर लिया है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह तर्क भी रखा है कि दस फीसदी आरक्षण ईडब्ल्यूएस को देने से 50 फीसदी सीमा का उल्लंघन होता है।
खैर, सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रहा है। ठीक वैसे ही जैसे यह करता रहा है।
1990 में जब मंडल कमीशन की आंशिक अनुशंसाओं को लागू किया गया तब ऊंची जाति के लोगों ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई और सात जजों की खंडपीठ ने फैसला सुनाया।
यह एक ऐतिहासिक फैसला था जिसे इंद्रा साहनी बनाम भारत सरकार मामले के नाम से जाना जाता है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर की बात कही और तत्कालीन पी वी नरसिंह राव हुकूमत ने मान भी लिया।
हालांकि तब उसके पास संसद में एक और विधेयक लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी बनाने का उपाय था लेकिन कांग्रेसी हुकूमत भला ऐसा क्यों करने लगी। कांग्रेसियों ने तो मंडल कमीशन की अनुशंसाओं को दस साल तक लटकाकर रखा था।
आज भी ओबीसी को सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्ष्ण संस्थानों में आरक्षण संसद में बने कानून के हिसाब से नहीं बल्कि केंद्रीय कार्मिक व शिकायत निवारण मंत्रालय के द्वारा जारी एक कार्यालय ज्ञापांक के आधार पर दिया जाता है, जिसे 1993 में जारी किया गया था। इसी में क्रीमी लेयर की सीमा का निधारण करने का प्रावधान है।

बहरहाल, मैं महाराष्ट्र सरकार के मामले में कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में सोच रहा हूं। सचमुच कुछ भी नहीं बदला है। फिर चाहे वह 1990 का दशक हो या 2000 का या फिर अभी का। ओबीसी के हितों को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी वही है, सरकारें भी वही हैं और बुद्धिजीवी भी वही हैं।
मुझे तो आश्चर्य होता है जब ओबीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में क्वांटिफिेडेबुल डाटा की मांग की जाती है। किसी कोर्ट ने राज्य को निर्देशित नहीं किया है कि वह जातिगत जनगणना कराए ताकि यह चक्कर ही खत्म हो। लेकिन कोर्ट को इससे कोई मतलब नहीं है। सरकार को भी कोई मतलब नहीं है। आम लोगों को भी कोई मतलब नहीं है। यदि मतलब होता तो बात निस्संदेह कुछ और होती।

नवल किशोर कुमार फॉरवर्ड प्रेस में संपादक हैं।




