रिपोर्ट बताती है कि चमक-दमक दिखाकर मुनाफा कूटने का माध्यम भर हैं निजी स्कूल और विद्यार्थी औसत ज्ञान में भी पीछे हैं
भारत में जब भी स्कूली शिक्षा के बदहाली की बात होती है तो इसका सारा ठीकरा सरकारी स्कूलों के मत्थे मढ़ दिया जाता है। इसके बरक्स प्राइवेट स्कूलों को श्रेष्ठ अंतिम विकल्प के तौर पर पेश किया जाता है। भारत में शिक्षा के संकट को सरकारी शिक्षा व्यवस्था के संकट में समेट दिया गया है और बहुत चुतराई से प्राइवेट शिक्षा व्यवस्था को बचा लिया गया है। भारत में सरकारों की मंशा और नीतियां भी ऐसी रही हैं जो सावर्जनिक शिक्षा व्यवस्था को हतोत्साहित करती हैं। लेकिन निजीकरण की लॉबी द्वारा जैसा दावा किया जाता है क्या वास्तव में प्राइवेट शिक्षा व्यवस्था उतनी बेहतर और चमकदार है ?
बदहाली के भागीदार
आम तौर पर हमें सरकारी स्कूलों के बदहाली से सम्बंधित अध्ययन रिपोर्ट और खबरें ही पढ़ने को मिलती है परन्तु इस साल जुलाई में जारी की गयी सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन की रिपोर्ट प्राइवेट स्कूल इन इंडिया में देश में प्राइवेट स्कूलों को लेकर दिलचस्प खुलासे किये गये हैं जिससे प्राइवेट स्कूलों को लेकर कई बनाये गये मिथक टूटते हैं। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि पिछले कुछ दशकों के दौरान प्राइवेट स्कूलों के दायरे में जबरदस्त उछाल आया है। आज भारत में प्राइवेट स्कूलों की संख्या और पहुंच इतनी है कि यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्कूली सिस्टम बन चुका है। स्कूली शिक्षा के निजीकरण की यह प्रक्रिया उदारीकरण के बाद बहुत तेजी से बढ़ी है। 1993 में करीब 9.2 प्रतिशत बच्चे ही निजी स्कूलों में पढ़ रहे थे जबकि आज देश के तकरीबन 50 प्रतिशत (12 करोड़) बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। जिसके चलते आज भारत में प्राइवेट स्कूलों का करीब 2 लाख करोड़ का बाजार बन चुका है।
गढ़ी गयी छवि के विपरीत प्राइवेट स्कूलों के इस फैलाव की कहानी में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी, मनमानेपन, पारदर्शिता की कमी जैसे दाग भी शामिल हैं। दरअसल भारत में निजी स्कूलों की संख्या तेजी से तो बढ़ी है लेकिन इसमें अधिकतर ‘बजट स्कूल’ हैं जिनके पास संसाधनों और गुणवत्ता की कमी है, लेकिन इसके बावजूद मध्य और निम्न मध्य वर्ग के लोग सरकारी स्कूलों के मुकाबले इन्हीं स्कूलों को चुनते हैं। सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन की रिपोर्ट बताती है कि करीब 70 प्रतिशत अभिभावक निजी स्कूल को 1,000 रुपये प्रतिमाह से कम फीस का भुगतान करते हैं, जबकि 45 प्रतिशत अभिभावक निजी स्कूलों में फीस के रूप में 500 रुपये महीने से कम भुगतान करते हैं।
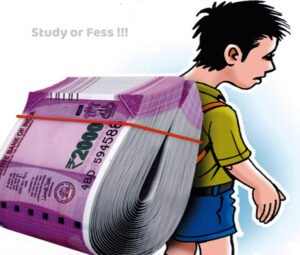
सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन की रिपोर्ट इस भ्रम को भी तोड़ती है कि प्राइवेट स्कूल गुणवत्ता वाली स्कूली शिक्षा दे रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत के ग्रामीण व छोटे शहरों में चलने वाले 60 प्रतिशत निजी स्कूलों में पांचवीं कक्षा के छात्र सामान्य प्रश्न को हल भी नहीं कर पाते हैं, जबकि पांचवीं कक्षा के 35 फीसदी छात्र दूसरी कक्षा का एक पैराग्राफ भी नहीं पढ़ पाते हैं। यह स्थिति ग्रामीण व छोटे शहरों में चलने वाले प्राइवेट स्कूलों की ही नहीं है, रिपोर्ट के अनुसार निजी स्कूलों में पढ़ने वाले सबसे संपन्न 20 फीसदी परिवारों के 8 से 11 साल के बीच के केवल 56 फीसदी बच्चे ही कक्षा 2 के स्तर का पैरा पढ़ सकते हैं।
बड़ी कक्षाओं और बोर्ड परीक्षाओं में भी प्राइवेट स्कूलों की स्थिति ख़राब है, राष्ट्रीय मूल्यांकन सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि निजी स्कूलों में दसवीं कक्षा के छात्रों का औसत स्कोर पांच में से चार विषयों में 50 प्रतिशत से कम था। कई राज्य और केंद्रीय बोर्ड परिक्षाओं में भी हम देखते हैं कि सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से बेहतर नतीजे दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर मध्य प्रदेश में इस वर्ष के दसवीं परीक्षा के जो नतीजे आये हैं उनमें प्राइवेट स्कूलों की अपेक्षा सरकारी स्कूल के छात्र आगे रहे। सरकारी स्कूलों के 63.6 प्रतिशत के मुकाबले प्राइवेट स्कूलों के 61.6 प्रतिशत परीक्षार्थी ही पास हुए हैं। यह स्थिति प्रदेश के सभी जिलों में रही है। यही हाल इस साल के बारहवीं के रिजल्ट का भी रहा है। इस वर्ष बारहवीं के एमपी बोर्ड के रिजल्ट में सरकारी स्कूलों के 71.4 प्रतिशत विद्यार्थी पास हुये जबकि प्राइवेट स्कूलों में पास होने वाले विद्यार्थियों का दर 64.9 प्रतिशत रहा है।
इन परिस्थितयों के बावजूद भारत में स्कूली शिक्षा के निजीकरण की लॉबी इस विचार को स्थापित करने में कामयाब रही है कि भारत में स्कूली शिक्षा के बदहाली के लिये अकेले सावर्जनिक शिक्षा व्यवस्था ही जिम्मेदार है और शिक्षा के निजीकरण से ही इसे ठीक किया जा सकता है । आज भी निजीकरण लॉबी की मुख्य तौर पर दो मांगें हैं । पहला स्कूल खोलने के नियम को ढीला कर दिया जाये। गौरतलब है कि हमारे देश में स्कूल खोलने का एक निर्धारित मापदंड है जिसे प्राइवेट लॉबी अपने लिये चुनौती और घाटे का सौदा मानती है । दूसरा जोकि उनका अंतिम लक्ष्य भी है, सरकारी स्कूलों के व्यवस्था को पूरी तरह से भंग करके इसे बाजार के हवाले कर दिया जाये।
[bs-quote quote=”सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन की रिपोर्ट इस भ्रम को भी तोड़ती है कि प्राइवेट स्कूल गुणवत्ता वाली स्कूली शिक्षा दे रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत के ग्रामीण व छोटे शहरों में चलने वाले 60 प्रतिशत निजी स्कूलों में पांचवीं कक्षा के छात्र सामान्य प्रश्न को हल भी नहीं कर पाते हैं, जबकि पांचवीं कक्षा के 35 फीसदी छात्र दूसरी कक्षा का एक पैराग्राफ भी नहीं पढ़ पाते हैं। यह स्थिति ग्रामीण व छोटे शहरों में चलने वाले प्राइवेट स्कूलों की ही नहीं है, रिपोर्ट के अनुसार निजी स्कूलों में पढ़ने वाले सबसे संपन्न 20 फीसदी परिवारों के 8 से 11 साल के बीच के केवल 56 फीसदी बच्चे ही कक्षा 2 के स्तर का पैरा पढ़ सकते हैं।” style=”style-2″ align=”center” color=”” author_name=”” author_job=”” author_avatar=”” author_link=””][/bs-quote]
दरअसल भारत में स्कूली शिक्षा की असली चुनौती सरकारी स्कूल नहीं बल्कि इसमें व्याप्त असमानता और व्यवसायीकरण है। आज भी हमारे अधिकतर स्कूल चाहे वे सरकारी हों या प्राइवेट, बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहे हैं जिसकी वजह से प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के बाद बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने की दर बहुत अधिक है। आजादी के बाद से ही हमारे देश में शिक्षा को वह प्राथमिकता नहीं मिल सकी जिसकी वह हकदार है। इतनी बड़ी समस्या होने के बावजूद हमारी सरकारें इसकी जवाबदेही को अपने ऊपर लेने से बचती रही हैं। एक दशक पहले शिक्षा अधिकार कानून को लागू किया गया लेकिन इसकी बनावट ही समस्या को संबोधित करने में नाकाम साबित्त हुई है।
यह भी पढ़ें :
समाज और व्यवस्था को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हर चीज मुनाफा कूटने के लिये नहीं है, जिसमें शिक्षा भी शामिल है। शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसे बुनियादी क्षेत्र हैं जिन्हें आप सौदे की वस्तु नहीं बना सकते हैं। इन्हें लाभ-हानि के गणित से दूर रखना होगा। शिक्षा में अवसर की उपलब्धता और पहुँच की समानता बुनियादी और अनिवार्य नियम है जिसे बाजारीकरण से हासिल नहीं किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार की सावर्जनिक शिक्षा व्यवस्था और जिन हालात में सरकारी स्कूल हैं वे भी इस लक्ष्य को हासिल करने में नाकाम साबित हुये हैं । इसलिये यह भी जरूरी है कि सावर्जनिक शिक्षा को मजबूती प्रदान करने के लिये इसमें समाज की जिम्मेदारी और सामुदायिक सक्रियता को बढ़ाया जाये,जिससे स्कूली शिक्षा के ऐसे मॉडल खड़े हो सकें जो शिक्षा में अवसर की समानता की बुनियाद पर तो खड़े ही हों, साथ ही शिक्षा के उद्देश्य और दायरे को भी विस्तार दे सकें। केवल तभी शिक्षा में ज्ञान और कौशल के साथ तर्क, समानता, बन्धुत्व के साथ जीवन जीने के मूल्य भी सिखाया जा सकेगा !
जावेद अनीस स्वतंत्र पत्रकार हैं और भोपाल में रहते हैं ।





[…] […]