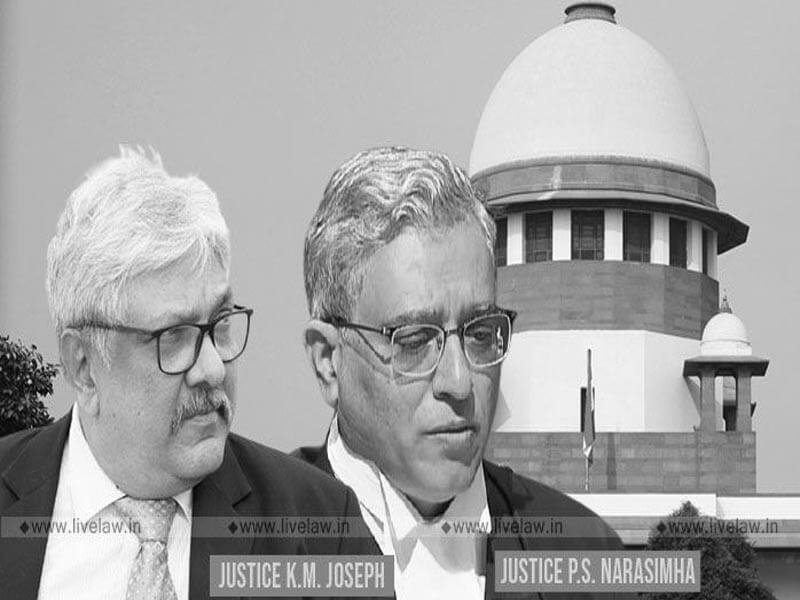जब हम किसी अर्थव्यवस्था को कृषि आधारित कहते हैं तो उसका अर्थ होता है कि व्यवस्था के अन्य अंग कृषि पर अवलंबित हैं। खेती में परिवर्तन से शेष प्रणाली में बदलाव हो जाएगा क्योंकि हर कड़ी एक-दूसरे से जुड़ी है। उस प्रणाली को ठप करना है तो किसानों से उनकी खेती छीन लेना पर्याप्त है। इस परस्परावलंबन की कड़ी में टूट के परिणाम को तुलसीदास ने कवितावली की इन पंक्तियों में दर्ज किया है-
खेती न किसान को भिखारी को न भीख बलि,
बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी |
जीविका विहीन लोग सीद्यमान सोच-बस,
कहैं एक एकन सों “कहाँ जाई का करी?” ||
(‘कवितावली’, 7/97)
किसान से खेती अपहृत कर ली जाए तो पूरी व्यवस्था भरभरा पड़ेगी। भिखारी को भीख में अन्न नहीं मिलेगा| बनिए का वाणिज्य रुक जाएगा। नौकरियाँ मिलनी बंद हो जाएंगी| मिली नौकरियाँ छूट जाएंगी। छीजते हुए जीविका विहीन लोग एक-दूसरे से पूछेंगे कि कहाँ चला जाए, क्या किया जाए? यह भय और उचाट की मनःस्थिति है। इस उजाड़ से बचने के लिए अधिकारी से लेकर भिखारी तक सबको किसान के साथ आना होगा। किसान बचेंगे तो ये भी बचेंगे। किसानी गई तो न व्यापार बचेगा न नौकरी, न धर्म रहेगा न धंधा| न भीख मिलेगी न शिक्षा। तब ज्ञानियों से लेकर श्रमिकों तक, व्यापारियों से लेकर भिखारियों तक सभी को किसानी बचाने की लड़ाई लड़नी होगी। तुलसीदास का यही मंतव्य है।यह किंकर्तव्यविमूढ़ता “कहाँ जाई का करी?” की स्थिति तक पहुँचने से पहले की चेतावनी है। जैसे चिकित्सा पेशा होते हुए भी धंधा नहीं है वैसे अन्न के क्रय-विक्रय के बावजूद किसानी व्यापार नहीं है। व्यापारियों को कृषि-क्षेत्र सौंपना पूरी प्रणाली को संकट के गर्त में डाल देना है। इस महादेश के अर्थशास्त्र को ध्यान में रखकर ही महाभारतकार ने व्यवस्था दी थी कि राष्ट्र की ‘समिति’ में ऐसे नेता न भेजे जाएं जो खेती नहीं करते, अन्न नहीं उपजाते। ‘समिति’ को आज की शब्दावली में संसद या विधानसभा कहेंगे- “न नः स समितिं गच्छेत् यश्च नो निर्वपेत् कृषिम्|” (‘उद्योगपर्व’, 36/31) अपनी किताब ‘पुराण-विमर्श’ में व्यास जी के इस कथन को उद्धृत करते हुए आचार्य बलदेव उपाध्याय ने टिप्पणी की है- “कृषि से अनभिज्ञ कुर्सी तोड़ बकवादी नेता भला किसानों का कोई मंगल कर सकता है?” (पृ. 358)
तुलसीदास का भरोसा रामराज्य में है। यह भरोसा रामराज्य की प्राथमिकताओं से उपजा है। किसानी अगर जीवन किंवा अर्थव्यवस्था का मूलाधार है तो रामराज्य में उसे प्रथम वरीयता दी गई है-
खेती बनि बिद्या बनिज, सेवा सिलिप सुकाज|
तुलसी सुरतरु सरिस सब, सुफल राम के राज ||
(‘रामाज्ञा-प्रश्न’, 7/2/7)
वरीयता-क्रम में सातों क्षेत्र हैं – खेती, मजदूरी, (‘बनि’ खेतिहर मजदूरी के लिए प्रयुक्त होता है), विद्या, वाणिज्य, सेवा (चिकित्सा, अभियांत्रिकी आदि क्षेत्र), शिल्पकारी-दस्तकारी, और राजकीय/सरकारी कामकाज।शासन-सत्ता की प्राथमिकताओं का यह क्रम-निर्धारण ध्यान देने योग्य है। मगर, इससे भी ज्यादा ध्यान देने योग्य बात दूसरी है। तुलसीदास उस ताकत की पहचान कराते हैं जो ऐसी प्राथमिकताओं वाले शासन में बाधक है। वे साफ-साफ़ कहते हैं कि देवसत्ता रामराज्य की, खुशहाल समाज की सबसे बड़ी शत्रु है। आज की राजनीतिक शब्दावली में देवसत्ता को दक्षिणपंथ कहेंगे। दक्षिणपंथ धर्म से वैधता हासिल करता है। अपने को देवताओं से जोड़ता है। स्वयं को प्रश्नातीत ठहराता है। इसकी कथनी और करनी में विलोम संबंध होता है। तुलसीदास ने ‘मानस’ के दूसरे सोपान में देवसत्ता का सविस्तार चित्रण किया है. राम को उत्तराधिकारी घोषित किया जाना है। अयोध्या की जनता परम प्रसन्न है। यह देवताओं को सहन नहीं। वे मलिन-मन के स्वार्थी लोग हैं| कुचक्र रचने में उन्हें महारत हासिल है- ‘तिन्हहिं सोहाय न अवध बधावा| चोरहिं चांदिनि राति न भावा||’ जैसे चोर अंधेरी रात में सहज महसूस करता है वैसे देवसत्ता भयाकुल-शोकाकुल जनसमाज में सुरक्षित अनुभव करती है| अपनी सत्ता को सुरक्षित बनाए रखने के लिए वह चार स्तरों पर कार्य करती है- वह जनता को भयग्रस्त रखती है, समाज को भ्रमित करती है, लोगों में अ-रति (नफरत/ दूरी/ विभाजन) फैलाती है और जनसामान्य में उचाट (निराशा/ अस्थिरता) भरती है-
सुर स्वार्थी मलीन मन, कीन्ह कुमंत्र कुठाटु|
रचि प्रपंच माया प्रबल भय भ्रम अरति उचाट||
(मानस, 2/295)
दक्षिणपंथी दावा यही करते हैं कि वे रामराज्य की स्थापना करेंगे| तुलसीदास चेताते हैं कि ये इतने झूठे, क्रूर और कायर हैं कि मरे हुए को मारकर मंगल की कामना करते हैं- ‘मुए मारि मंगल चहत|’ (मानस, 2/301) रामराज्य की स्थापना के सबसे बड़े विरोधी तथाकथित रामभक्त ही हैं-
बंचक भगत कहाइ राम के|
किंकर कंचन कोह काम के||
(मानस, 1/12/3)
अपने को रामभक्त कहने वाले ये ठग वास्तव में संपत्ति, हिंसा और काम-वासना के दास हैं| तुलसीदास इसीलिए कहते हैं रामराज्य में सबसे बड़ी बाधा यह देवसत्ता ही है-
राम राज बाधक बिबुध, कहब सगुन सति भाउ।
देखि देवकृत दोष दुख, कीजै उचित उपाउ।।
(‘रामाज्ञा-प्रश्न’, 7/6/3)
काव्यमीमांसाकार राजशेखर (नवीं-दसवीं शताब्दी) ने कवि के लिए वार्ता (-शास्त्र) का ज्ञान आवश्यक बताया था। इस विद्या में कृषि तथा पशुपालन आते हैं। वार्ता का ज्ञान न हो तो कवि उत्पादक तथा अनुत्पादक वर्गों में अंतर नहीं कर सकता। संत काव्य में वार्ता-विवेक सहज ही गुंथा हुआ है। तुलसीदास ने एक दोहे में दोनों की बड़ी सटीक तुलना की है। छल-बल में सिद्ध अनुत्पादक वर्ग शिखर पर वास करता है जबकि उत्पादक किसान व श्रमिक नीचे रहते हैं-
अति ऊँचे भूधरनि पर, भुजगन के अस्थान।
तुलसी अति नीचे सुखद, ऊख, अन्न अरु पान।।
(‘वैराग्य-संदीपिनी’, दो.सं. 39)
अत्यंत ऊँचे पर्वतों पर भुजगों (विषधरों) का वास है जबकि एकदम नीचे तलहटी में ईख, अन्न और पान की सुखद फसल होती है। जो परजीवी-पराश्रित है वह ऊपर है और जो उत्पादक है वह नीचे।परजीवी अपनी विषधर धूर्तता के दम पर बना हुआ है। वह नीचे वालों को चैन से बैठने नहीं देता। उसके कृत्य अत्यंत निकृष्ट हैं| दूसरों का सुख उससे देखा नहीं जाता- “ऊँच निवास नीच करतूती। देखि न सकहिं पराइ बिभूती।।” (मानस, 2/12/6)
ऐसी जनद्रोही सत्ता से कैसे निपटा जाए? तुलसीदास भरोसा देते हैं कि यह सत्ता अडिग-अपराजेय नहीं है। इसका अंत कौरवों जैसा होगा- “राज करत बिनु काज हीं, ठटहिं जे कूर कुठाट। तुलसी ते कुरुराज ज्यों, जइहैं बारह बाट।।” (‘दोहावली’, दो.सं. 417)| दुर्दिन लाने वाली सत्ता अपने-आप नहीं जाएगी। इस सत्ता को ‘बारह बाट’ भेजने के लिए संगठित प्रयत्न करने होंगे। सत्ताधारी को नरक का रास्ता दिखाना होगा-
जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी।
सो नृप अवसि नरक अधिकारी।।
(मानस, 2/71/6)
ऐसे राजा के साथ क्या सुलूक किया जाए, इस प्रश्न पर संत गरीबदास ज्यादा स्पष्ट हैं। वे कहते हैं कि विश्वंभर का रूप धरे लोभी-लालची, कामी और पाखंडी राजा को निश्चय करके, योजना बनाकर मार देना चाहिए-
काम लुब्ध पाखंड रचा
धरे बिसंभर रूप।
ऐसा निःचा चाहिये
मारे राजा भूप।
(‘गरीबदास की बानी’, ‘निश्चय का अंग’ 36, पृ. 74)
भय, भ्रम, अ-रति और उचाट की राजनीति इन दिनों उफान पर है। किसानों के आंदोलन को नष्ट-भ्रष्ट करने के लिए पुरज़ोर कोशिशें की जा रही हैं। किसानों को क्षेत्र, भाषा, वर्ग और धर्म के आधार पर बाँटकर आंदोलन को कमज़ोर करने का अभियान चल रहा है। इसमें सरकार को सफलता नहीं मिल रही है। मूल वजह कबीर ने पहचानी थी- ‘गई ठगौरी ठग पहिचाना|’ ठग की शिनाख्त कर ली जाए तो ठगी का जाल सिमटने लगता है। तब आसन्न उजाड़ के सम्मुख खड़े किसान खलिहान न जाकर बरबादी के स्रोत की घेराबंदी करते हैं। कॉर्पोरेट को असीमित भंडारण की छूट क्या किसानों और उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए है? कालाबाजारी को वैध बनाने से किसका भला होने जा रहा है? एपीएमसी एक्ट को निष्प्रभावी बना देने से किसान विशालकाय मगरमच्छों का ग्रास बनने से कैसे बच पाएंगे? मंडी व्यवस्था को सुधारने की बजाए समाप्त कर देने से क्या किसानों का सशक्तीकरण होगा? ठेके पर खेती आरंभ होने से क्या किसानी औपनिवेशिक दौर में नहीं पहुँच जाएगी? अन्नदाताओं को अनाज पैदा करने की बजाए लाभदायक कैश-क्रॉप (नगदी फसल जैसे तम्बाकू, नील, अफीम…) आदि उपजाने के लिए क्या मजबूर नहीं किया जाएगा? बहुराष्ट्रीय कंपनियां या कॉर्पोरेट प्लेयर्स दुर्भिक्ष के हालात पैदा करके कितना वसूलेंगे? दो शताब्दी पहले के संत-कवि पलटू साहिब ने चौगुने दाम पर बेचे जाने का अनुमान लगाया था-
सस्ते मँहै अनाज खरीद के राखते।
महँगी में डारैं बेचि चौगुना चाहते ।।
(‘पलटू बानी-2’, पृ. 68)
ठीक ऐसा ही अनुमान संत गरीबदास ने लगाया था। उनका साहूकार बेबस जनता को मूसने की पक्की योजना बनाता है। सोच-समझकर सौदा तय करता है। बेहद सस्ते में खरीदता है और अधिकतम महँगे में बेचता है-
महँगा सस्ता देख ले सौदा करे बिचार।
दुगुने तिगुने चौगुने करिहै साहूकार ।।
महँगा सस्ता देख ले सौदा करे समोय।
दूने तिगुने चौगुने कर ले जाता कोय।।
(‘गरीबदास जी की बानी’, ‘लै का अंग’ पृ. 51.)
‘समोय’ शब्द पर ध्यान देना चाहिए। घुसकर सौदा करने को समोय कहा गया है। सस्ते में खरीदी करने वाला सीधे खेत से, खलिहान से अनाज उठाता है। वह घर में घुसकर सौदा करता है। यहाँ उसका कोई प्रतिस्पर्धी नहीं होता। यहाँ वह हाकिम-हुक्काम की नज़र में आने से बचा रहता है। भंडारण के बाद मुनाफे का खेल शुरू होता है। दुगुने से शुरुआत होती है। फिर, तिगुने, चौगुने … जहाँ तक कीमत बढ़ायी जा सकती है, वह माल बेचा जाता है।
इसी तरह ‘कोय’ (कोई) शब्द पर ध्यान देना चाहिए। इससे पूर्व की पंक्ति में खरीदार की पहचान ज्ञात है। वह ‘साहूकार’ है। साहूकार को गाहे-बगाहे पकड़ा जा सकता है। उससे पूछा जा सकता है। लेकिन, ‘कोय’ को कैसे पहचाना जाएगा? जो घर में घुसकर सौदा तय करने वाला अनजाना खरीदार है उससे तो बकाये की रकम भी वसूली नहीं जा सकती। माल उठने के बाद उससे संपर्क कर पाना दुष्कर है। संत-कवि की यह आशंका नए कृषि कानून में साकार हुई है। किसान से उसकी फसल खरीदने के लिए अब लाइसेंस लेना आवश्यक नहीं रह गया है। बस, क्रेता (‘कोय’) के पास कहने को एक पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड में पता नहीं लिखा जाता!
संकट की विराटता, गहराई और भयावहता का अनुमान करके ही देश के किसान उद्वेलित हैं, संगठित हैं तथा संकल्पित हैं| किसानों की तबाही का असर जिन पर पड़ेगा वे तबके भी आंदोलन के हिस्सेदार हो रहे हैं| तबाही का प्रारूप तैयार करने, लागू करने वाले पाँचों शक्ति-केन्द्रों को अपने किए का हिसाब देना ही होगा| इसे न तो इतिहास भूलेगा, न भविष्य| यह परिघटना लोकचित्त में बनी रहने वाली है-
“खोटे वणजिए मनु तनु खोटा होय।”
(महला-1, सबद-23)
नए कृषि क़ानून खोटे, घटिया वाणिज्य को मजबूती देने के लिए लाए गए हैं। इसका असर पूरे सिस्टम पर पड़ेगा। यह मन और तन दोनों को विकृत करेगा|।हिंसा में उछाल आएगा। हत्याओं-आत्महत्याओं-मौतों का ग्राफ तेजी से बढ़ेगा। समाज के विभिन्न घटकों में पहले से चला आ रहा टकराव घातक शक्ल अख्तियार करेगा। दासता का वह विस्मृत दौर अधिक मजबूत होकर नए संस्करण में वापसी करेगा। आंदोलनकारी किसान इसे रोकना चाहते हैं। वे मोर्चे पर डटे हुए हैं। किसानी उनका दीन है, उनका धर्म है। वे अपने दीन की रक्षा में सन्नद्ध हैं-
सूरा सो पहिचानिये, जो लड़े दीन के हेत।
पुर्जा पुर्जा कट मरै, तऊ न छाड़े खेत ।।
संदर्भ सूची
-
- ‘कबीर ग्रन्थावली’ (संस्करण 1997), संपादक- डॉ. माताप्रसाद गुप्त, साहित्य भवन प्रा.लि. जीरोरोड, इलाहाबाद-3
- ‘गरीबदास जी की बानी’ (संस्करण 1998), बेलवीडियर प्रिंटिंग वर्क्स, इलाहाबाद-2
- ‘गुरु नानकदेव : वाणी और विचार’ (प्र.सं. 2003), रमेशचन्द्र मिश्र, संत साहित्य संस्थान, 3611, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली.
- ‘तुलसी ग्रंथावली द्वितीय खंड’ (सं.2031 वि), सं. रामचंद्र शुक्ल आदि, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी.
- ‘दरिया सागर’ (बिहार वाले दरिया साहिब) (छठा संस्करण, 2003), बेलवीडियर प्रिंटिंग वर्क्स, इलाहाबाद-2.
- ‘दरिया साहब’ (मारवाड़) (सातवीं बार, 2003), बेलवीडियर प्रिंटिंग वर्क्स, इलाहाबाद-2.
- ‘दोहावली’ (छब्बीसवाँ संस्करण, सं. 2044), गो. तुलसीदास, गीताप्रेस गोरखपुर
- ‘पलटू साहिब की बानी’ भाग-1, (संस्करण 1993) पलटूदास, बेलवीडियर प्रिंटिंग वर्क्स, इलाहाबाद.
- ‘पलटू साहिब की बानी’ भाग-3 (2001), बेलवीडियर प्रिंटिंग वर्क्स, इलाहाबाद.
- ‘पलटू साहिब की बानी’ भाग-2, (छठा रीप्रिंट, 1954) बेलवीडियर प्रिंटिंग वर्क्स, इलाहाबाद-2.
- ‘पुराण-विमर्श’ (1965, पुनर्मुद्रित 2013), आ. बलदेव उपाध्याय, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी-01.
- ‘बिहारी सतसई संजीवनी’ (1998), रामदेव शुक्ल, भवदीय प्रकाशन, अयोध्या, फैजाबाद.
- ‘मलूकदास की बानी’ (छठी बार, 1997), बेलवीडियर प्रिंटिंग वर्क्स, इलाहाबाद-2
- ‘रज्जब बानी’, (1963), सं. डॉ. ब्रजलाल वर्मा, उपमा प्रकाशन, प्रा. लि. कानपुर.
- ‘रामचरितमानस’ (सटीक मझला साइज, सं. 2073), गो. तुलसीदास, गीताप्रेस, गोरखपुर.
- ‘रैदास रचनावली’ (2006), सं. गोविंद रजनीश, अमरसत्य प्रकाशन, प्रीत विहार, दिल्ली-92.
- ‘संत रज्जब अली : वाणी और विचार’ (2002), डॉ. रमेशचन्द्र मिश्र, संत साहित्य संस्थान, दरियागंज, नई दिल्ली-02.
- ‘संत रोहल फ़कीर ग्रंथावली’ (2016), सं. डॉ. रमेशचन्द्र मिश्र, संत साहित्य संस्थान, दरियागंज, नई दिल्ली-2.
- ‘संत साहित्य संदर्भ कोश’ (पहला भाग, 2015), रमेशचन्द्र मिश्र, संत साहित्य संस्थान, दरियागंज, नई दिल्ली.
- ‘संत साहित्य संदर्भ कोश’ (चौथा भाग, 2015), रमेशचन्द्र मिश्र, संत साहित्य संस्थान, दरियागंज, नई दिल्ली.
- ‘संत सुधा सार’, (1969), वियोगी हरि, सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली.
- नए कृषि कानूनों पर अर्थशास्त्री जया मेहता लेख यहाँ उपलब्ध है- https://www.infoway24.com/an-analytical-review-of-three-agriculture-acts-by-the-modi-government-by-dr-jaya-mehta
- ‘सहजो बाई की बानी’ (सहज प्रकाश, संस्करण 2005), बेलवीडियर प्रिंटिंग वर्क्स, इलाहाबाद-2