बातचीत दूसरा हिस्सा
आप अपने उपन्यासों में खुद उपदेश देने के बजाय पात्रों के जरिए गंभीर बातें कहलाते हैं। मेवात जैसे अलक्षित क्षेत्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर केन्द्रित ‘काला पहाड़’ उपन्यास के पात्र ठेठ हिन्दुस्तान की कहानी कहते हैं। क्या ये पात्र प्रक्रिया की जटिलताओं और विकृतियों को पूरी से उघाड़ने में सफल हो पाते हैं?
किसी भी लेखक की पहली और सबसे बड़ी कोशिश यही रहती है कि वह अपने पात्रों के माध्यम से सामाजिक जटिलताओं और विकृतियों को उघाड़ पाए। अब यह लेखक की क्षमता, उसके नजरिए, उसकी राजनैतिक चेतना, जातीय स्मृतियों और उसके विवेक पर निर्भर करता है बल्कि इस मामले में उसका सामाजिक परिवेश और उसका लोक व्यवहार सबसे अधिक मायने रखता है। अगर देखा जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप, विशेष कर भारत की सामाजिक संरचना ही वैविध्यपूर्ण है। जिसे हम ठेठ हिन्दुस्तान कहते हैं उसका निर्माण हमारी जातीय स्मृतियों से हुआ है। जातीय स्मृतियों से मेरा तात्पर्य यह है कि हमारी नागरिक के रूप में पहचान अपने धर्म से अधिक समुदाय के रूप में है। हिन्दू या मुसलमान कम हम हिन्दुस्तानी या काला पहाड़ के संदर्भ में देखें तो मेव या हिन्दू के बजाय एक मेवाती के रूप में पहले हैं। इसीलिए हमारी चिंताएं, हमारे सुख-दुःख, हमारे सरोकार, हमारी ज़रूरतें सांझी ज़रूरते हैं और इन सबके निर्माण में जो सबसे बड़ा तथ्य काम करता है वह है हमारी सांझी विरासत। अब सवाल यह है कि आखिर हमारी यह सांझी विरासत है क्या ? सांझी विरासत का उत्स मूल रूप से हमारी सांस्कृतिक चेतना और उसके लोक में छिपा होता है। इसे अगर मैं उदाहरण देकर समझाऊँ तो महाभारत से अच्छा उदाहरण दूसरा नहीं हो सकता। मेरी राय में रामायण तो एक बार केवल और केवल हिन्दुओं का हो सकता है मगर ऐसा हम महाभारत के बारे में नहीं कह सकते। आखिर ऐसा क्या है कि जो स्वीकार्यता महाभारत को प्राप्त है, रामायण को नहीं है। इस स्वीकार्यता से मेरा तात्पर्य धार्मिक नहीं बल्कि उस सामूहिक स्वीकार्यता से जो हमारे लोक व्यवहार को प्रभावित करता है। यही कारण है कि आज भी महाभारत देश के अलग-अलग अंचलों में भिन्न रूपों में गाया-बजाया जाता है। मेवात में भी हिन्दुओं से कहीं अधिक महाभारत पर आधारित पंडून का कड़ा मेवों में गाया-बजाया जाता है। मेरा मानना है कि रामायण की अपेक्षा लोक-व्यवहार की जीवंत प्रस्तुति महाभारत में है और यही जीवंतता महाभारत को हिन्दू और मुस्लिम दोनों समुदायों में मान्य बनाती है। यह बात अलग है कि अन्य समाजों की तरह मेवाती समाज में पैदा हुई कुछ विशेष किस्म की जटिलताओं और विकृतियों के पनपने के कारण ऐसी सांस्कृतिक और सांझी परंपराएँ तेज़ी से दम तोड़ रही हैं। खासकर पिछले लगभग ढाई दशकों और इधर पिछले एक दशक में इन विकृतियों ने हमारी जातीय स्मृतियों और चेतना पर बहुत गहरी चोट की है। जिसका परिणाम यह हुआ कि मेवात की जिस सांस्कृतिक विरासत पर हम जैसे लोग इतराते फिरते थे, अब इसकी चिंता सी होने लगी है।
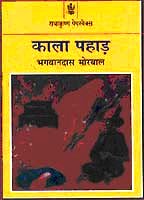
अब रही बात खुद उपदेश देने के बजाय पात्रों के ज़रिये गंभीर बात कहलवाने की, तो एक लेखक के रूप में अपने अनुभव के आधार पर मेरा यह मानना है कि आखिर लेखक खुद क्यों उपदेश दे? जिस बात को रचना के पात्र या चरित्र कह दें उसे लेखक द्वारा कहने की क्या जरूरत है। सबसे बड़ी बात यह कि किसी भी रचना के जो पात्र अपनी बात कहते हैं वास्तव में पात्र के रूप में वह खुद लेखक ही कह रहा होता है। अब यह लेखक के कौशल पर निर्भर करता है कि वह लेखक के बजाय अपने पात्रों का इस्तेमाल कितनी कुशलता से करता है। काला पहाड़ जो कि मेवात जैसे एक अलक्षित अंचल या क्षेत्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित है, उसके चलते तो यह चुनौती और बड़ी व जटिल हो जाती है। मेरे लिए संतोष की बात यह है कि एक हद तक काला पहाड़ के ज़्यादातर पात्र सामाजिक प्रक्रिया की जटिलताओं और प्रवृत्तियों को पाठक के सामने पूरी ईमानदारी के साथ लाते हैं।
‘काला पहाड़’ में आपने एक ओर ऐतिहासिक पात्र और मेवात नायक ‘हसन खां मेवाती’ की ओर पाठकों का ध्यान खींचा है वहीं दूसरी ओर अयोध्या के स्याह पक्ष को केन्द्रित करते हुए उसकी आग में झुलसने वाली बहुलतावादी संस्कृति को रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है, इससे आप पाठकों को क्या संदेश देना चाहते हैं?
जैसा कि मैंने ऊपर कहा है कि सांझी विरासत का उत्स मूल रूप से हमारी सांस्कृतिक चेतना, जातीय स्मृति और लोक में छिपा होता है। वास्तव में, हसन खां मेवाती खालिस मेवों का नायक नहीं अपितु यह पूरी सांझी विरासत का नायक है। यह सर्वविदित है कि हसन खां मेवाती पानीपत की लड़ाई में एक मुस्लिम धर्मावलंबी होने के बावजूद बाबर के साथ मिलकर राणा सांगा के खिलाफ युद्ध नहीं करता है बल्कि एक बाहरी हमलावर के खिलाफ राणा सांगा के साथ मिलकर युद्ध करता है और इसी युद्ध में यह खेत हो जाता है। दूसरी बात आपने यह कही कि काला पहाड़ में अयोध्या के स्याह पक्ष को केन्द्रित करते हुए उसकी आग में झुलसने वाली बहुलतावादी संस्कृति को रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है, इन दोनों संदर्भों से मैं क्या सन्देश देना चाहता हूँ? सन्देश इसका बहुत स्पष्ट है कि जिस मेवात की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपरा इतनी संपन्न और समतावादी रही हो, उसी मेवात को राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विध्वंस की प्रतिक्रिया में उपजे प्रायोजित सांप्रदायिक दंगों का शिकार सबसे पहले हसन खां मेवाती के वंशज होते हैं-ऐसा क्यों? असल बात यह है कि राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विध्वंस तो एक बहाना था, सच तो यह है कि जिस तरह हमारे समाज में सांप्रदायिक असहिष्णुता बढ़ती जा रही है यह उसका रिफ्लेक्शन था। राष्ट्रवाद की परिभाषा को जिस तरह अतिरंजित किया जा रहा है यह उसकी एक परिणति थी। एक तरह हमारी बहुलतावादी संस्कृति को खंडित करने के जिस तेज़ी के साथ प्रयास किए जा रहे हैं, उनके प्रति सचेत रहने का यह एक संकेत भर है।
[bs-quote quote=”मेरा मानना है कि हिंदी कथा साहित्य में क्षेत्रीय अस्मिता के स्वर को प्रबल बनाने के लिए जिस लेखक को श्रेय जाता है, निस्संदेह वह रेणु हैं। अगर मुझे दूसरा नाम लेना पड़े तो रेणु के बाद मैं राही मासूम रज़ा का नाम लूँगा। मैं पूरी ईमानदारी से यह स्वीकारता हूँ कि यदि मैला आँचल नहीं आया होता तो आज हिंदी कथा साहित्य में क्षेत्रीय अस्मिता का स्वर कहीं नज़र नहीं आता। इस स्वर को आधा गाँव उपन्यास ने और बल प्रदान किया। इसे मैं एक संयोग ही मानूँगा कि जिन उपन्यासों को पढ़कर मेरे लेखन में आपको क्षेत्रीय अस्मिता का स्वर नज़र आता है, वह स्वर मैला आँचल, आधा गाँव, काला जल, झीनी-झीनी बीनी चदरिया, परती परिकथा जैसे उपन्यासों की ही देन है, जिन्हें मैंने सबसे पहले पढ़ा। आपने पूछा है कि इस क्षेत्रीयता को उभारने के पीछे कहीं आपका उद्देश्य उस अंचल को साहित्य के केन्द्र में प्रतिष्ठित करना तो नहीं है? मेरा कहना है कि यह क्षेत्रीयता नहीं बल्कि आपके ही शब्दों में अस्मिता से जुड़ा सवाल है।” style=”style-2″ align=”center” color=”” author_name=”” author_job=”” author_avatar=”” author_link=””][/bs-quote]
आपके उपन्यासों में हाशिए के लोगों की उपस्थिति बहुत प्रभावी रूप में दिखाई पड़ती है। इसे आप किसी विचारधारा का प्रभाव मानते हैं या समाज के हाशिए के लोगों के प्रति संवेदनात्मक लगाव जो बाद में रचनात्मक अभिव्यक्ति में परिणत होता है?
मेरा निजी मत है कि वंचितों, उपेक्षितों और हाशिए के लोगों के प्रति जो संवेदनात्मक लगाव पैदा होता है, वह किसी न किसी विचारधारा से अवश्य प्रभावित होता है। मनुवादियों से तो कम से कम ऐसे संवेदनात्मक लगाव की उम्मीद करना बेमानी होगा। यह संवेदनात्मक लगाव लेखक के सामाजिक परिवेश, उसके जीवन-संघर्ष और उसके लोक व्यवहार से उसकी जो जीवन दृष्टि बनती है, उससे प्रभावित रहती है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि एक शूद्र और ब्राह्मण की संवेदना सर्वथा भिन्न-भिन्न होगी. कहीं न कहीं यह संवेदना संस्कारगत भी होती है। वंचितों, उपेक्षितों और हाशिए के लोगों के प्रति जो नजरिया शूद्र का होगा, ज़रूरी नहीं कि वही नजरिया एक ब्राह्मण का भी हो. कहीं न कहीं आपको स्पष्ट अंतर नज़र आ जाएगा. थोपा हुआ या बनाई गई संवेदना पाठक के अपने आप पकड़ में आ जाती है।
आपने ‘हलाला’ नामक एक लघु उपन्यास पूरा किया है। उसका एक अंश ‘बहुवचन’ पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। उसमें मुस्लिम परिवार की जो संरचना दिखती है वह तो उत्तर भारत के गांवों की अधिकांश घरों की कहानी है, इसे किस रूप में देखा जाए?
हमारे बहुत से समाजों का यह दुर्भाग्य है कि ग़रीबी और अशिक्षा के चलते हमारी बहुत-सी धार्मिक संहिताएँ, फतवे, फ़रमान हमारे धर्म गुरुओं की कूढ़ मगजता, उनके पुरुषवादी सोच और संकीर्णता के चलते बुराइयों में तब्दील हो चुकी है बल्कि कुछ ने तो कुप्रथाओं का रूप ले लिया है। दरअसल धार्मिक ना-समझी ने, बल्कि कहना उचित होगा कि धार्मिक मामलों ने जिस तरह सामाजिक बुराइयों का रूप ले लिया वह चिंताजनक है। हलाला वास्तव में सामाजिक समस्याओं से उपजी एक कुप्रथा है जिसे सामाजिक संदर्भों और दायरों में निपटाने के बजाय उसे हमने धर्म गुरुओं के हवाले कर दिया है। उनके अर्थों का अनर्थ किया जा रहा है, और ऐसा नहीं है कि यह केवल एक धर्म में हो रहा है बल्कि सभी धर्मों की एक जैसी स्थिति है। मजेदार तो यह है कि कुछ मामलों में, विशेषकर स्त्री के मामले में सब की मानसिकता और सोच एक जैसी है। हिन्दू धर्म की स्थिति तो सबसे बदतर है जबकि मुस्लिम धर्म को हम दूसरे नंबर पर रख सकते हैं। मनुस्मृति के तो कहने ही क्या? अगर आप हमारे धार्मिक ग्रंथों का बेहद बारीकी से अध्ययन करेंगे तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि स्त्रियों के संबंध में रची गईं कुछ आयतों और श्लोकों के अर्थों में कोई अंतर नहीं है। मेरा यह मानना है कि बाद में इनके अर्थों को हमारे धार्मिक गुरुओं ने इतना प्रचलित कर दिया कि उन्हीं के अनर्थों को सच मान लिया गया। चूंकि ज़्यादातर धार्मिक फैसले इन्हीं आयतों और श्लोकों के आधार पर बनाए गए हैं इसलिए उन पर आप सवाल भी नहीं खड़े कर सकते। यहाँ मैं ‘हलाला’ के संदर्भ में कुछ बात रखना चाहता हूँ। हलाला का अर्थ बिलकुल स्पष्ट है कि तलाक के बाद कोई भी औरत पहले शौहर के लिए तब तक हलाल नहीं हो सकती, जब तक वह किसी दूसरे व्यक्ति से निकाह न कर ले। हलाला के संदर्भ में खाली निकाह ही काफी नहीं है बल्कि औरत का consumate होना ज़रूरी है। मैंने दिल्ली के जामा मस्जिद के उर्दू बाज़ार से प्रकाशित होने वाली एक पत्रिका इसलाहे समाज में कई साल पहले इसके बारे में जो पढ़ा, वह यूं था- जब तक दूसरा मर्द निकाह के बाद उसका मज़ा न चख ले, तब तक वह उस औरत को तलाक़ नहीं दे सकता। दरअसल यह है अर्थ का अनर्थ यानी शब्दों का फूहड़ चयन। आम आदमी के मन पर इसका क्या असर होगा, आसानी से कल्पना की जा सकती है। मेरा मानना है कि किसी भी समाज में धर्म का सबसे ज्यादा दखल या कहिये धार्मिक पाखंड या महिमा मंडन ग़रीब और अशिक्षित समाज और परिवारों में ही होता है। मैं मनुष्य के धार्मिक होने या उसके धर्म भीरुता का विरोधी नहीं हूँ बल्कि मैं आडंबर और प्रपंच का विरोधी हूँ जो हमें हमारे मौलिक अधिकारों के साथ-साथ हमारी धार्मिक स्वतंत्रता पर चोट करता है। दरअसल किसी भी धर्म को पूरी समग्रता में समझने के लिए आदमी का शिक्षित होना ज़रूरी है। शिक्षा हमारे अंदर तर्क-वितर्क करने की ताक़त और धार्मिक उदारता पैदा करती है और यही ताक़त सही अर्थ को समझने में सहायक होती है। यह बात भी सही है कि धार्मिक विषय, विशेषकर जिस धर्म से आपका संबंध नहीं है, के ताने-बाने को केंद्र में रखकर कोई रचना लिखते हैं तो उसके खतरे कहीं ज्यादा होते हैं। क्योंकि धर्म ऐसा नाज़ुक विषय है कि आपका छोटा-सा दुराग्रह या पूर्वाग्रह आपको संकट में डाल सकता है। लेकिन मेरी कभी भी ऐसी मंशा नहीं रही और इसका उदाहरण है मेरा दूसरा उपन्यास बाबल तेरा देस में। इस उपन्यास में मैंने कुरआन से लेकर बहिश्ती ज़ेवर का भरपूर इस्तेमाल किया है।
यह भी पढ़ें :
पुरुषों के पेटूपन और भकोसने की आदत ने औरतों को नारकीय जीवन दिया है !
आपने हलाला के संदर्भ में एक बात कही है कि मुस्लिम परिवार की जो संरचना दिखती है वह तो उत्तर भारत के गांवों के अधिकांश घरों की कहानी है, इसे किस रूप में देखा जाए? दरअसल स्थिति इतनी खराब नहीं हैं जैसा हमें लगता है। दरअसल, समाज में सब तरह के अपवाद होते हैं लेकिन अपवाद कभी समाज का पूरा सच नहीं होता। एक लेखक जब किसी विषय को अपनी कहानी या उपन्यास की कथावस्तु बनाता है तो उसके आगामी और पहले के परिणामों, दुष्परिणामों को भी ध्यान में रखता है। यह सच है कि किसी रचना में यथार्थ आटे में नमक जितना होता है। मगर जब रचना पाठक के सामने आती है, तो होता इसके उलट है यानी कल्पना आटे का रूप ले लेती है। लेखक की कल्पना पाठक को समाज का पूरा सच नज़र आने लगता है. मैं इसी ‘सच’ को लेखक की सफलता मानता हूँ।
‘मुस्लिम समाज’ के जिन पात्रों को आपने ‘काला पहाड़‘,’बाबल तेरा देस में‘ और ‘हलाला’ के केंद्र में रखा है, क्या इसे हिंदी साहित्य में मुसलमानों के प्रति हुई उपेक्षा की भरपाई के रूप में देखा जा सकता है?
हिंदी के एक समर्थ कथाकार और काला जल जैसे उपन्यास के लेखक शानी प्राय: एक बात कहते थे कि हिंदी साहित्य में प्रेमचंद के बाद ऐसा कोई कथाकार नहीं हुआ है जिनकी रचनाओं में मुस्लिम समाज इस तरह आया हो जैसे प्रेमचंद की रचनाओं में आया है। यह अभाव हमें बाद के कथा-साहित्य में भी नज़र आता रहा। इसकी मैं एक वजह मानता हूँ और वह यह कि जिस तरह हिन्दुओं के धार्मिक आचार-व्यवहार से हमारा मुस्लिम समाज बावस्ता रहा है, उस तरह हिन्दू लेखक कभी नहीं रहे। इसलिए हम उनके धार्मिक आचार-व्यवहार से उतने परिचित नहीं रहे जितने वे रहे। दूसरी बात यह कि प्रेमचंद के ज़माने का जो भारतीय समाज था वह आज की अपेक्षा कहीं ज्यादा समन्वयकारी था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी रचनाओं में मुस्लिम परिवेश और पात्रों का आना इस पर निर्भर करता है कि आप जिस समाज में रहते हैं उसमें मुस्लिम समुदाय की सहभागिता कितनी और कैसी है। यहाँ मैं अपना ही उदाहरण देना चाहता हूँ कि ऐसी क्या वजह है कि मेरी रचनाओं में चाहे वे कहानियाँ हों या उपन्यास बार-बार मुस्लिम परिवेश और पात्र, वह भी मेवाती मुस्लिम परिवेश क्यों आते हैं? तो इसका उत्तर बहुत सीधा है कि मेरा सामाजिक परिवेश या कहिए लोक ही इस समाज से बना हुआ है। ज़ाहिर सी बात है कि मेरी जातीय, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक चेतना का निर्माण मेवात की स्थानीयता और लोकाचार से हुआ है। मेरी रचनाओं में बार-बार यहीं के लोकनायक और नागरिक ही तो आएंगे। मेरे पात्र यहीं की माटी की गंध और यहीं के नागरिकों के सुख-दुःख से सराबोर होंगे। मेरा तो मानना ही यही है कि बिना अपने लोक को समझे हम किसी भी विमर्श को नहीं जान सकते। मेरे तीनों उपन्यासों काला पहाड़, बाबल तेरा देस में और हलाला ही क्यों बल्कि भारत में तेज़ी से पनपती एनजीओ संस्कृति को केंद्र में रखकर लिखे गए तथा स्टेट, कॉर्पोरेट और सिविल सोसाइटी के गठजोड़ का पर्दाफाश करने वाले और हाल में प्रकाशित उपन्यास नरक मसीहा में भी मेवाती समाज आता है। अगर किसी कथाकार-उपन्यासकार का ज़्यादातर लेखन मुस्लिम पात्रों और परिवेश से लबरेज़ हो तो आप इसे हिंदी साहित्य में मुसलमानों के प्रति हुई उपेक्षा की भरपाई के रूप में देख सकते हैं।

आपके कथा साहित्य में क्षेत्रीय अस्मिता का स्वर बहुत प्रबल है। ग्रामीण बोली-बानी का प्रयोग भी आप खूब करते हैं। जिस तरह ‘काला पहाड़’, ‘बाबल तेरा देस में‘, ‘नरक मसीहा‘ और अभी-अभी लिखे गए लघु उपन्यास ‘हलाला‘ में मेवात की क्षेत्रीय अस्मिता को उभारा है उसी तरह ‘महराब’, ‘भूकंप‘, ‘अस्सी मॉडल उर्फ़ सूबेदार‘, ‘छल‘ सहित अनेक कहानियों में मेवात की संस्कृति देखने को मिलती है। क्षेत्रीयता को उभारने के पीछे कहीं आपका उद्देश्य उस अंचल को साहित्य के केन्द्र में प्रतिष्ठित करना तो नहीं है, जिस तरह से रेणु ने ‘मैला आंचल’ उपन्यास के माध्यम से किया था।
मेरा मानना है कि हिंदी कथा साहित्य में क्षेत्रीय अस्मिता के स्वर को प्रबल बनाने के लिए जिस लेखक को श्रेय जाता है, निस्संदेह वह रेणु हैं। अगर मुझे दूसरा नाम लेना पड़े तो रेणु के बाद मैं राही मासूम रज़ा का नाम लूँगा। मैं पूरी ईमानदारी से यह स्वीकारता हूँ कि यदि मैला आँचल नहीं आया होता तो आज हिंदी कथा साहित्य में क्षेत्रीय अस्मिता का स्वर कहीं नज़र नहीं आता। इस स्वर को आधा गाँव उपन्यास ने और बल प्रदान किया। इसे मैं एक संयोग ही मानूँगा कि जिन उपन्यासों को पढ़कर मेरे लेखन में आपको क्षेत्रीय अस्मिता का स्वर नज़र आता है, वह स्वर मैला आँचल, आधा गाँव, काला जल, झीनी-झीनी बीनी चदरिया, परती परिकथा जैसे उपन्यासों की ही देन है, जिन्हें मैंने सबसे पहले पढ़ा। आपने पूछा है कि इस क्षेत्रीयता को उभारने के पीछे कहीं आपका उद्देश्य उस अंचल को साहित्य के केन्द्र में प्रतिष्ठित करना तो नहीं है? मेरा कहना है कि यह क्षेत्रीयता नहीं बल्कि आपके ही शब्दों में अस्मिता से जुड़ा सवाल है। यह सही है कि देश की राजधानी से सटे मेवात जैसे क्षेत्र की पहचान साहित्य तो छोड़िए दूसरे क्षेत्रों में भी नहीं थी। जो थी वह इतनी नकारात्मक कि मेवात का नाम सुनते ही लोगों की ऐसे भौहें तन जाती मानो यह इस देश का नहीं किसी अनजान टापू का हिस्सा हो। शायद काला पहाड़ ने हिंदी के पाठकों की इस नकारात्मक छवि और धारणा को तोड़ा बल्कि यहाँ तक कहा जाने लगा कि यदि असली मेवात को जानना है तो काला पहाड़ को पढ़ा जाए। आखिर यह असली मेवात क्या है? इन सवालों का उत्तर यह उपन्यास बखूबी देता है। यह उपन्यास उस मेवाती बोली या उपभाषा से पहली बार पाठकों को परिचित कराता है जिसे ग्रियर्सन ने भारत की आठ उपभाषाओं में शामिल किया था। किसी भी क्षेत्रीय अस्मिता के कुछ मज़बूत स्तंभ और निकष होते हैं जो उसे प्रबलता प्रदान करते हैं, जैसे वहां की बोली-बानी, लोक साहित्य, सांस्कृतिक-ऐतिहासिक संपन्नता और सामाजिक संरचना. मेवाती समाज इन सभी पक्षों का प्रतिनिधित्व करता है। मैंने मेवाती बोली का जिस तरह अपने पात्रों के द्वारा उपयोग किया, पाठकों ने सबसे ज्यादा उसे ही पसंद किया। इसके बारे में जाने-माने समालोचक डॉ. विजय बहादुर सिंह ने लिखा है- ‘भाषा के दुहरे-तिहरे रूपों ने यहाँ एक और रंगीन किस्सागोई को उभारा है। हिंदी भाषा के कितने-कितने रूप और छटाएं हो सकती हैं, इसे व्याकरणबद्ध एकरस नगरीय भाषाभाषी नहीं समझ सकता जो अपनी मृतप्राय, अभिजात और चिकनी पदावली में खुद लाचारी का अनुभव करने लग गया है। हिंदी भाषा की बेधक मार्मिकता कहीं उसकी बोलियों में है। काला पहाड़ हमें इसका अनुभव बार-बार कराता है। ‘इसी तरह मेरे एक कहानी संग्रह अस्सी मॉडल उर्फ़ सूबेदार की भूमिका में डॉ. नित्यानंद तिवारी ने लिखा है- ‘जीवन के उन पहलुओं और स्रोतों को देख लेना जहां भाषा, धर्म, जाति के भेद गल जाते हैं और स्थानीय लोकाचार, भिन्न जीवन-परंपरा बन लेते हैं साहित्यिक रचना एक आवश्यक शर्त है।’ तो जो तत्व एक रचना को क्षेत्रीय अस्मिता के स्वर को प्रबल बनाते हैं मेरे उपन्यासों और कहानियों में पूरी शिद्दत के साथ दिखाई देते हैं। सच तो यह है कि मौजूदा दौर अस्मिताओं और विमर्शों का दौर है। ऐसे में कोई कृति या किसी लेखक का लेखन इन्हें ताक़त प्रदान करता है तो यही लेखन की सार्थकता कहलाती है। यही कारण है कि डॉ. नामवर सिंह के संपादन में प्रकाशित हुई आधुनिक हिंदी उपन्यास नामक पुस्तक में जिन उपन्यासों को शामिल किया गया है, उनमें काला पहाड़ भी है। मैं यहाँ किसी उपन्यास या कहानी को आंचलिक या क्षेत्रीय सीमा में बांधने के सख्त खिलाफ हूँ। मैला आँचल को आंचलिक उपन्यास कहने पर रेणु बहुत परेशान होते थे। दरअसल, आंचलिक कह कर हम किसी रचना की रेंज को कम कर देते हैं, जबकि समस्याएँ, मनुष्य के दुःख-दर्द, उसकी पीड़ा नगरीय या ग्रामीण नहीं होती. वे सबकी एक जैसी होती हैं।
अटल तिवारी पत्रकारिता के प्राध्यापक हैं और दिल्ली में रहते हैं
बातचीत क्रमशः





[…] प्रेमचंद के बाद ऐसा कोई कथाकार नहीं हु… […]