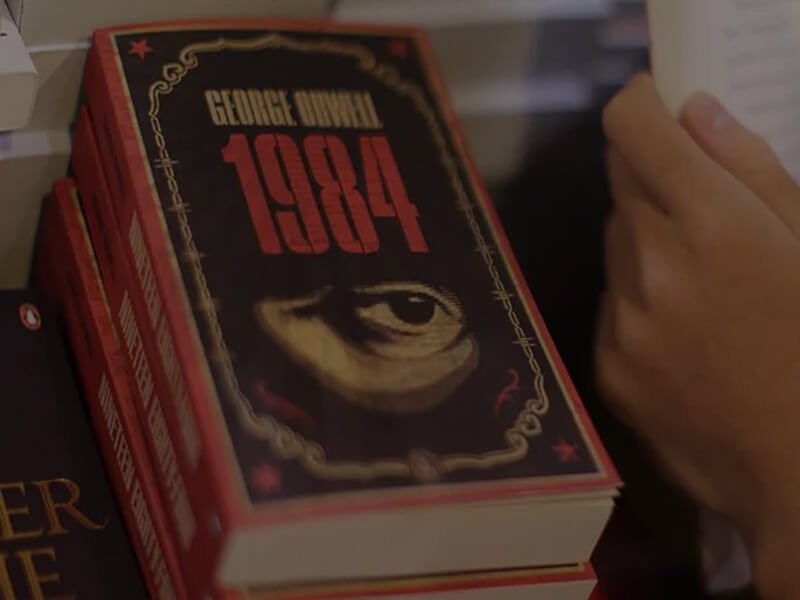बातचीत का तीसरा हिस्सा
लेखक का एक्टिविज्म से जुड़ना कितना जरूरी है ?
लेखक को हर उस चीज़ से जुड़ना चाहिए जो लोगों की ज़िन्दगी में सकारात्मक बदलाव लाए। चाहे वह राजनीति हो, सामाजिक कार्य या भ्रष्ट व्यवस्था के प्रति आक्रोश। राजनीति तो आज आम आदमी की रगों तक पैठ गई है। राजनीति का दोगलापन एक आम आदमी की आम दिनचर्या को भी प्रभावित करता है। एक ठेले वाला या पान वाला तक अपनी एक राजनीतिक समझ रखता है तो एक लेखक विचारधारा से हटकर लेखन कैसे कर सकता है। लेखक का पहला सरोकार अपने समय और समाज के प्रति है। वह लेखक अधिक असरदार होता है जो दोहरी ज़िन्दगी नहीं जीता। जो लिखता है, उस पर यकीन करता है और वही जीता है। जो लेखक अपने और अपने परिवार के प्रति ही ईमानदार नहीं होता, उससे किसी सामाजिक बदलाव की उम्मीद रखना एक खामखयाली है।
अक्सर देखा गया है कि अधिकांश लेखक इतने असामाजिक प्राणी होते हैं कि वे सिर्फ शाब्दिक क्रांति करते हैं, उनका वाक्जाल पाठकों को मोहता है और वह पूरे समाज की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लादते हुए समाज के प्रति अपनी जवाबदेही की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं पर अपने ही घर के सदस्यों के प्रति इस कदर गैर जिम्मेदार और गैर ईमानदार होते हैं कि उनका लेखन एक मोहक आवरण भर रह जाता है। आज इस मुहावरे को बदलने की ज़रूरत है कि लेखक समाज के आगे मशाल लेकर चलता है। कुछेक लेखक अपवाद स्वरूप बचे रह गए होंगे पर अधिकांश भ्रष्ट व्यवस्था, लंद–फंद, चाटुकारिता, पुरस्कारों की जोड़–तोड़, लेन–देन, औरतबाजी, मौकापरस्ती और दोगलेपन की लपेट में आ चुके हैं और इसे लेकर शर्मिन्दगी भी महसूस नहीं करते। यह सारा प्रपंच वे खुले आम डंके की चोट पर करते हैं।

एक्टिविज्म का एक रास्ता एन.जी.ओ. से होकर जाता है, क्या यह खतरनाक नहीं है ?
एक्टिविज्म के लिए एन.जी.ओ की जरूरत नहीं है। कम से कम ऐसे व्यक्ति हर शहर में उपस्थित हैं जो निस्वार्थ भाव से अपना काम करते हैं और बदले में किसी पुरस्कार, किसी प्रतिदान, किसी पहचान के मोहताज़ नहीं होते। सभी एन.जी.ओ भी एक जैसे नहीं होते। बहुत सा सार्थक काम भी वहां होता है। हां, यह ज़रूर है कि एन.जी.ओ को जिस तरह का आसान पैसा विदेश से फंडिंग के नाम पर मिल जाता है, उसे देखते हुए कुछ नॉन कमिटेड और नॉन सीरियस लोग समाज सेवा के नाम पर काम कम और दाम ज्यादा वसूलते नज़र आते हैंं। समाज में इस तरह की धांधली तो हर क्षेत्र में है। किस-किस पर ऊंगली उठाई जाए? जब चंद अच्छे लोग इस भ्रष्ट जमात में दिखाई दे जाते हैं तो लगता है–उम्मीद अभी बाकी है, सब कुछ चुक नहीं गया है।
[bs-quote quote=”अजीब बात है कि जब मैं किसी कथा समारोह या लेखकीय जमावड़े में जाती हूं तो अमूमन मेरा परिचय एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में दिया जाता है और जब मैं महिलाओं की कार्यशाला या किसी महिला अधिवेशन में जाती हूं तो मेरा परिचय हिन्दी की जानी मानी लेखिका कहकर करवाया जाता है।” style=”style-2″ align=”center” color=”” author_name=”” author_job=”” author_avatar=”” author_link=””][/bs-quote]
आप अपने को एक्टीविस्ट पहले मानती हैं या लेखिका ?
अपने बयालीस साल के लेखन काल में बहुत ही थोड़े से लेखन के बावजूद मैं पहले लेखिका ही हूं, बाद में कुछ और। हेल्प के साथ जुड़ जाना एक संयोग ही था। मैं अपने को खो रही थी। हेल्प ने मुझे अपने आप को तलाशने में मदद की और मैं बहुत सी अपने जैसी औरतों के सम्पर्क में आई जो अनजाने ही अपने आपको दूसरों की ज़िन्दगी संवारने–बनाने की प्रक्रिया में अपने आप को खो बैठती हैं और ऐसी औरतों के साथ संवाद करना ज़िन्दगी के रू–ब–रू खड़े होना था। यह एक चिकित्सा पद्धति थी जिसे करने से पहले प्रशिक्षण ज़रूरी था। इसने मुझे बहुत राहत पहुंचाई।

पिछले दो साल से मैं लगभग हर रोज़ डायरी लिख रही हूं। अपनी डायरी का एक पृष्ठ सुनाती हूं
इन दोनों के बीच मैं कहां हूं ?
अजीब बात है कि जब मैं किसी कथा समारोह या लेखकीय जमावड़े में जाती हूं तो अमूमन मेरा परिचय एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में दिया जाता है और जब मैं महिलाओं की कार्यशाला या किसी महिला अधिवेशन में जाती हूं तो मेरा परिचय हिन्दी की जानी मानी लेखिका कहकर करवाया जाता है। इन दोनों के बीच मैं कहां हूं? लेखिका कहलाए जाने में तो फिर भी मुझे ज्यादा संकोच नहीं होता क्योंकि मेरे जीवन भर की कमाई यही है अच्छा बुरा जैसा भी , थोड़ा बहुत ही सही , मैंने ज़िन्दगी भर बस यही एक काम –कागज काले करने का – किया है, पर सामाजिक कार्यकर्ता या एक्टीविस्ट कहलाए जाने में अब मुझे शर्मिन्दगी महसूस होने लगी है। यह अलग बात है कि औरतों की प्रताड़ना मुझे झकझोर कर रख देती थी और वह काम मेरी प्राथमिकता बन गया था। मैंने अपने लेखन को भी दूसरे नम्बर पर रखा । बुझी हुई औरतों के चेहरों पर एक मुस्कान या सुकून देखकर जो राहत या सुख मिलता है, वह एक कहानी लिखने से निश्चित रूप से बड़ा होता है। पर अब सचमुच लगता है कि एक्टीविस्ट होने के नाम पर मैं एक धब्बा हूं। दूसरी औरतों को अनाचार और अत्याचार से लड़ने के और अपना हक मांगने और सम्मानजनक रूप से जीने के तरीके सिखाती हुई मैंं अपनी निजी ज़िन्दगी में क्या हूं ? अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर और मुंह पर सेलोटेप लगाकर ज़िन्दगी के बेहतरीन पैंतीस साल काट दिए मैंने। अगर एक्टीविस्ट ऐसे होते हैं तो इससे अच्छी तो वे गांव खेड़े की अनपढ़ गंवार औरतें हैं जो अपनी ज़िन्दगी की बागडोर अपने हाथ में रखती हैं, मजदूरी करती हैं और घर भी चलाती हैं, बेवड़े पति को खाना खिलाती हैं, सिर ऊंचा करके जीती है और अपने आत्मसम्मान पर आंच नहीं आने देतीं। मैं लंबे पन्द्रह सालों तक पास पड़ोस, दुनिया-जहान की औरतों की बे’शुमार समस्याओं से जूझती हुई अपनी निजी परेशानियों को भूले रही, अपने जीने को मुल्तवी कर उनके जीने के रास्ते तलाशती रही। उनके चेहरे पर लौटती मुस्कान में मैंने अपनी मुस्कान के अक्स देखे। आज जब ऐसी औरतें अपने ज़िन्दा रह पाने और सिर उठाकर जीने के अहसास से मुग्ध मेरे पांव छू लेती हैं या मेरे लिए उपहार ले आती हैं तो मैं ज़मीन में गड़ जाती हूं। इन्हें राह दिखाने की कोशिश में अपनी ज़िन्दगी के साथ क्या किया मैंने? इस सारी प्रक्रिया में अपने होने को पूरी तरह नकारते हुए, अपनी निजी ज़िन्दगी को मैंने एक ऐसे अंधेरे कोने में धकेले रखा, जहां से वह मुझे दिखाई न दे, मुझसे कोई सवाल न पूछे और कागज सा बारीक सुरक्षा कवच, अपने इर्द गिर्द लपेटे हुए यह मानकर निश्चिंत रही कि औरतों की इस सुरसा की तरह फैली समस्याओं के बीच वह अपने कागजी कवच के भीतर महफूज़ है। सचमुच वह कागजी कवच ही था, छूते ही इस कदर भुरभुरा कर ढहा कि लगा वह कहीं था ही नहीं , उसके होने का भरम भर था और भरम तो एक झिल्ली भर होता है– हटा कि चीज़ों का खुला नंगापन आंखों को चुभने लगता है।

आपकी कहानी कैसे बनती है ?
इधर तो कहानियां लिखना बहुत कम हो गया है। औरत की दुनिया स्तंभ न होता तो शायद दुबारा लेखन में एक स्थायी अवरोध आ जाता। निजी दुनिया और लेखकीय दुनिया में टकराव चलता रहता है। कलम कई बार निजी दुनिया के झंझावातों में पतवार का काम करती है। कहानी तब तक नहीं लिखी जाती जब तक वह खुद बगावत कर सिस्टम से बाहर आने के लिए छटपटाने न लगे। कभी कोई कहानी एक सिटिंग में लिख ली जाती है– जैसे रहोगी तुम वही, कभी दस-पन्द्रह दिनों में, कभी एक कहानी को पूरा करने में कई साल लग जाते हैं। मैं उस तरह से बहुत दस से पांच की रूटीन बनाकर लिखने वालों में से नहीं हूं । इसीलिए मेरा लेखन नियमित नहीं हो पाता।
यह भी पढ़ें :
https://gaonkelog.com/i-tried-to-analyze-and-empower-the-different-layers-of-female-torture/
रहोगी तुम वही और सत्ता संवाद कैसे लिखी गई ?
रहोगी तुम वही 1993 में बारह साल की लम्बी चुप्पी के बाद लिखी गई। इन बारह सालों में मैंने किसी साहित्यिक पत्रिका में एक ख़त तक नहीं लिखा था। 1980 में मैंने बोलो, भ्रष्टाचार की जय कहानी लिखी थी। उसके बाद कुछ पारिवारिक निजी समस्याओं में लेखन पर पूर्णविराम लग गया, लेकिन न लिख पाने की एक बेचैनी और हताशा तोे मन में थी। रहोगी तुम वही की थीम लंबे अरसे से दिमाग़ में थी पर इसके लिए फॉर्मेट नहीं मिल रहा था। जैसे ही यह एकालाप शिल्प दिमाग़ में आया एक सिटिंग में कहानी लिख ली गई। कहानी जब हंस में छपी, मुझे यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि बारह साल के लंबे अंतराल के बाद भी पाठक मुझे भूले नहीं थे और इस कहानी पर सबसे उत्साही प्रतिक्रिया मैत्रेयी पुष्पा की मिली , जिन्होंने बेधड़क कहा कि उन्हें अपनी कहानी बारहवीं रात के लिए इस कहानी से प्रेरणा मिली। इस कहानी पर मिली कुछ नाराज़ प्रतिक्रियाओं के एवज में कहानी सत्ता संवाद लिखी गयी जब कुछ पुरुष ने कहा कि क्या बालने वाला पक्ष हमेशा पुरुष का ही होता है? क्या औरतें बोलती ही नहीं हैं ? मैंने कहा–बोलती क्यों नहीं पर वे ही औरतें बोल पाती हैं जिनके हाथ में अर्थ सत्ता हो। इस कहानी पर मेरी अग्रज और आत्मीय मित्र मन्नू जी ने हंसकर कहा –सुधा, तेरी इस कहानी को पढ़कर तो मुझे अपना समय याद आ गया। लगा जैसे तूने बिल्कुल मेरे संवाद लिख दिए हैं। मेरी ज़बान पर ऐसे ही छुरी कांटे उग आते थे जब कॉलेज से थकी हारी लौटकर घर भी संभालना पड़ता था, कई बार राजेंद्र को कड़वाहट में बहुत कुछ बोल जाती थी।
फिर भी दोनों कहानियों को पढ़कर यह आरोप तो मुझ पर लगाया ही जा सकता है कि जहां सिर्फ पुरुष बोलता है, वहां भी लेखिका की पक्षरता स्त्री के साथ है और जहां स्त्री बोलती है, वहां भी पुरुष सहानुभूति का पात्र नहीं बनता।
[bs-quote quote=”कई बार हम व्यक्तिगत जीवन में जो नहीं है या नहीे हो पाए, वह हमारे गढ़े हुए चरित्रें में दिखाई दे जाता है। कई बार व्यक्तिगत जीवन में कुछ निर्णय नहीं ले पाते पर हमारे पात्र वे निर्णय लेते दिखाई देते हैं। कभी कभी कोई चरित्र जिसे हम गढ़ना शुरु तो अपनी एक काल्पनिक तस्वीर से करते हैं पर स्थितियो के आगे बढ़ते चले जाने में वह पात्र लेखक के हाथ से बाहर छूट निकलता है।” style=”style-2″ align=”center” color=”” author_name=”” author_job=”” author_avatar=”” author_link=””][/bs-quote]
क्या आपके पात्र जब विद्रोही दिखाई देते हैं तो वह आपके व्यक्तिगत जीवन का विद्रोह है ? क्या आपके व्यक्तिगत जीवन में निर्णय न ले पाने की क्षमता पात्र् को कमजोर करती है ?
नहीं, कई बार हम व्यक्तिगत जीवन में जो नहीं है या नहीं हो पाए, वह हमारे गढ़े हुए चरित्रें में दिखाई दे जाता है। कई बार व्यक्तिगत जीवन में कुछ निर्णय नहीं ले पाते पर हमारे पात्र वे निर्णय लेते दिखाई देते हैं। कभी कभी कोई चरित्र जिसे हम गढ़ना शुरु तो अपनी एक काल्पनिक तस्वीर से करते हैं पर स्थितियों के आगे बढ़ते चले जाने में वह पात्र लेखक के हाथ से बाहर छूट निकलता है। लेखक कई बार वह विद्रोह नहीं दिखा पाता जो उसके पात्र करते हुए दिखते हैं। कई बार लेखक खुद भी अपने पात्र के चरित्र के ग्राफ से कुछ सीखता है– ठीक वैसे ही जैसे पाठक सीखता है क्योंकि अन्तत: हर पात्र लेखक के अपने जीवन या अपनी वैचारिक अवधारणा की अभिव्यक्ति नहीं होता। वह एक स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है।

अन्नपूर्णा निराशा में मृत्यु का वरण करती है फिर भी कहती है– ’ये दोनों अगर आसमान छूना चाहें …… इन्हें रोकना मत।’ यह कैसे कह गई अन्नपूर्णा ? क्या यह आरोपित नहीं लगता ?
आपका यह प्रश्न मुझे हैरत में डाल रहा हैे। आपने कहानी को बहुत बारीकी से पढ़ा है। कहानी जब वागर्थ में प्रकाशित हुई थी, सचमुच यह वाक्य उसमें नहीं था। लेकिन कहानी का पाठ जब मैंने वकोला स्थित ‘वीमेन्स सेंटर’ में किया, कई औरतों ने कहा कि पूरी तरह हताशा से भरी इस कहानी में कोई तो एक आशा का तंतु दिखाई दे। मुझे भी लगा कि जिस लड़की की सबसे बड़ी तकलीफ यह थी कि रेलवे की स्थायी सरकारी नौकरी वाले एक अदद सुदर्शन वर का रिश्ता आते ही उसे बी.ए. की सालाना परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया और दूसरे दर्जे की आरक्षित श्रेणी में बिठाकर विदा कर दिया, वह अवश्य यह चाहेगी कि उसकी बेटियों को पनपने के पूरे अवसर दिए जाएं। यह वाक्य निश्चत रूप से आरोपित लगता है लेकिन यह लेखकीय जिम्मेदारी के तहत जरूरी भी लगा।
बेशक इस वाक्य को लेखक का एक वक्तव्य मान लें जो कहानी के लिए गैर ज़रुरी हो सकता है पर इस कमेन्ट के बिना कहानी अधूरी रहती।
क्रमशः

पल्लव जाने-माने युवा आलोचक और बनास जन पत्रिका के संपादक हैं। फिलहाल वे हिन्दू कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं।