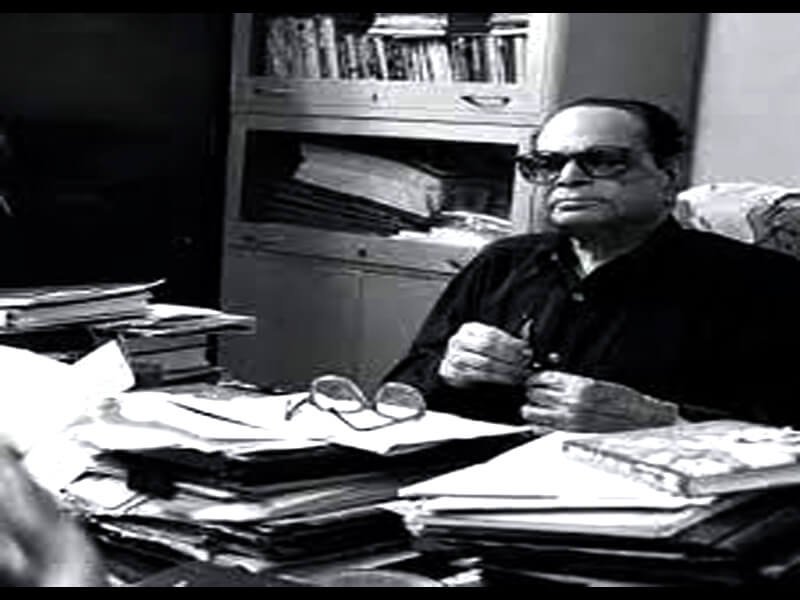(राजेंद्र यादव को दिवंगत हुये आठ वर्ष हो गए। बेशक इन आठ वर्षों में सुसंबद्ध और निर्भीक ढंग से भारत की संघर्षशील जनता की बात करनेवाली एक महान आवाज हमारे बीच नहीं है। वे हिन्दी के एकमात्र ऐसे बुद्धिजीवी थे जिनके सोच के दायरे में समूचा देश ही नहीं, सारी दुनिया और सारी इंसानियत थी। वे बातों में किसी का लिहाज नहीं करते थे और जिन मौकों पर अमूमन लोग आत्ममुग्ध और आत्मलिप्त हो जाया करते हैं वहाँ भी वे अपने से बाहर निकलकर बात को एक व्यापक आयाम दे देते थे। मुझे याद है एक बार साहित्य अकादेमी ने इंडिया इन्टरनेशनल सेंटर के सभागार में उनके व्यक्तित्व और लेखन को लेकर एक कार्यक्रम रखा। यह अकादेमी का नियमित कार्यक्रम था और मैं आधा दर्जन से अधिक लेखकों के कार्यक्रम सुन चुका था। प्रायः लेखक का जीवन-संघर्ष और उसकी सफलताएँ ही वहाँ का विमर्श होती थीं। और यह स्वाभाविक भी था। लेकिन राजेंद्र जी ने वहाँ अपने विषय में एक शब्द नहीं कहा। उन्होंने वर्तमान अभिभावकत्व और नई पीढ़ी के भविष्य को लेकर बेमिसाल वक्तव्य दिया। लगभग सवा घंटे वे शानदार ढंग से बोले और इस बात पर सवाल उठाया कि आखिर हमारे लिखे हुये का मतलब क्या है जब सारा भविष्य बाज़ार के रथ पर सवार साम्राज्यवाद के जबड़े में ही जाने वाला है। आखिर इससे लड़ने की हमारे पास परियोजना क्या है?
राजेंद्र यादव एक व्यक्ति और लेखक-संपादक के रूप में लाखों के प्रिय हैं और हमेशा रहेंगे। और इसी के साथ वे हजारों के लिए अप्रिय भी हैं और रहेंगे क्योंकि समाज के बड़े हिस्से की पक्षधरता और उसके उत्पीड़कों की खुलकर आलोचना की। उन्होंने अनगिनत लेखक-लेखिकाओं को मंच दिया। राजेंद्र जी ने केवल ब्राह्मणवाद, हिन्दुत्व और सामंतवाद के खिलाफ ही मोर्चा नहीं खोला बल्कि एक सोये हुये समाज को झकझोरकर जगाने का भी काम किया। उनकी अपनी संपादकीय परियोजना थी और वे सड़े-गले मूल्यों और व्यवस्थाओं को बेरहमी से बेनकाब किया। मुझे हमेशा उनकी वह निर्भीकता अपनी ओर खींचती है जो उनके लेखों की जान थी और जिसके कारण वे बात की उस तह तक पहुँचते थे जो अपनी संरचना के कारण छूट जाती अथवा निहित स्वार्थों के कारण छोड़ दी जाती है। आज उनकी 92वीं जयंती पर हम उनका एक छोटा सा किन्तु बेहतरीन संपादकीय प्रस्तुत कर रहे हैं। यह संपादकीय इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह जाति व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में ही नहीं बल्कि फासीवादी-पूंजीवादी परिप्रेक्ष्य में भी अत्यंत प्रासंगिक है। यह शोषक-शोषित और उत्पीड़क-उत्पीड़ित के बीच के स्पष्ट अंतर्विरोध को यादगार तरीके और मुहावरे में रखता है। – संपादक)
डॉ. अम्बेडकर पर आरोप लगाया जाता है कि जब गाँधीजी जैसे लोग स्वाधीनता संग्राम में लगे थे, अंग्रेजों से लड़ रहे थे, तब अम्बेडकर अंग्रेजों से मिलकर दलितों के लिए अलग ही खिचड़ी पका रहे थे। दूसरे शब्दों में वे सरकार के पिट्ठू थे। सुनते हैं, किसी पुराने कांग्रेसी नेता ने यह बात बंगलौर या महाराष्ट्र की एक सभा में उठाई तो दलित-समूह ने उत्तेजित होकर उनकी दुर्गति कर डाली। जितनी ग़लत ‘अपने त्राता’ के विरुद्ध कुछ भी न सुनने वाले दलितों की उत्तेजना थी, उतना ही झूठा और अनैतिहासिक नेताजी का वक्तव्य था। दलित सबसे पहले और हज़ारों सालों से मूलत: सवर्णों और ऊँची जातियों के अन्यायों, अत्याचारों और नृशंसताओं के ग़ुलाम थे। उनके लिए ‘स्वतंत्रता’ का वह अर्थ हो ही नहीं सकता था जो सवर्ण-वर्चस्व वाली कांग्रेस के लिए था। बल्कि कांग्रेसी ‘स्वतंत्रता’ में उन्हें अपने लिए और भी भयंकर यातनाओं, अत्याचारों की ‘स्वतंत्रता’ ही दिखाई देती थी। किसी भी स्थिति में वे दो मोर्चे एक साथ खोलने की हालत में नहीं थे। स्पष्ट ही अंग्रेजों और सवर्णों से मुक्ति उनके लिए दो अलग और समानांतर धरातलों पर लड़ी जाने वाली लड़ाइयाँ थीं। विकल्प यही था कि गाँधीवादी रूमानी आदर्शों की झोंक में ‘फिलहाल आपसी और भीतरी’ लड़ाई स्थगित करके वे कांग्रेस के स्वाधीनता संग्राम में शामिल हो जाते और सवर्ण नेताओं के पाख़ाना-पेशाब उठाते, बर्तन-कपड़े साफ करते और अलग बैठकर बाद में उनकी जूठन खाते हुए मन में समझते कि एक बड़े संग्राम में उनका भी योगदान है। (क्योंकि ‘हर व्यक्ति अपना हर काम खुद करें’ का कार्यक्रम कभी आंदोलन नहीं बना, केवल साबरमती आश्रम में ही कैद रहा और अपनी मौत मर गया) । यहाँ उनकी तक़दीर सवर्ण कांग्रेसी नेताओं पर निर्भर थी कि वे अभी जैसा है वैसा ही चलने दें और स्वतंत्र हो जाने पर अधिक मानवीय व्यवहार, न्याय और करुणा के आदर्श रखते हुए ऊँचों के हृदय परिवर्तन करें-
दूसरा रास्ता था कि अंग्रेजों के साथ और संरक्षण में पहले ख़ुद संगठित और सक्षम होकर सवर्णों की ग़ुलामी से मुक्त हों और यही सोच अम्बेडकर की ही क्यों, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन राय, बंकिम चंद्र, दयानंद इत्यादि की नहीं थी? क्या वे अंग्रेजों के संरक्षण में ही ‘समाज सुधार’ के कार्यक्रम नहीं चला रहे थे? सारी वैचारिक तेजस्विता के बावजूद विवेकानंद ने भी औपनिवेशिक सत्ता से टकराव बचाया ही और सर राधाकृष्णन को देश का राष्ट्रपति बनाते समय क्या किसी ने पूछा था कि स्वतंत्रता-संग्राम में वे कहाँ थे? आखिर यह दुमुँहापन हर जगह कैसे चलेगा कि युद्ध के प्रारम्भ में जब गाँधीजी और कांग्रेस सरकार के लिए रंगरूट भर्ती कराएँ, उसे मदद दें तो ‘देशभक्त’ और जब सन 1942 में हिटलर के फ़ासिज्म के ख़िलाफ़ कम्युनिस्ट ब्रिटेन का समर्थन करें तो ‘देशद्रोही’। कल्पना कीजिए, लाखों-करोड़ों मौत की सजा पाए कैदियों से भरी एक जेल है और अचानक दुश्मन हमला कर देता है, ऐसे में ये सारे के सारे कैदी जेल तोड़कर हमलावरों से न जा मिलें तो क्या करें? क्या इन्हें सिर्फ़ इसीलिए अपनी मौत का चुपचाप वरण कर लेना चाहिए कि वह उनकी अपनी सरकार दे रही है? यहाँ दुश्मनों से जा मिलना ‘राष्ट्रद्रोह’ नहीं, एक अन्यायी व्यवस्था के ख़िलाफ़ विद्रोह है। हो सकता है सुभाषचंद्र बोस जैसा अदूरदर्शी विद्रोह हो। गम्भीर से गम्भीर अपराध करने वाले कैदियों को तो कभी-कभी विजय इत्यादि के सुअवसरों पर मुक्त कर दिया जाता है, दलितों को तो ऐसी मुक्ति की भी आशा नहीं थी। यह तो स्वयं गाँधी जैसे क्रांतदर्शी और कांग्रेसी नेताओं को समझना चाहिए था कि विभीषण, जयचंद और मीर जाफ़र दुश्मनों के साथ मिलकर व्यक्तिगत ‘मोक्ष’ पा रहे थे, अम्बेडकर एक पूरे विराट समुदाय की मुक्ति मांग रहे थे। मगर जब आज इतने जागरूक, मानवीय और प्रबुद्ध हो जाने पर भी कुछ लोग भारतीय संस्कृति या देशहित के नाम पर सामंती व्यवस्था और सवर्ण हितों को ही सारे देश पर लादने का आग्रह करते हैं, तो साठ-सत्तर साल पहले के सवर्ण नेताओं की आँखों पर चढ़ी सामंती चर्बी का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। और क्या आज अवाजों (अडवानी, वाजपेयी, जोशी) की सवर्ण दहाड़ें सुनकर नहीं लगता कि इस निरंकुश स्वतंत्रता को लेकर अम्बेडकर का डर कितना सही, दूरदर्शी था। वर्ण और वर्ग स्वार्थों से अंधी नौकरशाही और न्यायपालिका से वे क्या उम्मीद कर सकते थे? अभी-अभी सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण-विरोध में आत्मदाह की कोशिश करने वाले राजीव गोस्वामी को तीन लाख का मुआवजा दिया है, रोज़ भूमिहीन मजदूरों और बंधुआ गुलामों के हितों के लिए लड़ने वाले नक्सली कहकर फाँसी पर चढ़ाए जाते हैं और ज़मींदारों-साहूकारों को मिलता है संरक्षण, भरपाई, मुआवज़ा और कानूनी-संरक्षण।
(मेरी तेरी उसकी बात, हंस, अक्तूबर 1991)