बातचीत का चौथा और अंतिम हिस्सा
भालचन्द्र नेमाडे को ज्ञानपीठ सम्मान देने के लिए आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि नरेन्द्र मोदी थे, जिसकी अध्यक्षता प्रगतिशील लेखक संघ के लम्बे समय तक अध्यक्ष रहे आलोचक नामवर सिंह ने की। उसी समारोह में यह बखान भी किया गया कि मोदी कवि और साहित्यकार भी हैं। ज्ञानपीठ के मंच से संचालक द्वारा किया गया मोदी का यह बखान आखिर हिंदी लेखकों की कौन सी छवि पेश कर रहा है?
जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि हमारे ज़्यादातर लेखक संघ एक तरह से वृद्धाश्रमों में तब्दील होकर रह गए हैं। दूसरा मैंने कहा है कि हिंदी के लेखक की आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं और उसकी दौड़ इतनी छोटी होती है कि वह कहाँ और कब फिसल जाए कुछ नहीं कह सकते। छोटे-छोटे स्वार्थों के लिए वह अपनी तथाकथित वैचारिकता को ताख पर रख कुछ भी समझौता कर सकता है। वास्तव में मौजूदा दौर वैचारिक द्वंद्व का है। रही बात भारतीय ज्ञानपीठ की तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह संस्था एक निजी प्रकाशन संस्था है। एक ऐसी संस्था जिसे हम अन्य प्रकाशन संस्थानों की तरह निजी दुकान भी कह सकते हैं। साहित्य और वैचारिक प्रतिबद्धता का उससे क्या वास्ता। यह उसका निजी विचार और उसकी निजी खोज है कि वह किसको लेखक मानती है और किसको नहीं। देश के प्रधानमंत्री को लेखक मानना या बताना इनकी कुछ विवशता भी हो सकती है, और जब विवशता आड़े आती है तो आदमी किसी को कुछ भी मान सकता है।
यह भी पढ़ें :
पुरुषों के पेटूपन और भकोसने की आदत ने औरतों को नारकीय जीवन दिया है !
पिछले कुछ समय से जिस तरह शिक्षा का भगवाकरण किया जा रहा है। किताबों, लेखकों और कलाकारों को कट्टरपंथी ताकतों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है और उस पर लेखकों, लेखक संगठनों और समाज का एकजुट न होना क्या यह नहीं साबित करता है कि आने वाले समय में और बड़ी चुनौती पेश आने वाली है?
अपने एक सवाल में आपने मेरे हवाले से कहा है कि वामपंथी लेखक संगठनों की भूमिका वृद्धाश्रम से अधिक नहीं रह गई है। वह महज कुछ लेखकों के हस्ताक्षर अभियान के मंच बनकर रह गए हैं। यह उस सच्चाई को प्रमाणित करता है जैसा मैंने कहा था। आप कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ़ हमारे लेखकों, लेखक संगठनों के एकजुट न होने की जो बात कर रहे हैं, तो उसके संदर्भ में सबसे पहले यह देखना होगा कि जिन लेखक संगठनों और उनसे जुड़े लेखकों से इस एकजुट की अपेक्षा की जानी चाहिए, वे तो खुद उन्हीं के आयोजनों में दावतें उड़ाते देखे जा रहे हैं. आखिर लेखक संघ भी तो इन्हीं लेखकों से मिल कर बने हैं। अगर इनके पदाधिकारी ही इन आयोजनों में जा रहे हैं तो फिर किससे उम्मीद की जाए. रही बात लेखकों, लेखक संगठनों और समाज के एकजुट न होने से आने वाले समय में पैदा होने वाली चुनौतियों की, तो एक लेखक के रूप में हमें खुद अपने गिरेबान में झाँक कर देखना चाहिए कि एक लेखक की आज उसके अपने समाज में क्या हैसियत रह गई है। जैसाकि एक आम नागरिक अगर समाज में किसी पर सबसे ज्यादा भरोसा करता
[bs-quote quote=”रही बात भारतीय ज्ञानपीठ की तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह संस्था एक निजी प्रकाशन संस्था है। एक ऐसी संस्था जिसे हम अन्य प्रकाशन संस्थानों की तरह निजी दुकान भी कह सकते हैं। साहित्य और वैचारिक प्रतिबद्धता का उससे क्या वास्ता। यह उसका निजी विचार और उसकी निजी खोज है कि वह किसको लेखक मानती है और किसको नहीं। देश के प्रधानमंत्री को लेखक मानना या बताना इनकी कुछ विवशता भी हो सकती है, और जब विवशता आड़े आती है तो आदमी किसी को कुछ भी मान सकता है। ” style=”style-2″ align=”center” color=”” author_name=”” author_job=”” author_avatar=”” author_link=””][/bs-quote]
है, तो एक लेखक पर करता है। लेकिन यह भरोसा भी समाज में तेज़ी से ख़त्म होता जा रहा है। समाज में हो रहे अच्छे-बुरे को लेकर लेखक का जो हस्तक्षेप होना चाहिए वह मात्र उसके हस्ताक्षर अभियान का हिस्सा बन कर रह गया है। ईमानदारी से देखें तो राजेन्द्र यादव के बाद आज हिंदी समाज में कोई पब्लिक इंटेलेक्चुअल नहीं है। जो होने का दावा करते हैं वे वास्तव में उन्हीं ताकतों के लिए काम करते हैं, जिसकी आपने बात की है। मुझे लगता है कि जब तक हमारे लेखक संघों को सवर्णवादी मानसिकता, सोच वाली ताकतों और एनजीओ संस्कृति से मुक्ति नहीं मिलेगी यह चुनौती और ज्यादा बड़ी होती चली जायेगी। मगर लगता है हमारे लेखक संघ इसके लिए तैयार नहीं हैं।
हिंदी प्रकाशन जगत में बड़ी मात्रा में स्तरहीन चीजें छप रही हैं। एकाएक एक ऐसी संस्कृति का उदय हुआ है कि कुछ तथाकथित सेलीब्रेटी, जो स्वभाव से लेखक नहीं हैं उन्हें भी लेखक बनाने का प्रयास किया जा रहा. दावा तो यह भी है कि उनकी हजारों में पुस्तकें बिक रही हैं और ये साठ-गांठ से पुस्तकालयों में पहुंचने भी लगी हैं। ऐसे में पाठकों (खासकर नए) के हाथ स्तरीय रचना पहुंचना मुश्किल होता जा रहा है। इस मसले पर बड़े से लेकर छोटे लेखक तक चुप्पी साधे हैं क्योंकि अधिकांश बड़े प्रकाशक बड़े लेखकों को अपने कब्जे में किये हैं। लेकिन क्या यह लेखकों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वह प्रकाशकों के इस गोरखधंधे के खिलाफ आवाज उठाएं?
यह सारा बाज़ार का खेल है जिसमें हम अच्छे-बुरे, नैतिक-अनैतिक, स्याह और सफ़ेद में अंतर करना भूल जाते हैं। बाज़ार का एक सिद्धांत और है कि उसमें प्राय: उसी को जगह मिलती है जो चमकती है। जिस तरह के तथाकथित सेलीब्रेटीज़ लेखन को बढ़ावा देने की बात है ऐसा नया नहीं है। दरअसल हम भूल जाते हैं प्रकाशक एक व्यापारी है वह वही छापेगा और बेचेगा जैसा उसके सलाहकार सलाह देते हैं। एक समय था जब हिंदी का प्रकाशक अपने यहाँ कुशल, भाषा मर्मज्ञ और साहित्य की गहरी समझ रखने वाले संपादक रखते थे, जिनसे लेखक बहुत कुछ सीखता था। पांडुलिपियों का इतनी कुशलता से संपादन करते थे कि खुद लेखक को ही पता नहीं चलता था कि उसकी मूल रचना में कहाँ-कहाँ संपादन हुआ है। लेकिन अब इनकी जगह इवेंट मैनेजर और सेल्स मैनेजर किस्म के तथाकथित सलाहकारों ने ले ली है, जो प्रकाशक को एक अलग दुनिया के सब्ज़बाग दिखाकर फ़िल्मी हस्तियों, राजनेताओं की तथाकथित आत्मकथाओं, अकबर-बीरबल के किस्से, हास्य-व्यंग्य के नाम पर विदूषक किस्म के कवियों और बड़े-बड़े ओहदों पर प्रस्थापित अफसरों और तथाकथित सेलीब्रेटीज़ की रचनाओं के साथ-साथ मेरठ से छपने वाले लुगदी साहित्य के लेखकों को प्रकाशित करने के लिए न केवल प्रोत्साहित करते हैं, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से तैयार भी करते हैं।
[bs-quote quote=”ब्रज के सबसे बड़े कवि अब्दुर्रहीम खानखाना की मां एक मेव सरदार हसन खां मेवाती की भतीजी थी। वही हसन खां मेवाती जिसने एक बाहर से आये हममज़हबी आततायी बाबर द्वारा आग्रह करने के बावजूद राणा सांगा के खिलाफ नहीं, बल्कि राणा सांगा के साथ मिलकर बाबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी। कितनों को पता है कि आज भी महाभारत पर आधारित ‘पंडून को कड़ा’ मेवात के मेवों में गाया-बजाया जाता है? कितनों को मालूम है कि आज भी मेवों में एक बहन अपने भाई से भात लेते समय वही गीत गाती है, जो पश्चिम-उत्तर भारत के हिन्दू परिवारों में गाया जाता है? ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो मेवात की सामाजिक समरसता और भाईचारा वाले विश्वास को दर्शाते हैं। दरअसल, हमारे सामाजिक समरसता के पहले सूत्र हमारे अपने समाज में छिपे हुए हैं. यह मेवात जैसे क्षेत्रों का दुर्भाग्य है कि यह सामाजिक समरसता और भाईचारा वाला विश्वास पिछले ढाई दशक, खासकर रथयात्रा, वह भी 1992 में विवादित राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद के ढहाने के बाद बड़ी तेज़ी से दरका है।” style=”style-2″ align=”center” color=”” author_name=”” author_job=”” author_avatar=”” author_link=””][/bs-quote]
रही बात प्रकाशक की सो उस बेचारे को ‘चार आने का तेल, तेल के चार आने’ करने से ही फुर्सत नहीं है इसलिए आसानी से वह इनके झांसे में आ जाता है। इन सलाहकारों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि इनकी हैसियत मालिकों से भी ज़्यादा हो गई है और लेखकों से ये जिस ऊंचाई से बात करते हैं, वह तो हैरान करती है। अगर आपको यक़ीन नहीं है तो पिछले कुछ वर्षों की हिंदी में प्रकाशित पुस्तकों को उठाकर देख लीजिये। इस पर तुर्रा यह कि हिंदी में पाठक नहीं हैं। रही बात इस मसले पर बड़े से लेकर छोटे लेखक तक चुप्पी साधने की, तो वह समय गया जब हमारे बड़े लेखकों की ऐसे मामलों में कोई हैसियत होती थी। अब
तो अधिकांश बड़े प्रकाशक बड़े लेखकों को अपने कब्जे में किये हुए हैं। इसलिए उनसे किसी तरह की अपेक्षा करना बेमानी है। अक्सर ऐसे मामलों में हमारा लेखक खामोश रहता है। कहीं न कहीं यह उसके भीतर का वह असुरक्षा बोध है जो प्रकाशकों के खिलाफ उसे बोलने से रोकता है। मेरा तो स्पष्ट मानना है कि एक लेखक के लिए जितना ज़रूरी प्रकाशक है, उससे कहीं ज्यादा प्रकाशक को लेखक की ज़रूरत है। लेखक के पास तो जीवनयापन के अनेक साधन हो सकते हैं मगर प्रकाशक का तो एकमात्र साधन और माध्यम लेखक ही है बल्कि अकेला प्रकाशक ही नहीं उसके यहाँ कार्यरत वे कर्मचारी भी लेखक पर आश्रित हैं जिनका परिवार उससे चलता है। यह बात लेखक और प्रकाशक दोनों को समझने की ज़रूरत है। मगर दुर्भाग्य से आज लेखक की हैसियत किसान और प्रकाशक की भूमिका महाजन जैसी हो गई है। लेखक की अपने समाज में क्या हैसियत है हम सब जानते हैं। यह सही है कि जातिवाद, सांप्रदायिकता, वर्ण व्यवस्था, सामंतवाद, शोषण के खिलाफ़ सबसे ज्यादा अगर समाज की कोई इकाई आवाज़ बुलंद करता है, तो वह है लेखक। मगर इसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि अपने ही समाज में इन व्याधियों का सबसे ज्यादा शिकार भी वही होता है।
यह भी पढ़ें :
आप मेवात (हरियाणा) से आते हैं और अपने कथा-साहित्य में मेवात को पूरी शिद्दत के साथ जीते भी हैं। मेवात की जमीन ने सामाजिक समरसता और भाईचारा वाला विश्वास कायम रखा है। आपसी मेलजोल के लिए मेवात की जमीन अलग तरह की मानी जाती रही है, लेकिन पिछले कुछ समय से पश्चिमी भारत में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं में तेज़ी से वृद्धि हुई है। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से मानी जाती है। इसी कड़ी में राजस्थान के मेवात स्थित गोबिंदगढ़ , उत्तर प्रदेश के कोसीकलां और हाल में हरियाणा के बल्लबगढ़ के अटाली गाँव में हिंसा की घटना शामिल है। आपने मेवात में 1992 के दौरान घटी घटनाओं का अपने पहले उपन्यास ‘काला पहाड़‘ में जिस तरह इस सामाजिक समरसता और भाईचारा वाले विश्वास का मार्मिक वर्णन किया है वह अप्रितम है। क्या कारण है कि मेवात में भी अब रिश्तों और संबंधों का ताना-बाना टूट रहा है और इसे कैसे बचाया जा सकता है?
आपने सही कहा है कि मेवात की ज़मीन सामाजिक समरसता और भाईचारे वाले विश्वास के लिए जानी जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह मुझे मेवात की वह सांस्कृतिक संपन्नता और वह सामुदायिक परंपरा रही है जो भारतीय समाज की सबसे बड़ी ताक़त है। पता नहीं कितने लोगों को मालूम है कि ब्रज के सबसे बड़े कवि अब्दुर्रहीम खानखाना की मां एक मेव सरदार हसन खां मेवाती की भतीजी थी। वही हसन खां मेवाती जिसने एक बाहर से आये हममज़हबी आततायी बाबर द्वारा आग्रह करने के बावजूद राणा सांगा के खिलाफ नहीं, बल्कि राणा सांगा के साथ मिलकर बाबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी। कितनों को पता है कि आज भी महाभारत पर आधारित ‘पंडून को कड़ा’ मेवात के मेवों में गाया-बजाया जाता है? कितनों को मालूम है कि आज भी मेवों में एक बहन अपने भाई से भात लेते समय वही गीत गाती है, जो पश्चिम-उत्तर भारत के हिन्दू परिवारों में गाया जाता है? ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो मेवात की सामाजिक समरसता और भाईचारा वाले विश्वास को दर्शाते हैं। दरअसल, हमारे सामाजिक समरसता के पहले सूत्र हमारे अपने समाज में छिपे हुए हैं. यह मेवात जैसे क्षेत्रों का दुर्भाग्य है कि यह सामाजिक समरसता और भाईचारा वाला विश्वास पिछले ढाई दशक, खासकर रथयात्रा, वह भी 1992 में विवादित राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद के ढहाने के बाद बड़ी तेज़ी से दरका है। 1990 के दौरान निकाली गई रथ यात्रा से इस देश के अल्पसंख्यकों में जो भय पैदा हुआ था, वह 1992 में देखने को मिला। यहाँ एक दिलचस्प तथ्य यह है कि मेवात में जितनी भी हिंसक घटनाएँ हुईं हैं वे मेवात के सीमांत में हुई हैं यानी जहां-जहां मेव अल्पसंख्यक की स्थिति में हैं वहां ये घटनाएं हो रही हैं। एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि इन सांप्रदायिक घटनाओं में हिन्दुओं की ओर से जो समुदाय प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसका संबंध कृषक समाज से है यानी वह जाट है। जाटों और मेवों के स्वभाव और मूल प्रवृत्ति समान हैं। इसीलिए इन दोनों समुदायों के बारे में मेवात में यह कहावत प्रचलित है कि ‘जाट को कहा हिन्दू और मेव को कहा मुसलमान। ‘ मेवों से तो जाट, गूजर, अहीर, यादव समुदाय के पारस्परिक सामाजिक संबंध बहुत ही सौहार्दपूर्ण और मधुर रहे हैं। दरअसल, जैसे-जैसे जाट, गूजर, अहीर, यादव समुदायों की आर्थिक संपन्नता बढ़ी है वैसे-वैसे इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में भी तेज़ी से वृद्धि हुई है। अगर देखा जाए तो आज एक राष्ट्रवादी राजनीतिक पार्टी इन समुदायों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल अल्पसंख्यकों के विरुद्ध कर रही है। इस पार्टी की सबसे बड़ी ताक़त ही ये समुदाय हैं. मुझे तो यह भी आशंका है कि जो नफ़रत आज मुसलमान अल्पसंख्यकों के प्रति है, आने वाले समय में वह दलितों के प्रति शुरू हो जायेगी।
रही बात कि मेवात में जिस तरह रिश्तों और संबंधों का ताना-बाना टूट रहा है तो उसे बचाने के लिए हमें सामाजिक परिवर्तनों की पुन: समीक्षा करनी होगी। समाज में जिस तरह धर्म का दखल बढ़ा है और उसके चलते सभी समुदायों में जिस तरह सांप्रदायिकता तेज़ी से घर करती जा रही, उसके प्रति लोगों की समझ बदलनी होगी!
अटल तिवारी पत्रकारिता के प्राध्यापक हैं और दिल्ली में रहते हैं


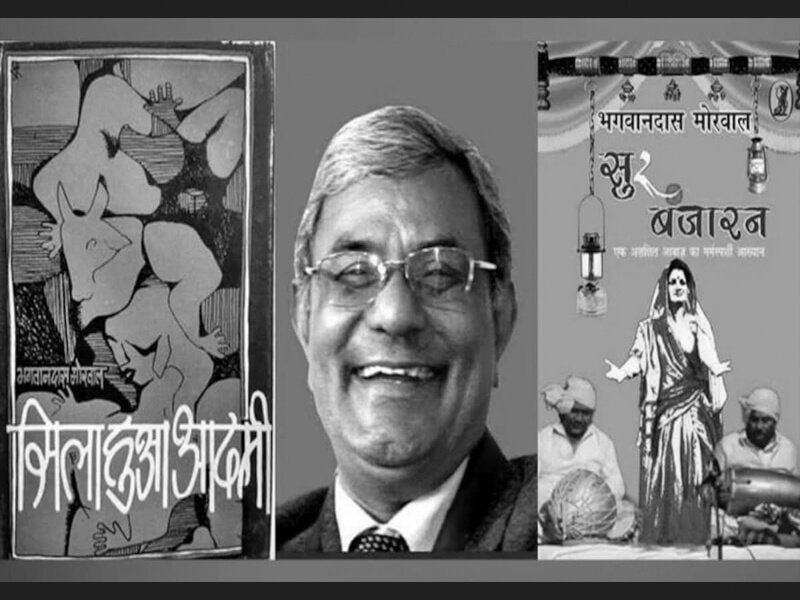


बेहतरीन समालोचना