‘लोकतंत्र ख़तरे में है’, क्या सचमुच! वैसे ये लोकतंत्र था कहाँ जो ख़तरे में आ गया! क़िताबों में जहाँ लोकतंत्र था, वहाँ तो आज भी है, जीवन में लोकतंत्र तो था नहीं फिर ये ख़तरे में आया कैसे! भारतीय समाज जाति आधारित समाज व्यवस्था को जीता है, पिछले कई सदियों से ये व्यवस्था अपनी जगह कायम है। कई तरह के धार्मिक एवं सामाजिक आन्दोलन इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, मंगोल, तुर्क, मुग़ल जैसे कितने ही बाहरी सुल्तान और बादशाह आये, लेकिन जाति व्यवस्था अपनी जगह क़ायम रही। 1947 के बाद देश को संविधान के ज़रिये चलाए जाने की कोशिश हुई लेकिन जाति आधारित समाज व्यवस्था का कुछ नहीं बिगड़ा। क्या जाति आधारित समाज व्यवस्था और लोकतंत्र का आपस में कोई रिश्ता हो सकता है?
जाति और जेंडर के आधार पर भेदभाव को जीता हुए समाज ने लोकतंत्र की चादर ओढ़ ली, इसमें एक खास सुविधा है, जब चाहे चादर ओढ़ी जा सकती है और जब चाहे फेंकी जा सकती है या तहा कर बक्शे में वक़्त ज़रुरत ओढ़ने के लिए रखी भी जा सकती है। लेकिन जाति और जेंडर के आधार पर व्यवहार को तो पल भर के लिए नहीं छोड़ा जा सकता, छोड़ा जाता भी नहीं। इसलिए शादी-ब्याह और लोक व्यवहार जाति व जेंडर के आधार पर होते रहते हैं और अक्सर तो ये सब लोकतंत्र की चादर ओढ़कर ही किये जाते हैं। अब जब लोकतंत्र की चादर अभी भी किसी कंधे पर, किसी की अलगनी पर, किसी के बक्शे में तो किसी वाशिंग मशीन में रखी ही है तो इस पर ख़तरा कहाँ से और कैसे आ गया!
भारत का समाज जो आधा-अधूरा आधुनिक हुआ, वो अंग्रेजों के दौरे हुकूमत में हुआ, ऐसा क्यों हुआ? इस पर विचार करने की ज़रुरत है। लेकिन जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा सोचने की ज़रुरत है वह ये कि हिंदुत्व की सियासत के साथ बहता समाज आजाद भारत में हासिल आधी-अधूरी आधुनिकता को रौंद कर पांच सदी पीछे जाने को बेचैन क्यों है?
विचार कीजिये, जब आप लोकतंत्र शब्द सुनते हैं या उच्चारित करते हैं तो आपके मन में क्या विचार आता है! राजनेता, चुनाव या संसद और विधानसभाएँ, यही न! क्या कभी आपने सोचा कि आप अपने जाति या धर्म के सबसे बड़े अपराधी को अपना वोट क्यों दे देते हैं और ये वोट जाति या धर्म के आधार पर ही क्यों देते हैं? एक दूसरा विचार करें, आपके घर में फ़ैसला कौन लेता है, क्या ये फ़ैसला परिवार के सभी सदस्य सामूहिक रूप से लेते हैं? क्या स्त्रियाँ भी फ़ैसले लेने की प्रक्रिया में शामिल होती हैं? विचार कीजिये कि ये सब हम क्यों नहीं करते? और अगर ये सब हम नहीं करते तो फिर लोकतंत्र कैसे सीखेंगे और कहाँ से सीखेंगे?
हमें सिखाया गया कि बड़ों और गुरु का सम्मान करो, ये नहीं सिखाया गया कि गुरु और ज्ञान दोनों पर सवाल करो, अगर ऐसा कोई करे तो उसे असभ्य माना जायेगा, यानि आज़ादी के इन तमाम सालों में हमारे स्कूल हमें लोकतंत्र के नाम पर भक्ति सिखाते रहे लोकतंत्र नहीं।
एक सामान्य-सा तहज़ीब हम नहीं सीख पाए कि ‘हर किसी को अपना मत व्यक्त करने की आज़ादी हो और उसके मत को सुना जाए,’ किसी के मत से सहमत या असहमत हुआ जा सकता है लेकिन बलात किसी पर अपना मत थोपा नहीं जा सकता। क्या हम परिवार और समाज में यही नहीं करते हैं?
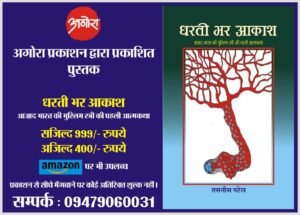
हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ युवक युवतियों को अपना जीवन साथी तक चुनने का अधिकार नहीं है, हालांकि यही युवक युवतियाँ देश एवं राज्य की सरकार चुनते हैं, कमाल देखिये, आज का युवा अपने जीवन साथी के चुनाव के हक़ के लिए लड़ता भी नहीं है, हालांकि ये लड़ाई बेहद आसान है। आज तो प्रशासन भी जाति और धर्म की दीवार तोड़ कर शादी करने वालों का बुलडोज़र से घर गिरा देता है। क्या ये बात आपको हैरान नहीं करती कि जिस समाज में लोगों को अपना जीवन साथी तक चुनने का हक़ न हो वो देश के लिए सांसद और विधायक कैसे चुन सकते हैं, लेकिन ये सब हो रहा है और वो भी लोकतंत्र के नाम पर।
आमतौर पर लोकतंत्र को एक नियम समझ लिया जाता है, जबकि ये तहज़ीब या संस्कृति है। जाति आधारित सर्वोच्चता और निम्नता की ग्रंथि से बजबजाते भारतीय समाज में क्या लोकतंत्र के एक तहज़ीब होने को हम कभी समझ पाएंगे! जब मैं कह रहा हूँ कि लोकतंत्र एक तरह की तहज़ीब है तो इसका अर्थ ये है एक व्यक्ति को समाज ने इतना सक्षम बनाया है कि वो जीवन के सभी क्षेत्रों में ज़रूरी निर्णय ले सकता है और समाज उसके निर्णय का सम्मान करने के लिए तैयार है। क्या भारत का समाज ऐसा है?
यह भी पढ़ें…
जाहिर-सी बात है कि भारत का समाज एक लोकतान्त्रिक समाज नहीं है। जाति व्यवस्था में सदियों से संस्कारित होते समाज में न्याय भावना का ही अभाव है। यही कारण है कि गाँव से लेकर शहर तक, सरपंच से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक हमें फ़ैसले तो दिखाई देते हैं लेकिन न्याय होता हुआ नज़र नहीं आता। सर्वोच्चता और निम्नता की ग्रंथि के साथ पले बढ़े लोगों में लोकतान्त्रिक मूल्य के लिए कोई जगह नहीं होती और एक गैर लोकतान्त्रिक समाज कभी न्याय भावना से युक्त नहीं हो सकता।
आप शासन और प्रशासन में जाति और धर्म के आधार पर होते फ़ैसले देख सकते हैं, यही नहीं जाति और धर्म के आधार किसी व्यक्ति या एक पूरे समूह का क़त्ल भी हमारे देश में कोई अनोखी बात नहीं है। ऐसे में जब कहा जाता है कि लोकतंत्र ख़तरे में है तो ये सवाल उठना लाज़िमी है कि वो कौन-सा लोकतंत्र है जो ख़तरे में हैं, क्योंकि जीवन में तो कहीं कोई लोकतंत्र है नहीं!
यह भी पढ़ें…
ये लेख पढ़ते हुए कई लोगों का मन आहत हो सकता है, लेकिन ज़रूरी है कि यहाँ उठाये गये प्रश्नों पर विचार किया जाए। सोचिये कि अगर भारत के जीवन से पश्चिम के ज्ञान, विज्ञान और तकनीक को माइनस कर दया जाये तो भारत आज आपको कहाँ खड़ा दिखाई देगा? जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, तब भारत के गाँव के गाँव महामरी से मर रहे होंगे, सड़कें नहीं होंगी, कारें नहीं होंगी, दवाइयां नहीं होंगी, आधुनिक भवन नहीं होंगे। अमीर लोग रथ पर चल रहे होंगे जिसकी स्पीड 10 किमी प्रति घंटा मुश्किल से होगी और लोगों का औसत जीवन 35 साल होगा। यानि भारत अपने बूते पर आज भी पांच सदी पीछे खड़ा है, उसके मूल्य, संस्कार और विचार पांच सदी पीछे वाले हैं। दुनिया से पाँच सदी पीछे खड़े भारत ने यूरोप का ज्ञान-विज्ञान और तकनीक तो ओढ़ लिया लेकिन क्या इस पहलु पर विचार नहीं होना चाहिए कि भारत मूल्यों के स्तर पर इतना पीछे क्यों है? क्यों एक भारतीय को ब्राह्मण के रूप में इतराने और शूद्र के रूप में हर पल अपमानित महसूस करने की ज़रुरत है? एक जैसी शक्ल और सूरत वाले दो इन्सान जो एक ही भौगोलिक वातावरण में पैदा हुए उनके सामाजिक हैसियत इतने अलग अलग क्यों हैं? जाहिर-सी बात है ऐसे समाज में लोकतंत्र को ख़तरा तो होगा ही, ऐसे समाज में लोकतंत्र अगर जगह बनाने की कोशिश करेगा तो उसका गला तो घोंटा ही जाएगा।
अपने आपसे सवाल पूछिए, आज़ादी के इतने सालों बाद सरकारी दफ्तरों में आरक्षण के अनुपात में भी आरक्षित वर्ग के लोग क्यों नहीं है? न्यायपालिका में एक ही जाति का वर्चस्व क्यों हैं? कम्युनिस्ट पार्टियाँ जो खुलेतौर पर जाति व्यवस्था और जेंडर असामनता की मोखाल्फ़त करती हैं, उनके भी शीर्ष नेतृत्व पर एक ही सवर्ण जाति का कब्ज़ा क्यों है, कम्युनिस्टों के घरों की महिलाओं का जीवन पारंपरिक परिवारों की महिलाओं के जीवन से किसी भांति अलग है क्या?
अगोरा प्रकाशन की किताबें Kindle पर भी….
ये भी सोचिये कि जब यूरोप में पुनर्जागरण हो रहा था या जब भारत से भी पिछड़ा रूस अपने नागरिकों को आधुनिक बना रहा था तब भारत क्या कर रहा था, क्यों भारत में पुनर्जागरण जैसा कोई काम नहीं हुआ, हालांकि अकबर उन दिनों देश का हुक्मरान था जिसके दरबार में देश के प्रतिष्ठित राजा और विद्वान सम्मान पाते थे, फिर भी भारत अपनी जाति आधारित सामाजिक आर्थिक व्यवस्था से बाहर क्यों नहीं निकल पाया? यहाँ तक कि इसका कोई सार्थक प्रयास तक नहीं हुआ, क्या ये बात आपको हैरान करती कि जब उत्तर भारत के तुलसीदास रामचरित मानस लिख रहे थे तब यूरोप आधुनिक दुनिया की बुनियादें निर्मित कर रहा था, भारत जिसकी सभ्यता यूरोप से कहीं ज़्यादा पुरानी है वो तालाब के पानी की तरह 15 वीं, 16वीं सदी आते आते ठहर गया और आज भी आधुनिकता के तमाम निशानात मिटाने को बेचैन हैं। सच तो ये है कि पूरा दक्षिण एशिया जहाँ हिन्दू, बौद्ध और इस्लाम मज़ाहिब के मानने वाले हैं, पुरातन मूल्यों से चिपका हुआ है और विज्ञान एवं तकनीक के मामले में पूरी तरह यूरोप पर निर्भर है।
भारत का समाज जो आधा-अधूरा आधुनिक हुआ, वो अंग्रेजों के दौरे हुकूमत में हुआ, ऐसा क्यों हुआ? इस पर विचार करने की ज़रुरत है। लेकिन जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा सोचने की ज़रुरत है वह ये कि हिंदुत्व की सियासत के साथ बहता समाज आजाद भारत में हासिल आधी-अधूरी आधुनिकता को रौंद कर पांच सदी पीछे जाने को बेचैन क्यों है? माना कि भारतीय फासीवादी सियासत को पूँजीपतियों का भरपूर समर्थन है, लेकिन एक कल्पना करें कि अगर पूँजीपतियों का समर्थन हट जाये तो क्या भारतीय समाज पुरातन एवं अमानवीय मूल्यों की ओर भागना छोड़ देगा? रोज़ी, रोटी के प्रश्न के बजाय धर्म आधारित पागलपंथी भारत को इतना आकर्षित कैसे कर लेती है कि एक भारतीय न सिर्फ़ अपना बल्कि सैकड़ों लोगों का जीवन दाँव पर लगा देता है!

भारत में सांस्कृतिक पिछड़ेपन पर कहने को बहुत कुछ है लेकिन ज़रूरी है कि इस पिछड़ेपन के कारणों की पड़ताल हो। सच तो ये है कि भारत में एक ऐसे आंदोलन की ज़रुरत है जो सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक स्तरों पर एक साथ लम्बे समय तक काम करे। अफ़सोस अभी तक ऐसा कोई संगठन नहीं है जो इस जिम्मेदारी को उठाये, पर सोचकर देखिये, क्या ऐसा ही एक संगठन बनाना हमारी ज़रुरत नहीं है?

सलमान अरशद स्वतंत्र पत्रकार हैं।
यह भी पढ़ें…






[…] […]
[…] […]
[…] […]